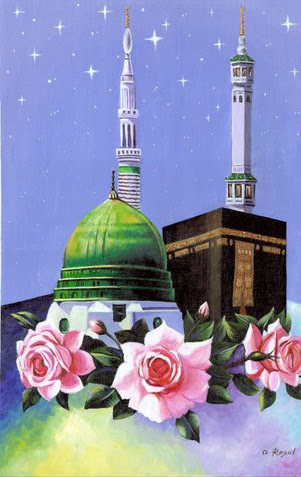ग़ालिब की डायरी है दस्तंबू
-
*फ़िरदौस ख़ान*
हिन्दुस्तान के बेहतरीन शायर मिर्ज़ा ग़ालिब ने उर्दू शायरी को नई ऊंचाई दी.
उनके ज़माने में उर्दू शायरी इश्क़, मुहब्बत, विसाल, हिज्र और हुस्...
डॉ. फ़िरदौस ख़ान
मानव सभ्यता में रंगों का काफ़ी महत्व रहा है. हर सभ्यता ने रंगों को अपने तरीक़े से अपनाया. दुनिया में रंगों के इस्तेमाल को जानना भी बेहद दिलचस्प है. कई सभ्यताओं को उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले रंगों की वजह से ही पहचाना गया. विक्टोरियन काल में ज़्यादातर लोग काला या स्लेटी रंग इस्तेमाल करते थे. एक तरह से ये रंग इनकी पहचान थे. फ़िरऔन हमेशा काले कपड़े पहनता था. वैसे भी हर रंग के अपने सकारात्मक और नकारात्मक असर होते हैं. इसलिए यह नहीं कर सकते कि काला रंग हमेशा बुरा ही होता है. हालांकि कई सभ्यताओं में इसे शोक का रंग माना जाता है. शिया मोहर्रम के दिनों में ज़्यादातर काले कपड़े ही पहनते हैं. विरोध जताने के लिए भी काले रंग का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे काले झंडे दिखाना, सर पर काला कपड़ा या काली पट्टी बांध लेना. ऐसा इस्लामी देशों में ज़्यादा होता है, लेकिन अब भारत में भी इस तरह विरोध जताया जाने लगा है, विशेषकर बाबरी मस्जिद की शहादत की बरसी यानी छह दिसंबर को मुस्लिम समुदाय के लोग काली पट्टी बांधकर ही अपना विरोध ज़ाहिर करते हैं.
महान दार्शनिक अरस्तु ने 4 ईसा पूर्व में नीले और पीले रंगों की गिनती शुरुआती रंगों में की. उन्होंने इसकी तुलना प्राकृतिक वस्तुओं से की, जैसे सूरज-चांद और दिन-रात आदि. उस वक़्त ज़्यादातर कलाकारों ने उनके सिद्धांत को माना और तक़रीबन दो हज़ार साल तक इसका असर देखने को मिला. इसी बीच मेडिकल प्रेक्टि्स के पितामाह कहे जाने वाले ग्यारहवीं शताब्दी के ईरान के चिकित्सा विशेषज्ञ हिप्पोकेट्स ने अरस्तु के सिद्धांत से अलग एक नया सिद्धांत पेश किया. उन्होंने रंगों का इस्तेमाल दवा के तौर पर किया और इसे इलाज के लिए बेहतर ज़रिया क़रार दिया. उनका मानना था कि सफ़ेद फूल और वॉयलेट फूल के अलग-अलग असर होते हैं. उन्होंने एक और सिद्धांत दिया, जिसके मुताबिक़ हर व्यक्ति की त्वचा के रंग से भी उसकी बीमारी का पता लगाया जा सकता है और रंगों के ज़रिये ही इसका इलाज भी मुमकिन है. उन्होंने इसका ख़ूब इस्तेमाल भी किया.
15वीं शताब्दी में स्विट्जरलैंड के चिकित्सक वॉन होहेनहैम ने ह्यूमन स्टडी पर काफ़ी शोध किया, लेकिन उनके तरीक़े हमेशा विवादों में रहे. उन्होंने ज़ख्म भरने के लिए रंगों का इस्तेमाल किया. 17-18वीं शताब्दी में न्यूटन के सिद्धांत ने अरस्तु के विशेष रंगों को सामान्य रंगों में बदल दिया. 1672 में न्यूटन ने रंगों पर अपना पहला परचा पेश किया. यह काफ़ी विवादों में रहा, क्योंकि अरस्तु के सिद्धांत के बाद इसे स्वीकार करना इतना आसान नहीं था. रंगों के विज्ञान पर काम करने वाले लोगों में जॉन्स वॉल्फगैंग वॉन गौथे भी शामिल थे. उन्होंने न्यूटन के सिद्धांत को पूरी तरह नकारते हुए थ्योरी ऑफ कलर पेश की. उनके सिद्धांत अरस्तु की थ्योरी से मिलते जुलते थे. उन्होंने कहा कि अंधेरे में से सबसे पहले नीला रंग निकलता है, वहीं सुबह के उगते हुए सूरज की किरणों से पीला रंग सामने आता है. नीला रंग गहरे रंगों का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि पीला रंग हल्के रंगों का. 19वीं शताब्दी में कलर थैरेपी का असर कम हुआ, लेकिन इसके बाद 20वीं शताब्दी में यह नए रूप में सामने आया. आज भी कई चिकित्सक कलर थैरेपी को इलाज का अच्छा ज़रिया मानते हैं और इससे अनेक बीमारियों का उपचार भी करते हैं. आयुर्वेद चिकित्सा में भी रंगों का विशेष महत्व है. रंग चिकित्सा के मुताबिक़ शरीर में रंगों के असंतुलन के कारण ही बीमारियां पैदा होती हैं. रंगों का समायोजन ठीक करके बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है. ऑस्टवाल्ड ने आठ आदर्श रंगों को विशेष क्रम में संयोजित किया. इस चक्र को ऑस्टवाल्ड वर्ण कहा जाता है. इसमें पीला, नारंगी, लाल, बैंगनी, नीला, आसमानी, समुद्री हरा और हरा रंग शामिल है. 60 के दशक में एंथ्रोपॉलिजिस्ट्स केन ने रंगों पर अध्ययन किया. उनके मुताबिक़ सभी सभ्यताओं ने रंगों को दो वर्गों में बांटा-पहला हल्के रंग और दूसरा गहरे रंग.
कौन-सा रंग क्या कहता है?
मूल रूप से इंद्रधनुष के सात रंगों को ही रंगों का जनक माना जाता है. ये सात रंग हैं लाल, नारंगी, पीला, हरा, आसमानी, नीला और बैंगनी. लाल रंग को रक्त रंग भी कहते हैं, क्योंकि ख़ून का रंग लाल होता है. यह शक्ति का प्रतीक है, जो जीने की इच्छाशक्ति और अभिलाषा को बढ़ाता है. यह प्रकाश का संयोजी प्राथमिक रंग है, जो क्यान रंग का संपूरक है. यह रंग क्रोध और हिंसा को भी दर्शाता है. हरा रंग प्रकृति से जुड़ा है. यह ख़ुशहाली का प्रतीक है. हमारे जीवन में इसका बहुत महत्व है. यह प्राथमिक रंग है. हरे रंग में ऑक्सीजन, एल्यूमीनियम, क्रोमियम, सोडियम, कैल्शियम, निकिल आदि होते हैं. इस्लाम में इसे पवित्र रंग माना जाता है. नीला रंग आसमान का रंग है. यह विशालता का प्रतीक है. भारत का क्रीड़ा रंग भी नीला ही है. यह धर्मनिरपेक्षता का भी प्रतीक है. यह एक संयोजी प्राथमिक रंग है. इसका संपूरक रंग पीला है. गहरा नीला रंग अवसाद और निराशा को भी प्रकट करता है. पीला रंग ख़ुशी और रंगीन मिज़ाजी को दर्शाता है. यह आत्मविश्वास बढ़ाता है. यह वैराग्य से भी संबंधित है. हिंदू धर्म में इसका विशेष महत्व है. विष्णु और कृष्ण को यह रंग प्रिय है. बसंत पंचमी तो इसी रंग से जुड़ा पर्व है. डल पीला रंग ईर्ष्या को दर्शाता है. स़फेद रंग पवित्रता और निर्मलता का प्रतीक माना जाता है. यह शांति और सुरक्षा का भाव पैदा करता है. यह अकेलेपन को भी प्रकट करता है. काला रंग रहस्य का प्रतीक है. यह बदलाव से रोकता है. यह नकारात्मकता को भी दर्शाता है.
(लेखिका स्टार न्यूज़ एजेंसी में सम्पादक हैं)
सरफ़राज़ ख़ान
विभिन्न संस्कृतियों के देश भारत में एक नहीं दो नहीं, बल्कि अनेक नववर्ष मनाए जाते हैं. यहां के अलग-अलग समुदायों के अपने-अपने नववर्ष हैं. अंग्रेज़ी कैलेंडर का नववर्ष एक जनवरी को शुरू होता है. इस दिन ईसा मसीह का नामकरण हुआ था. दुनियाभर में इसे धूमधाम से मनाया जाता है.
मोहर्रम महीने की पहली तारीख़ को मुसलमानों का नया साल हिजरी शुरू होता है. मुस्लिम देशों में इसका उत्साह देखने को मिलता है. इस्लामी या हिजरी कैलेंडर, एक चंद्र कैलेंडर है, जो न सिर्फ़ मुस्लिम देशों में इस्तेमाल होता है, बल्कि दुनियाभर के मुसलमान भी इस्लामिक धार्मिक पर्वों को मनाने का सही समय जानने के लिए इसी का इस्तेमाल करते हैं. यह चंद्र-कैलेंडर है, जिसमें एक वर्ष में बारह महीने, और 354 या 355 दिन होते हैं, क्योंकि यह सौर कैलेंडर से 11 दिन छोटा है इसलिए इस्लामी तारीखें, जो कि इस कैलेंडर के अनुसार स्थिर तिथियों पर होतीं हैं, लेकिन हर वर्ष पिछले सौर कैलेंडर से 11 दिन पीछे हो जाती हैं. इसे हिजरी इसलिए कहते हैं, क्योंकि इसका पहला साल वह वर्ष है जिसमें हज़रत मुहम्मद की मक्का शहर से मदीना की ओर हिजरत या वापसी हुई थी. हिन्दुओं का नववर्ष नव संवत्सर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा में पहले नवरात्र से शुरू होता है. इस दिन ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की थी. जैन नववर्ष दीपावली से अगले दिन होता है. महावीर स्वामी की मोक्ष प्राप्ति के अगले दिन यह शुरू होता है. इसे वीर निर्वाण संवत कहते हैं. बहाई धर्म में नया वर्ष ‘नवरोज’ हर वर्ष 21 मार्च को शुरू होता है. बहाई समुदाय के ज़्यादातर लोग नव वर्ष के आगमन पर 2 से 20 मार्च अर्थात् एक महीने तक व्रत रखते हैं. गुजराती 9 नवंबर को नववर्ष ‘बस्तु वरस’ मनाते हैं. अलग-अलग नववर्षों की तरह अंग्रेजी नववर्ष के 12 महीनों के नामकरण भी बेहद दिलचस्प है.
जनवरी: रोमन देवता 'जेनस' के नाम पर वर्ष के पहले महीने जनवरी का नामकरण हुआ. मान्यता है कि जेनस के दो चेहरे हैं. एक से वह आगे और दूसरे से पीछे देखता है. इसी तरह जनवरी के भी दो चेहरे हैं. एक से वह बीते हुए वर्ष को देखता है और दूसरे से अगले वर्ष को. जेनस को लैटिन में जैनअरिस कहा गया. जेनस जो बाद में जेनुअरी बना जो हिन्दी में जनवरी हो गया.
फ़रवरी: इस महीने का संबंध लैटिन के फैबरा से है. इसका अर्थ है 'शुद्धि की दावत' . पहले इसी माह में 15 तारीख को लोग शुद्धि की दावत दिया करते थे. कुछ लोग फरवरी नाम का संबंध रोम की एक देवी फेबरुएरिया से भी मानते हैं. जो संतानोत्पत्ति की देवी मानी गई है इसलिए महिलाएं इस महीने इस देवी की पूजा करती थीं.
मार्च: रोमन देवता 'मार्स' के नाम पर मार्च महीने का नामकरण हुआ. रोमन वर्ष का प्रारंभ इसी महीने से होता था. मार्स मार्टिअस का अपभ्रंश है जो आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है. सर्दियों का मौसम खत्म होने पर लोग शत्रु देश पर आक्रमण करते थे, इसलिए इस महीने का नाम मार्च रखा गया.
अप्रैल: इस महीने की उत्पत्ति लैटिन शब्द 'एस्पेरायर' से हुई. इसका अर्थ है खुलना. रोम में इसी माह बसंत का आगमन होता था इसलिए शुरू में इस महीने का नाम एप्रिलिस रखा गया. इसके बाद वर्ष के केवल दस माह होने के कारण यह बसंत से काफ़ी दूर होता चला गया. वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के सही भ्रमण की जानकारी से दुनिया को अवगत कराया तब वर्ष में दो महीने और जोड़कर एप्रिलिस का नाम पुनः सार्थक किया गया.
मई: रोमन देवता मरकरी की माता 'मइया' के नाम पर मई नामकरण हुआ. मई का तात्पर्य 'बड़े-बुजुर्ग रईस' हैं. मई नाम की उत्पत्ति लैटिन के मेजोरेस से भी मानी जाती है.
जून: इस महीने लोग शादी करके घर बसाते थे. इसलिए परिवार के लिए उपयोग होने वाले लैटिन शब्द जेन्स के आधार पर जून का नामकरण हुआ. एक अन्य मान्यता के मुताबिक रोम में सबसे बड़े देवता जीयस की पत्नी जूनो के नाम पर जून का नामकरण हुआ.
जुलाई: राजा जूलियस सीजर का जन्म एवं मृत्यु दोनों जुलाई में हुई. इसलिए इस महीने का नाम जुलाई कर दिया गया.
अगस्त: जूलियस सीजर के भतीजे आगस्टस सीजर ने अपने नाम को अमर बनाने के लिए सेक्सटिलिस का नाम बदलकर अगस्टस कर दिया जो बाद में केवल अगस्त रह गया.
सितम्बर: रोम में सितंबर सैप्टेंबर कहा जाता था. सेप्टैंबर में सेप्टै लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है सात और बर का अर्थ है वां यानी सेप्टैंबर का अर्थ सातवां, लेकिन बाद में यह नौवां महीना बन गया.
अक्टूबर: इसे लैटिन 'आक्ट' (आठ) के आधार पर अक्टूबर या आठवां कहते थे, लेकिन दसवां महीना होने पर भी इसका नाम अक्टूबर ही चलता रहा.
नवम्बर: नवंबर को लैटिन में पहले 'नोवेम्बर' यानी नौवां कहा गया. ग्यारहवां महीना बनने पर भी इसका नाम नहीं बदला एवं इसे नोवेम्बर से नवम्बर कहा जाने लगा.
दिसम्बर: इसी प्रकार लैटिन डेसेम के आधार पर दिसम्बर महीने को डेसेंबर कहा गया. वर्ष का बारहवां महीना बनने पर भी इसका नाम नहीं बदला.
कुहरे में सूरज नया, मलता दीखे आँख
स्वयं जनवरी हो गई, धूप नहाई शाख।।
तिथियों के अक्षत सजा, नए साल का भाल
जी भर बतियाएँ चलो, ओढ़ गुनगुना शॉल।।
लहरें जितनी तेज़ हैं, उतनी मंथर चाल
नए साल की नाव पर, तना हवा का पाल।।
नए साल का आइना, देता है आवाज़
पल पल गुड़हल हो रही, चेहरा पढ़ती लाज।।
सेंदुर टिकुली चन्द्रमा, सबकी अपनी बात
नया साल लो आ गया, हाथों में ले हाथ।।
क्या क्या बतलाएं भला, वेणी ख़ुशबू गीत
नए साल के होंठ पर, दहक रहा है शीत।।
खटमिट्ठी है बतकही, शब्दों में है लोच
नए साल में चल सके, कहां पुरानी सोच।।
क्षितिज हथेली के सजे, अरुणोदय से गाल
हाथों में हर दिशा के, पूजा वाला थाल।।
गया साल अब भी जिए, चुक जाने के बाद
नए साल की आँख से, टपक रही है याद।।
मन उजला करने लगी, नए साल की भोर
छंद छंद छूने लगे, कई अनछुए छोर।।
नए साल ने ले लिया, नए समय को अंक
गए साल के घाट पर, छूटे, सीपी शंख।।
-यश मालवीय
एक साल जाता है एक साल आता है।
जाने और आने में जाने क्या नाता है।।
उगते का अभिनन्दन,
ढलते की यादें हैं।
मन-मोहक हैं बंधन,
अनगिनत मुरादें हैं।।
शीत झेल, ग्रीष्म झेल, बारिश में नहाता है।
नस्लों में, फ़स्लों में, काल झिलमिलाता है।।
जाते को हाथ हिला,
आत्मिक विदाई है।
आते से हाथ मिला,
हृदय से बधाई है।।
बीते का प्रतिबिम्बन, पीर-सी जगाता है।
आगत का भाव-बोध, प्रीत बन लुभाता है।।
-कैलाश मनहर
जाते हुए साल पर एक पुराना गीत
एक याद सिरहाने रखकर...
एक याद सिरहाने रखकर
एक याद पैताने रखकर
चला गया ये साल, साल ये चला गया
खाली से पैमाने रखकर
भरे-भरे अफ़साने रखकर
चला गया ये साल, साल ये चला गया
लम्बी छोटी हिचकी रखकर
थोड़े आँसू, सिसकी रखकर
टूटे सपनों के बारे में
बातें इसकी उसकी रखकर
गुड़ घी ताल मखाने रखकर
चिड़ियों वाले दाने रखकर
चला गया ये साल, साल ये चला गया
उजियारा, कुछ स्याही रखकर
कल की नई गवाही रखकर
लाल गुलाबी हरे बैगनी
रंग कत्थई काही रखकर
भूले बिसरे गाने रखकर
गानों में कु़छ माने रखकर
चला गया ये साल, साल ये चला गया
नीली आँखों, चिठ्ठी रखकर
इमली कु़छ खटमिठ्ठी रखकर
मुँह में शुभ संकेतों वाली
बस थोड़ी सी मिट्टी रखकर
सच के सोलह आने रखकर
बच्चों के दस्ताने रखकर
चला गया ये साल, साल ये चला गया।
-यश मालवीय
चल दिया दिसम्बर मास आज
लो वर्ष हुआ नौ दो ग्यारह।
कुछ आशाएँ फलवती हुईं
कुछ सपने ठेंगा दिखा गये
कुछ नाम जुड़ गए सूची में
कुछ नाम पुराने कटा गए
कुछ जग-प्रपंच को छोड़ गए
कुछ करते रहे तीन-तेरह।।
'मैं' लड़ता था मेरे 'मैं' से
'तुमने' 'उसने'तो प्यार दिया
'इसने''उसने'जाने 'किसने'
मेरे सपनों को मार दिया
यह अपराजेय समर जारी
चल रहा आज तक भी अहरह।।
आ गया नए परिधान पहन
चौखट पर देता है दस्तक
यह नया वर्ष ही है शायद
ले आया सपनों की पुस्तक
कल जो होगा सो होगा ही
उल्लास अभी आता बह-बह।।
जो बीत गया मृत हुआ आज
डालो अब धूल असंगत पर
जो अतिथि खड़ा दरवाजे पर
दें ध्यान उसी के स्वागत पर
चेतना उमग कर नदी बनी
उठतीं उमंग-लहरें रह-रह।।
-डॉ. रामसनेहीलाल शर्मा 'यायावर'
विगत वर्ष में कुछ हुए, सपने चकनाचूर।
आगत में आशा करें, नहीं सफलता दूर।।
स्वागत आगत वर्ष का, करने लिए उमंग।
अक्षत, कुंकुम, दीप ले, मन में विपुल तरंग।
आने वाला आयगा, जाने वाला जाय।
स्वागत आगत का करें,कहें विगत को 'बाय'।।
प्रश्न यक्ष के आज तक , कब सुलझे हैं मित्र!
मन में आगत का रखें, शुभागमन का चित्र।।
अंतिम साँसें ले रहा, दो हजार पच्चीस।
खड़ा हुआ है द्वार पर, दो हजार छब्बीस।।
-डॉ. रामस्नेहीलाल शर्मा 'यायावर'
-डॉ. रामस्नेहीलाल शर्मा 'यायावर'
लाल बिहारी लाल
नव वर्ष उत्सव मनाने की परंपरा 4000 वर्ष पहले बेबीलोन(मध्य ईराक) से शुरु हुई थी जो 21 मार्च को मनाया जाता था, पर रोम के शासक जुलियस सीजर ने ईसा से 45 ई. पूर्व जूलियन कैलेंडर की स्थापना विश्व में पहली बार की तब ईसा पूर्व इसके 1 साल पहले का वर्ष यानी 46वें ईसा पूर्व वर्ष को 445 दिनों का कर दिया और इसे 1 जनवरी को नव वर्ष मनाया तभी से हर साल 1 जनवरी को नव वर्ष मनाते आ रहे है।
एक अमेरिकी फिजीशियन एलाँयासिस लिलिअस ने एक ग्रिगेरियन कैलेंडर की शुरुआत 15 अक्टूबर ,1582 में की इसके तहत साल दस महिने का था । इसमें भी 1 जनवरी को नया साल मनाने की शुरुआत हुई पर ईसाई इसे क्रिसमस दिवस को ही मनाते है नया साल । नया साल मनाने का मुख्य उदेश्य की जीवन में नये चेतना का संचार करना यानी जीवन चक्र को रिचार्ज करना है। इस दिन हर्ष और उल्लास से काम धाम में लग जाते है। आज सारी दुनिया में 1 जनवरी को ही अधिकांश देश नव वर्ष मनाते है। यहुदियों(हिब्रू) का नव वर्ष 5 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच आता है। इस्लामी कैलेंडर की नया साल मुहरर्म के दिन से शुरु होता है जो ग्रीगेरियन से प्रेरित है।
भारत देश की बात करे तो यहा अनेक जाति धर्म के लोग रहते है और अपनी संस्कृति एंव परंपराओं के अनुसार अलग-अलग समय पर नव वर्ष मनाते है। हिन्दुओं के नया वर्ष चैत मास के प्रतिपदा (पहले) के दिन मनाते है।इसी दिन सिंधी चोटी चंड मनाते है। इसी दिन सूर्योदय से ब्रम्हा जी ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की थी। बात करे पंजाब की तो फसलों के तैयार होने पर 13 अप्रैल को वैशाखी के दिन मनाते है। वही बंगाल औऱ बंगला देश में पोहेला बोइसाख( बैसाखी) 14 और 15 अप्रैल को मनाते है। वही आंध्र प्रदेश में उगादी औऱ तमिलनाड़ू में विशु 13 या 14 अप्रैल को मनाते है जबकि 15 जनवरी को पोंगल अधिकारिक रुप से मनाया जाता है। और कर्नाटक में उगाड़ी, महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा मनाते है । माड़वाड़ी दीपावली को दिन मनाते है जबकि गुजराती दीपावली के दूसरे दिन मनाते है। इसी दिन जैन धर्म के अनुआयी भी नव वर्ष मनते है। यह त्योवहार अक्टूबर –नवंबर में आता है। काश्मिरी कैलेंडर के हिसाब से नवरेह 19 मार्च को मनाते है। चैत प्रतिपदा के दिन ही सम्राट विक्रमादित्य ने राज पाट संभाला था इन्हीं के नाम पर विक्रम समवत की शुरुआत हुई जो चैत महिने का पहला दिन हैं ,तो आप भी खुशियों के साथ नये दिन की शुरुआत करे । आप सभी को नव वर्ष मंगलमय हो।
(लेखक साहित्य टीवी, नई दिल्ली के संपादक हैं)
कुतुबमीनार के सहन में मौजूद ये कब्र हिंदुस्तान की मंगोलों से हिफाजत करने वाले सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की है 4 जनवरी 1316 ई. को दिल्ली में 50 साल की उम्र में खिलजी की वफात हो गयी थी। उनकी वफात के बाद उन्हें कुतुबमीनार के सहन में उनके तामीर किये हुए मदरसे में दफन किया गया था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को हिंदुस्तान को मंगोल हमलावरों से बचाने अलावा उनकी इन्तेजामि इस्लाहात, मेहसुलात और सल्तनत मे कीमतों पर कंट्रोल समेत ढेरों काम के लिए याद किया जाता है।
जब सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने हुकूमत संभाली थी तब मंगलों ने दुनिया भर में अफरा-तफरी मचा रखी थी। ख़्वारज़्म से लेकर ईरान, इराक समेत बगदाद जैसे बड़े शहर को मंगोलो ने खाक में मिला दिया था। अब जब मंगोल हिंदुस्तान को रौंदते हुए मंगोलिया जाने की कोशिस कर रहे थे। तब अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी जहानत से उनकी कोशिशों को नाकाम बना दिया। और मंगोलों से हुयी एक झड़प के बाद 8000 मंगोलो के सर को कलम कर के दिल्ली में उस वक्त बन रहे सीरी फोर्ट के मीनारों में चुनवा दिया, और मंगोलो को तजाकिस्तान के रास्ते से होकर गुजरने के लिए मजबूर कर दिया।
इसके अलावा सुल्तान बनते ही अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले टैक्स सिस्टम को सुधारा उन्होंने सिस्टम से बिचौलियों को हटाकर सीधे आम आदमी से जोड़ा बिचौलियों के हटने किसानों और गरीबो को बहुत फायदा हुआ। इस टैक्स सिस्टम को शेर शाह सूरी से लेकर मुग़लों तक ने इस्तेमाल किया।
कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की किताब "The Cambridge Economic History of India" में इस बात का ज़िक़्र है, की ख़िलजी का टैक्स सिस्टम हिंदुस्तान का सबसे अच्छा टैक्स सिस्टम था जो अंग्रेजों के आने तक चला।
अलाउद्दीन खिलजी ने सुल्तान बनते ही बड़ी तेजी से अपनी सल्तनत को फैलाया रणथम्भौर, चित्तौड़, मालवा, सिवान, जालोर, देवगिरी, वरंगल, जैसी सारी रियासतें सुल्तान के झोली में आ गिरीं। ख़िलजी ने अपनी जिंदगी की कोई भी जंग नहीं हारी लेकिन एक बीमारी से हार गया और कम उम्र (49-50 वर्ष) में ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया था।
सुल्तान अलाउद्दीन ख़िलजी के गुज़र जाने के दसियों बरस बाद भी लोग उनके दौर को ये कह कर हसरत से याद करते रहे की मरहूम सुल्तान के वक़्त में रोटी की इतनी क़ीमत नहीं थी और ज़िन्दगी बसर करना इतना मुश्किल नहीं था।
सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के दौर में 11 ग्राम चांदी के एक सिक्के के एवज़ में 85 किलो गेंहू मिला करता था। खाने की चीज़ों के ऐसे कम दाम उनकी हुकूमत के ख़त्म होने तक क़ायम रहे। बारिश हो या ना हो, फ़सल अच्छी हो या ख़राब हो जाये, खाने की चीज़ों के दाम रत्ती भर भी नहीं बढ़ते थे।
-आरिफ़ ख़लील रज़ा
रोहतक के टीपू सुल्तान रिसालदार बशारत अली राव, राव बाबर खाँ और राव साबर खाँ, जिन्होंने रोहतक जेल पर अपना झंडा फहरा दिया था!
रोहतक ज़िले के रांघड़ मुस्लिम बड़ी संख्या में ईस्ट इंडिया कंपनी की रेगुलर रेजिमेंट में बतौर सैनिक काम कर रहे थे। वो छुटियों में अपने अपने गाँव आ कर लोगों को अंग्रेज़ों के खिलाफ बग़ावत के लिए तैयार करने लगे, जिसकी भनक लगते ही रोहतक के कलेक्टर 'जॉन एडम लोच' ने छुट्टी पर गये सभी सैनिकों को हेडक्वार्टर में वापस आने के आदेश जारी कर दिए।
लेकिन तब तक लोगों में बग़ावत ज़ोर पकड़ने लगी और इस आग में घी का काम बहादुर शाह ज़फर के दूत तफ़ज़्ज़ुल हुसैन ने किया जो एक छोटी फ़ौज की टुकड़ी लेकर रांघड़ो से मिल गया। रोहतक के कलेक्टर जॉन एडम लोच ने बागियों का सामना न कर पाने की हालत में अपने अधिकारियों सहित वहाँ से भाग जाना ज़्यादा मुनासिब समझा।
अँगरेज़ अफसरों के भागने के बाद अपने सामने खुला मैदान देख रोहतक के राँघड़ो ने सरकारी ऑफिस और बंगलो में आग लगा दी और रोहतक जेल से कैदियों को आज़ाद करा लिया। राँघड़ो के हाथों कोई अंग्रेज़ तो मारा नहीं गया लेकिन उन्होंने अंग्रेजी सरकार के संस्थानों को काफी नुक़सान पहुँचा कर अपना झंडा फहरा दिया।
बागियों को क़ाबू करने के लिए थॉमस सीटोन के नेतृत्व में जॉन एडम लोच 60th regiment native infantry के साथ रोहतक पहुंचा, उन्होंने रेजिमेंट के साथ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रोहतक में कैंप बनाया। बाग़ी हालातों को देख कर अँगरेज़ अधिकारियो को सैनिकों पर भरोसा नहीं था और हुआ भी वही रेजिमेंट में बग़ावत हो गयी
रांघड़ो ने इस मौक़े का फायदा उठाया व राव बाबर खाँ की क़यादत में बग़ावत को और सख़्त कर दिया। रंघड़ो का विद्रोह सबसे खतरनाक दो वजहों से रहा एक तो बड़ी तादाद में रांघड़ सैनिकों की रेजिमेंट का विद्रोहियों के साथ शामिल हो जाना और दूसरा उन्हें बशारत अली और बाबर खाँ जैसे अच्छे लीडर मिल जाना।
बशारत अली की क़यादत में रंघड़ो ने रोहतक का बड़ा हिस्सा अंग्रेज़ों से आज़ाद करा लिया, दिल्ली पंजाब जीटी रोड पर बढ़ने से रोकने लिए मेजर जनरल विल्सन ने लेफ्टिनेंट हडसन को 6 अँगरेज़ अधिकारियों और हथियारबंद 361 सिपाहियों के साथ रोहतक भेजा।
इस खबर के मिलते ही रिसालदार बशारत अली राव ने राँघड़ो के साथ खरखौदा के लंबरदार की हवेली में पोजीशन बना ली। और यहीं हडसन की फ़ौज से रांघड़ो का सामना हुआ।
ख़ुद हडसन का कहना है कि रांघड़ रिसालदार की क़यादत में बेमिसाल बहादुरी से लड़े (They fought like devil) लेकिन रिसालदार बशारत अली, अंग्रेजों के अच्छे हथियार और ज़्यादा तादाद में होने की वजह से अपने 25 साथियों के साथ लड़ते हुए शहीद हो गए।
मुश्किल से हडसन ने ये लड़ाई ख़त्म ही की थी, उसे ख़बर मिली कि राव साबर खाँ की क़यादत में रांघड़ कभी भी हमला कर सकते हैं। हडसन इस ख़बर के मिलते ही राव साबर खाँ का सामना करने के लिए निकल पड़ा। तड़के ही लेफ्टिनेंट हडसन की सेना पर 300 रांघड़ घुड़सवार और 1,000 रांघड़ बाग़ी बिजली की तरह टूट पड़े। इस भीषण हमले के बाद हडसन और उसके बचे खुचे साथियों को जींद के राजा और जाटों की मदद से दिल्ली भगाना पड़ा।
प्रस्तुति : आमिर ख़ान मेव
Source: Haryana state Gazetteer
सुल्तान उल-हिंद हज़रत ख़्वाजा ग़रीब नवाज़ का ऊर्स मुबारक
आप सब को अता-ए-रसूल, सुल्तान-उल-हिंद हजरत सैयद ख़्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी अजमेरी हसनी वल हुसैनी अल-मारूफ ख़्वाजा ग़रीब नवाज़ (कद्दस अल्लाहू सिर्राहु) के 811 वा उर्स मुबारक हो।
हज़रत ख़्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती (क़द्दास अल्लाहु सिर्राहु) का जन्म 537 एएच (इस्लामिक वर्ष) में सिजिस्तान (वर्तमान ईरान में) के एक क्षेत्र संजर नामक स्थान पर हुआ था। आपका असली नाम मोइनुद्दीन हसन है और आप प्यारे पैगंबर ﷺ कि आल से हुसैनी सैयद हैं। आपके लक़ब सुल्तान उल-हिंद, ग़रीब नवाज, अता-ए-रसूल, वारिस उन-नबी, हिंद अल-वली, नायब अल-रसूल फिल-हिंद और ख़्वाजा-ए-बुजुर्ग हैं।
आपने इल्म हासिल करने के लिए 15 साल की छोटी सी उम्र में सफर करना शुरू कर दिया । मुक़द्दस इल्म को हासिल करने के लिए आपने समरखंड, बुखा़रा, बग़दाद, मक्का अल-मुकर्रमाह और मदीना अल-मुनव्वराह का सफर किया।
आप बाहरी इस्लामी विज्ञानों के माहिर शेख़ बन चुके थे, लेकिन आप को एक पीर ओ मुर्शिद की तलाश थी जो आपको अंदरूनी इस्लामी विज्ञान (मारिफत) सिखा सकें और अल्लाह सुभानहू वा ताआला के क़रीब ले आएँ ।
बाद में आपने हज़रत ख़्वाजा उस्मान हारूनी (क़द्दास अल्लाहु सिर्राहु) के हाथों पर बैत ली और चिश्ती तरीक़े में दाख़िल हुए । आप अपने शेख़ की ख़िदमत में 30 साल रहे।
हज़रत ख़्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती (कद्दास अल्लाहू सिर्राहु) ने एक बार फरमाया, "जब मैं हज़रत ख़्वाजा उस्मान हारूनी से मिला, और उनका मुरीद बना, तो मैंने 8 साल इस तरह से गुज़ारे कि मैंने आराम नहीं किया। मेरी सिर्फ़ एक फिक्र होती की मैं अपनी ख़िदमत और अकी़दत से उन्हें ख़ुश कर सकूँ। जब मेरे पीर ओ मुर्शिद दौरों पे जाते, तो मैं उनके बिस्तर और खाने को अपने सिर पर रख के चलता। मेरे पीर ओ मुर्शिद ने मेरी ख़िदमत को क़ुबूल फरमाया। उन्होंने मुझ से ख़ुश हों के मुझे ऐसे तोहफे अता किए जिनको बयान ही नही कर सकते । मैं उनके तोहफों और मेहेरबानी के लिए उनका शुक्रगुज़ार हूं।"
हज़रत ख़्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती (कद्दस अल्लाहु सिर्राहु) को नबी ए पाक ﷺ ने मदीना मुनवराह, सऊदी अरब में हुकुम दिया के वह हिंदुस्तान में मोहब्बत, इंसानियत और ईमान फैलाएँ । हज़रत ख़्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती (कद्दस अल्लाहु सिर्राहु) ने अजमेर, हिंदुस्तान के लिए रवाना होने से पहले हज़रत दाता गंज बख़्श अली हिजवेरी (कद्दस अल्लाह सिर्राहु) के मक़ाम के पास 40 दिन का चिल्ला निकाला।
आप अजमेर, हिंदुस्तान में एक ज़ालिम हुकुमरान के ख़िलाफ खड़े हुए और वाक़ई में आप गरीब नवाज़ थे। आपने जाति, वर्ग, धर्म के बावजूद किसी के साथ भेदभाव नहीं किया और गरीबों को खिलाने और उनकी मदद करने के लिए आप बेपनाह सख़ावत के लिए जाने जाते थे। आपने अपने मुबारक हाथों से 90 लाख से अधिक लोगों को इस्लाम में दाख़िल किया, और आपके कई मोजज़ात रहे।
आप इशा (रात की नमाज़) के वुज़ू के साथ अपनी फज्र (सुबह की नमाज़) पढ़ने के लिए जाने जाते थे और रोज़ाना क़ुरान ए पाक को दो बार पड़ने के लिए जाने जाते थे।
आपकी आरामगाह अजमेर शरीफ, हिंदुस्तान में है। आपसे फैज़ ओ बरकात हासिल करने के लिए सभी अलग-अलग जगह से लाखों की तादाद में लोग हाज़री की लिए आपके दरबार में आते हैं।
अजमेर, हिंदुस्तान में आपकी दरगाह में आज भी आपका लंगर ख़ाने में बड़ी मख़दार में देगों में खाना पकाया जाता है जो बग़ैर किसी से पैसे लिए हर दिन हजारों लोगों को खाना खिलाने के लिए मशहूर है।
दुआ:
या मेरे अल्लाह जुमला अंबिया के वास्ते,
हाजतें बरला मेरी कुल औलिया के वास्ते
सिलसिला-ए-आलिया ख़ुशहालिया
आप सब को अता-ए-रसूल, सुल्तान-उल-हिंद हजरत सैयद ख़्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी अजमेरी हसनी वल हुसैनी अल-मारूफ ख़्वाजा ग़रीब नवाज़ (कद्दस अल्लाहू सिर्राहु) के 811 वा उर्स मुबारक हो।
हज़रत ख़्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती (क़द्दास अल्लाहु सिर्राहु) का जन्म 537 एएच (इस्लामिक वर्ष) में सिजिस्तान (वर्तमान ईरान में) के एक क्षेत्र संजर नामक स्थान पर हुआ था। आपका असली नाम मोइनुद्दीन हसन है और आप प्यारे पैगंबर ﷺ कि आल से हुसैनी सैयद हैं। आपके लक़ब सुल्तान उल-हिंद, ग़रीब नवाज, अता-ए-रसूल, वारिस उन-नबी, हिंद अल-वली, नायब अल-रसूल फिल-हिंद और ख़्वाजा-ए-बुजुर्ग हैं।
आपने इल्म हासिल करने के लिए 15 साल की छोटी सी उम्र में सफर करना शुरू कर दिया । मुक़द्दस इल्म को हासिल करने के लिए आपने समरखंड, बुखा़रा, बग़दाद, मक्का अल-मुकर्रमाह और मदीना अल-मुनव्वराह का सफर किया।
आप बाहरी इस्लामी विज्ञानों के माहिर शेख़ बन चुके थे, लेकिन आप को एक पीर ओ मुर्शिद की तलाश थी जो आपको अंदरूनी इस्लामी विज्ञान (मारिफत) सिखा सकें और अल्लाह सुभानहू वा ताआला के क़रीब ले आएँ ।
बाद में आपने हज़रत ख़्वाजा उस्मान हारूनी (क़द्दास अल्लाहु सिर्राहु) के हाथों पर बैत ली और चिश्ती तरीक़े में दाख़िल हुए । आप अपने शेख़ की ख़िदमत में 30 साल रहे।
हज़रत ख़्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती (कद्दास अल्लाहू सिर्राहु) ने एक बार फरमाया, "जब मैं हज़रत ख़्वाजा उस्मान हारूनी से मिला, और उनका मुरीद बना, तो मैंने 8 साल इस तरह से गुज़ारे कि मैंने आराम नहीं किया। मेरी सिर्फ़ एक फिक्र होती की मैं अपनी ख़िदमत और अकी़दत से उन्हें ख़ुश कर सकूँ। जब मेरे पीर ओ मुर्शिद दौरों पे जाते, तो मैं उनके बिस्तर और खाने को अपने सिर पर रख के चलता। मेरे पीर ओ मुर्शिद ने मेरी ख़िदमत को क़ुबूल फरमाया। उन्होंने मुझ से ख़ुश हों के मुझे ऐसे तोहफे अता किए जिनको बयान ही नही कर सकते । मैं उनके तोहफों और मेहेरबानी के लिए उनका शुक्रगुज़ार हूं।"
हज़रत ख़्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती (कद्दस अल्लाहु सिर्राहु) को नबी ए पाक ﷺ ने मदीना मुनवराह, सऊदी अरब में हुकुम दिया के वह हिंदुस्तान में मोहब्बत, इंसानियत और ईमान फैलाएँ । हज़रत ख़्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती (कद्दस अल्लाहु सिर्राहु) ने अजमेर, हिंदुस्तान के लिए रवाना होने से पहले हज़रत दाता गंज बख़्श अली हिजवेरी (कद्दस अल्लाह सिर्राहु) के मक़ाम के पास 40 दिन का चिल्ला निकाला।
आप अजमेर, हिंदुस्तान में एक ज़ालिम हुकुमरान के ख़िलाफ खड़े हुए और वाक़ई में आप गरीब नवाज़ थे। आपने जाति, वर्ग, धर्म के बावजूद किसी के साथ भेदभाव नहीं किया और गरीबों को खिलाने और उनकी मदद करने के लिए आप बेपनाह सख़ावत के लिए जाने जाते थे। आपने अपने मुबारक हाथों से 90 लाख से अधिक लोगों को इस्लाम में दाख़िल किया, और आपके कई मोजज़ात रहे।
आप इशा (रात की नमाज़) के वुज़ू के साथ अपनी फज्र (सुबह की नमाज़) पढ़ने के लिए जाने जाते थे और रोज़ाना क़ुरान ए पाक को दो बार पड़ने के लिए जाने जाते थे।
आपकी आरामगाह अजमेर शरीफ, हिंदुस्तान में है। आपसे फैज़ ओ बरकात हासिल करने के लिए सभी अलग-अलग जगह से लाखों की तादाद में लोग हाज़री की लिए आपके दरबार में आते हैं।
अजमेर, हिंदुस्तान में आपकी दरगाह में आज भी आपका लंगर ख़ाने में बड़ी मख़दार में देगों में खाना पकाया जाता है जो बग़ैर किसी से पैसे लिए हर दिन हजारों लोगों को खाना खिलाने के लिए मशहूर है।
दुआ:
या मेरे अल्लाह जुमला अंबिया के वास्ते,
हाजतें बरला मेरी कुल औलिया के वास्ते
सिलसिला-ए-आलिया ख़ुशहालिया
फ़िरदौस ख़ान
हिंदुस्तान के बेहतरीन शायर मिर्ज़ा ग़ालिब ने उर्दू शायरी को नई ऊंचाई दी. उनके ज़माने में उर्दू शायरी इश्क़, मुहब्बत, विसाल, हिज्र और हुस्न की तारी़फों तक ही सिमटी हुई थी, लेकिन ग़ालिब ने अपनी शायरी में ज़िंदगी के विभिन्न रंगों को शामिल किया. उनकी शायरी में हक़ीक़त के रंग हैं, तो फ़लसफ़े की रोशनीभी है. हालांकि उस व़क्त कुछ लोगों ने उनका मज़ाक़ भी उ़डाया, लेकिन उन्होंने इसकी परवाह नहीं की. यहां तक कि ब्रिटिश हुकूमत को भी उन्होंने काफ़ी सराहा. उन्होंने 1857 के आंदोलन के दौरान रूदाद लिखी. फ़ारसी में लिखी इस रूदाद को दस्तंबू नाम से प्रकाशित कराया गया फ़ारसी में दस्तंबू का मतलब है फूलों का गुलदस्ता.
हाल में राजकमल ने दस्तंबू का हिंदी अनुवाद प्रकाशित किया है. फ़ारसी से इसका हिंदी अनुवाद डॉ. सैयद ऐनुल हसन और संपादन अब्दुल बिस्मिल्लाह ने किया है. मिर्ज़ा ग़ालिब दस्तंबू के ज़रिए अंग्रेजों से कुछ आर्थिक सहायता हासिल करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मुंशी हरगोपाल तफ्त को कई लंबे-लंबे ख़त लिखकर किताब को जल्द प्रकाशित कराने का अनुरोध किया. इन ख़तों को भी इस किताब में प्रकाशित किया गया है. इसके साथ ही किताब के आख़िर में क्वीन विक्टोरिया की शान में लिखा क़सीदा भी है, जिससे अंग्रेज़ों के प्रति ग़ालिब की निष्ठा को समझा जा सकता है, भले ही वह उनकी मजबूरी ही क्यों न हो!
दरअसल, मिर्ज़ा ग़ालिब की इस डायरी में 1857 के हालात को पेश किया गया है. अंग्रेज़ों के दमन से परेशान होकर जब हिंदुस्तान के जांबाज़ों ने 31 मई, 1857 को सामूहिक विद्रोह करने का फ़ैसला किया, तब सैनिक मंगल पांडे ने 29 मार्च, 1857 को चर्बी लगे कारतूसों का इस्तेमाल करने से इंकार करके इस आंदोलन की शुरुआत की. नतीजतन, मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया और 8 अप्रैल, 1857 को उन्हें अंतत: फांसी दे दी गई. इस पर भारतीय सैनिकों ने बग़ावत करते हुए 10 मई, 1857 को ब्रिटिश हुकूमत के ख़िलाफ़ आंदोलन छेड़ दिया. आंदोलन की आग सबसे पहले मेरठ में भड़की. इसके बाद सैनिक दिल्ली आ गए और कर्नल रिप्ले को मार दिया. आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेज़ों ने भी सख्ती बरती और नरसंहार शुरू हो गया. उस वक़्त ग़ालिब पुरानी दिल्ली के बल्लीमारान इलाक़े में रहते थे. उन्होंने क़त्लेआम अपनी आंखों से देखा था. उनके कई दोस्त मारे जा चुके थे और कई दोस्त दिल्ली छो़डकर चले गए थे. ग़ालिब अकेले अपने घर में मुसीबत से भरी ज़िंदगी जी रहे थे. दस्तंबू में उन्होंने अपने तल्ख़ अनुभवों को मार्मिकता से पेश किया है. इसमें उन्होंने 11 मई, 1857 की हालत का काव्यात्मक वर्णन भी किया है. ख़ास बात यह है कि उन्होंने अंग्रेजों की प्रशंसा करते हुए बाग़ियों को ख़ूब खरी-खोटी सुनाई है.
किताब की शुरुआत हम्द यानी ईश प्रार्थना से हुई है और इसके बाद ग़ालिब ने अपनी रूदाद लिखी है. वह लिखते हैं-
मैं इस किताब में जिन शब्दों के मोती बिखेर रहा हूं, पाठकगण उनसे अनुमान लगा सकते हैं कि मैं बचपन से ही अंग्रेज़ों का नमक खाता चला आ रहा हूं. दूसरे शब्दों में कहना चाहिए कि जिस दिन से मेरे दांत निकले हैं, तब से आज तक इन विश्वविजेताओं ने ही मेरे मुंह तक रोटी पहुंचाई है. ज़ाहिर है कि ग़ालिब ने जिस अंग्रेज़ सरकार का नमक खाया था, वह उनकी नज़र में बेहद इंसाफ़ पसंद और मासूम सरकार थी. हालांकि ग़ालिब का रिश्ता मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र से भी था और ज़फ़र की शायरी के वह उस्ताद थे. शहंशाह बहादुर शाह ज़फ़र ने उन्हें दबीर-उल-मुल्क और नज़्म-उद्दौला के ख़िताब से नवाज़ा. बाद में उन्हें मिर्ज़ा नोशा के ख़िताब से भी सम्मानित किया गया. वह बहादुर शाह ज़फ़र के दरबार में महत्वपूर्ण दरबारी थे. उन्हें बहादुर शाह ज़फ़र के ब़डे बेटे फ़क़रुद्दीन मिर्ज़ा का शिक्षक तैनात किया गया. इसके अलावा वह म़ुगल दरबार के शाही इतिहासकार भी रहे. इसके बावजूद वह बादशाह से मुतमईन नहीं थे. वे लिखते हैं-
मैं हफ्ते में दो बार बादशाह के महल में जाता था और अगर उसकी इच्छा होती, तो कुछ समय वहां बैठता था, अन्यथा बादशाह के व्यस्त होने की वजह से थोड़ी देर में ही दीवान-ए-ख़ास से उठकर अपने घर की ओर चल देता था. इस बीच जांची हुई रचनाओं को या तो ख़ुद वहां पहुंचा देता या बादशाह के दूतों को दे देता था, ताकि वे बादशाह तक पहुंचा दें. बस, मेरा इतना ही काम था और दरबार से मेरा इतना ही नाता था. हालांकि यह छोटा-सा सम्मान, मानसिक और शारीरिक दृष्टि से आरामदायक और दरबारी झगड़ों से दूर था, लेकिन आर्थिक दृष्टि से सुखप्रद नहीं था. उस पर भी ग्रहों का चक्कर मेरे इस छोटे-से सम्मान को मिट्टी में मिला देने पर तुला हुआ था.
अंग्रज़ों से ग़ालिब को आर्थिक संरक्षण भी मिला और सम्मान भी. लिहाज़ा वह उनके प्रशंसक हो गए. अंग्रेजों और भारतीयों की तुलना करते हुए वह लिखते हैं-
एक वह आदमी, जो नामवर और सुविख्यात था, उसकी सारी प्रतिष्ठा धूल में मिल गई थी. दूसरा वह, जिसके पास न इज्ज़त थी और न ही दौलत, उसने अपना पांव चादर से बाहर फैला दिया.
दरअसल, ग़ालिब शासक को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि मानते थे, इसलिए उनकी नज़र में राजद्रोह का मतलब देशद्रोह था. वह ख़ुद कहते हैं-
ख़ुदा जिसे शासन प्रदान करता है, निश्चय ही उसे धरती को जीतने की शक्ति भी प्रदान करता है. इसलिए जो व्यक्ति शासकों के विरुद्ध कार्य करता है, वह इसी लायक़ है कि उसे सिर पर जूते पड़ें. शासित का शासक से लड़ना अपने आपको मिटाना है.
ग़ालिब पहले शायर नहीं थे, जिन्होंने राज दरबार के प्रति अपनी निष्ठा ज़ाहिर की, बल्कि उस दौर के अनेक साहित्यकारों ने ब्रिटिश हुकूमत का साथ दिया. भारतेन्दु हरिश्चंद्र पर भी इस तरह के आरोप लगे, लेकिन ग़ालिब का अपना अंदाज़ था. हालांकि भारतेन्दु ने अंग्रेज़ी शासन की आलोचना भी की. भले ही ग़ालिब ने दस्तंबू में अंग्रेज़ी हुकूमत की सराहना की है, लेकिन शायरी के लिहाज़ से यह किताब लाजवाब है. अंग्रेज़ों की मौत का ज़िक्र करते हुए वे लिखते हैं-
दुख होता है उन रूपवती, कोमल, चंद्रमुखी और चांदी जैसे बदन वाली अंग़्रेज महिलाओं की मौत पर. उदास हो जाता है मन, उन अंग्रेज़ बालकों के असामयिक अंत पर, जो अभी संसार को भली-भांति देख भी नहीं पाए थे. स्वयं वे फूलों की भांति थे और फूलों को देखकर हंस पड़ते थे.
उन्होंने विद्रोह के दौरान दिल्ली के बाशिंदों की बदहाली का भी बेहद मार्मिक वर्णन किया है. वह लिखते हैं-
15 सितंबर से हर घर बंद प़डा हुआ है. न तो कोई सौदा बेचने वाला है और न ही कोई ख़रीदने वाला. गेहूं बेचने वाले कहां हैं कि उनसे गेहूं ख़रीदकर आटा पिसवा सकूं. धोबी कहां, जो कपड़ों की बदबू दूर हो. नाई कहां, जो बाल काटे. भंगी कहां, जो घर का कूड़ा साफ़ करे.
जब दिल्ली में क़त्लेआम हो रहा था, तब ग़ालिब अपने घर में बंद थे. वह लिखते हैं-ऐसे वातावरण में मुझे कोई भय नहीं था. ऐसे में मैंने ख़ुद से कहा कि मैं क्यों किसी से भयभीत रहूं. मैंने तो कोई पाप किया नहीं है, इसलिए मैं सज़ा का पात्र नहीं हूं. न तो अंग्रेज़ बेगुनाह को मारते हैं, और न ही नगर की हवा मेरे प्रतिकूल है. मुझे क्या पड़ी है कि ख़ुद को हलकान करूं. मैं एक कोने में, अपने घर में ही बैठा अपनी क़लम से बातें करूं और क़लम की नोक से आंसू बहाऊं. यही मेरे लिए अच्छा है.
मेरी खोली ख़ाली है
मेरे आशा-तरु के पत्ते झड़ चुके हैं
या ख़ुदा ! मैं कब तक इस बात से ख़ुश होता रहूं
कि मेरी शायरी हीरा है
और ये हीरे मेरी ही खान के ख़ज़ाने हैं
ग़ालिब क़िस्मत पर बहुत यक़ीन करते थे, तभी तो वह लिखते हैं-
जन्म से जो भाग्य में लिखा है, उसे बदला नहीं जा सकता. हर जन्मी का भाग्य एक अदृश्य फ़रमान में बंद है, जिसमें न कोई आरंभ है और न कोई अंत. सभी को वही मिला है, जो उस फ़रमान में लिखा हुआ है. हमारे सुख और दुख उसी से संचालित हैं. इसलिए हमें बुज़दिल और डरपोक नहीं होना चाहिए, बल्कि छोटे बच्चों की भांति वक़्त के रंगों का हंसी-ख़ुशी तमाशा देखना चाहिए.
बहरहाल, इस किताब के ज़रिये राजकमल प्रकाशन ने हिंदी पाठकों को मिर्ज़ा ग़ालिब की दस्तंबू से रूबरू होने का मौक़ा दिया है, जो सराहनीय है. दरअसल, अनुवाद के ज़रिए हिंदी पाठक उर्दू, फ़ारसी और अन्य भाषाओं की महान कृतियों को पढ़ पाते हैं. किताब के आख़िर में मुश्किल शब्दों का अर्थ दिया गया है, जिससे पाठकों को इसे समझने में आसानी होगी. कुल मिलाकर यह एक बेहतरीन किताब है.
समीक्ष्य कृति : दस्तंबू
लेखक : मिर्ज़ा ग़ालिब
प्रकाशक : राजकमल प्रकाशन
क़ीमत : 200 रुपये
ज़मीर बेचने वालों ने इंतेहा कर दी
बुझे चराग़ को भी आफ़ताब लिखने लगे
वो जिसने ऐन से इज़्ज़त कभी नहीं लिक्खा
उसे भी सरफिरे इज़्ज़त मआब लिखने लगे
ये इंतक़ाम लिया अपनी बदनसीबी से
हम अपने नाम से पहले नवाब लिखने लगे
ताल्लुक़ात का कुछ तो भरम रखा होता
ज़रा सा दूर चले और हिसाब लिखने लगे
हसीब सोज़
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने आज नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में वीरता, सामाजिक सेवा, पर्यावरण, खेल, कला एवं संस्कृति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धियों के लिए बच्चों को ‘प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार’ प्रदान किए. उन्होंने इस मौक़े पर केरल के पालक्कड़ के ग्यारह साल के मोहम्मद सिद्दान को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार-2025 प्रदान कर सम्मानित किया.
मोहम्मद सिद्दान को यह पुरस्कार अपने दो दोस्तों की जान बचाने के लिए दिया गया है. जब उनके दोस्तों को करंट लग गया था, तब सिद्दान ने दिलेरी दिखाते हुए अपनी जान की परवाह किए बिना लकड़ी के डंडे की मदद से उनकी जान बचाई. उनके इस जज़्बे के लिए उन्हें बहादुरी के लिए इस राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया.
इस अवसर पर राष्ट्रपति ने ‘प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार’ प्राप्त करने वाले सभी बच्चों को बधाई दी. उन्होंने कहा कि पुरस्कार विजेता बच्चों ने अपने परिवारों, समुदायों और पूरे देश का गौरव बढ़ाया. उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ये पुरस्कार देश भर के सभी बच्चों को प्रेरित करेंगे. उन्होंने कहा कि यह पुरस्कार उन्हें प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रदान किए गए. उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ये पुरस्कार देश के सभी बच्चों को प्रेरित करेंगे.
राष्ट्रपति ने कहा कि किसी देश की महानता तब निश्चित होती है, जब उसके बच्चे देशभक्ति और उच्च आदर्शों से परिपूर्ण होते हैं. उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि बच्चों ने वीरता, कला एवं संस्कृति, पर्यावरण, नवाचार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा और खेल जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अपनी असाधारण प्रतिभा का प्रदर्शन किया है. उन्होंने कहा कि सात वर्षीय वाका लक्ष्मी प्रग्निका जैसे प्रतिभाशाली बच्चों के कारण ही भारत को विश्व पटल पर शतरंज की महाशक्ति माना जाता है. अजय राज और मोहम्मद सिदान पी, जिन्होंने अपनी वीरता और सूझबूझ से दूसरों की जान बचाई, प्रशंसा के पात्र हैं. नौ वर्षीय बेटी व्योमा प्रिया और ग्यारह वर्षीय बहादुर बेटे कमलेश कुमार ने अपने साहस से दूसरों की जान बचाते हुए अपनी प्राण गंवा दिए. दस वर्षीय श्रवण सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान युद्ध से जुड़े जोखिमों के बावजूद अपने घर के पास सीमा पर तैनात भारतीय सैनिकों को नियमित रूप से पानी, दूध और लस्सी पहुंचाई. वहीं दिव्यांग बेटी शिवानी होसुरू उप्पारा ने आर्थिक और शारीरिक सीमाओं को पार करते हुए खेल जगत में असाधारण उपलब्धियां हासिल की हैं. वैभव सूर्यवंशी ने अत्यंत प्रतिस्पर्धी और प्रतिभा-समृद्ध क्रिकेट जगत में अपनी अलग पहचान बनाई है और कई रिकॉर्ड स्थापित किए. श्रीमती मुर्मु ने विश्वास व्यक्त किया कि ऐसे साहसी और प्रतिभाशाली बच्चे आगे भी अच्छे कार्य करते रहेंगे और भारत के भविष्य को उज्ज्वल बनाएंगे.
26 दिसम्बर 2025
श्रीनगर के महज़ तेरह साल के मुस्लिम छात्र उज़ैर मलिक ने कोडिंग की दुनिया में इतिहास रच दिया है. उन्होंने अब तक 31 मोबाइल और वेब ऐप्स बनाए हैं.
जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर शहर के सैदपुरा ईदगाह इलाक़े के रहने वाले उज़ैर मलिक को मोबाइल का बहुत शौक़ है. यह शौक़ मोबाइल में वीडियो सर्च करने का नहीं, बल्कि मोबाइल मोबाइल और वेब एप्लिकेशन बनाने का है. ख़ास बात यह भी है कि उन्होंने ख़ुद से कोडिंग सीखकर मोबाइल वेब ऐप्स बनाए हैं. इनमें एजुकेशनल, यूटिलिटी और फ्रीलांसिंग से जुड़े ऐप्स शामिल हैं.
असम के आर्यन ज़िशान अहमद ने अंतरिक्ष में दो नये एस्टेरॉयड खोजे हैं. इसके लिए नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (नासा) ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया है.
आर्यन ज़िशान अहमद असम के कामरूप ज़िले के रंगिया के रहने वाले हैं. वे मेघालय की यूनिवर्सिटी ऑफ़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के पहले सेमेस्टर के बी.टेक छात्र हैं. उन्होंने नासा-सपोर्टेड एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में हिस्सा लिया और मंगल-बृहस्पति के बीच मुख्य क्षुद्रग्रह पट्टी में दो नये एस्टेरॉयड खोजे. अब ये दोनों आधिकारिक तौर पर 2024 VE8 और 2024 VC23 नाम से दर्ज हैं. नासा ने उनके योगदान को एक 'प्रतिष्ठित मान्यता' दी है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सम्मान है. इस कामयाबी के बाद उनके संस्थान ने भी उन्हें सम्मानित किया.
उनके पिता मिराजुल इस्लाम और माँ रूमा नज़रीन बेटे की कामयाबी पर बहुत ख़ुश हैं. उनका कहना है कि उनके बेटे ने परिवार ही नहीं, बल्कि दुनियाभर में भारत का नाम रौशन किया है. उन्हें अपने बेटे पर गर्व है.

















.jpg)