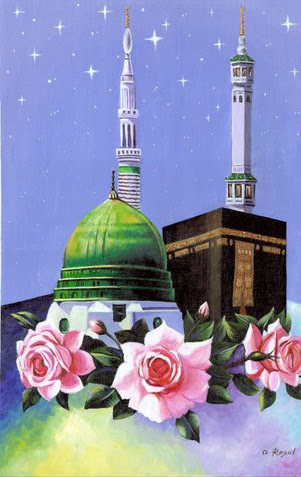अरविंद कुमार सिंह
28 मई, 2023 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया था, तभी से परिसीमन और सीटों की संख्या में वृद्धि के कयास तेज हो गए थे। क्योंकि नए भवन में लोक सभा चैबर में सीटों की संख्या 888 और राज्य सभा में 384 सांसदों के बैठने की व्यवस्था की गयी। पुराने संसद भवन में लोक सभा चैंबर में 545 और राज्य सभा में 245 सीटें थीं। सीटें तो अभी भी इतनी ही हैं। पुराने भवन में काम चल सकता था लेकिन सरकार ने नए संसद भवन को बनाने में जो जल्दबाजी दिखाई उससे राजनीतिक हलकों में यह संदेश गया कि नया परिसीमन, एक देश एक चुनाव जैसे एजेंडे पर सरकार आगे बढ़ेगी। इसी के बाद नए संसद भवन में महिला आरक्षण विधेयक भी पारित हुआ तो इन बातों को और हवा मिली। लेकिन सरकार ने इस बीच में इनके लिए सबसे अहम 2021 की जगगणना के बारे में कोई गंभीर पहल नहीं की, यह टलती रही।
अब जैसे जैसे 2025 को चक्र घूम रहा है, फिर से यह मामला गरमाने लगा है। दक्षिण से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टैलिन ने परिसीमन की जो मुहिम चंद माह पहले आरंभ की थी, उसकी आंच अब देश के दूसरे हिस्से तक पहुंच गयी है। दक्षिण के सत्तारूढ राजनीतिक दलों में ही नहीं पंजाब से लेकर कई राज्यों में इस मुद्दे पर सुगबुगाहट तेज होती दिख रही है। बीजेडी, आप, शिरोमणि अकाली दल और बीजेडी भी इस मुहिम का हिस्सा बन चुकी है। नवीन पटनायक के इस मुहिम में शामिल होने से भाजपा हैरान है। इन्होंने साफ किया है कि वे परिसीमन के खिलाफ नहीं पर यह निष्पक्ष होना चाहिए। इन दलों ने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि न्यायसंगत परिसीमन के लिए इसे 2026 से आगे 25 वर्षों के लिए बढ़ाया जाये। इसका मतलब यह हुआ कि 1971 की जनगणना के आधार पर हुए परिसीमन के तहत ही मौजूदा सीटें बनी रहें।
राजनीति औऱ अर्थव्यवस्था में दक्षिण की अहमियत
दक्षिणी राज्य भारत की अर्थव्यवस्था में बेहद अहम भूमिका में हैं। दक्षिणी राज्यों में भारत की 19 फीसदी आबादी निवास करती है जिनका देश की जीडीपी में वे 36 फीसदी का योगदान है। विकास के विभिन्न संकेतकों में ही नहीं जनसंख्या नियंत्रण नीति को अमलीजामा पहनाने में भी उनका बेहतरीन योगदान रहा है। दक्षिणी राज्यों ने परिसीमन से जुड़ी चिताओं को अपनी पहचान से जोड़ा है और कहा है कि संसद में हमारा प्रतिनिधित्व किसी हालत में कम नहीं हो। इसका राजनीतिक संकेत यह भी जा रहा है कि भाजपा दक्षिण की सीटों में कटौती करके उत्तर में होने वाली बढ़ोतरी से अपने लिए राजनीतिक लाभ के गणित को देख रही है। जिन राज्यों में वह राजनीतिक शक्ति नहीं है, वहां सीटें कम हो सकती हैं। वहीं नवीन पटनायक ने यह लाइन ली है कि संसदीय सीटों की संख्या निर्धारण में महज आबादी ही मानदंड नहीं हो। इसीलिए चेन्नई में 22 मार्च को हुई बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि महज जनगणना के आंकड़ों पर आधारित परिसीमन स्वीकार्य नहीं होगा।
विवादों का पिटारा
दरअसल 1971 से ही परिसीमन पर विवाद रहा है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1976 में 30 साल के परिसीमन को रोकने के साथ इस बात की परिकल्पना की थी कि इस बीच में आबादी नियंत्रण के साथ कई असंतुलन दूर हो जाएंगे। पर 2001 में जब यही मुद्दा अटलजी के सामने आया तो उस समय एनडीए के नेताओं ने व्यापक विचार मंथन के बाद लोकसभा सीटों की तादाद यथावत रखने का फैसला किया। पर उस दौरान राज्यों के भीतर निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को समायोजित करने का फैसला किया जिससे प्रति प्रति सांसद आबादी अनुपात में संतुलन आ सके। 2001 की जनगणना के आधार पर अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के उम्मीदवारों के लिए सीटें आरक्षित करने का फैसला भी हुआ।
परिसीमन की जटिलताएं अपनी जगह है। इसके लिए आबादी से इतर आधार बनना भी कोई सहज काम नही है। इसीलिए 1975-76 और 2001 में जो रास्ता तत्कालीन सरकारों ने अपनाया था वही समाधान इस बार भी दोहराया जाएगा या सरकार कोई ऐसी नयी और सर्वमान्य पहल खोजेगी इस पर सबकी निगाह लगी हुई है। यह एक बेहद संवेदनशील मुद्दा है। अगर इसे ठीक से हल नहीं किया गया तो कई राज्यों में काफी समस्याएं और जटिल होगी।
संवैधानिक प्रावधान
भारत में परिसीमन की व्यवस्था के लिए संविधान के अनुच्छेद 82,170, 330 और 332 के तहत प्रावधान हैं। इसके तहत लोक सभा, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन होता है। हर 10 वर्ष पर जनगणना और उनसे मिले आंकड़ों के आधार परिसीमन की व्यवस्था सीमित कालखंड तक चली। 2001 में निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं का फिर से निर्धारण हुआ पर लोक सभा या विधानसभाओं की सीटें यथावत बनी रहीं। इस समय लोक सभा में जो सीटों की संख्या है वह मौजूदा सीटें 1971 की आबादी के हिसाब से तय है जब हमारी कुल आबादी 54 करोड़ थी जबकि अब हम 140 करोड़ पार कर गए हैं। अब जो भी आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति उत्तर प्रदेश बनने जा रहा है। 2026 की आबादी के हिसाब से अगर परिसीमन हुआ तो उत्तर प्रदेश की मौजूदा सीटें 80 से बढ कर 143 हो जाएंगी, लेकिन तमिलनाडु में 49 होगी औऱ केरल में तो एक भी सीट नहीं बढेगी। यह स्थिति बनी तो टकराव होना तय है।
परिसीमन का आधार केवल आबादी हो जरूरी नहीं है। जैसे पडोसी नेपाल में 2015 में नए संविधान के तहत आधी आबादी वाले तराई क्षेत्र को पहाड़ी क्षेत्रों की तुलना में कम सीटें आवंटित हुई क्योंकि निर्वाचन क्षेत्र का सीमांकन आबादी की जगह भौगोलिक आधार पर हुआ। निष्पक्ष प्रतिनिधित्व के क्रम में जनसंख्या, विकास सूचकांक, आर्थिक योगदान जैसे पक्षों को अगर ध्यान में रखा जाता है तो एक रास्ता निकल सकता है, पर इसके लिए आम सहमति सबसे पहले राजनीतिक दलों को बनानी होगी।
संविधान के तहत तहत 17 अप्रैल,1952 को जब पहली लोक सभा का विधिवत गठन हुआ तब सांसदों की संख्या 499 थी। उसके बाद नए राज्य बने और कई व्यवस्थाओं के बाद 31वें संविधान संशोधन 1973 में लोक सभा की सीटें 525 होते हुए फिलहाल 543 पर कायम है। लोक सभा में देश के हर हिस्से का प्रतिनिधित्व है और हर राज्य औऱ संघ शासित प्रदेश को निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है।
परिसीमन उच्चाधिकार प्राप्त आयोग करता है, जिसके फैसले को किसी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। देश में चार बार ऐसे आयोग बने हैं। आखिरी आयोग 2002 में परिसीमन अधिनियम के तहत बना था, अब जो आयोग बनेगा वो पांचवां होगा, पर आयोग का गठन और अन्य बातों पर फिलहाल सरकार मौन है।
2023 में असम में परिसीमन प्रस्ताव पर निर्वाचन आयोग ने सार्वजनिक सुनवाई की थी तो आयोग के समक्ष भौगोलिक विशेषताओं के साथ जनसंख्या घनत्व, प्रशासनिक इकाइयों जैसे कई आधारों पर बातें उठी थीं। जनसांख्यिकीय प्रारूप में बदलाव पर ध्यान देने की बात भी आयी क्योंकि कुछ जिलों में जनसंख्या वृद्धि दर कम थी औऱ कुछ जिलों में असामान्य रूप से अधिक। लिहाजा इनमें किसी का नुकसान न हो, सीटों की संख्या में कमी न हो ऐसी बातें भी उठी थीं। कोई सामाजिक समूह अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के कारण अलग-थलग महसूस न करे, चिंता का यह प्रमुख बिंदु था।
बढती आबादी पर स्थिर सीटें कब तक
आबादी की बात करें तो 19 अप्रैल 2023 को जब संयुक्त राष्ट्र पापुलेशन फंड ने भारत की आबादी करीब 142.86 करोड़ आंकते हुए इसे विश्व में अव्वल बताया। 2050 तक हमारी आभादी 166.8 करोड़ होगी जबकि इस दौरान चीन 131.7 करोड़ पर खड़ा होगा। 2000 में हमारी आबादी 106 करोड़ थी जो 2011 तक 123 करोड़ हो गयी। 2019 में वाजपेयी स्मारक संभाषण में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुकर्जी ने लोकतंत्र की मजबूती के लिए संसद के दोनों सदनों की सीटों को एक हजार करने पर जोर दिया था। पर इसे विचार से अधिक महत्व न तो सरकार ने दिया न विपक्ष ने।
सबसे शक्तिमान बनेगा उत्तर प्रदेश
परिसीमन अगर आबादी पर होगा तो बेशक उत्तर प्रदेश भाग्यविधाता प्रांत बनेगा ही। करीब 23 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश से लोक सभा के 80 और राज्य सभा के 31 सदस्य चुने जाते हैं। विधान परिषद में 100 और विधान सभा के 404 सदस्य हैं। लेकिन राजनीतिक शक्ति अपार होने के बाद भी उत्तर प्रदेश कई मानको पर पिछड़ा है।
उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों में 22 पश्चिमी उत्तर प्रदेश, 32 पूर्वी उत्तर प्रदेश, 14 मध्य उत्तर प्रदेश और 7 बुंदेलखंड के जिलों से संबंधित हैं। 2014 और 2019 मे भाजपा ने यहां सबसे अच्छी सफलता हासिल की। 2014 में तो वह 71 सीटें जीत गयी थी। पर इसी राज्य ने 2024 में भाजपा को बहुमत में आने से रोक दिया और एनडीए के घटक दलों पर निर्भरता बढा दी। भाजपा 80 में 33 सीटो पर आ गयी जबकि सपा 5 से 37 सीटों पर। पर उत्तर प्रदेश से अब तक 9 प्रधानमंत्री हुए हैं। उत्तर प्रदेश की शक्ति को देख कर ही नरेंद्र मोदी ने यहां की वाराणसी सीट को चुना। 2000 में उत्तराखंड के अलग होने के बाद भी राज्य के शक्ति संतुलन में कोई असर नहीं पड़ा है। राजनीतिक हैसियत कायम है,
इसलिए परिसीमन का मुद्दा गरमा गया है तो विपक्षी दुविधा के साथ यह साफ दिख रहा है कि वास्तव में क्या रास्ता लें इस पर सत्ता पक्ष भी कुछ स्पष्ट नहीं है।
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार और संसदीय मामलों के जानकार हैं)