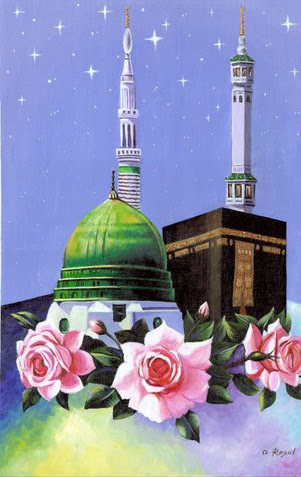अच्छा इंसान
-
अच्छा इंसान बनना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी. एक
अच्छा इंसान ही दुनिया को रहने लायक़ बनाता है. अच्छे इंसानों की वजह से ही
दुनिय...
Showing posts with label पर्यावरण. Show all posts
Showing posts with label पर्यावरण. Show all posts
ऐसे कई बांस प्रजाति होते हैं जिन्हें बगीचों में लगाया जाता है। बांस दो तरह से लगाया जाता है - संधिताक्षी और एकलाक्षी। जो बांस संधिताक्षी विधि से लगाए जाते हैं वे धीरे-धीरे बढ़ते हैं, क्योंकि इस तरह की विधि से लगाए जाने वाले पौधों की जड़ें धीरे-धीरे फैलती हैं। एकलाक्षी विधि से लगाए जाने वाले बांस बहुत तेजी से बढ़ते हैं इसलिए उनकी विशेष देखभाल की जरूरत पड़ती है। ये बांस मुख्यत: अपनी जड़ों से और कुछ मामलों में अपनी मूल गांठों के जरिए बढ़ते हैं। वे जमीन के अंदर तेजी से फैलते हैं और उनकी नई-नई कोंपलें फूटकर बाहर निकल आती हैं। एकलाक्षी बांसों की प्रजातियों में बहुत विविधता है। कुछ तो एक साल में ही बहुत बढ़ जाती हैं तो कुछ लंबे समय तक एक ही जगह फैलती रहती हैं। यदि बांस में कभी-कभार फूल भी आ जाते हैं, लेकिन अलग-अलग किस्मों के बांस में फूल आने की बारंबारता भी अलग-अलग होती है। एक बार जब फूल आ जाते हैं तो पौधा मुरझाना शुरू हो जाता है और फिर मर जाता है। फूलों में जो बीज होते हैं उन्हें उस प्रजाति को दोबारा जिंदा करने के काम में लाया जा सकता है। लेकिन फूल आने की वजह से प्रजाति के बदल जाने की संभावना रहती है। इस तरह नई प्रजाति विकसित हो जाती है। ऐसे कई प्रजातियां हैं जिनका कई दशकों पहले कोई वजूद नहीं था। उन्हें फूलों ने विकसित किया। बीजों का जीवन आम तौर पर तीन से 12 महीनों का होता है। बीजों को ठंडे वातावरण में रखकर उसकी उपादेयता को कायम रखा जा सकता है। इससे उन्हें 4-8 सप्ताहों तक बोया जा सकता है। यद्यपि बांसों की कुछ ही प्रजातियों में एक समय में फूल आते हैं लेकिन जो लोग किसी विशेष प्रजाति के बाँस को लगाना चाहते हैं तो वे बीजों की प्रतीक्षा करने के बजाए पहले से ही लगे पौधों से काम चला सकते हैं।
बांस जब एक बार झुरमुट में विकसित हो जाते हैं तो बांसों को तब तक नष्ट नहीं किया जा सकता जब तक जमीन खोदकर उसकी गाँठों को समूल नष्ट न कर दिया जाए। यदि बांसों को खत्म करना है तो एक विकल्प और है, और वह यह है कि उसे काट दिया जाए और जब भी नई कोंपलें निकलें उन्हें फौरन तोड़ दिया जाए। यह काम तब तक किया जाए जब तक उसकी जड़ों का दाना-पानी न बंद हो जाए। अगर एक भी पत्ती फोटोसेंथेसिस का कार्य करने के लिए कायम रही तो बांस जी उठेगा और उसका बढ़ना जारी रहेगा। बांसों की बढत क़ो नियंत्रित करने के लिए रासायनिक तरीका भी इस्तेमाल किया जाता है।
एकलाक्षी बांस को अगल-बगल फैलने से रोकने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि उसकी गांठों को लगातार छांटा जाता रहे, ताकि वहां से निकलकर बांस अपनी परिधि से बाहर नहीं जाए। इस कार्य के लिए कई औजार काम में आते हैं। अनुकूल मृदा परिस्थितियों में बांस की जड़ वाली गांठें जमीन की सतह के काफी निकट स्थित होती हैं। यानी तीन इंच तक या एक फुट तक। इसकी छंटाई साल में एक बार की जानी चाहिए लेकिन वसंत, ग्रीष्म या शीत के समय इसकी जांच जरूर की जाए। कुछ प्रजातियां ऐसी होती हैं जो बड़ी गहराई में होती हैं यहां तक कि फावड़ा उन तक नहीं पहुंच पाता।
बांस के झुरमुट को यहां-वहां फैलने से रोकने का दूसरा तरीका है कि झुरमुट के चारों तरफ बाड़ लगा दी जाए। ये तरीका सजावटी बांसों के लिए बहुत खतरनाक होता क्योंकि इससे बांस बंध जाते हैं और ऐसा लगता है कि पौधा बहुत दुखी है। ऐसे हालात में इस बात का भी अंदेशा रहता है कि गांठ ऊपर आ जाए और बाड़ तोड़कर बाहर निकल जाए। इस तरह की स्थिति में जो बांस रखे जाते हैं वे प्राय: नष्ट हो जाते हैं या उनकी बढत बाधित हो जाती है या कुछ का जीवन कम हो जाता है। उनकी बढत भी भरपूर नहीं होती, उनकी पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, उनकी जड़ों को पर्याप्त भोजन नहीं मिलता और पत्तियां झड़ने लगती हैं। बाड़ प्राय: ईंट-गारे की और विशेष एचडीपीई प्लास्टिक की बनी होती हैं। ये बाड़ कभी न कभी नाकाम हो ही जाती है या इसके अंदर के बांस को बहुत नुकसान पहुंचता है। पांच-छह सालों में प्लास्टिक की बाड़ टूटने लगती है और उसके अंदर से गांठें बाहर निकलने लगती हैं। छोटे स्थान में नियमित रखरखाव ही बांस को फैलने से रोकने का एकमात्र तरीका है। निर्बाध फलने-फूलने वाले बांसों की तुलना में बाड़ों में कैद बांसों को नियंत्रित करना खासा कठिन काम है। संधिताक्षी बांसों के लिए बाड़ या उन्हें तराशना जरूरी नहीं है। इस तरह के बांस अगर बढ़ जाएं तो उनके एक हिस्से को काट दिया जाता है।
आओ !
पौधे लगाएं
अपनी धरा को
सुंदर बनाएं
वातावरण को स्वच्छ बनाएं
आओ
मिलकर पौधे लगाएं
घर-आंगन में
जूही, बेला, गुलाब, चम्पा
और चमेली लगाएं
अपने आस-पड़ौस में
पौधे लगाएं
नीम, बरगद और पीपल लगाएं
पलाश, अमलतास और गुलमोहर से
गांव-शहर को ख़ूब सजाएं
आओ
हम सब मिलकर
पौधे लगाएं
अपनी धरा को सुंदर बनाएं...
-सरफ़राज़ ख़ान
पौधे लगाएं
अपनी धरा को
सुंदर बनाएं
वातावरण को स्वच्छ बनाएं
आओ
मिलकर पौधे लगाएं
घर-आंगन में
जूही, बेला, गुलाब, चम्पा
और चमेली लगाएं
अपने आस-पड़ौस में
पौधे लगाएं
नीम, बरगद और पीपल लगाएं
पलाश, अमलतास और गुलमोहर से
गांव-शहर को ख़ूब सजाएं
आओ
हम सब मिलकर
पौधे लगाएं
अपनी धरा को सुंदर बनाएं...
-सरफ़राज़ ख़ान
फ़िरदौस ख़ान
शहज़ादी को गूलर से बहुत प्यार था. उनके बंगले के पीछे तीन बड़े-बड़े गूलर के पेड़ थे. वे इतने घने थे कि उसकी शाखें दूर-दूर तक फैली थी. स्कूल से आकर वह अपने छोटे भाइयों और अपनी सहेलियों के साथ गूलर के पेड़ के नीचे घंटों खेलती. उसकी दादी उसे डांटते हुए कहतीं, भरी दोपहरी में पेड़ के नीचे नहीं खेलते. पेड़ पर असरात (जिन्नात) होते हैं और वह बच्चों को गूलर के पेड़ पर असरात होने की तरह-तरह की कहानियां सुनाया करतीं. लेकिन बच्चे थे कि लाख ख़ौफ़नाक कहानियां सुनने के बाद भी डरने का नाम नहीं लेते थे. दोपहरी में जैसे ही दादी जान ज़ुहर (दोपहर) की नमाज़ पढ़ कर सो जातीं, बच्चे गूलर के पेड़ के नीचे इकट्ठे हो जाते और फिर घंटों खेलते रहते. उनकी देखा-देखी आस-पड़ौस के बच्चे भी आ जाते.
जब गूलर का मौसम आता और गूलर के पेड़ लाल फलों से लद जाते तो, शहज़ादी की ख़ुशी का ठिकाना नहीं रहता. स्कूल में वह सबको बताती कि उनके गूलर के पेड़ फलों से भर गए हैं और वह सबको घर आकर गूलर खाने की दावत देती. उसकी सहेलियां घर आतीं और बच्चे गूलर के पेड़ पर चढ़कर गूलर तोड़ते. दादी जान देख लेतीं, तो खू़ब डांटती और कहतीं, गूलर की लकड़ी कमज़ोर होती है. ज़रा से बोझ से टूट जाती है. ख़ैर, बच्चों ने पेड़ पर चढ़ना छोड़ दिया. चढ़ते भी तो नीचे तने के पास मोटी शाख़ों पर ही रहते. कोई भी ज़्यादा ऊपर नहीं चढ़ता. एक बार शहज़ादी का भाई गूलर पर चलने की कोशिश कर रहा था, और दादी आ गईं. डर की वजह से वह घबरा गया और नीचे गिर गया. उसके हाथ की एक हड्डी पर चोट आई. महीनों प्लास्तर चढ़ा रहा. इस हादसे के बाद बच्चों ने गूलर पर चढ़ना छोड़ दिया. बच्चे एक पतले बांस की मदद से गूलर तोड़ने लगे. वक़्त बदलता रहा और एक दिन उसके घर वालों ने वह बंगला बेच दिया. शहज़ादी जब कभी उस तरफ़ से गुज़रती, तो गूलर के पेड़ को नज़र भर के देख लेती. कुछ दिन बाद बंगले के नये मालिक ने गूलर के तीनों पेड़ कटवा दिए. शहज़ादी को पता चला, तो उसे बहुत दुख हुआ. उसे लगा मानो बचपन के साथी बिछड़ गए. बरसों तक या यूं कहें कि गूलर के पेड़ उसकी यादों में बस गए थे. शहज़ादी बड़ी हुई और दिल्ली में नौकरी करने लगी. एक दिन वह हज़रत शाह फ़रहाद के मज़ार पर गई. वहां उसने गूलर का पेड़ देखा. यह गूलर का पेड़ उतना घना नहीं था, जितने घने उसके बंगले में लगे पेड़ थे. पेड़ की शाख़ें काट दी गई थीं, शायद इसलिए क्योंकि आसपास बहुत से घर थे. पेड़ पर पके गूलर लगे थे और ज़मीन पर कुएं के पास भी कुछ गूलर पड़े थे. शहज़ादी ने गूलर उठाया, उसे धोया और खा लिया. मानो ये गूलर न होकर जन्नत की कोई नेमत हों. वह अकसर जुमेरात को दरगाह पर जाती और गूलर को देख कर ख़ुश होती. इस बार काफ़ी दिनों बाद उसका मज़ार पर जाना हुआ, लेकिन इस बार उसे गूलर का पेड़ नहीं मिला, क्योंकि उसे काट दिया गया था. शहज़ादी को बहुत दुख हुआ. अब वह उस मज़ार पर नहीं जाती, क्योंकि उसे गूलर याद आ जाता. किसी पेड़ का कटना उसे बहुत तकलीफ़ देता है. वह सोचती है कि काश कभी उसके पास एक ऐसा घर हो, जिसमें बड़ा सा आंगन हो और वह उसमें गूलर का पेड़ लगाए. उसका अपना गूलर का पेड़. उसे उम्मीद है कि कभी तो वह वक़्त आएगा, जब उसकी यादों में बसे गूलर के पेड़ उसके आंगन में मुस्कराएंगे.
जल संरक्षण के लिए समर्पित विश्व विख्यात संस्था ‘ड्रॉप डेड फ़ाउंडेशन’ ने फ़िरदौस ख़ान को उनके पानी बचाने के लिए किये जा रहे उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया है. संस्था ने उन्हें साल 2023-2024 के बेस्ट वालंटियर अवॉर्ड से नवाज़ा है.
ग़ौरतलब है कि सुप्रसिद्ध साहित्यकार, चित्रकार, कार्टूनिस्ट और पर्यावरणविद आबिद सुरती ने साल 2007 में मुम्बई में ड्रॉप डेड फ़ाउंडेशन की शुरुआत की थी. इसकी टैगलाइन है- सेव एवरी ड्रॉप ऑर ड्रॉप डेड. इसका मक़सद जल संरक्षण को बढ़ावा देना है. इस मुहिम को देश ही नहीं, बल्कि दुनियाभर में सराहा जा रहा है. संयुक्त राष्ट्र भी इसे तवज्जो दे रहा है. संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के पूर्व कार्यकारी निदेशक एरिक सोल्हेम ने भी कई बार इसकी तारीफ़ की है.
मार्च 2008 में फ़िल्म निर्माता शेखर कपूर जल संरक्षण पर फ़िल्म बना रहे थे. उन्होंने अपनी वेबसाइट पर इस मुहिम की ख़ूब तारीफ़ की थी. सुप्रसिद्ध अभिनेता शाहरुख़ ख़ान ने भी इसे सराहा है. सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने भी जल संरक्षण की इस मुहिम की सराहना करते हुए इसकी टीम को मुबारकबाद दी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मुहिम की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए इस पर ‘वाटर वारियर’ नामक फ़िल्म बनवाई है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल भी इससे बहुत मुतासिर हैं. उन्होंने आबिद सुरती साहब को दिल्ली बुलाया और उनके वॉटर मॉडल को अपने राज्य में लागू करने का फ़ैसला किया. देश की राजधानी दिल्ली भी जल संकट से जूझ रही है.
फ़िरदौस ख़ान कहती हैं कि ज़मीन का दो तिहाई हिस्सा पानी से घिरा हुआ है, लेकिन इसमें से पीने लायक़ पानी बहुत कम यानी सिर्फ़ ढाई फ़ीसद है. इस पानी का भी दो तिहाई हिस्सा बर्फ़ के रूप में है. दुनियाभर में जितना पानी है, उसका महज़ 0.08 फ़ीसद हिस्सा ही इंसानों के लिए मुहैया है. इंसानों की ख़ामियों की वजह से ये पानी भी लगातार दूषित होता जा रहा है. कारख़ानों और नालों की गंदगी नदियों के पानी को ज़हरीला बना रही है. पहाड़ों में मुसलसल खनन होने और जंगलों को काटने की वजह से बारिश पर असर पड़ रहा है. जब हम पानी पैदा नहीं कर सकते, तो फिर हमें इसे बर्बाद करने का क्या हक़ है?
वे कहती हैं कि जो रब से मुहब्बत करता है, वह उसकी क़ुदरत के ज़र्रे-ज़र्रे से भी मुहब्बत करता है. और जिस चीज़ से मुहब्बत की जाती है, तो उसकी हिफ़ाज़त करना भी लाज़िमी हो जाता है. वैसे भी पानी की हर बूंद अनमोल है. पानी के बिना ज़िन्दगी का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता. हर जानदार चीज़ को पानी की ज़रूरत होती है. इसलिए पानी को फ़िज़ूल न बहायें, क्योंकि इससे कितने ही लोगों के गले तर हो सकते हैं.
वे बताती हैं कि हमारे देश की ज़्यादातर आबादी धार्मिक है. इसलिए जल संरक्षण का संदेश देने के लिए विभिन्न धर्मों के पोस्टर बनवाए गये हैं. हर धार्मिक स्थल पर रोज़ाना सैकड़ों से लेकर हज़ारों लोग आते हैं. वे इन संदेशों को बार-बार देखेंगे, तो इस पर विचार करेंगे और पानी बचाने पर ध्यान देंगे. मुम्बई के बाद दिल्ली और उत्तर प्रदेश के धार्मिक स्थलों पर भी जल संरक्षण का संदेश छपे पोस्टर लगाए जा रहे हैं. इस मुहिम को भरपूर जनसमर्थन मिल रहा है. आबिद सुरती साहब चाहते हैं कि ये मुहिम दुनिया के हर कोने तक पहुंचे. वे लोगों से अपील करती हैं कि वे इस मुहिम में बढ़ चढ़कर शिरकत करें, ताकि आने वाली पीढ़ियों को जल संकट से न जूझना पड़े.
दिल्ली से प्रकाशित दैनिक मयूर संवाद
2 मई 2024
दिल्ली से प्रकाशित दैनिक हमारा मैट्रो
2 मई 2024
दिल्ली से प्रकाशित दैनिक क़लम की दुनिया
2 मई 2024
2 मई 2024
प्रभुनाथ शुक्ल
गौरैया हमारी प्राकृतिक सहचरी है। कभी वह नीम के पेड़ के नीचे फूदकती और बिखेरे गए चावल या अनाज के दाने को चुगती। कभी प्यारी गौरैया घर की दीवार पर लगे आइने पर अपनी हमशक्ल पर चोंच मारती दिख जाती है। लेकिन बदलते वक्त के साथ आज गौरैया का बयां बेहद कम दिखाई नहीं देता है । एक वक्त था जब बबूल के पेड़ पर सैकड़ों की संख्या में घोसले लटके होते और गौरैया के साथ उसके चूजे चीं-चीं-चीं का शोर मचाते। बचपन की यादें आज भी जेहन में ताजा हैं लेकिन वक्त के साथ गौरैया एक कहानी बन गई है। हालांकि पर्यावरण के प्रति जागरूकता के चलते हाल के सालों में यह दिखाई देने लगी है । गौरैया इंसान की सच्ची दोस्त भी है और पर्यावरण संरक्षण में उसकी खास भूमिका भी है। दुनिया भर में 20 मार्च को गैरैया संरक्षण दिवस के रुप में मनाया जाता है। प्रसिद्ध पर्यावरणविद मो. ई दिलावर के प्रयासों से इस दिवस को चुलबुली चंचल गौरैया के लिए रखा गया। 2010 में पहली बार यह दुनिया में मनाया गया। प्रसिद्ध उपन्यासकार भीष्म साहनी जी ने अपने बाल साहित्य में गैरैया पर बड़ी अच्छी कहानी लिखी है। जिसे उन्होंने गौरैया नाम दिया। हालांकि, जागरुकता की वजह से गौरैया की आमद बढ़ने लगी है। हमारे लिए यह शुभ संकेत है।
गौरैया का संरक्षण हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इंसान की भोगवादी संस्कृति ने हमें प्रकृति और उसके साहचर्य से दूर कर दिया है। विज्ञान और विकास हमारे लिए वरदान साबित हुआ है। लेकिन दूसरा पहलू कठिन चुनौती भी पेश किया है। गौरैया एक घरेलू और पालतू पक्षी है। यह इंसान और उसकी बस्ती के पास अधिक रहना पसंद करती है। पूर्वी एशिया में यह बहुतायत पायी जाती है। यह अधिक वजनी नहीं होती हैं। इसका जीवन काल दो साल का होता है। यह पांच से छह अंडे देती है। आंध्र यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन में गौरैया की आबादी में 60 फीसदी से अधिक की कमी बताई गई है। ब्रिटेन की ‘रॉयल सोसाइटी आफ प्रोटेक्शन आफ बर्डस‘ ने इस चुलबुली और चंचल पक्षी को ‘रेड लिस्ट‘ में डाल दिया है। दुनिया भर में ग्रामीण और शहरी इलाकों में गौरैया की आबादी घटी है। गौरैया की घटती आबादी के पीछे मानव विकास सबसे अधिक जिम्मेदार हैं। गौरैया पासेराडेई परिवार की सदस्य है. लेकिन इसे वीवरपिंच परिवार का भी सदस्य माना जाता है। इसकी लंबाई 14 से 16 सेंटीमीटर होती है। इसका वनज 25 से 35 ग्राम तक होता है। यह अधिकांश झुंड में रहती है। यह अधिक दो मिल की दूरी तय करती है। गौरैया को अंग्रेजी में पासर डोमेस्टिकस के नाम से बुलाते हैं। मानव जहां-जहां गया गौरैया उसका हम सफर बन कर उसके साथ गयी। शहरी हिस्सों में इसकी छह प्रजातियां पाई जाती हैं. जिसमें हाउस स्पैरो, स्पेनिश, सिंउ स्पैरो, रसेट, डेड और टी स्पैरो शामिल हैं. यह यूरोप, एशिया के साथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के अधिकतर हिस्सों में मिलती है। गौरैया घास के बीजों को अपने भोजन के रुप में अधिक पसंद करती है। पर्यावरण प्रेमियों के लिए यह चिंता का सवाल है। इस पक्षी को बचाने के लिए वन और पर्यावरण मंत्रालय की ओर से कोई खास पहल नहीं दिखती है। दुनिया भर के पर्यावरणविद इसकी घटती आबादी पर चिंता जाहिर कर चुके हैं।
बढ़ती आबादी के कारण जंगलों का सफाया हो रहा है। ग्रामीण इलाकों में पेड़ काटे जा रहे हैं। ग्रामीण और शहरी इलाकों में बाग-बगीचे खत्म हो रहे हैं। इसका सीधा असर इन पर दिख रहा है। गांवों में अब पक्के मकान बनाए जा रहे हैं। जिसका कारण है कि मकानों में गौरैया को अपना घोंसला बनाने के लिए सुरक्षित जगह नहीं मिल रही है। पहले गांवों में कच्चे मकान बनाए जाते थे, उसमें लड़की और दूसरी वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाता था। कच्चे मकान गौरैया के लिए प्राकृतिक वारावरण और तापमान के लिहाज से अनुकूल वातावरण उपलब्ध करते थे।लेकिन आधुनिक मकानों में यह सुविधा अब उपलब्ध नहीं होती है। यह पक्षी अधिक तापमान में नहीं रह सकता है। गगन चुम्बी ऊंची इमारतें और संचार क्रांति इनके लिए अभिशाप बन गयी। शहर से लेकर गांवों तक मोबाइल टावर एवं उससे निकलते रेडिएशन से इनकी जिंदगी संकट में है।
खेती-किसानी में रसायनिक उर्वरकों का बढ़ता प्रयोग बेजुबान पक्षियों और गौरैया के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। केमिलयुक्त रसायनों के अंधाधुंध प्रयोग से कीड़े मकोड़े भी विलुप्त हो चले हैं। जिससे गौरैयों भोजन का भी संकट खड़ा हो गया है। दूसरा बड़ा कारण मकर सक्रांति पर पतंग उत्सवों के दौरान काफी संख्या में हमारे पक्षियों की मौत हो जाती है। पतंग की डोर से उड़ने के दौरान इसकी जद में आने से पक्षियों के पंख कट जाते हैं। हवाई मार्गों की जद में आने से भी इनकी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ बच्चों की ओर से चिड़ियों को रंग दिया जाता है। जिससे उनका पंख गीला हो जाता है और वे उड़ नहीं पाती। हिंसक पक्षी जैसे बाज़ इत्यादि हमला कर उन्हें मौत की नींद सुला देते हैं।
दुनिया भर में कई तरह के खास दिन हैं ठीक उसी तरह 20 मार्च का दिन भी गौरैया संरक्षण के लिए निर्धारित है। लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम होगा की इसकी शुरुवात सबसे पहले भारत के महाराष्ट्र से हुई। गौरैया गिद्ध के बाद सबसे संकट ग्रस्त पक्षी है। दुनिया भर में प्रसिद्ध पर्यावरणविद मोहम्मद ई दिलावर नासिक से हैं और वह बाम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी से जुड़े हैं। उन्होंने यह मुहिम 2008 से शुरु की थी। आज यह दुनिया के 50 से अधिक मुल्कों तक पहुंच गयी है।
गौरैया के संरक्षण के लिए सरकारों की तरफ से कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखती है. हलांकि, यूपी में 20 मार्च को गौरैया संरक्षण दिवस के रुप में रखा गया है. दिलावर के विचार में गैरैया संरक्षण के लिए लकड़ी के बुरादे से छोटे-छोटे घर बनाएं जाएं और उसमें खाने की भी सुविधा भी उपलब्ध हो। अमेरिका और अन्य विकसित देशों में पक्षियों का व्यौरा रखा जाता है लेकिन भारत में ऐसा नहीं हैं। पक्षियों के संरक्षण के लिए कॉमन बर्ड मॉनिटरिंग आफ इंडिया के नाम से साइट बनायी है। जिस पर आप भी पक्षियों से संबंधी जानकारी और आंकड़ा दे सकते हैं। कुछ सालों से उनकी संस्था गौरैया को संरिक्षत करने वालों को स्पैरो अवॉर्ड्स देती है। घरों के आसपास आधुनिक घोंसले बनाएं जाएं। उसमें चिड़ियों के चुगने के लिए भोजन की सुविधा भी उपलब्ध करायी जाए। घोंसले सुरक्षित स्थान पर हों जिससे गौरैयों के अंडों और चूजों को हिंसक पक्षी और जानवर शिकार न बना सकें ।
विज्ञान और विकास के बढ़ते कदम ने हमारे सामने कई चुनौतियां भी खड़ी की हैं। जिससे निपटना हमारे लिए आसान नहीं है। विकास की महत्वाकांक्षी इच्छाओं ने हमारे सामने पर्यावरण की विषम स्थिति पैदा की है। जिसका असर इंसानी जीवन के अलावा पशु-पक्षियों पर साफ दिखता है। इंसान के बेहद करीब रहने वाली कई प्रजाति के पक्षी और चिड़िया आज हमारे बीच से गायब हैं। उसी में एक है स्पैरो यानी नन्ही सी वह गौरैया। समय रहते इन विलुप्त होती प्रजाति पर ध्यान नहीं दिया गया तो वह दिन दूर नहीं जब गिद्धों की तरह गैरैया भी इतिहास बन जाएगी और यह सिर्फ गूगल और किताबों में ही दिखेगी। सिर्फ सरकार के भरोसे हम इंसानी दोस्त गौरैया को नहीं बचा सकते हैं।प्रकृति प्रेमियों को अभियान चलाकर लोगों को मानव जीवन में पशु-पक्षियों के योगदान की जानकारी देनी होगी. इकसे अलावा स्कूली पाठ्यक्रमों में हमें गैरैया और दूसरे पक्षियों को शामिल करना होगा। आज के 20 साल पूर्व प्राथमिक स्कूलों के पाठ्यक्रम में गौरैया की उपस्थिति थी। लेकिन आज अंग्रेजी संस्कृति हम पर इतनी हावी हो गयी की हम खुद अपनी प्राकृतिक विरासत से दूर होते जा रहे हैं। इस पर हमें गंभीरता से विचार करना होगा।
गौरैया हमारी प्राकृतिक सहचरी है। कभी वह नीम के पेड़ के नीचे फूदकती और बिखेरे गए चावल या अनाज के दाने को चुगती। कभी प्यारी गौरैया घर की दीवार पर लगे आइने पर अपनी हमशक्ल पर चोंच मारती दिख जाती है। लेकिन बदलते वक्त के साथ आज गौरैया का बयां बेहद कम दिखाई नहीं देता है । एक वक्त था जब बबूल के पेड़ पर सैकड़ों की संख्या में घोसले लटके होते और गौरैया के साथ उसके चूजे चीं-चीं-चीं का शोर मचाते। बचपन की यादें आज भी जेहन में ताजा हैं लेकिन वक्त के साथ गौरैया एक कहानी बन गई है। हालांकि पर्यावरण के प्रति जागरूकता के चलते हाल के सालों में यह दिखाई देने लगी है । गौरैया इंसान की सच्ची दोस्त भी है और पर्यावरण संरक्षण में उसकी खास भूमिका भी है। दुनिया भर में 20 मार्च को गैरैया संरक्षण दिवस के रुप में मनाया जाता है। प्रसिद्ध पर्यावरणविद मो. ई दिलावर के प्रयासों से इस दिवस को चुलबुली चंचल गौरैया के लिए रखा गया। 2010 में पहली बार यह दुनिया में मनाया गया। प्रसिद्ध उपन्यासकार भीष्म साहनी जी ने अपने बाल साहित्य में गैरैया पर बड़ी अच्छी कहानी लिखी है। जिसे उन्होंने गौरैया नाम दिया। हालांकि, जागरुकता की वजह से गौरैया की आमद बढ़ने लगी है। हमारे लिए यह शुभ संकेत है।
गौरैया का संरक्षण हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इंसान की भोगवादी संस्कृति ने हमें प्रकृति और उसके साहचर्य से दूर कर दिया है। विज्ञान और विकास हमारे लिए वरदान साबित हुआ है। लेकिन दूसरा पहलू कठिन चुनौती भी पेश किया है। गौरैया एक घरेलू और पालतू पक्षी है। यह इंसान और उसकी बस्ती के पास अधिक रहना पसंद करती है। पूर्वी एशिया में यह बहुतायत पायी जाती है। यह अधिक वजनी नहीं होती हैं। इसका जीवन काल दो साल का होता है। यह पांच से छह अंडे देती है। आंध्र यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन में गौरैया की आबादी में 60 फीसदी से अधिक की कमी बताई गई है। ब्रिटेन की ‘रॉयल सोसाइटी आफ प्रोटेक्शन आफ बर्डस‘ ने इस चुलबुली और चंचल पक्षी को ‘रेड लिस्ट‘ में डाल दिया है। दुनिया भर में ग्रामीण और शहरी इलाकों में गौरैया की आबादी घटी है। गौरैया की घटती आबादी के पीछे मानव विकास सबसे अधिक जिम्मेदार हैं। गौरैया पासेराडेई परिवार की सदस्य है. लेकिन इसे वीवरपिंच परिवार का भी सदस्य माना जाता है। इसकी लंबाई 14 से 16 सेंटीमीटर होती है। इसका वनज 25 से 35 ग्राम तक होता है। यह अधिकांश झुंड में रहती है। यह अधिक दो मिल की दूरी तय करती है। गौरैया को अंग्रेजी में पासर डोमेस्टिकस के नाम से बुलाते हैं। मानव जहां-जहां गया गौरैया उसका हम सफर बन कर उसके साथ गयी। शहरी हिस्सों में इसकी छह प्रजातियां पाई जाती हैं. जिसमें हाउस स्पैरो, स्पेनिश, सिंउ स्पैरो, रसेट, डेड और टी स्पैरो शामिल हैं. यह यूरोप, एशिया के साथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के अधिकतर हिस्सों में मिलती है। गौरैया घास के बीजों को अपने भोजन के रुप में अधिक पसंद करती है। पर्यावरण प्रेमियों के लिए यह चिंता का सवाल है। इस पक्षी को बचाने के लिए वन और पर्यावरण मंत्रालय की ओर से कोई खास पहल नहीं दिखती है। दुनिया भर के पर्यावरणविद इसकी घटती आबादी पर चिंता जाहिर कर चुके हैं।
बढ़ती आबादी के कारण जंगलों का सफाया हो रहा है। ग्रामीण इलाकों में पेड़ काटे जा रहे हैं। ग्रामीण और शहरी इलाकों में बाग-बगीचे खत्म हो रहे हैं। इसका सीधा असर इन पर दिख रहा है। गांवों में अब पक्के मकान बनाए जा रहे हैं। जिसका कारण है कि मकानों में गौरैया को अपना घोंसला बनाने के लिए सुरक्षित जगह नहीं मिल रही है। पहले गांवों में कच्चे मकान बनाए जाते थे, उसमें लड़की और दूसरी वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाता था। कच्चे मकान गौरैया के लिए प्राकृतिक वारावरण और तापमान के लिहाज से अनुकूल वातावरण उपलब्ध करते थे।लेकिन आधुनिक मकानों में यह सुविधा अब उपलब्ध नहीं होती है। यह पक्षी अधिक तापमान में नहीं रह सकता है। गगन चुम्बी ऊंची इमारतें और संचार क्रांति इनके लिए अभिशाप बन गयी। शहर से लेकर गांवों तक मोबाइल टावर एवं उससे निकलते रेडिएशन से इनकी जिंदगी संकट में है।
खेती-किसानी में रसायनिक उर्वरकों का बढ़ता प्रयोग बेजुबान पक्षियों और गौरैया के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। केमिलयुक्त रसायनों के अंधाधुंध प्रयोग से कीड़े मकोड़े भी विलुप्त हो चले हैं। जिससे गौरैयों भोजन का भी संकट खड़ा हो गया है। दूसरा बड़ा कारण मकर सक्रांति पर पतंग उत्सवों के दौरान काफी संख्या में हमारे पक्षियों की मौत हो जाती है। पतंग की डोर से उड़ने के दौरान इसकी जद में आने से पक्षियों के पंख कट जाते हैं। हवाई मार्गों की जद में आने से भी इनकी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ बच्चों की ओर से चिड़ियों को रंग दिया जाता है। जिससे उनका पंख गीला हो जाता है और वे उड़ नहीं पाती। हिंसक पक्षी जैसे बाज़ इत्यादि हमला कर उन्हें मौत की नींद सुला देते हैं।
दुनिया भर में कई तरह के खास दिन हैं ठीक उसी तरह 20 मार्च का दिन भी गौरैया संरक्षण के लिए निर्धारित है। लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम होगा की इसकी शुरुवात सबसे पहले भारत के महाराष्ट्र से हुई। गौरैया गिद्ध के बाद सबसे संकट ग्रस्त पक्षी है। दुनिया भर में प्रसिद्ध पर्यावरणविद मोहम्मद ई दिलावर नासिक से हैं और वह बाम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी से जुड़े हैं। उन्होंने यह मुहिम 2008 से शुरु की थी। आज यह दुनिया के 50 से अधिक मुल्कों तक पहुंच गयी है।
गौरैया के संरक्षण के लिए सरकारों की तरफ से कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखती है. हलांकि, यूपी में 20 मार्च को गौरैया संरक्षण दिवस के रुप में रखा गया है. दिलावर के विचार में गैरैया संरक्षण के लिए लकड़ी के बुरादे से छोटे-छोटे घर बनाएं जाएं और उसमें खाने की भी सुविधा भी उपलब्ध हो। अमेरिका और अन्य विकसित देशों में पक्षियों का व्यौरा रखा जाता है लेकिन भारत में ऐसा नहीं हैं। पक्षियों के संरक्षण के लिए कॉमन बर्ड मॉनिटरिंग आफ इंडिया के नाम से साइट बनायी है। जिस पर आप भी पक्षियों से संबंधी जानकारी और आंकड़ा दे सकते हैं। कुछ सालों से उनकी संस्था गौरैया को संरिक्षत करने वालों को स्पैरो अवॉर्ड्स देती है। घरों के आसपास आधुनिक घोंसले बनाएं जाएं। उसमें चिड़ियों के चुगने के लिए भोजन की सुविधा भी उपलब्ध करायी जाए। घोंसले सुरक्षित स्थान पर हों जिससे गौरैयों के अंडों और चूजों को हिंसक पक्षी और जानवर शिकार न बना सकें ।
विज्ञान और विकास के बढ़ते कदम ने हमारे सामने कई चुनौतियां भी खड़ी की हैं। जिससे निपटना हमारे लिए आसान नहीं है। विकास की महत्वाकांक्षी इच्छाओं ने हमारे सामने पर्यावरण की विषम स्थिति पैदा की है। जिसका असर इंसानी जीवन के अलावा पशु-पक्षियों पर साफ दिखता है। इंसान के बेहद करीब रहने वाली कई प्रजाति के पक्षी और चिड़िया आज हमारे बीच से गायब हैं। उसी में एक है स्पैरो यानी नन्ही सी वह गौरैया। समय रहते इन विलुप्त होती प्रजाति पर ध्यान नहीं दिया गया तो वह दिन दूर नहीं जब गिद्धों की तरह गैरैया भी इतिहास बन जाएगी और यह सिर्फ गूगल और किताबों में ही दिखेगी। सिर्फ सरकार के भरोसे हम इंसानी दोस्त गौरैया को नहीं बचा सकते हैं।प्रकृति प्रेमियों को अभियान चलाकर लोगों को मानव जीवन में पशु-पक्षियों के योगदान की जानकारी देनी होगी. इकसे अलावा स्कूली पाठ्यक्रमों में हमें गैरैया और दूसरे पक्षियों को शामिल करना होगा। आज के 20 साल पूर्व प्राथमिक स्कूलों के पाठ्यक्रम में गौरैया की उपस्थिति थी। लेकिन आज अंग्रेजी संस्कृति हम पर इतनी हावी हो गयी की हम खुद अपनी प्राकृतिक विरासत से दूर होते जा रहे हैं। इस पर हमें गंभीरता से विचार करना होगा।
वन और पर्यावरण संरक्षण के व्यापक मुद्दे पर जागरूकता बढ़ाने के लिए 1972 से दुनिया भर में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है. इस वर्ष के विश्व पर्यावरण दिवस का विषय ‘लोगों को प्रकृति से जोड़ना’ है. इस दिवस के अवसर पर लोगों को घरों से बाहर निकलकर प्रकृति के संसर्ग में उसकी सुंदरता की सराहना करने तथा जिस पृथ्वी पर रहते हैं, उसके संरक्षण का आग्रह किया जाता है.
इन वर्षों में शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लोगों का प्रकृति से अलगाव बढ़ रहा है.
आधुनिक व्यक्ति के जीवन में व्यस्तता है और उसका दिमाग तो और भी व्यस्त है. ऐसी परिस्थितियों में मन को शांत करने के लिए प्रकृति के साथ दोबारा जुड़ना अति महत्वपूर्ण है. शहरों में उपलब्ध हरित स्थानों विशेष रूप से वृक्षों और पार्कों के जरिये लोगों को प्रकृति से दोबारा जुड़ने का अवसर मिलता है.
प्रकृति से दोबारा जुड़ने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान (एनईएसी) शुरू किया है. इस कार्यक्रम के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों, महिला और युवा संगठनों को पर्यावरण के मुद्दों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है. प्रकृति के संरक्षण और पर्यावरण संबंधित समस्याओं के समाधान से जुड़े कार्यक्रम आयोजित करने में लगभग 12000 संगठन शामिल हैं.
पारम्परिक रूप से तीर्थयात्रा के केंद्र मुख्य रूप से प्राकृतिक परिवेश विशेष रूप से पहाड़ों या नदियों के तटों पर स्थित होते हैं. हिमालय में चार धाम यात्रा इसका उत्कृष्ट उदाहरण है कि कैसे हमारी संस्कृति देश भर के लोगों को श्रद्धा से वृक्षों, नदियों और पहाड़ों की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने का अवसर प्रदान करती है. ऋषिकेश में गंगा नदी के तट से शुरू होने वाली इस यात्रा का मार्ग यमुना और गंगा नदी के उद्गम स्थल तक का है, जो पवित्र तीर्थस्थल हैं और करोड़ों लोग वहां जाते हैं.
जम्मू-कश्मीर में अमरनाथ गुफा और चीन के तिब्बती पठार में कैलाश मानसरोवर की तीर्थयात्रा के मार्ग में भी कई असाधारण प्राकृतिक सौंदर्य के स्थल हैं, जिनका आम आदमी के लिए काफी आध्यात्मिक महत्व है. तीर्थयात्रा के ये मार्ग प्रकृति के साथ दोबारा जुड़ने के मुख्य तरीके हैं और मानव, प्रकृति तथा आध्यात्मिकता के बीच अंतर संयोजनात्मकता को दर्शाते हैं.
इसी प्रकार नर्मदा परिक्रमा भी एक और परम्परागत तीर्थयात्रा का मार्ग है, जिसमें लोग नर्मदा नदी के तट के साथ-साथ चलते हुए नदी की सुंदरता और प्राकृतिक परिवेश की सराहना करना सीखते हैं.
देश के कुल भगौलिक क्षेत्र के दो प्रतिशत इलाकों में बने मौजूदा 166 राष्ट्रीय उद्यान और 515 वन्यजीव अभ्यारण्यों से भी लोगों को प्रकृति से दोबारा जुड़ने, वन्य जीवन और देश के हरित स्थलों को आनंद लेने का अवसर मिलता है.
प्राकृतिक संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय ने शहरों में सार्वजनिक स्थलों पर हरियाली को बढ़ावा देने तथा सभी प्रकार के अपशिष्ट को कम करने की दिशा में कई कदम उठाए हैं. शहरी क्षेत्रों में सड़क निर्माण और खुले स्थानों पर फर्श तथा सीमेंट लगाने के जुनून के कारण युवा पीढ़ी प्रकृति से दूर हो गई है. सड़कों को चौड़ा करने के लिए पुराने वृक्षों को गिराने और पैदल यात्री तथा साईकिल चालकों से अधिक स्थान वाहनों के लिए रखने से शहरी नागरिकों का प्रकृति से जुड़ाव और कम हुआ है. सभी हितधारकों तथा समुदाय की सक्रिय भागीदारी से शहरी पारिस्थितिकी को कायम रखा जा सकता है.
प्रकृति के साथ दोबारा जुड़ना आधुनिक समय के तनाव को कम करने तथा व्यक्ति और समुदाय में सद्भाव लाने में मददगार होता है. हरियाली से न केवल शोर और ध्वनि प्रदूषण कम होता, बल्कि तापमान कम करने में भी मदद मिलती है, जो जलवायु परिवर्तन के असर को कम करने में सहायक है.
भारत सरकार विश्व पर्यावरण दिवस पर देश भर के 4000 शहरों में विशाल अपशिष्ट प्रबंधन अभियान शुरू कर रही है. इस अभियान के अंतर्गत इन शहरों में कूड़ा एकत्र करने के नीले और हरे रंग के डिब्बे वितरित किए जाएंगे तथा आम लोगों को अपनी जीवन शैली में स्वच्छता की संस्कृति अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा.
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ में कहा, “मुझे दृढ़ विश्वास है कि हम स्वच्छता हासिल करने की दिशा में संस्कृति विकसित करेंगे और उसे जारी रखने के लिए नये कदम उठाएंगे. तभी हम गांधीजी के उस सपने को साकार कर सकेंगे, जो उन्होंने स्वच्छता के लिए देखा था”.
सरकार का उद्देश्य मूल स्थान पर ही सूखे और गीले कूड़े को अलग-अलग करने में लोगों की आदत में बदलाव लाना है ताकि तद्नुसार कूड़े का प्रबंधन किया जा सके. यह शहरों की स्वच्छता का आधार होगा, जिससे शहर अधिक प्रकृति अनुकूल बनेंगे तथा रहने के लिए स्वच्छ बुनियादी स्थिति उपलब्ध होगी. यह स्वच्छ भारत अभियान (एसबीए) का तार्किक अनुकरण है, जिसके तहत शहरी क्षेत्रों में कूड़े के ढ़ेर के निपटान की समस्या से निपटने की आवश्यकता है, क्योंकि इससे भूजल पर प्रतिकूल असर पड़ता है तथा कूड़े के ढ़ेर के आसपास की हवा की गुणवत्ता प्रभावित होती है. यह एक चुनौती भरा कार्य है क्योंकि लोगों की आदत बदलने की आवश्यकता है, ताकि कूड़े को अलग करने का कर्तव्य या धर्म निभाने के लिए प्रत्येक परिवार के ये लोग बदलाव के दूत बनें.
भारतीय संस्कृति में प्रकृति के साथ जुड़ना ज्ञान और शांति प्राप्त करने का आधार है. संत या ऋषि जंगलों या अरण्य संस्कृति से ज्ञान प्राप्त करते हैं. वे प्रकृति के साथ सद्भाव से रहते हैं और अपने प्राकृतिक परिवेश से अधिकतर ज्ञान आत्मसात करते हैं.
प्रकृति के साथ दोबारा जुड़ने के लिए हमें इन विचारों को अपनी दैनिक गतिविधियों में शामिल करने की आवश्यकता है. आम व्यक्ति के लिए ये जानना आवश्यक है कि जो सांस वह लेता है, पानी पीता है, भोजन खाता है, वे सभी प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति के उत्पाद हैं और प्रकृति से जुड़ाव मानव जाति के जीवित रहने का आधार है.
(लेखक कर्नाटक में स्वतंत्र पत्रकार और स्तंभकार हैं)
फ़िरदौस ख़ान
दुनियाभर में हर्बल पदार्थों का चलन तेज़ी से बढ़ रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक़ अमेरिका में 33 फीसदी लोग हर्बल पद्धति में विश्वास करते हैं। अमेरिका में आयुर्वेद विश्वविद्यालय खुल रहे हैं और जर्मनी, जापान, आस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, नीदरलैंड, रूस और इटली में भी आयुर्वेद पीठ स्थापित हो रहे हैं।
विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के मुताबिक विश्व में 62 अरब अमेरिकी डॉलर के मूल्यों के हर्बल पदार्थों की मांग है और यह मांग वर्ष 2050 तक पांच ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। एक अनुमान के मुताबिक चीन द्वारा सलाना क़रीब 22 हज़ार करोड़ रुपये के औषधीय पौधों पर आधारित पदार्थों का निर्यात किया जा रहा है. रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्यमंत्री श्रीकांत जेना के मुताबिक भारतीय उद्योग मॉनिटरिंग केन्द्र नवम्बर 2009 के अनुसार 2009-10 के दौरान औषधों की बिक्री में 8.7 प्रतिशत वृध्दि की आशा है। 2007-08 के दौरान औषध बाज़ार का कुल बाज़ार आकार 78610 करोड़ रुपये था। भावी वर्षों के लिए बाज़ार के आकार का कोई आधिकारिक प्राक्कलन नहीं किया गया है, लेकिन चिन्ता की बात यह है कि औषधीय पौधों की बढ़ती मांग के कारण इनका अत्यधिक दोहन हो रहा है, जिसके चलते हालत यह हो गई है कि औषधीय पौधों की अनेक प्रजातियां लुप्त होने के क़गार पर हैं।
औषधीय पौधों के अंधाधुंध दोहन को रोकने के लिए नवम्बर, 2000 में केन्द्र सरकार ने स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत मेडिसनल प्लांट बोर्ड का गठन किया था। इस बोर्ड ने भारतीय जलवायु के मद्देनज़र 32 प्रकार के ऐसे औषधीय पौधों की सूची बनाई है, जिनकी खेती करके किसान ज़्यादा आमदनी हासिल कर सकते हैं। इस प्रकार इन औषधीय पौधें की एक ओर उपलब्धता बढ़ेगी तो दूसरी ओर उनके लुप्त होने का ख़तरा भी नहीं रहेगा। बढ़ती आबादी और घटती कृषि भूमि ने किसानों की हालत को बद से बदतर कर दिया है. लेकिन ऐसी हालत में जड़ी-बूटी आधारित कृषि किसानों के लिए आजीविका कमाने का एक नया रास्ता खोलती है।
एक रिपोर्ट के मुताबिक़ अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में आंवला, अश्वगंधा, सैना, कुरु, सफ़ेद मूसली, ईसबगोल, अशोक, अतीस, जटामांसी, बनककड़ी, महामेदा, तुलसी, ब्राहमी, हरड़, बेहड़ा, चंदन, धीकवर, कालामेधा, गिलोय, ज्वाटे, मरूआ, सदाबहार, हरश्रृंगार, घृतकुमारी, पत्थरचट्टा, नागदौन, शंखपुष्पी, शतावर, हल्दी, सर्पगंधा, विल्व, पुदीना, अकरकरा, सुदर्शन, पुर्नवादि, भृंगराज, लहसुन, काला जीरा और गुलदाऊदी की बहुत मांग है।
भारत में हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहां सरकार औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने पर ख़ास ज़ोर दे रही है। राज्य में शामलात भूमि पर औषधीय पौधे लगाए जा रहे हैं। इससे पंचायत की आमदनी में बढ़ोतरी होने के साथ-साथ किसानों को औषधीय पौधों की खेती की ओर आकर्षित करने में भी मदद मिलेगी। राज्य के यमुनानगर ज़िले के चूहड़पुर में चौधारी देवीलाल हर्बल पार्क स्थापित किया गया है। इसका उद्धाटन तत्कालीन राष्टपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने किया था।
क़ाबिले ग़ौर है कि डॉक्टर कलाम ने भी अपने कार्यकाल में राष्ट्रपति भवन में औषधीय पौधों का बग़ीचा तैयार करवाया था। हरियाणा में परम्परागत नदी फ़सलों की खेती करने वाले किसानों का रुझान अब औषधीय पौधों की खेती की तरफ़ बढ़ रहा है। कैथल ज़िले के गांव चंदाना निवासी कुशलपाल सिरोही अन्य फ़सलों के साथ-साथ औषधीय पौधों की खेती भी करते हैं। इस समय उनके खेत में लेमन ग्रास, गुलाब, तुलसी, अश्वगंधा, सर्पगंधा, धतूरा, करकरा और शंखपुष्पी जैसे अनेक औषधीय पौधे लगे हैं। उनका कहना है कि औषधीय पौधे ज्यादा आमदनी देते हैं। गुलाब का असली अर्क़ तीन से चार लाख रुपये प्रति लीटर बिकता है।
आयुर्वेद की पढ़ाई कर रहे यमुनानगर ज़िले के गांव रुलेसर निवासी इरशाद अहमद ने अपने खेत में रुद्राक्ष, चंदन और दारूहरिद्रा के अनेक पौधे लगाए हैं। ख़ास बात यह है कि जहां रूद्राक्ष के वृक्ष चार साल के बाद फल देना शुरू करते हैं, वहीं उनके पौधे महज़ ढाई साल के कम अरसे में ही फलों से लद गए हैं। इरशाद अहमद के मुताबिक़ रूद्राक्ष के पौधों को पालने के लिए उन्होंने देसी पद्धति का इस्तेमाल किया है। उन्होंने गोबर और घरेलू जैविक खाद को पौधों की जड़ों में डाला और गोमूत्र से इनकी सिंचाई की। दीमक व अन्य हानिकारक कीटों से निपटने के लिए उन्होंने पौधों पर हींग मिले पानी का छिड़काव किया।
रूद्राक्ष व्यापारी राजेश त्रिपाठी कहते हैं कि रूद्राक्ष एक फल की गुठली है। फल की गुठली को साफ़ करने के बाद इसे पालिश किया जाता है, तभी यह धारण करने योग्य बनता है। गले का हार या अन्य अलंकरण बनाने के लिए इन पर रंग किया जाता है। आमतौर पर रूद्राक्ष का आकार 1.3 से.मी. तक होता है। ये गोल या अंडाकार होते हैं। इनकी क़ीमत इनके मुखों के आधार पर तय होती है। अमूमन रूद्राक्ष एक से 21 मुख तक का होता है। लेकिन 1, 18, 19, 20, और 21 मुख के रूद्राक्ष कम ही मिलते हैं। असली रूद्राक्ष की कीमत हज़ारों से लेकर लाखों रुपये तक आंकी जाती है। इनमें सबसे ज़्यादा क़ीमती रूद्राक्ष एक मुख वाला होता है।
रूद्राक्ष की बढ़ती मांग के चलते आजकल बाज़ार में नकली रूद्राक्षों की भी भरमार है। नक़ली रूद्राक्ष लकड़ी के बनाए जाते हैं। इनकी पहचान यह है कि ये पानी में तैरते हैं, जबकि असली रूद्राक्ष पानी में डूब जाता है।ग़ौरतलब है कि भारतीय संस्कृति से रूद्राक्ष का गहरा संबंध है। आध्यात्मिक दृष्टि से भी इसे बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। यहां के समाज में मान्यता है कि रूद्राक्ष धारण करने से अनेक प्रकार की बीमारियों से निजात पाई जा सकती है। रूद्राक्ष के प्राकृतिक वृक्ष उत्तर-पूर्वी भारत और पश्चिमी तटों पर पाए जाते हैं। नेपाल में इसके वृक्षों की संख्या सबसे ज़्यादा है। ये मध्यम आकार के होते हैं। मई और जून के महीने में इस पर सफ़ेद फूल लगते हैं और सितम्बर से नवम्बर के बीच फल पकते हैं। अब मैदानी इलाक़ों में भी इसे उगाया जाने लगा है।
वैज्ञानिकों का मानना है कि औषधीय पौधों की खेती कर किसान प्रति एकड़ दो से ढाई लाख रुपये सालाना अर्जित कर सकते हैं। बस, ज़रूरत है किसानों को थोड़ा-सा जागरूक करने की। इसमें कृषि विभाग महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। गांवों में कार्यशालाएं आयोजित कर किसानों को औषधीय पौधों की खेती की जानकारी दी जा सकती है। उन्हें बीज व पौधे आदि उपलब्ध कराने के अलावा पौधों की समुचित देखभाल का तरीका बताया जाना चाहिए। लेकिन इस सबसे ज़रूरी यह है कि किसानों की फ़सल को सही दामों पर बेचने की व्यवस्था करवाई जाए।
अंबरीश कुमार
यह यमुना है .इस यमुना के किनारे जब गए तो बिसलरी की खाली हो रही बोतल निकाली और उसे भर लिया .फिर खुद पिया और अरविंद को भी पिलाया .हम सोच रहे थे कि यही यमुना जब दिल्ली पहुंचती है तो कोई इसका पानी पी सकता है क्या? कांदिखाल से करीब चालीस मिनट में हम यमुना पुल तक पहुंच गये .आगे चकराता के रास्ते पर जाना था .कुछ दूरी के बाद ही हिमाचल की सीमा आ जाती है .यमुना पुल से पहले यमुना का विहंगम दृश्य देखने वाला था .यहां यमुना एक नदी सी लगती है .पहाड़ों को लांघती हुई ,घेरती हुई आती है और उसका प्रवाह देखने वाला होता है .
जाते समय पुल के पहले बंगाली रेस्तरां वाले को बता दिया था कि करीब बारह लोग लौट कर खाना यही खायेंगे .वह मछली रोटी और चावल की थाली सत्तर रूपये में देता है .शाकाहारी लोगों के लिए सब्जी दही भी रखता है .यह बंगाली परिवार कई साल पहले चौबीस परगना से आया था और अब यमुना के पानी से गुजारा कर रहा है .सुबह यमुना से जो मछली पकड़ी जाती है वह खरीद लेता है और दिन रात ट्रक वालों के साथ कुछ सैलानियों को मछली भात परोसता है .साथ में जो पानी होता है वह भी यमुना का .हम लोग यमुना नदी के तट तक गये पर उसका प्रवाह देख कर आगे नहीं बढे .फिर जौनसार बाबर मंदिर की तरफ जाना था इसलिए आगे बढ़ गये .यमुना साथ साथ थी और एक बड़े पहाड़ की परिक्रमा करती नजर आ रही थी .यह बहुत ही हरा भरा इलाका है .एक तरफ खेत तो दूसरी तरफ पहाड़ .खेतों की तरफ ही कुछ हजार फुट नीचे यमुना .पर फल के पेड़ बहुत कम दिखे .हां एक ट्रक दिखा तो जबर सिंह ने बताया कि ये हिमाचल का सेब लेकर नीचे जा रहा है .
.इस रास्ते पर चकराता करीब चालीस किलोमीटर दूरी पर है .करीब बीस साल पहले सविता के साथ गया था और वहा के एकमात्र डाक बंगले में तीन दिन रहा था .वह बहुत ही रोमांचक यात्रा थी और एक बड़े हादसे से सविता बच कर आ गई थी .वहा से शिमला का भी शार्ट कट है .यह सब याद कर रहा था तभी जौनसार आ गया .यह अद्भुत क्षेत्र है .यह समूचा क्षेत्र जनजाति के लिए आरक्षित है .यह काम साठ सत्तर के दशक के बीच हुआ था .जिसके चलते यहां के बाभन और ठाकुर बिरादरी को आरक्षण का लाभ मिलता है और जो दलित है उनसे ज्यादा फायदे में अगड़ी जातियां रहती है .यहां दलित किसी की जमीन इसलिए नही ले सकता क्योंकि वह जनजाति वाले की होती है भले ही वह ठाकुर हो .जो महासू देवता का मंदिर है उसपर भी ठाकुर बिरादरी का दबदबा है .कोई दलित यहां प्रवेश नहीं कर सकता .इसपर लिख रहा हूँ .मंदिर परिसर में कई मोटे बकरे नजर आये जो मंदिर की संपति होते है और वे चढ़ावे में आते है इनके लिए एक बाड़ा भी बना है .मंदिर में अपने साथ कई दलित नौजवान इस मंदिर में पहली बार गये .पुजारी ने प्रबंधको को इशारा किया कि सबका ब्यौरा ले और इनसे बासद में निपटा जायेगा .खैर यह मुद्दा अलग है और इसपर खबर भी लिखना है इसलिए मूल मुद्दे पर आता हूं .नदी और पानी के मुद्दे पर .पर्यावरण के मुद्दे पर .यमुना को दिल्ली में देखता रहा हूं .कभी नहाने की हिम्मत तक नहीं हुई उसी यमुना का बोतल भर पानी पिया तो मिनरल वाटर से बेहतर लगा .यमुना का हरा रंग और तलहटी तक दिखाई देने वाला पानी जिसे हमने दिल्ली तक पहुंचाते पहुंचाते जहरीला बना दिया .असली यमुना तो यहां दिखी .एक हरे भरे पहाड़ की परक्रमा कर रही यमुना की फोटो ली तो कुछ देर खड़ा रहा गया .ऐसा दृश्य बहुत कम दिखता है .फिर चले तो उसी यमुना पुल के बंगाली रेस्तरां या ढाबा पर रुके .अरविंद की इच्छा थी और झारखंड बंगाल के भी कुछ लोग मछली खाना चाहते थे .यह छोटी मछली थी जिसे उसने सही शब्दों में मछली की दाल बनाकर दे दिया था .सिर्फ नमक हल्दी मिर्च वाले पानी में उबली हुई .पर यमुना से सुबह ही पकड़ी गई मछली बहुत ताज़ी थी इसलिए स्वादिष्ट लगी .साथ में यमुना का पानी भी . फोटो वही की है .
यह यमुना है .इस यमुना के किनारे जब गए तो बिसलरी की खाली हो रही बोतल निकाली और उसे भर लिया .फिर खुद पिया और अरविंद को भी पिलाया .हम सोच रहे थे कि यही यमुना जब दिल्ली पहुंचती है तो कोई इसका पानी पी सकता है क्या? कांदिखाल से करीब चालीस मिनट में हम यमुना पुल तक पहुंच गये .आगे चकराता के रास्ते पर जाना था .कुछ दूरी के बाद ही हिमाचल की सीमा आ जाती है .यमुना पुल से पहले यमुना का विहंगम दृश्य देखने वाला था .यहां यमुना एक नदी सी लगती है .पहाड़ों को लांघती हुई ,घेरती हुई आती है और उसका प्रवाह देखने वाला होता है .
जाते समय पुल के पहले बंगाली रेस्तरां वाले को बता दिया था कि करीब बारह लोग लौट कर खाना यही खायेंगे .वह मछली रोटी और चावल की थाली सत्तर रूपये में देता है .शाकाहारी लोगों के लिए सब्जी दही भी रखता है .यह बंगाली परिवार कई साल पहले चौबीस परगना से आया था और अब यमुना के पानी से गुजारा कर रहा है .सुबह यमुना से जो मछली पकड़ी जाती है वह खरीद लेता है और दिन रात ट्रक वालों के साथ कुछ सैलानियों को मछली भात परोसता है .साथ में जो पानी होता है वह भी यमुना का .हम लोग यमुना नदी के तट तक गये पर उसका प्रवाह देख कर आगे नहीं बढे .फिर जौनसार बाबर मंदिर की तरफ जाना था इसलिए आगे बढ़ गये .यमुना साथ साथ थी और एक बड़े पहाड़ की परिक्रमा करती नजर आ रही थी .यह बहुत ही हरा भरा इलाका है .एक तरफ खेत तो दूसरी तरफ पहाड़ .खेतों की तरफ ही कुछ हजार फुट नीचे यमुना .पर फल के पेड़ बहुत कम दिखे .हां एक ट्रक दिखा तो जबर सिंह ने बताया कि ये हिमाचल का सेब लेकर नीचे जा रहा है .
.इस रास्ते पर चकराता करीब चालीस किलोमीटर दूरी पर है .करीब बीस साल पहले सविता के साथ गया था और वहा के एकमात्र डाक बंगले में तीन दिन रहा था .वह बहुत ही रोमांचक यात्रा थी और एक बड़े हादसे से सविता बच कर आ गई थी .वहा से शिमला का भी शार्ट कट है .यह सब याद कर रहा था तभी जौनसार आ गया .यह अद्भुत क्षेत्र है .यह समूचा क्षेत्र जनजाति के लिए आरक्षित है .यह काम साठ सत्तर के दशक के बीच हुआ था .जिसके चलते यहां के बाभन और ठाकुर बिरादरी को आरक्षण का लाभ मिलता है और जो दलित है उनसे ज्यादा फायदे में अगड़ी जातियां रहती है .यहां दलित किसी की जमीन इसलिए नही ले सकता क्योंकि वह जनजाति वाले की होती है भले ही वह ठाकुर हो .जो महासू देवता का मंदिर है उसपर भी ठाकुर बिरादरी का दबदबा है .कोई दलित यहां प्रवेश नहीं कर सकता .इसपर लिख रहा हूँ .मंदिर परिसर में कई मोटे बकरे नजर आये जो मंदिर की संपति होते है और वे चढ़ावे में आते है इनके लिए एक बाड़ा भी बना है .मंदिर में अपने साथ कई दलित नौजवान इस मंदिर में पहली बार गये .पुजारी ने प्रबंधको को इशारा किया कि सबका ब्यौरा ले और इनसे बासद में निपटा जायेगा .खैर यह मुद्दा अलग है और इसपर खबर भी लिखना है इसलिए मूल मुद्दे पर आता हूं .नदी और पानी के मुद्दे पर .पर्यावरण के मुद्दे पर .यमुना को दिल्ली में देखता रहा हूं .कभी नहाने की हिम्मत तक नहीं हुई उसी यमुना का बोतल भर पानी पिया तो मिनरल वाटर से बेहतर लगा .यमुना का हरा रंग और तलहटी तक दिखाई देने वाला पानी जिसे हमने दिल्ली तक पहुंचाते पहुंचाते जहरीला बना दिया .असली यमुना तो यहां दिखी .एक हरे भरे पहाड़ की परक्रमा कर रही यमुना की फोटो ली तो कुछ देर खड़ा रहा गया .ऐसा दृश्य बहुत कम दिखता है .फिर चले तो उसी यमुना पुल के बंगाली रेस्तरां या ढाबा पर रुके .अरविंद की इच्छा थी और झारखंड बंगाल के भी कुछ लोग मछली खाना चाहते थे .यह छोटी मछली थी जिसे उसने सही शब्दों में मछली की दाल बनाकर दे दिया था .सिर्फ नमक हल्दी मिर्च वाले पानी में उबली हुई .पर यमुना से सुबह ही पकड़ी गई मछली बहुत ताज़ी थी इसलिए स्वादिष्ट लगी .साथ में यमुना का पानी भी . फोटो वही की है .
फ़िरदौस ख़ान
त्यौहारों का मज़ा तब ही है, जब वे ख़ुशियों के साथ संपन्न हों. होली है तो रंग भी होंगे. रंगों के साथ हुड़दंग भी होगा, ढोल-ताशे भी होंगे. यही सब तो होली की रौनक़ है. होली रंगों का त्यौहार है, हर्षोल्लास का त्यौहार है, उमंग का त्यौहार है. लेकिन दुख तो तब होता है, जब ज़रा सी लापरवाही से रंग में भंग पड़ जाता है. इंद्रधनुषी रंगों के इस त्यौहार की ख़ुशियां बरक़रार रहें, इसके लिए काफ़ी एहतियात बरतने की ज़रूरत होती है. अकसर देखने में आता है कि रसायनिक रंगों, भांग और शराब की वजह से कई परेशानियां पैदा हो जाती हैं.
बाज़ार में रंगों की बहार है. ज़्यादातर रंगों में रासायन मिले होते हैं, जो आंखों और त्वचा के लिए नुक़सानदेह हो सकते हैं. चिकित्सकों के मुताबिक़ रंगों ख़ासकर गुलाल में मिलाए जाने वाले चमकदार अभ्रक से कॉर्निया को नुक़सान हो सकता है. रसायनिक रंगों में भारी धातु जैसे सीसा हो सकती हैं, जिससे आंख, त्वचा को नुक़सान पहुंचने के अलावा डर्माटाइटिस, त्वचा का सूखना या चैपिगं, स्किन कैंसर, राइनाइटिस, अस्थमा और न्यूमोनिया जैसी बीमारियां हो सकती हैं. एम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक़ हरे और नीले रंगों का संबंध ऑक्युलर टॉक्सिसिटी से है. ज़्यादातर 'प्लेजिंग टू आई' रंग बाज़ार में मौजूद हैं, जो टॉक्सिक होते हैं और इनकी वजह से गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं. मैलाशाइट ग्रीन का इस्तेमाल होली के रंगों में बहुत होता है और इसकी वजह से आंखों में गंभीर खुजली की हो जाती है और एपिथीलियल को नुक़सान होता है. इसलिए इसे कॉर्नियाल के आसपास नहीं लगाना चाहिए. इसके अलावा सस्ते रसायन जैसे सीसा, एसिड, एल्कलीज, कांच के टुकड़े से न सिर्फ़ त्वचा संबंधी समस्या होती है, बल्कि एब्रेशन, खुजली या झुंझलाहट के साथ ही दृष्टि असंतुलित हो जाती है और सांस संबंधी समस्या हो सकती है. इससे कैंसर का ख़तरा भी बना रहता है. एल्कलीन वाले रंगों से ज़ख़्म हो सकते है. अमूमन बाज़ार में तीन तरह के रंग बिकते हैं, पेस्ट, सूखा पाउडर और पानी वाले रंग. परेशानी तब बढ़ जाती है, जब इन्हें तेल के साथ मिलाकर त्वचा पर इस्तेमाल किया जाता है. ज़्यादातर रंग या गुलाल में दो तत्व होते हैं- एक कलरेंट जो टॉक्सिक हो सकता है और दूसरा एस्बेसटस या सिलिका होता है. दोनों से ही स्वास्थ्य संबंधी ख़तरे होते हैं. सिलिका से त्वचा पर बुरा असर पड़ता है, जबकि एस्बेसटस से कैंसर हो सकता है.
होली खेलने के लिए प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल करना सबसे अच्छा है. बाज़ार में हर्बल रंग भी मिलते हैं, लेकिन इनकी क़ीमत ज़्यादा होती है. वैसे घर पर भी प्राकृतिक रंग बनाए जा सकते हैं. पीले रंग के लिए हल्दी सबसे अच्छी है. टेसू के फूलों को पानी में उबालकर पीला रंग तैयार किया जा सकता है. अमलतास और गेंदे के फूलों को पानी में उबालकर भी पीला रंग बनाया जा सकता है. लाल रंग के लिए लाल चंदन पाउडर का इस्तेमाल किया जा सकता है. गुलाब और गुड़हल के सूखे फूलों को पीसकर गुलाल बनाया जा सकता है. गुलाबी रंग के लिए चुकंदर को पीसकर उबाल लें. कचनार के फूलों को पीसकर पानी में मिलाने से क़ुदरती गुलाबी या केसरिया रंग बनाया जा सकता है. हरा रंग बनाने के लिए मेहंदी का इस्तेमाल किया जा सकता है. मेहंदी के पत्तों को पीसकर प्राकृतिक हरा रंग बनाया जा सकता है. नीले रंग के लिए नील का इस्तेमाल किया जा सकता है.
कुछ लोग होली के दिन पक्के रंगों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे रंग कई दिन तक नहीं उतरता. इससे कई बार मनमुटाव भी हो जाता है. कुछ लोग होली खेलना पसंद नहीं करते. ऐसे लोगों को जबरन रंग लगाया जाता है, तो लड़ाई-झगड़ा भी हो जाता है. बच्चे सादे या रंगीन पानी से भरे ग़ुब्बारे एक-दूसरे पर फेंकते हैं. ग़ुब्बारा आंख के पास लग जाने से आंख को नुक़सान हो सकता है. ये ग़ुब्बारे अकसर लड़ाई-झगड़ों की वजह भी बन जाते हैं. होली खेलने के दौरान कुछ सावधानियां बरत कर इस पर्व की ख़ुशी को बरक़रार रखा जा सकता है. बच्चों को ग़ुब्बारों से न खेलने दें. दांतों के बचाव के लिए डेंटल कैप्स का इस्तेमाल करना चाहिए. नुक़सानदेह रंगों से बचाव के लिए धूप के चश्मे का इस्तेमाल किया जा सकता है. शरीर को रंगों के द्ष्प्रभाव से बचाने के लिए पूरी बांह के कपड़े पहनने चाहिए. चमकदार और गहरे रंग के पुराने कपड़ों को तरजीह दी जानी चाहिए. जब कोई जबरन रंग लगाने की कोशिश करे, तो आंखें और होंठ बंद रखते हुए अपना बचाव करना चाहिए. बालों में तेल ज़रूर लगा लेना चाहिए, ताकि उन पर रंगों का बुरा असर न पड़े. रंगों को साफ़ करने के लिए गुनगुने पानी का इस्तेमाल करना चाहिए. अगर आंख में रंग पड़ गया है, तो फ़ौरन इसे बहते हुए नल से धो लेना चाहिए. रंग में में रसायनिक तत्व होंगे, तो इससे आंखों में हल्की एलर्जी होगी या फिर बहुत तेज़ जलन होने लगेगी. व्यक्ति को एलर्जी की समस्या, कैमिकल बर्न, कॉर्नियल एब्रेशन और आंखों में ज़ख़्म की समस्या हो सकती है. होली के दौरान आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले ज़्यादातर रंग हल्के लाल रंग के होते हैं और इसका असर 48 घंटे तक रहता है. अगर साफ़ दिखाई न दे, तो मरीज़ को फ़ौरन इमरजेंसी में दाख़िल कराया जाना चाहिए.
होली पर भांग और शराब का सेवन आम है. चिकित्सकों के मुताबिक़ भांग के सेवन की वजह से दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, जिससे मस्तिष्क को नुक़सान पहुंचने का ख़तरा बना रहता है. भांग से से मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है, जिससे व्यक्ति ख़ुद को संभाल नहीं पाता. शराब पीने वालों के साथ भी अकसर ऐसा होता है. ज़्यादा शराब पीने के बाद व्यक्ति अपनी सुधबुध खो बैठता है. इसकी वजह से सड़क हादसे का खतरा भी बढ़ जाता है.
होली प्रेम का पावन पर्व है, इसलिए इसे सावधानी पूर्वक प्रेमभाव के साथ ही मनाना चाहिए.
त्यौहारों का मज़ा तब ही है, जब वे ख़ुशियों के साथ संपन्न हों. होली है तो रंग भी होंगे. रंगों के साथ हुड़दंग भी होगा, ढोल-ताशे भी होंगे. यही सब तो होली की रौनक़ है. होली रंगों का त्यौहार है, हर्षोल्लास का त्यौहार है, उमंग का त्यौहार है. लेकिन दुख तो तब होता है, जब ज़रा सी लापरवाही से रंग में भंग पड़ जाता है. इंद्रधनुषी रंगों के इस त्यौहार की ख़ुशियां बरक़रार रहें, इसके लिए काफ़ी एहतियात बरतने की ज़रूरत होती है. अकसर देखने में आता है कि रसायनिक रंगों, भांग और शराब की वजह से कई परेशानियां पैदा हो जाती हैं.
बाज़ार में रंगों की बहार है. ज़्यादातर रंगों में रासायन मिले होते हैं, जो आंखों और त्वचा के लिए नुक़सानदेह हो सकते हैं. चिकित्सकों के मुताबिक़ रंगों ख़ासकर गुलाल में मिलाए जाने वाले चमकदार अभ्रक से कॉर्निया को नुक़सान हो सकता है. रसायनिक रंगों में भारी धातु जैसे सीसा हो सकती हैं, जिससे आंख, त्वचा को नुक़सान पहुंचने के अलावा डर्माटाइटिस, त्वचा का सूखना या चैपिगं, स्किन कैंसर, राइनाइटिस, अस्थमा और न्यूमोनिया जैसी बीमारियां हो सकती हैं. एम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक़ हरे और नीले रंगों का संबंध ऑक्युलर टॉक्सिसिटी से है. ज़्यादातर 'प्लेजिंग टू आई' रंग बाज़ार में मौजूद हैं, जो टॉक्सिक होते हैं और इनकी वजह से गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं. मैलाशाइट ग्रीन का इस्तेमाल होली के रंगों में बहुत होता है और इसकी वजह से आंखों में गंभीर खुजली की हो जाती है और एपिथीलियल को नुक़सान होता है. इसलिए इसे कॉर्नियाल के आसपास नहीं लगाना चाहिए. इसके अलावा सस्ते रसायन जैसे सीसा, एसिड, एल्कलीज, कांच के टुकड़े से न सिर्फ़ त्वचा संबंधी समस्या होती है, बल्कि एब्रेशन, खुजली या झुंझलाहट के साथ ही दृष्टि असंतुलित हो जाती है और सांस संबंधी समस्या हो सकती है. इससे कैंसर का ख़तरा भी बना रहता है. एल्कलीन वाले रंगों से ज़ख़्म हो सकते है. अमूमन बाज़ार में तीन तरह के रंग बिकते हैं, पेस्ट, सूखा पाउडर और पानी वाले रंग. परेशानी तब बढ़ जाती है, जब इन्हें तेल के साथ मिलाकर त्वचा पर इस्तेमाल किया जाता है. ज़्यादातर रंग या गुलाल में दो तत्व होते हैं- एक कलरेंट जो टॉक्सिक हो सकता है और दूसरा एस्बेसटस या सिलिका होता है. दोनों से ही स्वास्थ्य संबंधी ख़तरे होते हैं. सिलिका से त्वचा पर बुरा असर पड़ता है, जबकि एस्बेसटस से कैंसर हो सकता है.
होली खेलने के लिए प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल करना सबसे अच्छा है. बाज़ार में हर्बल रंग भी मिलते हैं, लेकिन इनकी क़ीमत ज़्यादा होती है. वैसे घर पर भी प्राकृतिक रंग बनाए जा सकते हैं. पीले रंग के लिए हल्दी सबसे अच्छी है. टेसू के फूलों को पानी में उबालकर पीला रंग तैयार किया जा सकता है. अमलतास और गेंदे के फूलों को पानी में उबालकर भी पीला रंग बनाया जा सकता है. लाल रंग के लिए लाल चंदन पाउडर का इस्तेमाल किया जा सकता है. गुलाब और गुड़हल के सूखे फूलों को पीसकर गुलाल बनाया जा सकता है. गुलाबी रंग के लिए चुकंदर को पीसकर उबाल लें. कचनार के फूलों को पीसकर पानी में मिलाने से क़ुदरती गुलाबी या केसरिया रंग बनाया जा सकता है. हरा रंग बनाने के लिए मेहंदी का इस्तेमाल किया जा सकता है. मेहंदी के पत्तों को पीसकर प्राकृतिक हरा रंग बनाया जा सकता है. नीले रंग के लिए नील का इस्तेमाल किया जा सकता है.
कुछ लोग होली के दिन पक्के रंगों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे रंग कई दिन तक नहीं उतरता. इससे कई बार मनमुटाव भी हो जाता है. कुछ लोग होली खेलना पसंद नहीं करते. ऐसे लोगों को जबरन रंग लगाया जाता है, तो लड़ाई-झगड़ा भी हो जाता है. बच्चे सादे या रंगीन पानी से भरे ग़ुब्बारे एक-दूसरे पर फेंकते हैं. ग़ुब्बारा आंख के पास लग जाने से आंख को नुक़सान हो सकता है. ये ग़ुब्बारे अकसर लड़ाई-झगड़ों की वजह भी बन जाते हैं. होली खेलने के दौरान कुछ सावधानियां बरत कर इस पर्व की ख़ुशी को बरक़रार रखा जा सकता है. बच्चों को ग़ुब्बारों से न खेलने दें. दांतों के बचाव के लिए डेंटल कैप्स का इस्तेमाल करना चाहिए. नुक़सानदेह रंगों से बचाव के लिए धूप के चश्मे का इस्तेमाल किया जा सकता है. शरीर को रंगों के द्ष्प्रभाव से बचाने के लिए पूरी बांह के कपड़े पहनने चाहिए. चमकदार और गहरे रंग के पुराने कपड़ों को तरजीह दी जानी चाहिए. जब कोई जबरन रंग लगाने की कोशिश करे, तो आंखें और होंठ बंद रखते हुए अपना बचाव करना चाहिए. बालों में तेल ज़रूर लगा लेना चाहिए, ताकि उन पर रंगों का बुरा असर न पड़े. रंगों को साफ़ करने के लिए गुनगुने पानी का इस्तेमाल करना चाहिए. अगर आंख में रंग पड़ गया है, तो फ़ौरन इसे बहते हुए नल से धो लेना चाहिए. रंग में में रसायनिक तत्व होंगे, तो इससे आंखों में हल्की एलर्जी होगी या फिर बहुत तेज़ जलन होने लगेगी. व्यक्ति को एलर्जी की समस्या, कैमिकल बर्न, कॉर्नियल एब्रेशन और आंखों में ज़ख़्म की समस्या हो सकती है. होली के दौरान आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले ज़्यादातर रंग हल्के लाल रंग के होते हैं और इसका असर 48 घंटे तक रहता है. अगर साफ़ दिखाई न दे, तो मरीज़ को फ़ौरन इमरजेंसी में दाख़िल कराया जाना चाहिए.
होली पर भांग और शराब का सेवन आम है. चिकित्सकों के मुताबिक़ भांग के सेवन की वजह से दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, जिससे मस्तिष्क को नुक़सान पहुंचने का ख़तरा बना रहता है. भांग से से मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है, जिससे व्यक्ति ख़ुद को संभाल नहीं पाता. शराब पीने वालों के साथ भी अकसर ऐसा होता है. ज़्यादा शराब पीने के बाद व्यक्ति अपनी सुधबुध खो बैठता है. इसकी वजह से सड़क हादसे का खतरा भी बढ़ जाता है.
होली प्रेम का पावन पर्व है, इसलिए इसे सावधानी पूर्वक प्रेमभाव के साथ ही मनाना चाहिए.
सिराज केसर
फाल्गुन आते ही फाल्गुनी हवा मौसम के बदलने का अहसास करा देती है। कंपकपाती ठंड से राहत लेकर आने वाला फाल्गुन मास लोगों के बीच एक नया सुख का अहसास कराता है। फाल्गुन मास से शुरू होने वाली बसंत ऋतु किसानों के खेतों में नई फसलों की सौगात देता है। पतझड़ के बाद धरती के चारों तरफ हरियाली की एक नई चुनरी ओढ़ा देता है बसंत, हर छोटे–बड़े पौधों में फूल खिला देता है बसंत, ऐसा लगता है एक नये सृजन की तैयारी लेकर आता है बसंत। ऐसे में हर कोई बसंत में अपनी जिंदगी में भी हँसी, खुशी और नयापन भर लेना चाहता हैं। इसी माहौल को भारतीय चित्त ने एक त्योहार का नाम दिया होली। जैसे बसंत प्रकृति के हर रूप में रंग बिखेर देता है। ऐसे ही होली मानव के तन-मन में रंग बिखेर देती है। जीवन को नये उल्लास से भर देती है।
होली नई फसलों का त्योहार है, प्रकृति के रंगो में सराबोर होने का त्योहार है। मूलतः होली का त्योहार प्रकृति का पर्व है। इस पर्व को भक्ति और भावना से इसीलिए जोड़ा जाता है कि ताकि प्रकृति के इस रूप से आदमी जुड़े और उसके अमूल्य धरोहरों को समझे जिनसे ही आदमी का जीवन है।
होली के इस अवसर पर, होली के दिन दिल पर पत्थर रखकर हमें दुखी मन से पानी बचाने की अपील करनी पड़ रही है। पानी की कमी से रंगो की होली की जगह खून की होली होना आये दिन सुनने और पढ़ने को मिल रही है पिछले एक साल के अंदर मध्य प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में दर्जनों लोगों की मौत पानी के कारण हुए झगड़ों में हुई। संभ्रात शहरियों ने अपने झील, तालाब को निगल डाले हैं। तालाबों को लील चुकीं ये बड़ी इमारतें बेहिसाब धरती की कोख का पानी खाली कर रही हैं। अंधाधुंध दोहन से पीने के पानी में आर्सेनिक, युरेनियम, फ्लोराइड तमाम तरह के जहर पानी जैसे अमृत तत्व में घुल चुके हैं। भावी भविष्य के समाज के जीवन में पानी का हम कौन सा रंग भरना चाहते हैं। क्या हमको यह हिसाब लगाने की जरूरत नहीं है। होली के नाम पर जल स्रोतों में सैंकड़ो टन जहरीले केमिकल हम डाल देंगें। क्या यह उन लोगों के साथ जो खरीद कर पानी नहीं पी सकते अत्याचार नहीं है। बेहिसाब पानी की बर्बादी प्रकृति के अमूल्य धरोहरों की बर्बादी हैं। सत्य यही है कि पंच तत्वों से बनी मानव जाति यदि पानी खो देगी तो अपना अस्तित्व भी खो देगी।
प्रतिदिन हम बगैर सोचे-समझे पानी का उपयोग और उपभोग करते जाते हैं। यह एक अवसर है कि हम अपने भीतर झाँकें और अपना अन्तर्मन टटोलें कि रंगों के इस शानदार त्योहार पर हम पानी की बर्बादी न करें…
बिना पानी के एक दिन गुज़ारने की कल्पना करें तो हम काँप उठेंगे। इस होली पर अपने जीवन में रंगों को उतारें जरूर, लेकिन साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि हमारे आसपास की दुनिया में जलसंकट तेजी से पैर पसार रहा है। इसलिये त्योहार की मौजमस्ती में हम कुछ बातें याद रखें ताकि प्रकृति की इस अनमोल देन को अधिक से अधिक बचा सकें…
होली पर पानी बचाने हेतु कुछ नुस्खे…
• होली खेलने के लिये आवश्यकतानुसार पानी की एक निश्चित मात्रा तय कर लें, उतना पानी स्टोर कर लें फ़िर सिर्फ़ और सिर्फ़ उतने ही पानी से होली खेलें, अधिक पानी खर्च करने के लालच में न पड़ें…
• सूखे रंगों का अधिकाधिक प्रयोग करें।
• सम्भव हो तो प्राकृतिक रंगों का उपयोग करें, क्योंकि वे आसानी से साफ़ भी हो जाते हैं।
• गुब्बारों में पानी भरकर होली खेलने से बचें।
• जब होली खेलना पूरा हो जाये तभी नहाने जायें, बार-बार नहाने अथवा हाथ-मुँह धोने से पानी का अपव्यय होता है।
होली खेलने के दौरान पानी की बचत के टिप्स
• किसी अलग जगह अथवा किसी बगीचे में होली खेलें, पूरे घर में होली खेलने से घर गन्दा होगा तथा उसे धोने में अतिरिक्त पानी खर्च होगा।
• पुराने और गहरे रंगों वाले कपड़े पहनें ताकि बाद इन्हें आसानी से धोया जा सकता है।
• होली खेलने से पहले अपने बालों में तेल लगा लें, यह एक तरह से बचाव परत के रूप में काम करता है। इसकी वजह से चाहे जितना भी रंग बालों में लगा हो एक ही बार धोने पर निकल जाता है।
• इसी तरह अपनी त्वचा पर भी कोई क्रीम या लोशन लगाकर बाहर निकलें, इससे आपकी त्वचा रूखेपन और अत्यधिक बुरे रासायनिक रंगों के इस्तेमाल की वजह से खराब नहीं होगी।
• अपने नाखूनों पर भी नेलपॉलिश अवश्य कर लें ताकि रंगों और पानी से वे खराब होने से बचें और होली खेलने के बाद भी अपने पहले जैसे स्वरूप में रहें।
• मान लें कि आप बालों में तेल और त्वचा पर क्रीम लगाना भूल भी गये हों तो होली खेलने के तुरन्त बाद शावर अथवा पानी से नहाना न शुरु करें, बल्कि रंग लगी त्वचा और बालों पर थोड़ा नारियल तेल हल्के-हल्के मलें, रंग निकलना शुरु हो जायेंगे और फ़िर कम से कम पानी में ही आपका काम हो जायेगा।
• यदि आप घर के अन्दर अथवा छत पर होली खेल रहे हों, तो कोशिश करें कि फ़र्श पर एक तारपोलीन की शीट बिछा लें, जब होली के रंग का काम समाप्त हो जाये तो वह तारपोलीन आसानी से कम पानी में धोया जा सकता है, जबकि फ़र्श अथवा छत के रंग छुड़ाने में अधिक पानी और डिटर्जेण्ट लगेगा।
पानी के कम से कम उपयोग द्वारा घर की सफ़ाई हेतु टिप्स -
दिन भर होली खेलने के बाद घर-आँगन और छत की धुलाई एक बड़ा काम होता है, लेकिन हमें इस काम में कम से कम पानी का उपयोग करना चाहिये। इस हेतु निम्न सुझाव हैं -
1. दो बाल्टी पानी भर लें, एक बाल्टी में साबुन / डिटर्जेण्ट का पानी लें और दूसरी में सादा-साफ़ पानी लें।
2. दो स्पंज़ के बड़े-बड़े टुकड़े लें।
3. फ़र्श अथवा घर के जिस हिस्से में सबसे अधिक रंग लगे हों वहाँ साबुन के पानी वाले स्पंज से धीरे-धीरे साफ़ करें।
4. इसके बाद साफ़ पानी वाले स्पंज से उस जगह को साफ़ कर लें।
5. सबसे अन्त में एक बार साफ़ पानी से उस जगह को धो लें।
6. सबसे अन्त में सूखे कपड़े अथवा वाइपर से जगह को सुखा लें।
इस विधि से पानी की काफ़ी बचत होगी ही साथ ही रंग साफ़ करने में मेहनत भी कम लगेगी। अधिक गहरे रंगों को साफ़ करने के लिये वॉशिंग सोडा भी उपयोग करें यह अधिक प्रभावशाली होता है, लेकिन इसका उपयोग बहुत कम मात्रा में होना चाहिये वरना अधिक झाग की वजह से पानी अधिक भी लग सकता है। यह करते समय दस्ताने अथवा प्लास्टिक या रबर हाथों में पहनना न भूलें, क्योंकि सोडा अथवा साबुन के लिक्विड आदि हाथों की त्वचा के लिये खतरनाक हो सकते हैं।
पर्यावरण बचाने में सहयोग करें -
यह संयोग ही है कि मार्च के महीने में ही होली और विश्व जल दिवस एक साथ आ रहे हैं। समूचे विश्व और भारत के बढ़ते जलसंकट के मद्देनज़र हमें पानी बचाने के लिये एक साथ मिलकर काम करना चाहिये और होली जैसे अवसर पर पानी की बर्बादी रोकना चाहिये। इस धरती पर लगभग 6 अरब की आबादी में से एक अरब लोगों के पास पीने को भी पानी नहीं है। जब मनुष्य इतनी बड़ी आपदा से जूझ रहा हो ऐसे में हमें अपने त्योहारों को मनाते वक्त संवेदनशीलता दिखानी चाहिये। इस होली पर जितना सम्भव हो अधिक से अधिक पानी बचाने का संकल्प लें…
फ़िरदौस ख़ान
प्लास्टिक ज़िन्दगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है. अमूमन हर चीज़ के लिए प्लास्टिक का इस्तेमाल हो रहा है, वो चाहे दूध हो, तेल, घी, आटा, चावल, दालें, मसालें, कोल्ड ड्रिंक, शर्बत, सनैक्स, दवायें, कपड़े हों या फिर ज़रूरत की दूसरी चीज़ें सभी में प्लास्टिक का इस्तेमाल हो रहा है. बाज़ार से फल या सब्ज़ियां ख़रीदो, तो वे भी प्लास्टिक की ही थैलियों में ही मिलते हैं. प्लास्टिक के इस्तेमाल की एक बड़ी वजह यह भी है कि टिन के डिब्बों, कपड़े के थैलों और काग़ज़ के लिफ़ाफ़ों के मुक़ाबले ये सस्ता पड़ता है. पहले कभी लोग राशन, फल या तरकारी ख़रीदने जाते थे, तो प्लास्टिक की टोकरियां या कपड़े के थैले लेकर जाते थे. अब ख़ाली हाथ जाते हैं, पता है कि प्लास्टिक की थैलियों में सामान मिल जाएगा. अब तो पत्तल और दोनो की तर्ज़ पर प्लास्टिक की प्लेट, गिलास और कप भी ख़ूब चलन में हैं. लोग इन्हें इस्तेमाल करते हैं और फिर कूड़े में फेंक देते हैं. लेकिन इस आसानी ने कितनी बड़ी मुश्किल पैदा कर दी है, इसका अंदाज़ा अभी जनमानस को नहीं है.
दरअसल, प्लास्टिक कचरा पर्यावरण के लिए एक गंभीर संकट बन चुका है. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक़ देश में सबसे ज़्यादा प्लास्टिक कचरा बोतलों से आता है. साल 2015-16 में करीब 900 किलो टन प्लास्टिक बोतल का उत्पादन हुआ था. राजधानी दिल्ली में अन्य महानगरों के मुक़ाबले सबसे ज़्यादा प्लास्टिक कचरा पैदा होता है. साल 2015 के आंकड़ों की मानें, तो दिल्ली में 689.52 टन, चेन्नई में 429.39 टन, मुंबई में 408.27 टन, बेंगलुरु में 313.87 टन और हैदराबाद में 199.33 टन प्लास्टिक कचरा पैदा होता है. सिर्फ़ दस फ़ीसद प्लास्टिक कचरा ही रि-साइकिल किया जाता है, बाक़ी का 90 फ़ीसद कचरा पर्यावरण के लिए नुक़सानदेह साबित होता है.
रि-साइक्लिंग की प्रक्रिया भी प्रदूषण को बढ़ाती है. रि-साइकिल किए गए या रंगीन प्लास्टिक थैलों में ऐसे रसायन होते हैं, जो ज़मीन में पहुंच जाते हैं और इससे मिट्टी और भूगर्भीय जल विषैला बन सकता है. जिन उद्योगों में पर्यावरण की दृष्टि से बेहतर तकनीक वाली रि-साइकिलिंग इकाइयां नहीं लगी होतीं. उनमें रि-साइक्लिंग के दौरान पैदा होने वाले विषैले धुएं से वायु प्रदूषण फैलता है. प्लास्टिक एक ऐसा पदार्थ है, जो सहज रूप से मिट्टी में घुल-मिल नहीं सकता. इसे अगर मिट्टी में छोड़ दिया जाए, तो भूगर्भीय जल की रिचार्जिंग को रोक सकता है. इसके अलावा प्लास्टिक उत्पादों के गुणों के सुधार के लिए और उनको मिट्टी से घुलनशील बनाने के इरादे से जो रासायनिक पदार्थ और रंग आदि उनमें आमतौर पर मिलाए जाते हैं, वे भी अमूमन सेहत पर बुरा असर डालते हैं.
स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि प्लास्टिक मूल रूप से नुक़सानदेह नहीं होता, लेकिन प्लास्टिक के थैले अनेक हानिकारक रंगों, रंजक और अन्य तमाम प्रकार के अकार्बनिक रसायनों को मिलाकर बनाए जाते हैं. रंग और रंजक एक प्रकार के औद्योगिक उत्पाद होते हैं, जिनका इस्तेमाल प्लास्टिक थैलों को चमकीला रंग देने के लिए किया जाता है. इनमें से कुछ रसायन कैंसर को जन्म दे सकते हैं और कुछ खाद्य पदार्थों को विषैला बनाने में सक्षम होते हैं. रंजक पदार्थों में कैडमियम जैसी जो धातुएं होती हैं, जो सेहत के लिए बेहद नुक़सानदेह हैं. थोड़ी-थोड़ी मात्रा में कैडमियम के इस्तेमाल से उल्टियां हो सकती हैं और दिल का आकार बढ़ सकता है. लम्बे समय तक जस्ता के इस्तेमाल से मस्तिष्क के ऊतकों का क्षरण होने लगता है.
हालांकि पर्यावरण और वन मंत्रालय ने रि-साइकिंल्ड प्लास्टिक मैन्यूफैक्चर एंड यूसेज़ रूल्स-1999 जारी किया था. इसे 2003 में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम-1968 के तहत संशोधित किया गया है, ताकि प्लास्टिक की थैलियों और डिब्बों का नियमन और प्रबंधन सही तरीक़े से किया जा सके. भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने धरती में घुलनशील प्लास्टिक के 10 मानकों के बारे में अधिसूचना जारी की थी, मगर इसके बावजूद हालात वही 'ढाक के तीन पात' वाले ही हैं.
हालांकि दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में पॉलीथिन और प्लास्टिक से बनी सामग्रियों पर रोक लगाने का ऐलान किया जा चुका है. इसका उल्लंघन करने पर जुर्माने और क़ैद का प्रावधान भी है.प्लास्टिक के इस्तेमाल से होने वाली समस्याएं ज़्यादातर कचरा प्रबंधन प्रणालियों की ख़ामियों की वजह से पैदा हुई हैं. प्लास्टिक का यह कचरा नालियों और सीवरेज व्यवस्था को ठप कर देता है. इतना ही नहीं नदियों में भी इनकी वजह से बहाव पर असर पड़ता है और पानी के दूषित होने से मछलियों की मौत तक हो जाती है. नदियों के ज़रिये प्लास्टिक का ये कचरा समुद्र में भी पहुंच रहा है. वर्ल्ड इकोनॉमिक फ़ोरम की रिपोर्ट के मुताबिक़ हर साल तकरीबन 80 लाख टन कचरा समंदरों में मिल रहा है. समंदरों में जो प्लास्टिक कचरा मिल रहा है, उसका तक़रीबन 90 फ़ीसद हिस्सा दस नदियों से आ रहा है, जिनमें यांग्त्जे, गंगा, सिंधु, येलो, पर्ल, एमर, मिकांग, नाइल और नाइजर नदियां शामिल हैं. इनमें से आठ नदियां एशिया की हैं. इनमें सबसे ज़्यादा पांच नदियां चीन की, जबकि दो नदियां भारत और एक अफ़्रीका की है. चीन ने 46 शहरों में कचरे को क़ाबू करने का निर्देश जारी किया है, ताकि नदियों के प्रदूषण को कम किया जा सके. प्लास्टिक पशुओं की मौत का भी सबब बन रहा है. कूड़े के ढेर में पड़ी प्लास्टिक की थैलियों को खाकर आवारा पशुओं की बड़ी तादाद में मौतें हो रही हैं.
प्लास्टिक के कचरे की समस्या से निजात पाने के लिए प्लास्टिक थैलियों के विकल्प के रूप में जूट से बने थैलों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया जाना चाहिए. साथ ही प्लास्टिक कचरे का समुचित इस्तेमाल किया जाना चाहिए. देश में सड़क बनाने और दीवारें बनाने में इसका इस्तेमाल शुरू हो चुका है. प्लास्टिक को इसी तरह अन्य जगह इस्तेमाल करके इसके कचरे की समस्या से निजात पाई जा सकती है. बहरहाल, प्लास्टिक कचरे से निपटने के लिए बेहद ज़रूरी है कि इसके प्रति जनमानस को जागरूक किया जाए, क्योंकि इस मुहिम में जनमानस की भागीदारी बहुत ज़रूरी है. इसके लिए जन आंदोलन चलाया जाना चाहिए.
प्लास्टिक ज़िन्दगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है. अमूमन हर चीज़ के लिए प्लास्टिक का इस्तेमाल हो रहा है, वो चाहे दूध हो, तेल, घी, आटा, चावल, दालें, मसालें, कोल्ड ड्रिंक, शर्बत, सनैक्स, दवायें, कपड़े हों या फिर ज़रूरत की दूसरी चीज़ें सभी में प्लास्टिक का इस्तेमाल हो रहा है. बाज़ार से फल या सब्ज़ियां ख़रीदो, तो वे भी प्लास्टिक की ही थैलियों में ही मिलते हैं. प्लास्टिक के इस्तेमाल की एक बड़ी वजह यह भी है कि टिन के डिब्बों, कपड़े के थैलों और काग़ज़ के लिफ़ाफ़ों के मुक़ाबले ये सस्ता पड़ता है. पहले कभी लोग राशन, फल या तरकारी ख़रीदने जाते थे, तो प्लास्टिक की टोकरियां या कपड़े के थैले लेकर जाते थे. अब ख़ाली हाथ जाते हैं, पता है कि प्लास्टिक की थैलियों में सामान मिल जाएगा. अब तो पत्तल और दोनो की तर्ज़ पर प्लास्टिक की प्लेट, गिलास और कप भी ख़ूब चलन में हैं. लोग इन्हें इस्तेमाल करते हैं और फिर कूड़े में फेंक देते हैं. लेकिन इस आसानी ने कितनी बड़ी मुश्किल पैदा कर दी है, इसका अंदाज़ा अभी जनमानस को नहीं है.
दरअसल, प्लास्टिक कचरा पर्यावरण के लिए एक गंभीर संकट बन चुका है. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक़ देश में सबसे ज़्यादा प्लास्टिक कचरा बोतलों से आता है. साल 2015-16 में करीब 900 किलो टन प्लास्टिक बोतल का उत्पादन हुआ था. राजधानी दिल्ली में अन्य महानगरों के मुक़ाबले सबसे ज़्यादा प्लास्टिक कचरा पैदा होता है. साल 2015 के आंकड़ों की मानें, तो दिल्ली में 689.52 टन, चेन्नई में 429.39 टन, मुंबई में 408.27 टन, बेंगलुरु में 313.87 टन और हैदराबाद में 199.33 टन प्लास्टिक कचरा पैदा होता है. सिर्फ़ दस फ़ीसद प्लास्टिक कचरा ही रि-साइकिल किया जाता है, बाक़ी का 90 फ़ीसद कचरा पर्यावरण के लिए नुक़सानदेह साबित होता है.
रि-साइक्लिंग की प्रक्रिया भी प्रदूषण को बढ़ाती है. रि-साइकिल किए गए या रंगीन प्लास्टिक थैलों में ऐसे रसायन होते हैं, जो ज़मीन में पहुंच जाते हैं और इससे मिट्टी और भूगर्भीय जल विषैला बन सकता है. जिन उद्योगों में पर्यावरण की दृष्टि से बेहतर तकनीक वाली रि-साइकिलिंग इकाइयां नहीं लगी होतीं. उनमें रि-साइक्लिंग के दौरान पैदा होने वाले विषैले धुएं से वायु प्रदूषण फैलता है. प्लास्टिक एक ऐसा पदार्थ है, जो सहज रूप से मिट्टी में घुल-मिल नहीं सकता. इसे अगर मिट्टी में छोड़ दिया जाए, तो भूगर्भीय जल की रिचार्जिंग को रोक सकता है. इसके अलावा प्लास्टिक उत्पादों के गुणों के सुधार के लिए और उनको मिट्टी से घुलनशील बनाने के इरादे से जो रासायनिक पदार्थ और रंग आदि उनमें आमतौर पर मिलाए जाते हैं, वे भी अमूमन सेहत पर बुरा असर डालते हैं.
स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि प्लास्टिक मूल रूप से नुक़सानदेह नहीं होता, लेकिन प्लास्टिक के थैले अनेक हानिकारक रंगों, रंजक और अन्य तमाम प्रकार के अकार्बनिक रसायनों को मिलाकर बनाए जाते हैं. रंग और रंजक एक प्रकार के औद्योगिक उत्पाद होते हैं, जिनका इस्तेमाल प्लास्टिक थैलों को चमकीला रंग देने के लिए किया जाता है. इनमें से कुछ रसायन कैंसर को जन्म दे सकते हैं और कुछ खाद्य पदार्थों को विषैला बनाने में सक्षम होते हैं. रंजक पदार्थों में कैडमियम जैसी जो धातुएं होती हैं, जो सेहत के लिए बेहद नुक़सानदेह हैं. थोड़ी-थोड़ी मात्रा में कैडमियम के इस्तेमाल से उल्टियां हो सकती हैं और दिल का आकार बढ़ सकता है. लम्बे समय तक जस्ता के इस्तेमाल से मस्तिष्क के ऊतकों का क्षरण होने लगता है.
हालांकि पर्यावरण और वन मंत्रालय ने रि-साइकिंल्ड प्लास्टिक मैन्यूफैक्चर एंड यूसेज़ रूल्स-1999 जारी किया था. इसे 2003 में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम-1968 के तहत संशोधित किया गया है, ताकि प्लास्टिक की थैलियों और डिब्बों का नियमन और प्रबंधन सही तरीक़े से किया जा सके. भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने धरती में घुलनशील प्लास्टिक के 10 मानकों के बारे में अधिसूचना जारी की थी, मगर इसके बावजूद हालात वही 'ढाक के तीन पात' वाले ही हैं.
हालांकि दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में पॉलीथिन और प्लास्टिक से बनी सामग्रियों पर रोक लगाने का ऐलान किया जा चुका है. इसका उल्लंघन करने पर जुर्माने और क़ैद का प्रावधान भी है.प्लास्टिक के इस्तेमाल से होने वाली समस्याएं ज़्यादातर कचरा प्रबंधन प्रणालियों की ख़ामियों की वजह से पैदा हुई हैं. प्लास्टिक का यह कचरा नालियों और सीवरेज व्यवस्था को ठप कर देता है. इतना ही नहीं नदियों में भी इनकी वजह से बहाव पर असर पड़ता है और पानी के दूषित होने से मछलियों की मौत तक हो जाती है. नदियों के ज़रिये प्लास्टिक का ये कचरा समुद्र में भी पहुंच रहा है. वर्ल्ड इकोनॉमिक फ़ोरम की रिपोर्ट के मुताबिक़ हर साल तकरीबन 80 लाख टन कचरा समंदरों में मिल रहा है. समंदरों में जो प्लास्टिक कचरा मिल रहा है, उसका तक़रीबन 90 फ़ीसद हिस्सा दस नदियों से आ रहा है, जिनमें यांग्त्जे, गंगा, सिंधु, येलो, पर्ल, एमर, मिकांग, नाइल और नाइजर नदियां शामिल हैं. इनमें से आठ नदियां एशिया की हैं. इनमें सबसे ज़्यादा पांच नदियां चीन की, जबकि दो नदियां भारत और एक अफ़्रीका की है. चीन ने 46 शहरों में कचरे को क़ाबू करने का निर्देश जारी किया है, ताकि नदियों के प्रदूषण को कम किया जा सके. प्लास्टिक पशुओं की मौत का भी सबब बन रहा है. कूड़े के ढेर में पड़ी प्लास्टिक की थैलियों को खाकर आवारा पशुओं की बड़ी तादाद में मौतें हो रही हैं.
प्लास्टिक के कचरे की समस्या से निजात पाने के लिए प्लास्टिक थैलियों के विकल्प के रूप में जूट से बने थैलों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया जाना चाहिए. साथ ही प्लास्टिक कचरे का समुचित इस्तेमाल किया जाना चाहिए. देश में सड़क बनाने और दीवारें बनाने में इसका इस्तेमाल शुरू हो चुका है. प्लास्टिक को इसी तरह अन्य जगह इस्तेमाल करके इसके कचरे की समस्या से निजात पाई जा सकती है. बहरहाल, प्लास्टिक कचरे से निपटने के लिए बेहद ज़रूरी है कि इसके प्रति जनमानस को जागरूक किया जाए, क्योंकि इस मुहिम में जनमानस की भागीदारी बहुत ज़रूरी है. इसके लिए जन आंदोलन चलाया जाना चाहिए.
फ़िरदौस ख़ान
बरसात का मौसम शुरू ही देश के कई राज्य बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं. बाढ़ से जान व माल का भारी नुक़सान होता है. लाखों लोग बाढ़ से प्रभावित होते हैं. कितने ही लोग बाढ़ की वजह से मौत की आग़ोश में समा जाते हैं. सैकड़ों मकान क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, हज़ारों लोगों को बेघर होकर शरणार्थी जीवन गुज़ारने को मजबूर होना पड़ता हैं. खेतों में खड़ी फ़सलें तबाह हो जाती हैं.
देश में बाढ़ आने के कई कारण हैं. बाढ़ अमूमन उत्तर पूर्वी राज्यों को ही निशाना बनाती है. इसकी सबसे बड़ी वजह है कि चीन और ऊपरी पहाड़ों में भारी बारिश होती है और वर्षा का यह पानी भारत के निचले इलाक़ों की तरह बहता है. फिर यही पानी तबाही की वजह बनता है. नेपाल में भारी बारिश का पानी भी बिहार की कोसी नदी को उफ़ान पर ला देता है, जिससे नदी के रास्ते में आने वाले इलाक़े पानी में डूब जाते हैं. ग़ौरतलब है कि कोसी नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है. यह नदी बिहार में भीम नगर के रास्ते भारत में दाख़िल होती है. कोसी बिहार में भारी तबाही मचाती है, इसलिए इसे बिहार का शोक या अभिशाप भी कहा जाता है. कोसी नदी हर साल अपनी धारा बदलती रहती है. साल 1954 में भारत ने नेपाल के साथ समझौता करके इस पर बांध बनाया था. हालांकि बांध नेपाल की सीमा में बनाया गया है, लेकिन इसके रखरखाव का काम भारत के ज़िम्मे है. नदी के तेज़ बहाव के कारण यह बांध कई बार टूट चुका है. आधिकारिक जानकारी के मुताबिक़ बांध बनाते वक्त आकलन किया गया था कि यह नौ लाख क्यूसेक पानी के बहाव को सहन कर सकता है और बांध की उम्र 25 साल आंकी गई थी. पहली बार यह बांध 1963 में टूटा. इसके बाद 1968 में पांच जगहों से यह टूटा. उस वक़्त कोसी का बहाव नौ लाख 13 हज़ार क्यूसेक मापा गया था. फिर साल 1991 नेपाल के जोगनिया और 2008 में नेपाल के ही कुसहा नामक स्थान पर बांध टूट गया. हैरानी की बात यह रही कि उस वक़्त नदी का बहाव महज़ एक लाख 44 हज़ार क्यूसेक था. फ़िलहाल कोसी पर बने बांध में जगह-जगह दरारें पड़ी हुई हैं.
कोसी की तरह गंडक नदी भी नेपाल के रास्ते बिहार में दाख़िल करती है. गंडक को नेपाल में सालिग्राम और मैदान में नारायणी कहते हैं. यह पटना में आकर गंगा में मिल जाती है. बरसात में गंडक भी उफ़ान पर होती है और इसके आसपास के इलाक़े बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं. ग़ौरतलब है कि बांग्लादेश के बाद भारत ही दुनिया का दूसरा सर्वाधिक बाढ़ग्रस्त देश है. देश में कुल 62 प्रमुख नदी प्रणालियां हैं, जिनमें से 18 ऐसी हैं जो अमूमन बाढ़ग्रस्त रहती हैं. उत्तर-पूर्व में असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश तथा दक्षिण में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु बाढ़ग्रस्त इलाके माने जाते हैं, लेकिन कभी-कभार देश के अन्य राज्य भी बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं. पश्चिम बंगाल की मयूराक्षी, अजय, मुंडेश्वरी, तीस्ता और तोर्सा नदियां तबाही मचाती हैं, ओडिशा में सुवर्णरेखा, बैतरनी, ब्राह्मणी, महानंदा, ऋषिकुल्या, वामसरदा नदियां उफ़ान पर रहती हैं. आंध्रप्रदेश में गोदावरी और तुंगभद्रा, त्रिपुरा में मनु और गुमती, महाराष्ट्र में वेणगंगा, गुजरात और मध्य-प्रदेश में नर्मदा नदियों की वजह से इनके तटवर्ती इलाक़ों में बाढ़ आती है.
बाढ़ से हर साल करोड़ों रुपये का नुक़सान होता है, लेकिन नुक़सान का यह अंदाज़ा वास्तविक नहीं होता. बाढ़ से हुए नुक़सान की सही राशि का अंदाज़ा लगाना आसान नहीं है, क्योंकि बाढ़ से मकान व दुकानें क्षतिग्रस्त होती हैं. फ़सलें तबाह हो जाती हैं. लोगों का कारोबार ठप हो जाता है. बाढ़ के साथ आने वाली बीमारियों की वजह से स्वास्थ्य सेवाओं पर भी काफ़ी पैसा ख़र्च होता है. लोगों को बाढ़ से नुक़सान की भरपाई में काफ़ी वक़्त लग जाता है. यह कहना ग़लत न होगा कि बाढ़ किसी भी देश, राज्य या व्यक्ति को कई साल पीछे कर देती है. बाढ़ से उसका आर्थिक और सामाजिक विकास ठहर जाता है. इसलिए बाढ़ से होने वाले नुक़सान का सही अंदाज़ा लगाना बेहद मुश्किल है.
जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक़, देश में पिछले साढ़े छह दशक के दौरान बाढ़ से सालाना औसतन 1654 लोगों की मौत हुई और 92763 पशुओं की जान गई. इससे सालाना औसतन 71.69 लाख हेक्टेयर इलाक़े पर असर पड़ा और तकरीबन 1680 करोड़ रुपये फ़सलें तबाह हो गईं. बाढ़ से सालाना 12.40 लाख मकानों को नुक़सान पहुंचा. साल 1953 से 2017 के कुल नुक़सान पर नज़र डालें, तो देश में बाढ़ की वजह से 46.60 करोड़ हेक्टेयर इलाक़े में 205.8 करोड़
लोग बुरी तरह प्रभावित हुए हैं. इस दौरान 8.06 करोड़ मकानों को नुक़सान पहुंचा है. अफ़सोस की बात है कि हर साल बाढ़ से होने वाले जान व माल के नुकसान में बढ़ोतरी हो रही है, जो बेहद चिंताजनक है.
पिछले सात दशकों में देश में अनेक बांध बनाए गए हैं. साथ ही पिछले क़रीब तीन दशकों से बाढ़ नियंत्रण में मदद के लिए रिमोट सेंसिंग और भौगोलिक सूचना व्यवस्था का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन संतोषजनक नतीजे सामने नहीं आ पा रहे हैं. बाढ़ से निपटने के लिए 1978 में केंद्रीय बाढ़ नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया था. देश के कुल 32.9 करोड़ हेक्टेयर में से तक़रीबन 4.64 करोड़ हेक्टेयर भूमि बाढ़ प्रभावित इलाक़े में आती है. देश में हर साल तक़रीबन 4000 अरब घन मीटर बारिश होती है.
हैरत का बात यह भी है कि बाढ़ एक राष्ट्रीय आपदा है, इसके बावजूद इसे राज्य सूची में रखा गया है. इसके तहत केंद्र सरकार बाढ़ से संबंधित कितनी ही योजनाएं बना ले, लेकिन उन पर अमल करना राज्य सरकार की ज़िम्मेदारी है. प्रांतवाद के कारण राज्य बाढ़ से निपटने के लिए पर्याप्त उपाय नहीं कर पाते. एक राज्य की बाढ़ का पानी समीपवर्ती राज्य के इलाक़ों को भी प्रभावित करता है. मसलन हरियाणा का बाढ़ का पानी राजधानी दिल्ली में छोड़ दिया जाता है, जिससे यहां के इलाक़े पानी में डूब जाते हैं. राज्यों में हर साल बाढ़ की रोकथाम के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं, मगर प्रशासनिक लापरवाही की वजह से इन योजनाओं पर ठीक से अमल नहीं हो पाता. नतीजतन, यह योजनाएं महज़ काग़जों तक ही सिमट कर जाती हैं. हालांकि बाढ़ को रोकने के लिए सरकारी स्तर पर योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनमें बाढ़ प्रभावित इलाकों में बांध बनाना, नदियों के कटान वाले इलाक़ों में कटान रोकना, पानी की निकासी वाले नालों की सफ़ाई और उनकी सिल्ट निकालना, निचले इलाक़ों के गांवों को ऊंचा करना, सीवरेज व्यवस्था को सुधारना और शहरों में नालों के रास्ते आने वाले कब्ज़ों को हटाना आदि शामिल है.
क़ाबिले-ग़ौर है कि विकसित देशों में आगजनी, तूफ़ान, भूकंप और बाढ़ के लिए क़स्बों का प्रशासन भी पहले से तैयार रहता है. उन्हें पहले से पता होता है कि किस पैमाने पर, किस आपदा की दशा में, उन्हें क्या-क्या करना है. वे बिना विपदा के छोटे पैमाने पर इसका अभ्यास करते रहते हैं. गली-मोहल्लों के हर घर तक यह सूचना मीडिया या डाक के ज़रिये संक्षेप में पहुंचा दी जाती है कि किस दशा में उन्हें क्या करना है. संचार व्यवस्था के टूटने पर भी वे प्रशासन से क्या उम्मीद रख सकते हैं. पहले तो वे इसकी रोकथाम की कोशिश करते हैं. इसमें विशेषज्ञों की सलाह ली जाती है. इस प्रक्रिया को आपदा प्रबंधन कहते हैं. आग तूफ़ान और भूकंप के दौरान आपदा प्रबंधन एक ख़र्चीली प्रक्रिया है, लेकिन बाढ़ का आपदा नियंत्रण उतना ख़र्चीला काम नहीं है. इसे बख़ूबी बाढ़ आने वाले इलाक़ों में लागू किया जा सकता है. विकसित देशों में बाढ़ के आपदा प्रबंधन में सबसे पहले यह ध्यान रखा जाता है कि मिट्टी, कचरे वगैरह के जमा होने से इसकी गहराई कम न हो जाए. इसके लिए नदी के किनारों पर ख़ासतौर से पेड़ लगाए जाते हैं, जिनकी जड़ें मिट्टी को थामकर रखती हैं. नदी किनारे पर घर बसाने वालों के बग़ीचों में भी अनिवार्य रूप से पेड़ लगवाए जाते हैं. जहां बाढ़ का ख़तरा ज़्यादा हो, वहां नदी को और अधिक गहरा कर दिया जाता है. गांवों तक में पानी का स्तर नापने के लिए स्केल बनी होती है.
हमारे देश में भी प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए पहले से ही तैयार रहना होगा. इसके लिए जहां प्रशासन को चाक-चौबंद रहने की ज़रूरत है, वहीं जनमानस को भी प्राकृतिक आपदा से निपटने का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए. स्कूल, कॉलेजों के अलावा जगह-जगह शिविर लगाकर लोगों को यह प्रशिक्षण दिया जा सकता है. इसमें स्वयंसेवी संस्थाओं की भी मदद ली जा सकती है. इस तरह प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुक़सान को कम किया जा सकता है.
बरसात का मौसम शुरू ही देश के कई राज्य बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं. बाढ़ से जान व माल का भारी नुक़सान होता है. लाखों लोग बाढ़ से प्रभावित होते हैं. कितने ही लोग बाढ़ की वजह से मौत की आग़ोश में समा जाते हैं. सैकड़ों मकान क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, हज़ारों लोगों को बेघर होकर शरणार्थी जीवन गुज़ारने को मजबूर होना पड़ता हैं. खेतों में खड़ी फ़सलें तबाह हो जाती हैं.
देश में बाढ़ आने के कई कारण हैं. बाढ़ अमूमन उत्तर पूर्वी राज्यों को ही निशाना बनाती है. इसकी सबसे बड़ी वजह है कि चीन और ऊपरी पहाड़ों में भारी बारिश होती है और वर्षा का यह पानी भारत के निचले इलाक़ों की तरह बहता है. फिर यही पानी तबाही की वजह बनता है. नेपाल में भारी बारिश का पानी भी बिहार की कोसी नदी को उफ़ान पर ला देता है, जिससे नदी के रास्ते में आने वाले इलाक़े पानी में डूब जाते हैं. ग़ौरतलब है कि कोसी नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है. यह नदी बिहार में भीम नगर के रास्ते भारत में दाख़िल होती है. कोसी बिहार में भारी तबाही मचाती है, इसलिए इसे बिहार का शोक या अभिशाप भी कहा जाता है. कोसी नदी हर साल अपनी धारा बदलती रहती है. साल 1954 में भारत ने नेपाल के साथ समझौता करके इस पर बांध बनाया था. हालांकि बांध नेपाल की सीमा में बनाया गया है, लेकिन इसके रखरखाव का काम भारत के ज़िम्मे है. नदी के तेज़ बहाव के कारण यह बांध कई बार टूट चुका है. आधिकारिक जानकारी के मुताबिक़ बांध बनाते वक्त आकलन किया गया था कि यह नौ लाख क्यूसेक पानी के बहाव को सहन कर सकता है और बांध की उम्र 25 साल आंकी गई थी. पहली बार यह बांध 1963 में टूटा. इसके बाद 1968 में पांच जगहों से यह टूटा. उस वक़्त कोसी का बहाव नौ लाख 13 हज़ार क्यूसेक मापा गया था. फिर साल 1991 नेपाल के जोगनिया और 2008 में नेपाल के ही कुसहा नामक स्थान पर बांध टूट गया. हैरानी की बात यह रही कि उस वक़्त नदी का बहाव महज़ एक लाख 44 हज़ार क्यूसेक था. फ़िलहाल कोसी पर बने बांध में जगह-जगह दरारें पड़ी हुई हैं.
कोसी की तरह गंडक नदी भी नेपाल के रास्ते बिहार में दाख़िल करती है. गंडक को नेपाल में सालिग्राम और मैदान में नारायणी कहते हैं. यह पटना में आकर गंगा में मिल जाती है. बरसात में गंडक भी उफ़ान पर होती है और इसके आसपास के इलाक़े बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं. ग़ौरतलब है कि बांग्लादेश के बाद भारत ही दुनिया का दूसरा सर्वाधिक बाढ़ग्रस्त देश है. देश में कुल 62 प्रमुख नदी प्रणालियां हैं, जिनमें से 18 ऐसी हैं जो अमूमन बाढ़ग्रस्त रहती हैं. उत्तर-पूर्व में असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश तथा दक्षिण में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु बाढ़ग्रस्त इलाके माने जाते हैं, लेकिन कभी-कभार देश के अन्य राज्य भी बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं. पश्चिम बंगाल की मयूराक्षी, अजय, मुंडेश्वरी, तीस्ता और तोर्सा नदियां तबाही मचाती हैं, ओडिशा में सुवर्णरेखा, बैतरनी, ब्राह्मणी, महानंदा, ऋषिकुल्या, वामसरदा नदियां उफ़ान पर रहती हैं. आंध्रप्रदेश में गोदावरी और तुंगभद्रा, त्रिपुरा में मनु और गुमती, महाराष्ट्र में वेणगंगा, गुजरात और मध्य-प्रदेश में नर्मदा नदियों की वजह से इनके तटवर्ती इलाक़ों में बाढ़ आती है.
बाढ़ से हर साल करोड़ों रुपये का नुक़सान होता है, लेकिन नुक़सान का यह अंदाज़ा वास्तविक नहीं होता. बाढ़ से हुए नुक़सान की सही राशि का अंदाज़ा लगाना आसान नहीं है, क्योंकि बाढ़ से मकान व दुकानें क्षतिग्रस्त होती हैं. फ़सलें तबाह हो जाती हैं. लोगों का कारोबार ठप हो जाता है. बाढ़ के साथ आने वाली बीमारियों की वजह से स्वास्थ्य सेवाओं पर भी काफ़ी पैसा ख़र्च होता है. लोगों को बाढ़ से नुक़सान की भरपाई में काफ़ी वक़्त लग जाता है. यह कहना ग़लत न होगा कि बाढ़ किसी भी देश, राज्य या व्यक्ति को कई साल पीछे कर देती है. बाढ़ से उसका आर्थिक और सामाजिक विकास ठहर जाता है. इसलिए बाढ़ से होने वाले नुक़सान का सही अंदाज़ा लगाना बेहद मुश्किल है.
जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक़, देश में पिछले साढ़े छह दशक के दौरान बाढ़ से सालाना औसतन 1654 लोगों की मौत हुई और 92763 पशुओं की जान गई. इससे सालाना औसतन 71.69 लाख हेक्टेयर इलाक़े पर असर पड़ा और तकरीबन 1680 करोड़ रुपये फ़सलें तबाह हो गईं. बाढ़ से सालाना 12.40 लाख मकानों को नुक़सान पहुंचा. साल 1953 से 2017 के कुल नुक़सान पर नज़र डालें, तो देश में बाढ़ की वजह से 46.60 करोड़ हेक्टेयर इलाक़े में 205.8 करोड़
लोग बुरी तरह प्रभावित हुए हैं. इस दौरान 8.06 करोड़ मकानों को नुक़सान पहुंचा है. अफ़सोस की बात है कि हर साल बाढ़ से होने वाले जान व माल के नुकसान में बढ़ोतरी हो रही है, जो बेहद चिंताजनक है.
पिछले सात दशकों में देश में अनेक बांध बनाए गए हैं. साथ ही पिछले क़रीब तीन दशकों से बाढ़ नियंत्रण में मदद के लिए रिमोट सेंसिंग और भौगोलिक सूचना व्यवस्था का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन संतोषजनक नतीजे सामने नहीं आ पा रहे हैं. बाढ़ से निपटने के लिए 1978 में केंद्रीय बाढ़ नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया था. देश के कुल 32.9 करोड़ हेक्टेयर में से तक़रीबन 4.64 करोड़ हेक्टेयर भूमि बाढ़ प्रभावित इलाक़े में आती है. देश में हर साल तक़रीबन 4000 अरब घन मीटर बारिश होती है.
हैरत का बात यह भी है कि बाढ़ एक राष्ट्रीय आपदा है, इसके बावजूद इसे राज्य सूची में रखा गया है. इसके तहत केंद्र सरकार बाढ़ से संबंधित कितनी ही योजनाएं बना ले, लेकिन उन पर अमल करना राज्य सरकार की ज़िम्मेदारी है. प्रांतवाद के कारण राज्य बाढ़ से निपटने के लिए पर्याप्त उपाय नहीं कर पाते. एक राज्य की बाढ़ का पानी समीपवर्ती राज्य के इलाक़ों को भी प्रभावित करता है. मसलन हरियाणा का बाढ़ का पानी राजधानी दिल्ली में छोड़ दिया जाता है, जिससे यहां के इलाक़े पानी में डूब जाते हैं. राज्यों में हर साल बाढ़ की रोकथाम के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं, मगर प्रशासनिक लापरवाही की वजह से इन योजनाओं पर ठीक से अमल नहीं हो पाता. नतीजतन, यह योजनाएं महज़ काग़जों तक ही सिमट कर जाती हैं. हालांकि बाढ़ को रोकने के लिए सरकारी स्तर पर योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनमें बाढ़ प्रभावित इलाकों में बांध बनाना, नदियों के कटान वाले इलाक़ों में कटान रोकना, पानी की निकासी वाले नालों की सफ़ाई और उनकी सिल्ट निकालना, निचले इलाक़ों के गांवों को ऊंचा करना, सीवरेज व्यवस्था को सुधारना और शहरों में नालों के रास्ते आने वाले कब्ज़ों को हटाना आदि शामिल है.
क़ाबिले-ग़ौर है कि विकसित देशों में आगजनी, तूफ़ान, भूकंप और बाढ़ के लिए क़स्बों का प्रशासन भी पहले से तैयार रहता है. उन्हें पहले से पता होता है कि किस पैमाने पर, किस आपदा की दशा में, उन्हें क्या-क्या करना है. वे बिना विपदा के छोटे पैमाने पर इसका अभ्यास करते रहते हैं. गली-मोहल्लों के हर घर तक यह सूचना मीडिया या डाक के ज़रिये संक्षेप में पहुंचा दी जाती है कि किस दशा में उन्हें क्या करना है. संचार व्यवस्था के टूटने पर भी वे प्रशासन से क्या उम्मीद रख सकते हैं. पहले तो वे इसकी रोकथाम की कोशिश करते हैं. इसमें विशेषज्ञों की सलाह ली जाती है. इस प्रक्रिया को आपदा प्रबंधन कहते हैं. आग तूफ़ान और भूकंप के दौरान आपदा प्रबंधन एक ख़र्चीली प्रक्रिया है, लेकिन बाढ़ का आपदा नियंत्रण उतना ख़र्चीला काम नहीं है. इसे बख़ूबी बाढ़ आने वाले इलाक़ों में लागू किया जा सकता है. विकसित देशों में बाढ़ के आपदा प्रबंधन में सबसे पहले यह ध्यान रखा जाता है कि मिट्टी, कचरे वगैरह के जमा होने से इसकी गहराई कम न हो जाए. इसके लिए नदी के किनारों पर ख़ासतौर से पेड़ लगाए जाते हैं, जिनकी जड़ें मिट्टी को थामकर रखती हैं. नदी किनारे पर घर बसाने वालों के बग़ीचों में भी अनिवार्य रूप से पेड़ लगवाए जाते हैं. जहां बाढ़ का ख़तरा ज़्यादा हो, वहां नदी को और अधिक गहरा कर दिया जाता है. गांवों तक में पानी का स्तर नापने के लिए स्केल बनी होती है.
हमारे देश में भी प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए पहले से ही तैयार रहना होगा. इसके लिए जहां प्रशासन को चाक-चौबंद रहने की ज़रूरत है, वहीं जनमानस को भी प्राकृतिक आपदा से निपटने का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए. स्कूल, कॉलेजों के अलावा जगह-जगह शिविर लगाकर लोगों को यह प्रशिक्षण दिया जा सकता है. इसमें स्वयंसेवी संस्थाओं की भी मदद ली जा सकती है. इस तरह प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुक़सान को कम किया जा सकता है.
फ़िरदौस ख़ान
देश की नदियां दिनोदिन प्रदूषित होती जा रही हैं. जल प्रदूषण रोकने के लिए क़ानून तो बने, लेकिन उन पर अमल नहीं किया गया. मुंबई का कचरा समुद्र और कालू नदी में बहाया जा रहा है. इसी तरह दिल्ली की गंदगी यमुना, कोलकाता की हुगली और दामोदर में, चेन्नई की कुअम में, बनारस, हरिद्वार, कानपूर की गंदगी गंगा में डाली जा रही है. नतीजतन, गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, गोदावरी सहित देश की 27 नदियां जल प्रदूषण की चपेट में हैं. जल प्रदूषण सेहत के लिए बेहद ख़तरनाक है. विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक़ दुनिया भर में हर साल डेढ़ करोड़ लोग प्रदूषित जल के कारण मौत के शिकार हो जाते हैं. भारत में प्रति लाख पर तक़रीबन 360 लोगों की मौत हो जाती है. अस्पतालों में दाख़िल होने वाले मरीज़ों में से 50 फ़ीसद मरीज़ ऐसे होते है, जिनकी बीमारी की वजह दूषित पानी होता है. अविकसित देशों की हालत तो और भी ज़्यादा बुरी है, क्योंकि यहां 80 फ़ीसद बीमारियों का कारण दूषित पानी है. जल प्रदूषण से इंसान ही नहीं, जलीय जीव-जंतु, जलीय पादप और पशु-पक्षी भी बुरी तरह प्रभावित होते हैं.
जल प्रदूषण का असर लोगों की रोज़मर्राह की ज़िन्दगी पर भी पड़ रहा है. हाल में यमुना के पानी में अचानक अमोनिया की मात्रा बढ़ने की वजह से दिल्ली के वज़ीराबाद और चंद्रावल जल शोधन संयंत्रों को बंद कर बंद करना पड़ा. इन संयंत्रों के बंद होने से 222 एमजीडी (मिलियन गैलन प्रतिदिन) पेयजल की आपूर्ति रुक गई. वज़ीराबाद जल शोधन संयंत्र की क्षमता 124 एमजीडी और चंद्रावल जल शोधन संयंत्र की क्षमता 98 एमजीडी है.
इसकी वजह से दिल्ली के एनडीएमसी सहित उत्तरी दिल्ली, उत्तर-पश्चिम दिल्ली, मध्य दिल्ली और पश्चिमी और दक्षिणी दिल्ली के कई इलाक़े प्रभावित हो गए, जिनमें चांदनी चौक, आज़ाद मार्केट, सदर बाज़ार, दरियागंज, जामा मस्जिद, सिविल लाइंस, सुभाष पार्क, मुखर्जी नगर, शक्ति नगर, आदर्श नगर, मॉडल टॉउन, जहांगीरपुरी, वज़ीरपुर इंडस्ट्रीयल एरिया, पंजाबी बाग़, गुलाबी बागग़, हिन्दूराव, झंडेवालान, मोतिया ख़ान, पहाड़गंज, करोलबाग़, ओल्ड राजेंद्र नगर, नया बाज़ार, ईस्ट और वेस्ट पटेल नगर, मल्कागंज और वज़ीराबाद आदि शामिल हैं.
दिल्ली जल बोर्ड के मुताबिक़ पानीपत ड्रेन से प्रदूषित पानी नदी में गिरने की वजह से अमोनिया की मात्रा बढ़ गई. ग़ौरतलब है कि अमोनिया एक तीक्ष्ण गंध वाली रंगहीन गैस है. यह हवा से हल्की होती है और इसका वाष्प घनत्व 8.5 है. यह जल में अति विलेय है. अमोनिया के जलीय घोल को लिकर अमोनिया कहा जाता है. यह प्रकृति क्षारीय होती है. कई रसायनों और रासायनिक खादों को बनाने में अमोनिया का इस्तेमाल किया जाता है. बर्फ़ के कारख़ाने में शीतलक के रूप में अमोनिया का इस्तेमाल होता है. अमोनिया गैस बहुत ज़हरीली होती है. इसे सूंघने पर इंसान की जान तक जा सकती है.
इससे पहले जनवरी और 27 दिसंबर में भी यमुना में अमोनिया की मात्रा बढ़ गई थी, जिससे वज़ीराबाद और चंद्रावल जल शोधन संयंत्रों को बंद कर गया था. दिल्ली के बहुत से इलाक़े जल संकट से जूझ रहे हैं. पिछले काफ़ी अरसे से जो जल आपूर्ति की जा रही है, उसका पानी पीने के क़ाबिल नहीं है. पानी को कुछ देर रखने के बाद देखें, तो बर्तन की तली में गंदगी की एक पर्त जम जाती है. जो लोग पैसे वाले हैं, उन्होंने आरओ लगवा रखे हैं, कुछ लोग बाज़ार से पानी की बोतलें ख़रीदते हैं. जो ये सब नहीं कर सकते, वो पानी को उबालकर, छानकर इस्तेमाल कर रहे हैं. महिलाओं का कहना है कि गैस भी कोई सस्ती नहीं है. पानी गर्म करने की वजह से उनका सिलेंडर जल्द ख़त्म हो जाता है.
यमुना में अमोनिया का स्तर बढ़ने पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (एनजीटी) ने दिल्ली जल बोर्ड को फटकार लगाते हुए जवाब तलब किया था. एक रिपोर्ट के आधार पर ग्रीन बेंच ने दिल्ली जल बोर्ड से पूछा था कि अमोनिया स्तर बढ़ने के मामले पर आपका पक्ष क्या है? इस संबंध में अभी तक आपने क्या किया? बोर्ड के वकील इन सवालों का संतोषजनक जवाब न दे सके. इसके बाद बेंच ने पर्यावरण मंत्रालय, जल संसाधन मंत्रालय और दिल्ली जल बोर्ड के आला अधिकारियों को तलब किया था. बेंच ने इस मामले में निर्मल यमुना पुनरुद्धार योजना-2017 के चेयरमैन एवं दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ को भी तलब किया था. क़ाबिले-ग़ौर है कि निर्मल यमुना पुनरुद्धार योजना के लिए बनाई गई प्रधान समिति में पर्यावरण मंत्रालय के सचिव, जल संसाधन मंत्रालय के संयुक्त सचिव, दिल्ली के मुख्य सचिव, डीडीए के वाइस चेयरमैन, दिल्ली नगर निगमों के कमिश्नर्स, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के राज्य सचिव को शामिल किया गया था. पिछले दिनों आई एक रिपोर्ट में कहा गया था कि यमुना में अमोनिया का स्तर 2 से 2.5 पार्ट्स प्रति मिलियन (पीपीएम) पाया गया है. इसके बाद दिल्ली जल मंत्री कपिल मिश्रा ने केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती को पत्र लिखकर बताया था कि अगर अमोनिया की मात्रा 0.5 पीपीएम या उससे ज़्यादा हुई, तो यह पानी सेहत के लिए काफ़ी नुक़सानदएह हो सकता है. अगर उच्च अमोनिया युक्त पानी में शोधन के लिए क्लोरीन मिलाया जाए, तो यह कैंसर पैदा कर सकता है.
एनजीटी ने बीते साल दिल्ली सरकार और संबंधित प्राधिकरणों से यमुना के शोधन मामले में एसटीपी, सीईटीपी के लिए ख़र्च की गई रक़म का हिसाब मांगा था. वहीं दिल्ली जल बोर्ड ने बताया था कि उसका सालाना बजट 1400 करोड़ रुपये का है. यमुना की सफ़ाई के तमाम सरकारी दावों के बावजूद यह नदी एक गंदे नाले में तब्दील हो चुकी है. कुछ ही दिनों बाद गर्मी का मौसम शुरू हो जाएगा. दिल्ली को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होगी. अगर यही हाल रहा, तो एक प्रदूषित यमुना लोगों के गले कैसे तर कर पाएगी.
नई दिल्ली. देश में सफ़ाई अभियान को लेकर शहरी विकास मंत्रालय ने देश के विभिन्न शहरों की स्वच्छता को लेकर स्वच्छता रैंकिंग की फ़ेहरिस्त जारी की है. देश के सबसे साफ़-सुथरे शहरों में कर्नाटक का मैसूर अव्वल है, जबकिश के सबसे गंदे शहरों में झारखंद का धनबाद सबसे आगे हैं. देशभर में पिछले माह किए गये प्रमुख 73 शहरों के स्वच्छता सर्वेक्षण के परिदृश्य में कर्नाटक का मैसूर शहर सबसे स्वच्छ शहर की श्रेणी पर जबकि झारखंड का धनबाद शहर सबसे निचले पायदान पर है.
शहरी विकास मंत्री एम.वैंकेया नायडू ने आज देशभर में पिछले माह किए गये प्रमुख 73 शहरों के स्वच्छता सर्वेक्षण-2016 की रिपोर्ट जारी की. इस सर्वेक्षण के लिए 10 लाख से ज़्यादा की आबादी के 53 शहरों और इससे अधिक की आबादी न रखने वाली 22 राजधानियों का चयन किया गया था. नोयडा और कोलकाता ने अगले दौर के सर्वेक्षण में शामिल होने की इच्छा जताई है. स्वच्छता और सफ़ाई के संबंध में प्रमुख 10 शहरों की श्रेणी में– मैसूर, चंडीगढ़, तिरूचनापल्ली (तमिलनाडु), नई दिल्ली नगरपालिका परिषद, विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश), सूरत और राजकोट (गुजरात) गंगटोक (सिक्किम) और पिंपरी छिंदवाड़ और ग्रेटर मुंबई (महाराष्ट्र) शामिल हैं. इस साल के सर्वेक्षण में 10 प्रमुख स्वच्छ शहरों में स्थान बनाते हुए विशाखापत्तनम (आंध्रप्रदेश), सूरत, राजकोट (गुजरात) और गंगटोक (सिक्किम) ने अपनी श्रेणियों में सुधार किया है.
निचले पायदान के 10 शहरों में कल्याण डोम्बीवली (महाराष्ट्र 64वीं श्रेणी), जमशेदपुर (झारखंड), जमशेदपुर (झारखंड), वाराणसी, गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश), रायपुर (छत्तीसगढ़), मेरठ (उत्तर प्रदेश), पटना (बिहार), र्इटानगर (अरुणाचल प्रदेश), आसनसोलन (पश्चिम बंगाल) और धनबाद (झारखंड) 73वीं श्रेणी पर हैं.
स्वच्छता के लिए पिछला सर्वेक्षण एक लाख और इससे अधिक की आबादी वाले 476 शहरों में साल 2014 में किया गया था. इस सर्वेक्षण को प्रधानमंत्री के पिछले साल अक्टूबर में शुरू किए गए स्वच्छ भारत अभियान से पूर्व किया गया था. इन शहरों के 2014 के सर्वेक्षण के परिणाम स्वच्छ भारत अभियान के घटकों जैसे शौचालयों का निर्माण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अैर व्यक्तिगत निगरानी और व्यापक मानदंडों के संबंध में उनके प्रदर्शन पर आधारित थे. इससे स्वच्छ भारत अभियान के प्रभाव के आकलन के लिए दोनों सर्वेक्षणों के परिणामों की तुलना करने में मदद मिली.
इस साल के सर्वेक्षण के परिणामों के साथ आगे भी तुलना करने के लिए 2014 में अपनी श्रेणियों में पहुंचे अंकों के आधार पर 73 शहरों के सर्वेक्षण में उनको इस बार भी श्रेणियां प्रदान की गईं. दो सर्वेक्षणों के अंकों और श्रेणियों की तुलना के आधार पर वैकेया नायडू ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान ने स्वच्छता में सुधार, नागरिकों और स्थानीय शहरी निकायों के नज़रिये में ज़मीनी स्तर पर सुधार की दिशा में बढ़ाए गये प्रयासों के संदर्भ में शहरी क्षेत्रों में सकारात्मक प्रभाव बनाया है. स्वच्छता की ओर प्रगति के मामले में शहर विभिन्न स्तरों पर हैं और एक दूसरे से बेहतर बनने की होड़ में आगे निकलने के लिए एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा जारी है. कुल मिलाकर दक्षिण और पश्चिम के शहरों ने बेहतर प्रदर्शन किया है, लेकिन देश के अन्य क्षेत्रों ख़ासतौर पर उत्तर में पारंपरिक प्रमुखों तक पहुंचने की शुरूआत कर रहे हैं. पूर्व और उत्तर के कुछ क्षेत्रों में धीमी गति पर चल रहे चिन्हित शहरों के लिए प्रयासों को बढ़ाने की ज़रूरत है. प्रमुखों के तौर पर शहरों की श्रेणीकरण, महत्वाकांक्षी प्रमुख, अपने प्रयासों को गति देने की इच्छा रखने वाले और धीमी गति से आगे बढ़ रहे शहरों के बीच एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. सर्वेक्षण के निष्कर्षों को सार्वजनिक कर देने के फलस्वरूप शहरों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि जिस चीज़ को भी मापा जाता है, उसे बाक़ायदा किया जाता है और प्रतिस्पर्धा किसी को भी बेहतर प्रयास करने के लिए प्रेरित करती है. स्वच्छ सर्वेक्षण-2016 व्यापक, प्रोफेशनल, साक्ष्य आधारित और सहभागितापूर्ण था.
उन्होंने कहा कि जिन 73 शहरों में सर्वेक्षण किया गया, उनमें से 32 शहरों की रैंकिंग में पिछले सर्वेक्षण के मुक़ाबले सुधार देखने को मिला है. इनमें उत्तर भारत के 17 शहर, पश्चिमी भारत के 6 शहर, दक्षिण भारत के 5 शहर और पूर्वी एवं पूर्वोत्तर भारत के 2-2 शहर शामिल हैं. इससे यह साबित हो जाता है कि उत्तर भारत के शहर अब साफ़-सफ़ाई के लिए कहीं ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं और शीर्ष स्वच्छ शहरों में शामिल दक्षिण एवं पश्चिमी भारत के शहरों के वर्चस्व को नये शहर चुनौती दे रहे हैं.
इन 32 शहरों में शामिल जिन शीर्ष 10 शहरों ने साल 2016 के सर्वेक्षण में अपनी रैंकिंग में काफ़ी ज़्यादा सुधार किया है, उनमें इलाहाबाद (रैंकिंग में 45 पायदानों का सुधार), नागपुर (40 पायदानों का सुधार), विशाखापत्तनम (39 पायदानों का सुधार), ग्वालियर (34 पायदानों का सुधार), भुवनेश्वर (32 पायदानों का सुधार), हैदराबाद (31 पायदानों का सुधार), गुड़गांव (29 पायदानों का सुधार), विजयवाड़ा (23 पायदानों का सुधार) और लखनऊ (23 पायदानों का सुधार) शामिल हैं.
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली में नगरपालिका निकायों के बीच नई दिल्ली नगरपालिका परिषद की रैंकिंग साल 2014 के सातवें पायदान से सुधर कर साल 2016 में चौथे पायदान पर पहुंच गई. इसी तरह दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की रैंकिंग 47वें पायदान से सुधर कर 39वें पायदान पर और उत्तरी दिल्ली नगर निगम की रैंकिंग 47वें स्थान से सुधर कर 43वें स्थान पर आ गई है, जबकि पूर्वी दिल्ली नगर निगम की रैंकिंग साल 2014 के 47वें पायदान से फिसल कर साल 2016 में 52वें पायदान पर आ गई है.
साल 2016 में जिन शीर्ष 10 शहरों की रैंकिंग काफ़ी नीचे आई है, उनमें जमशेदपुर, कोच्चि, शिलांग, चेन्नई, गुवाहाटी, आसनसोल, बेंगलुरू, रांची, कल्याण-डोम्बीवली और नासिक शामिल हैं. जहां एक ओर जमशेदपुर की रैंकिंग इस साल 53 पायदान नीचे आ गई है, वहीं नासिक की रैंकिंग 23 पायदान फिसल गई है.
अपनी रैंकिंग में बहुत ज़्यादा सुधार करने वाले शीर्ष शहरों में से चार शहर उत्तर भारत के हैं, जबकि अपनी रैंकिंग में बेहद कमी दर्शाने वाले शीर्ष 10 शहरों में से कोई भी शहर उत्तर भारत का नहीं है.
साफ़-सफ़ाई की ओर अपने प्रयासों और ज़मीनी हालत में सुधार करने के दौरान साल 2016 में कुल मिलाकर 33 शहरों की रैंकिंग पिछले सर्वेक्षण के मुक़ाबले घट गई है. सर्वेक्षण में शामिल उत्तर भारत के 28 शहरों में से 11 शहर, दक्षिण भारत के 15 शहरों में से 8 शहर, पश्चिमी भारत के 15 शहरों में से 7 शहर, पूर्वी भारत के 7 शहरों में से 5 शहर और पूर्वोत्तर क्षेत्र के 8 शहरों में से 2 शहर अपनी रैंकिंग में गिरावट दर्शाने वाले इन 33 शहरों में शामिल हैं.
स्वच्छ सर्वेक्षण-2016 के लिए अपनाए गए तरीक़ों का ज़िक्र करते हुए नायडू ने सूचित किया कि 73 शहरों के प्रयासों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए तय किए गए कुल 2,000 अंकों में से 60 फ़ीसद अंक ठोस कचरे के प्रबंधन से संबंधित पैमानों के लिए तय किए गए थे, जबकि शौचालय निर्माण के लिए 21 फ़ीसद अंक और शहर स्तरीय स्वच्छता रणनीति तथा व्यवहार परिवर्तन संबंधी संचार के लिए 5-5 फ़ीसद अंक तय किए गए थे.
यह सर्वेक्षण करने वाली भारतीय गुणवत्ता परिषद ने हर शहर में 42 स्थानों का दौरा करने के लिए 3-3 प्रशिक्षित सर्वेक्षकों की 25 टीमें तैनात की थीं, जिन्होंने प्रमुख क्षेत्रों जैसे कि रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों, धार्मिक स्थलों, प्रमुख बाज़ार स्थलों, झुग्गियों एवं शौचालय परिसरों समेत नियोजित एवं ग़ैर-नियोजित आवासीय क्षेत्रों को कवर किया. सर्वेक्षण में शामिल टीमों ने साक्ष्य के तौर पर अपने दौरे वाले स्थानों की भौगोलिक जानकारी संबंधी कुल 3,066 तस्वीरें लीं और उन्हें वेबसाइट पर अपलोड किया गया.
उन्होंने कहा कि सभी 73 शहरों को अग्रिम तौर पर काफ़ी पहले ही विस्तृत रूप से जानकारी दे दी गई थी, ताकि साफ़-सफ़ाई में बेहतरी के साथ-साथ सर्वेक्षण वाली टीमों द्वारा सत्यापन के लिए अपने प्रयासों के दस्तावेई प्रमाण पेश किए जा सकें. एक लाख से भी ज़्यादा नागरिकों ने संबंधित शहरों में साफ़-सफ़ाई पर अपने फ़ीडबैक पेश किए, जिससे साल 2016 में किया गया सर्वेक्षण साक्ष्य आधारित और सहभागितापूर्ण साबित हुआ है.
अम्बरीश कुमार
उत्तर प्रदेश में बहराइच जिले के कतरनिया घाट से करीब दस कोस दूर एक नदी है, जो नेपाल से आती है- गेरुआ. आगे जाकर यह नेपाल से ही आई एक अन्य नदी कौडियाला से मिलकर दो धाराओं में बंट जाती है. बाद में ये घाघरा के नाम से जानी जाती हैं और कुछ दूरी तक इसका पानी बहुत साफ भी रहता है.
इसी से कुछ दूरी पर सरयू नदी भी है. इन दोनों नदियों का पानी इस अंचल में बहुत साफ नजर आता है. खासकर गेरुआ नदी का पानी. बहुत से लोगों को इस बात पर हैरत हो सकती है कि इस नदी के उद्गम के आसपास अब भी नदी का पानी लोग सीधे पीते हैं. जरवल रोड के करीब घाघरा घाट पर इस नदी का करीब एक किलोमीटर चौड़ा पाट इसका असली रूप भी दिखाता है. यहां तक यह नदी बहुत स्वच्छ नजर आती है. इसका पानी चूंकि पेट की बीमारियों के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है, इसलिए लोग सीधे इसे पीते हैं.
अपने उद्गम स्थल से लेकर आगे तक गेरुआ नदी सिर्फ जंगल के बीच से गुजरती है और किसी भी शहर से इसका कोई वास्ता नहीं पड़ता. यही वजह है कि इस नदी में किसी शहर का कोई नाला नहीं गिरता, और वनक्षेत्र से गुजरने की वजह से बहुत-सी जड़ी बूटियां इसके पानी में गिरकर इसे और समृद्ध करती है. एक गौर करने वाली बात यह भी है कि इस नदी में मछली के शिकार पर रोक है, क्योंकि इसमें बड़ी संख्या में मगरमच्छ और घडि़याल रहते है. वन्य जीव अभयारण्य के बीच से निकलने की वजह से इस पर अभयारण्य के नियम-कायदे भी लागू हैं. इस नदी में डॉल्फिन से लेकर रोहू, टेंगन, भाकुर और महाशीर जैसी मछलियां पाई जाती हैं, जिनका शिकार घडि़याल और मगरमच्छ से लेकर बड़े परिंदे करते हैं. नदी का पानी पारदर्शी है और ऊपर से देखने पर हरा नजर आता है. इसकी स्वच्छता का आलम यह है कि इसे नाव से पार करने वाले लोग बोतल में इसका पानी भरकर पीते हैं.
नदी से कुछ किलोमीटर बाद ही नेपाल का बर्दिया जिला शुरू हो जाता है. इसलिए नदी पर आवाजाही बनी रहती है. हर कोई इस नदी को देखकर देश की दूसरी नदियों से तुलना करना नहीं भूलता. जैसे, लखनऊ से गुजरने वाली गोमती नदी का पानी बुरी तरह जहरीला हो चुका है और इसे लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भी कई बार चेतावनी दे चुका है. बावजूद इसके सीतापुर में चीनी मिलों का जहरीला कचरा इसमें डाला जा रहा है, तो बाराबंकी में बूचड़खानों का कचरा इसमें मिलता है.
ऐसे में, करीब 150 किलोमीटर दूर गेरुआ नदी को देखने से एक असली नदी की कल्पना की जा सकती है. जाहिर है, जो भी नदी किसी शहर से बची रही, वह आज भी जिंदा है. देश में दूसरा उदाहरण चंबल नदी का है, जिसका पानी आज भी साफ है. गौर से देखें, तो यह कहानी दरअसल नदियों की नहीं है, बल्कि उन तमाम शहरों की है, जो अपने आसपास से गुजरने वाली नदियों को जिंदा रहने लायक नहीं छोड़ते.
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)
लाल बिहारी लाल
दिल्ली. आज दिल्ली विश्व में टोकियो के बाद सर्वाधिक प्रदूषित शहर है. सन 2014 में टोकियो की आबादी 3.80 करोड़ थी, जबकि दिल्ली की 2.5 करोड़ आबादी थी. बढ़ती हुई आबादी के दर को देख के कहा जा सकता है कि सन 2030 तक दिल्ली दूसरे नंबर पर ही प्रदूशित शहरों की श्रेणी में रहेगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन(WHO) एंव यूरोपियन यूनियन ने पी.एम. 2.5 प्रदूषण का स्तर प्रतिघन मीटर 25 माइक्रोग्राम निर्धारित किया है, जबकि अमेरिका इससे भी कड़ा यह स्तर
12 माइक्रोग्राम निर्धारित किया है. दिल्ली में यह स्तर सामान्यतः 317 है कभी कभार इससे ज्यादा भी हो जाता है. यह स्तर अमेरिका से लगभग 30 गुना और विश्व स्वास्थ्य संगठन के तय मानको से 15 गुना ज्यादा है. इससे कैंसर,दिल की
बीमारियां, अस्थमा एवं अन्य घातक बिमारियां होने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है. भारी यातायात,स्थानीय उद्योग,थर्मल पावर प्लांट एवं झूग्गियों में कोयले पर खाना बनाना दिल्ली में वायू प्रदूषण के स्तर को बढ़ाने में काफी योगदान करते है. अतः दिल्ली की जनता प्रदूषण से काफी बेहाल है. आज जरूरत है कि इससे निजात
के लिए कुछ किया जाए.
भारत की भूमी दुनिया के 2.4 प्रतिशत जबकि आबादी लगभग 18 प्रतिशत है. इस तरह प्रति ब्यक्ति संसाधनों पर अन्य देशों की वनिस्पत काफी दबाव है, जिससे तेजी से शहरीकरण एवं औद्योदिकरण हो रहा है. सन 1947 में वर्ष 2002
तक पानी की उपलब्धता 70 प्रतिशत घटकर 1822 घनमीटर प्रति व्यक्ति रह गया है. अगर इसी तरह संसाधनों का दोहन तेजी से होता रहा तो मावव जल के बिना मछली की तरह तड़प-तड़प कर जान दे देगा. भारत में वनों का औसत भौगोलिक
क्षेत्रफल 18.34 प्रतिशत है, जो कि 33 प्रतिशत के मनदंड से काफी कम है. इसमें भी 50 प्रतिशत म.प्र.(20.7) और पूर्वोत्तर के राज्यो में (25.7) प्रतिशत है बाकी के राज्य वन के मामले में काफी निर्धन है. वन की कमी से जलवायु परिवर्तन हो
रहा है. अभी तामिलनाड्ड़ू जल गांडव से ग्रस्त है.
प्रदूषण के मामले में केन्द्र एवं राज्य सरकारें नियम तो बना रखा है पर इस पर सख्ती से अमल नहीं हो पाता है. यही कारण है की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का ग्राफ काफी तेजी से बढ़ा है। यहा पर सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था काफी लचर
है. आम आदमी की नई सरकार बनी थी तो लोगो ने सोचा की काफी सुधार होगा पर यह सरकार पिछली सरकार से भी फिसड्डी साबित हुई। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायधीश जस्टीश टी.एस. ठाकुर के फटकार पर दिल्ली सरकार ने फौरी तौर पर
गाड़ियो के ओड एंव इभेन नंबर एक-एक दिन चलाने के प्रस्ताव पर बिचार कर रही है, पर यह स्थायी समाधान नही हो सकता है. इसलिए जरूरी है कि दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए और नियमों पर सख्ती से
अमल हो तथा लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जाए. जब राजनीतिज्ञों को वोट की राजनीति से बाहर आकर ही देशहित एवं समाजहित में कुछ किया जाए, तभी देशवासियो एवं दिल्ली वासियों का भला हो सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिसंबर 2015 को केन्द्र एवं राच्य सरकार को सुझाव के साथ तलब किया है. देखें जनप्रतिनिधि जनता के हितों की रक्षा के लिए क्या ठोस कदम उठाते हैं.
(लेखक-पर्यावरणप्रेमी और लाल कला मंच के सचिव हैं)
कल्पना
पालखीवाला
देखने
में सर्वत्र परिचित, सर्वव्यापी एवं कभी ज्यादा संख्या में दिखाई पड़ने वाली घरेलू गौरैया,
अब एक रहस्यमय पक्षी बन गई है और पूरे विश्व में तेजी से दुर्लभ होती जा रही है. फुर्तीली
और चहलकदमी करने वाली घरेलू गौरैया को हमेशा शरदकालीन एवं शीतकालीन फसलों के दौरान,
खेत-खलिहानों में अनेक छोटे-छोटे पक्षियों के साथ फुदकते देखा गया है, लेकिन अब तो
कई सप्ताह इन्हें बिना देखे ही निकल जाते हैं. कई बड़े शहरों से तो ये गायब ही हो गई
हैं, लेकिन छोटे शहरों और गांवों में अभी भी इन्हें देखा जा सकता है.
पिछले
कुछ वर्षों में, भारत के साथ-साथ विश्व के मानचित्र पर भी गौरैया की संख्या में भारी
कमी देखी गई है. यूरोप के बड़े हिस्से में कभी सामान्य रूप से दिखाई पड़ने वाली इन चिड़ियों
की संख्या अब घट रही है. नीदरलैंड में तो घरेलू गौरैया को अब दुलर्भ प्रजाति के वर्ग
में रखा जाता है. नीदरलैंड में इनकी घटती संख्या के कारण इन्हें रेड लिस्ट में रखा
गया है. इसकी आबादी में ऐसी ही कमी ब्रिटेन में भी दर्ज की गई है. फ्रांसीसी पक्षीविज्ञानी
ने पेरिस एवं अन्य शहरों में गौरैया की संख्या में तेजी से गिरावट की रूप रेखा तैयार
की है. इससे ज्यादा गिरावट जर्मनी, चेक गणराज्य, बैल्जियम, इटली तथा फिनलैंड के शहरी
इलाकों में देखी गई.
इतिहास
ऐसा
समझा जाता है कि भूमध्य क्षेत्र घरेलू गौरैया का उद्गम स्थल है और सभ्यता के विकास
के साथ-साथ यह यूरोप भर में पहुंच गई. मानव संपर्क में रहने की अपनी विशेषता के कारण
गौरैया ने अटलांटिक से लेकर अमेरिका तक का सफर कर डाला. 1850 में, ग्रीन ईंच वर्म नामक
कीट न्यूयार्क के सेंट्रल पार्क में पौधों को नुकसान पहुंचा रहे थे. चूंकि ब्रिटेन
में घरेलू गौरैया का प्रमुख भोजन ग्रीन वर्म ही हैं, ऐसा विचार किया गया कि अगर गौरैया
को न्यूयार्क सिटी लाया गया तो सैंट्रल पार्क की कीट समस्या हल हो जाएगी. कुछ लोगों
ने यह भी सोचा कि गौरैया फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों को भी समाप्त करने में
सहायक होगी.
गौरैया
से प्रथम परिचय 1851 में अमेरिका के ब्रुकलिन इंस्टीटयूट ने कराया था. गौरैया की आठ
जोड़ियों को आरंभ में यहां से छोड़ा गया, लेकिन इनमें से कोई भी जलवायु परिवर्तन के कारण
बच नहीं पाई, लेकिन बार-बार के प्रयासों से अंतत: चिड़िया ने अपने को ठंडे मौसम के अनुकूल
बना लिया और इनकी संख्या बढ़ने लगी. घोड़ों को खिलाने के लिए बिखेरे गए दाने तथा लोगों
द्वारा तैयार किए गए कृत्रिम घोंसले गौरैया के लिए काफी समय तक मददगार साबित हुए. गौरेयों
ने लोगों का विश्व के कई हिस्सों में जैसे - उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका,
आस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड तक सफलतापूर्वक पीछा किया.
भोजन
घरेलू
गौरैया एक बुध्दिमान चिड़िया है, जिसने घोंसला स्थल, भोजन तथा आश्रय परिस्थितियों में
अपने को उनके अनुकूल बनाया है जैसे. अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण यह विश्व में सबसे
ज्यादा पाई जाने वाली चहचहाती चिड़िया बन गई.
गौरैया
बहुत ही सामाजिक पक्षी है और ज्यादातर पूरे वर्ष झुंड में उड़ती है. एक झुंड 1.5-2 मील
की दूरी तय करता है, लेकिन अगर भोजन तलाश करने की बात हो, तो यह ज्यादा दूरी भी तय
कर सकती है. गौरैया का प्रमुख आहार अनाज के दाने, जमीन में बिखरे दाने तथा पशु आहार
है. अगर अनाज उपलब्ध न हो तो यह अन्य आहार से भी अपना पेट भर लेती है. ऐसे में ये खर-पतवार
तथा खासकर प्रजनन मौसम के दौरान कीटों को भी खा लेती है. घरेलू गौरैया की परजीवी प्रकृति
साफ देखी जा सकती है, क्योंकि ये घरों से बाहर फेंके गए कूड़े करकट में भी अपना आहार
ढूंढ लेती है. बसंत के मौसम में, फूलों की (खासकर पीले रंग के) क्रोकूसेस, प्राइमरोजेस
तथा एकोनाइट्ज फूलों की प्रजातियां घरेलू गौरैया को ज्यादा आकर्षित करती हैं. ये तितलियों
का भी शिकार करती हैं.
आवास
घरेलू
गौरैया साधारणत: भवनों की ओर आराम करने, घोंसला बनाने तथा आश्रय खोजने के लिए आकर्षित
होती है. ये अपना घोंसला बनाने के लिए मानव-निर्मित एकांत स्थानों या दरारों को तलाश
करती हैं. घोंसला बनाने के लिए इनके अन्य स्थल हैं अलगनी का खुला हुआ किनारा, बरामदा,
बगीचा इत्यादि. गौरैया अपना घर मानव आवास के निकट ही बनाती हैं.
वर्गीकरण
घरेलू
गौरैया विश्व के पुराने गौरैया परिवार पासेराडेई की सदस्य है. कुछ लोग इसे वीवर फिंच
परिवार से संबंधित मानते हैं. इनकी कई भौगोलिक प्रजातियों का नामकरण हुआ है और उन्हें
आकार एवं रंग के आधार पर अलग किया गया है. पश्चिमी प्रदेशों में इनका रंग धूसर एवं
पूर्वी इलाकों में ये सफेद रंगों में मिलती हैं. नर गौरैया को उसके सीने के रंग से
पहचाना जा सकता है. पश्चिमी गोलार्ध की चिड़िया उष्णकटिबंधी दक्षिण एशियाई चिड़िया की
तुलना में बड़ी होती है.
भारत
के, हिन्दी भाषी क्षेत्रों में यह गौरैया के नाम से लोकप्रिय है. तमिलनाडु तथा केरल
में यह कूरूवी के नाम से जानी जाती है. तेलगू भाषा में इसे पिच्चूका कहते हैं. कन्नड़
भाषा में गुब्बाच्ची तथा गुजरात के लोग इसे चकली कहते हैं. मराठी इसे चिमानी बुलाते
हैं. पंजाब में इसे चिड़ी के नाम से जाना जाता है, जम्मू तथा कश्मीर में चेर, पश्चिम
बंगाल में चराई पाखी तथा ओड़िशा में घरचटिया कहते हैं. उर्दू भाषा में इसे चिड़िया तथा
सिंधी भाषा में इसे झिरकी कहा जाता है.
रूप-रेखा
यह
14 से 16 से.मी. लम्बी चिड़िया है जिसके पंख का फैलाव 19-25 से.मी. होता है. यह एक छोटी,
चहचहाने वाली चिड़िया है जिसका वजन 26 से 32 ग्राम होता है. नर गौरैया का सिर, गाल तथा
अंदर का भाग धूसर होता है तथा गला, सीने के ऊपर, चोंच एवं आंखों के बीच का भाग काला
होता है. गर्मी में इनकी चोंच का रंग नीला-काला तथा पैर भूरे रंग का हो जाता है. सर्दी
में पक्षति का रंग मंदा होकर फीका पीला हो जाता है तथा चोंच पीले भूरे रंग की. मादा
के सिर या गले पर काला रंग नहीं होता और सिर के ऊपर भूरे रंग की धारी होती है. गौरैया
की सामान्य पहचान उस छोटी सी चंचल प्रकृति की चिड़िया से है जो हल्के धातु रंग की होती
है तथा चीं चीं करती हुई यहां से वहां फुदकती रहती है. छोटी होते हुए भी यह चिड़िया
लम्बी उड़ान भरती है . इसके एक त्रऽतु में कम से कम तीन बच्चे होते हैं.
प्रजनन
इनके
घोंसले भवनों की सूराखों या चट्टानों में, घर या नदी के किनारे, समुद्र तट या झाड़ियों
में, आलों या प्रवेश द्वारों जैसे विभिन्न स्थानों पर होते हैं. इनके घोंसले घास के
तिनकों से बने होते हैं और इनमें पंख भरे होते हैं.
घरेलू
गौरैया अन्य चिड़ियों के घोंसले हड़पने में भी बहुत आक्रामक होती है. गौरैया ज्यादातर
किसी दूसरी चिड़िया द्वारा तैयार किए गए घोंसले को जबरदस्ती हड़प जाती हैं या कभी-कभी
इस्तेमाल हो रहे घोंसले के ऊपर ही अपना घोंसला बना लेती हैं. इनके अंडे अलग-अलग आकार
और पहचान के होते हैं. अंडे को मादा गौरैया सेती है. गौरैया की अंडा सेने की अवधि
10-12 दिनों की होती है जो सभी चिड़ियों की अंडे सेने की अवधि में सबसे छोटी है. इसकी
प्रजनन सफलता उम्र के साथ बढ़ती है और यह प्रजनन समय में परिवर्तन लाती है, बड़ी चिड़िया
ऋतु से पहले अंडा देती है.
कमी
का कारण
गौरैया
की संख्या में आकस्मिक कमी के विभिन्न कारण हैं, जिनमें से सबसे चौकाने वाला कारण है
सीसा रहित पेट्रोल का उपयोग, जिसके जलने पर मिथाइल नाइट्रेट नामक यौगिक तैयार होता
है. यह यौगिक छोटे जन्तुओं के लिए काफी जहरीला है. अन्य कारण हैं पनपते खर-पतवार की
कमी या गौरैया को खुला आमंत्रण देने वाले ऐसे खुले भवनों की कमी जहां वह अपने घोंसले
बनाया करती थी. पक्षीविज्ञानी एवं वन्यप्राणी विशेषज्ञों का यह मानना है कि आधुनिक
युग में पक्के मकान, लुप्त होते बाग-बगीचे, खेतों में कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग तथा
भोज्य-पदार्थ स्त्रोतों की उपलब्धता में कमी इत्यादि प्रमुख विभिन्न कारक हैं जो इनकी
घटती आबादी के लिए जिम्मेवार हैं.
भारतीय
कुलंग एवं आर्दभूमि कार्यसमूह के केएस गोपी सुन्दर ने कहा कि यह सच है कि पिछले कुछ
सालों से घरेलू चिड़िया की संख्या में कमी जरूर आ रही है. इसके लिए उन्होंने अनेक कारण
बताये हैं. किसानों द्वारा फसलों पर कीटनाशकों के छिड़काव के कारण कीट मर जाते हैं जिनके
ऊपर ये निर्भर हैं. कोयंबटूर स्थित सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक विज्ञान केन्द्र
के डा. वीएस विजयन के अनुसार यद्यपि अभी पृथ्वी के दो-तिहाई हिस्से की उड़ने वाली प्राजतियों
का पता लगाया जाना बाकी है, फिर भी ये बड़ी ही विडंबना है की बात है कि जो प्रजाति कभी
बहुलता में यहां थी, कम हो रही है. जीवनशैली तथा इमारतों के आधुनिक रूप से आये परिवर्तन
ने पक्षियों के आवासों तथा खाद्य स्रोतों को बर्बाद कर दिया है . खत्म होते बगीचे भी
इसके लिए जिम्मेदार हैं.
आज
के घर के बाहर चिड़ियों का झाडियों की डाली पर उछलना और उनका चहचहाना किसी को शायद ही
दिखाई पड़ता है. हम महादेवी वर्मा की कहानी गौरेया को याद कर सकते हैं जिसमें गौरया
उनके हाथ से दाना खाती है, उनके कंधों पर उछलती फिरती है और उनके साथ लुक्का-छिप्पी
खेलती है. आज हर कोई चाहता है कि गौरेया महादेवी वर्मा की कहानी में सिमटकर न रह जाए
बल्कि वह एक बार फिर हमारे शहरों में पहले की तरह वापस आ जाए.