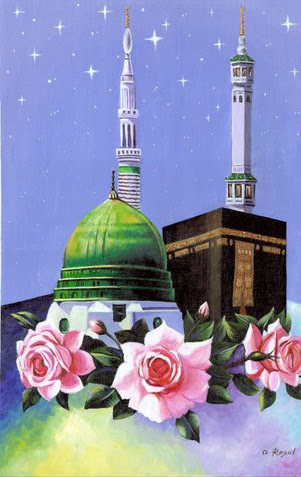अच्छा इंसान
-
अच्छा इंसान बनना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी. एक
अच्छा इंसान ही दुनिया को रहने लायक़ बनाता है. अच्छे इंसानों की वजह से ही
दुनिय...
Showing posts with label पर्यटन. Show all posts
Showing posts with label पर्यटन. Show all posts
फ़िरदौस ख़ास
पर्यटन भी ज़िन्दगी का एक अहम हिस्सा है. कुछ लोग क़ुदरत की ख़ूबसूरती निहारने के लिए दूर-दराज़ के इलाक़ों में जाते हैं, तो कुछ लोगों को अक़ीदत इबादतगाहों और मज़ारों तक ले जाती है. पर्यटन रोज़गार का भी एक बड़ा साधन है. हमारे देश भारत में लाखों लोग पर्यटन से जुड़े हैं. यहां मज़हबी पर्यटन ख़ूब फल-फूल रहा है. हर साल विदेशों से लाखों लोग भारत भ्रमण के लिए आते हैं, जिनमें एक बड़ी तादाद धार्मिक स्थलों पर आने वाले ज़ायरीनों यानी पर्यटकों की होती है.
देश की राजधानी दिल्ली में जामा मस्जिद पर्यटकों का पसंदीदा स्थल है. यह मस्जिद लाल पत्थरों और संगमरमर से बनी हुई है. मुग़ल बादशाह शाहजहां ने इसे बनवाया था. इसके ख़ूबसूरत गुम्बद, शानदार मीनारें और हवादार झरोखे इसे बहुत ही दिलकश बनाते हैं. मस्जिद में उत्तर और दक्षिण के दरवाज़ों से दाख़िल हुआ जा सकता है. पूर्व का दरवाज़ा सिर्फ़ जुमे के दिन ही खुलता है. यह दरवाज़ा शाही परिवार के दाख़िले के लिए हुआ करता था.
इसके अलावा ज़ायरीन दिल्ली में दरगाहों पर भी हाज़िरी लगाते हैं. यहां बहुत सी दरगाहें अक़ीदत का मर्कज़ हैं, ख़ासकर सूफ़ियाना सिलसिले से जुड़े लोग यहां अपनी अक़ीदत के फूल चढ़ाते हैं. यहां महबूबे-इलाही हज़रत शेख़ निजामुद्दीन औलिया और उनके प्यारे मुरीद हज़रत अमीर खुसरो साहब की मज़ारें हैं. ज़ायरीन हज़रत ख़्वाजा क़ुतुबुद्दीन बख़्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत ख़्वाजा अब्दुल अज़ीज़ बिस्तामी, हज़रत ख़्वाजा बाक़ी बिल्लाह, हज़रत ख़्वाजा अलीअहमद एहरारी, हज़रत सैयद बदरुद्दीन शाह समरकंदी, हज़रत सैयद महमूद बहार, हज़रत सैयद सदरुद्दीन शाह, हज़रत सैयद आरिफ़ अली शाह, हज़रत सैयद अबुल कासिम सब्ज़वारी, हज़रत सैयद हसन रसूलनुमा, हज़रत सैयद शाह आलम, हज़रत मौलाना शेख़ जमाली और कमाली, हज़रत मौलाना फ़ख़रुद्दीन फ़ख़्र-ए-जहां, हज़रत मौलाना शेख़ मजदुद्दीन हाजी, हज़रत मौलाना नासेहुद्दीन, हज़रत शम्सुल आरफ़ीन तुर्कमान शाह, हज़रत शाह तुर्कमान बयाबानी सुहरवर्दी, हज़रत शाह सरमद शहीद, हज़रत शाह सादुल्लाह गुलशन, हज़रत शाह वलीउल्लाह, हज़रत शाह मुहम्मद आफ़ाक़, हज़रत शाह साबिर अली चिश्ती साबरी, हज़रत शेख़ सैयद जलालुद्दीन चिश्ती, हज़रत शेख़ कबीरुद्दीन औलिया, हज़रत शेख़ जैनुद्दीन अली, हज़रत शेख़ यूसुफ़ कत्ताल, हज़रत शेख़ नसीरुद्दीन महमूद चिराग़-ए-देहली, ख़लीफ़ा शेख़ चिराग़-ए-देहली, हज़रत शेख़ नजीबुद्दीन मुतवक्किल चिश्ती, हज़रत शेख़ नूरुद्दीन मलिक यारे-पर्रा, हज़रत शेख़ शम्सुद्दीन औता दुल्लाह, हज़रत शेख़ शहाबुद्दीन आशिक़उल्लाह, हज़रत शेख़ ज़ियाउद्दीन रूमी सुहरवर्दी, हज़रत मख़मूद शेख़ समाउद्दीन सुहरवर्दी, हज़रत शेख़ नजीबुद्दीन फ़िरदौसी, हज़रत शेख़ रुकनुद्दीन फ़िरदौसी, हज़रत शेख़ एमादुद्दीन इस्माईल फ़िरदौसी, हज़रत शेख़ उस्मान सय्याह, हज़रत शेख़ सलाहुद्दीन, हज़रत शेख़ अल्लामा कमालुद्दीन, हज़रत शेख़ बाबा फ़रीद (पोते), हज़रत शेख़ अलाउद्दीन, हज़रत शेख़ फ़रीदुद्दीन बुख़ारी, हज़रत शेख़ अब्दुलहक़ मुहद्दिस देहलवी, हज़रत शेख़ सुलेमान देहलवी, हज़रत शेख़ मुहम्मद चिश्ती साबरी, हज़रत मिर्ज़ा अब्दुल क़ादिर बेदिल, हज़रत शेख़ नूर मुहम्मद बदायूंनी, हज़रत शेख़ शाह कलीमुल्लाह, हज़रत शेख़ मुहम्मद फ़रहाद, हज़रत शेख़ मीर मुहम्मदी, हज़रत शेख़ हैदर, हज़रत क़ाज़ी शेख़ हमीदुद्दीन नागौरी, हज़रत अबूबकर तूसी हैदरी, हज़रत नासिरुद्दीन महमूद, हज़रत इमाम ज़ामिन, हज़रत हाफ़िज़ सादुल्लाह नक़्शबंदी, हज़रत शेख़ुल आलेमीन हाजी अताउल्लाह, हज़रत मिर्ज़ा मुल्लाह मज़हर जाने-जानां, हज़रत मीरानशाह नानू और शाह जलाल, हज़रत अब्दुस्सलाम फ़रीदी, हज़रत ख़ुदानुमा, हज़रत नूरनुमा और हज़रत मख़दूम रहमतुल्लाह अलैह की मज़ारों पर भी जाते हैं. यहां हज़रत बीबी हंबल साहिबा, हज़रत बीबी फ़ातिमा साम और हज़रत बीबी ज़ुलैख़ा की मज़ारें भी हैं, जहां महिला ज़ायरीन जाती हैं. यहां पंजा शरीफ़, शाहेमर्दां, क़दम शरीफ़ और चिल्लागाह पर भी ज़ायरीन हाज़िरी लगाते हैं.
यूं तो हर रोज़ ही मज़ारों पर ज़ायरीनों की भीड़ होती है, लेकिन जुमेरात के दिन यहां का माहौल कुछ अलग ही होता है. क़व्वाल क़व्वालियां गाते हैं. दरगाह के अहाते में अगरबत्तियों की भीनी-भीनी महक और उनका आसमान की तरफ़ उठता सफ़ेद धुआं कितना भला लगता है. ज़ायरीनों के हाथों में फूलों और तबर्रुक की तबाक़ होते हैं. मज़ारों के चारों तरफ़ बनी जालियों के पास बैठी औरतें क़ुरान शरीफ़ की सूरतें पढ़ रही होती हैं. कोई औरत जालियों में मन्नत के धागे बांध रही होती है, तो कोई दुआएं मांग रही होती है.
राजस्थान के अजमेर में ख़्वाजा मोईनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्ला अलैह का मज़ार है. ख़्वाजा अल्लाह के रसूल हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलादों में से हैं. ख़्वाजा की वजह से अजमेर को अजमेर शरीफ़ भी कहा जाता है. सूफ़ीवाद का चिश्तिया तरीक़ा हज़रत अबू इसहाक़ शामी ने ईरान के शहर चश्त में शुरू किया था. इसलिए इस तरीक़े या सिलसिले का नाम चिश्तिया पड़ गया. जब ख़्वाजा मोईनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्ला अलैह हिन्दुस्तान आए, तो उन्होंने इसे दूर-दूर तक फैला दिया. हिन्दुस्तान के अलावा पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी चिश्तिया सिलसिला ख़ूब फलफूल रहा है. दरअसल यह सिलसिला भी दूसरे सिलसिलों की तरह ही दुनियाभर में फैला हुआ है. यहां भी दुनियाभर से ज़ायरीन आते हैं.
महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में सैयद हाजी अली शाह बुख़ारी का मज़ार है. हाजी अली भी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलादों में से हैं. यह मज़ार मुम्बई के वर्ली तट के क़रीब एक टापू पर बनी मस्जिद के अन्दर है. सफ़ेद रंग की यह मस्जिद बहुत ही ख़ूबसूरत लगती है. मुख्य सड़क से मज़ार तक जाने के लिए एक पुल बना हुआ है. इसके दोनों तरफ़ समन्दर है. शाम के वक़्त समन्दर का पानी ऊपर आने लगता है और यह पुल पानी में डूब जाता है. सुबह होते ही पानी उतरने लगता है. यहां भी हिन्दुस्तान के कोने-कोने के अलावा दुनियाभर से ज़ायरीन आते हैं.
हरियाणा के पानीपत शहर में शेख़ शराफ़ुद्दीन बू अली क़लंदर का मज़ार है. यह मज़ार एक मक़बरे के अन्दर है, जो साढ़े सात सौ साल से भी ज़्यादा पुराना है. कहा जाता है कि शेख़ शराफ़ुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने लम्बे अरसे तक पानी में खड़े होकर इबादत की थी. जब उनकी इबादत क़ुबूल हुई, तो उन्हें बू अली का ख़िताब मिला. दुनिया में अब तक सिर्फ़ साढ़े तीन क़लन्दर हुए हैं. शेख़ शराफ़ुद्दीन बू अली क़लंदर, लाल शाहबाज़ क़लंदर और शम्स अली कलंदर. हज़रत राबिया बसरी भी क़लंदर हैं, लेकिन औरत होने की वजह से उन्हें आधा क़लंदर माना जाता है. बू अली क़लंदर रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के क़रीब ही उनके मुरीद हज़रत मुबारक अली शाह का भी मज़ार है. यहां भी दूर-दूर से ज़ायरीन आते हैं.
उत्तर प्रदेश के बाराबंकी ज़िले के देवा नामक क़स्बे में हाजी वारिस अली शाह का मज़ार है. आप अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलादों में से हैं. उनके वालिद क़ुर्बान अल्ली शाह भी जाने-माने औलिया थे.
उत्तर प्रदेश के ही कानपुर ज़िले के गांव मकनपुर में हज़रत बदीउद्दीन शाह ज़िन्दा क़ुतबुल मदार का मज़ार है.
इनके बारे में कहा जाता है कि ये योगी दुर्वेश थे और अकसर योग के ज़रिये महीनों साधना में रहते थे. एक बार वह योग समाधि में ऐसे लीन हुए कि लम्बे अरसे से तक उठे नहीं. उनके मुरीदों ने समझा कि उनका विसाल हो गया है. उन्होंने हज़रत बदीउद्दीन शाह को दफ़न कर दिया. दफ़न होने के बाद उन्होंने सांस ली. उनके मुरीद यह देखकर हैरान रह गए कि वे ज़िन्दा हैं. वे क़ब्र खोदकर उन्हें निकालने वाले ही थे, तभी एक बुज़ुर्ग ने हज़रत बदीउद्दीन शाह से मुख़ातिब होकर कहा कि दम न मार यानी अब तुम ज़िन्दा ही दफ़न हो जाओ. फिर उस क़ब्र को ऐसे ही छोड़ दिया गया. इसलिए उन्हें ज़िन्दा पीर भी कहा जाता है. आपकी उम्र मुबारक तक़रीबन छह सौ साल थी.
इनके अलावा देशभर में और भी औलियाओं की मज़ारें हैं, जहां दूर-दराज़ के इलाक़ों से ज़ायरीन आते हैं और सुकून हासिल करते हैं.
(लेखिका स्टार न्यूज़ एजेंसी में सम्पादक हैं)
ये कहानी है दिल्ली के ’शहज़ादे’ और हिसार की ’शहज़ादी’ की. उनकी मुहब्बत की... गूजरी महल की तामीर का तसव्वुर सुलतान फ़िरोज़शाह तुगलक़ ने अपनी महबूबा के रहने के लिए किया था...यह किसी भी महबूब का अपनी महबूबा को परिस्तान में बसाने का ख़्वाब ही हो सकता था और जब गूजरी महल की तामीर की गई होगी...तब इसकी बनावट, इसकी नक्क़ाशी और इसकी ख़ूबसूरती को देखकर ख़ुद वह भी इस पर मोहित हुए बिना न रह सका होगा...
हरियाणा के हिसार क़िले में स्थित गूजरी महल आज भी सुल्तान फ़िरोज़शाह तुग़लक और गूजरी की अमर प्रेमकथा की गवाही दे रहा है. गूजरी महल भले ही आगरा के ताजमहल जैसी भव्य इमारत न हो, लेकिन दोनों की पृष्ठभूमि प्रेम पर आधारित है. ताजमहल मुग़ल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ की याद में 1631 में बनवाना शुरू किया था, जो 22 साल बाद बनकर तैयार हो सका. हिसार का गूजरी महल 1354 में फ़िरोज़शाह तुग़लक ने अपनी प्रेमिका गूजरी के प्रेम में बनवाना शुरू किया, जो महज़ दो साल में बनकर तैयार हो गया. गूजरी महल में काला पत्थर इस्तेमाल किया गया है, जबकि ताजमहल बेशक़ीमती सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया है. इन दोनों ऐतिहासिक इमारतों में एक और बड़ी असमानता यह है कि ताजमहल शाहजहां ने मुमताज़ की याद में बनवाया था. ताज एक मक़बरा है, जबकि गूजरी महल फिरोज़शाह तुग़लक ने गूजरी के रहने के लिए बनवाया था, जो महल ही है.
गूजरी महल की स्थापना के लिए बादशाह फ़िरोज़शाह तुग़लक ने क़िला बनवाया. यमुना नदी से हिसार तक नहर लाया और एक नगर बसाया. क़िले में आज भी दीवान-ए-आम, बारादरी और गूजरी महल मौजूद हैं. दीवान-ए-आम के पूर्वी हिस्से में स्थित कोठी फ़िरोज़शाह तुग़लक का महल बताई जाती है. इस इमारत का निचला हिस्सा अब भी महल-सा दिखता है. फ़िरोज़शाह तुग़लक के महल की बंगल में लाट की मस्जिद है. अस्सी फ़ीट लंबे और 29 फ़ीट चौड़े इस दीवान-ए-आम में सुल्तान कचहरी लगाता था. गूजरी महल के खंडहर इस बात की निशानदेही करते हैं कि कभी यह विशाल और भव्य इमारत रही होगी.
सुल्तान फ़िरोज़शाह तुग़लक और गूजरी की प्रेमगाथा बड़ी रोचक है. हिसार जनपद के ग्रामीण इस प्रेमकथा को इकतारे पर सुनते नहीं थकते. यह प्रेम कहानी लोकगीतों में मुखरित हुई है. फ़िरोज़शाह तुग़लक दिल्ली का सम्राट बनने से पहले शहज़ादा फ़िरोज़ मलिक के नाम से जाने जाते थे. शहज़ादा अकसर हिसार इलाक़े के जंगल में शिकार खेलने आते थे. उस वक़्त यहां गूजर जाति के लोग रहते थे. दुधारू पशु पालन ही उनका मुख्य व्यवसाय था. उस काल में हिसार क्षेत्र की भूमि रेतीली और ऊबड़-खाबड़ थी. चारों तरफ़ घना जंगल था. गूजरों की कच्ची बस्ती के समीप पीर का डेरा था. आने-जाने वाले यात्री और भूले-भटके मुसाफ़िरों की यह शरणस्थली थी. इस डेरे पर एक गूजरी दूध देने आती थी. डेरे के कुएं से ही आबादी के लोग पानी लेते थे. डेरा इस आबादी का सांस्कृतिक केंद्र था.
एक दिन शहज़ादा फ़िरोज़ शिकार खेलते-खेलते अपने घोड़े के साथ यहां आ पहुंचा. उसने गूजर कन्या को डेरे से बाहर निकलते देखा, तो उस पर मोहित हो गया. गूजर कन्या भी शहज़ादा फ़िरोज़ से प्रभावित हुए बिना न रह सकी. अब तो फ़िरोज़ का शिकार के बहाने डेरे पर आना एक सिलसिला बन गया. फ़िरोज़ ने गूजरी के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा, तो उस गूजर कन्या ने विवाह की मंज़ूरी तो दे दी, लेकिन दिल्ली जाने से यह कहकर इंकार कर दिया कि वह अपने बूढ़े माता-पिता को छोड़कर नहीं जा सकती. फ़िरोज़ ने गूजरी को यह कहकर मना लिया कि वह उसे दिल्ली नहीं ले जाएगा.
1309 में दयालपुल में जन्मा फ़िरोज़ 23 मार्च 1351 को दिल्ली का सम्राट बना. फ़िरोज़ की मां हिन्दू थी और पिता तुर्क मुसलमान था. सुल्तान फ़िरोज़शाह तुग़लक ने इस देश पर साढ़े 37 साल शासन किया. उसने लगभग पूरे उत्तर भारत में कलात्मक भवनों, क़िलों, शहरों और नहरों का जाल बिछाने में ख्याति हासिल की. उसने लोगों के लिए अनेक कल्याणकारी काम किए. उसके दरबार में साहित्यकार, कलाकार और विद्वान सम्मान पाते थे.
दिल्ली का सम्राट बनते ही फ़िरोज़शाह तुग़लक ने महल हिसार इलाक़े में महल बनवाने की योजना बनाई. महल क़िले में होना चाहिए, जहां सुविधा के सब सामान मौजूद हों. यह सोचकर उसने क़िला बनवाने का फ़ैसला किया. बादशाह ने ख़ुद ही करनाल में यमुना नदी से हिसार के क़िले तक नहरी मार्ग की घोड़े पर चढ़कर निशानदेही की थी. दूसरी नहर सतलुज नदी से हिमालय की उपत्यका से क़िले में लाई गई थी. तब जाकर कहीं अमीर उमराओं ने हिसार में बसना शुरू किया था.
किवदंती है कि गूजरी दिल्ली आई थी, लेकिन कुछ दिनों बाद अपने घर लौट आई. दिल्ली के कोटला फ़िरोज़शाह में गाईड एक भूल-भूलैया के पास गूजरी रानी के ठिकाने का भी ज़िक्र करते हैं. तभी हिसार के गूजरी महल में अद्भुत भूल-भूलैया आज भी देखी जा सकती है.
क़ाबिले-ग़ौर है कि हिसार को फ़िरोज़शाह तुग़लक के वक़्त से हिसार कहा जाने लगा, क्योंकि उसने यहां हिसार-ए-फ़िरोज़ा नामक क़िला बनवाया था. 'हिसार' फ़ारसी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है 'क़िला'. इससे पहले इस जगह को 'इसुयार' कहा जाता था. अब गूजरी महल खंडहर हो चुका है. इसके बारे में अब शायद यही कहा जा सकता है-
हरियाणा के हिसार क़िले में स्थित गूजरी महल आज भी सुल्तान फ़िरोज़शाह तुग़लक और गूजरी की अमर प्रेमकथा की गवाही दे रहा है. गूजरी महल भले ही आगरा के ताजमहल जैसी भव्य इमारत न हो, लेकिन दोनों की पृष्ठभूमि प्रेम पर आधारित है. ताजमहल मुग़ल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ की याद में 1631 में बनवाना शुरू किया था, जो 22 साल बाद बनकर तैयार हो सका. हिसार का गूजरी महल 1354 में फ़िरोज़शाह तुग़लक ने अपनी प्रेमिका गूजरी के प्रेम में बनवाना शुरू किया, जो महज़ दो साल में बनकर तैयार हो गया. गूजरी महल में काला पत्थर इस्तेमाल किया गया है, जबकि ताजमहल बेशक़ीमती सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया है. इन दोनों ऐतिहासिक इमारतों में एक और बड़ी असमानता यह है कि ताजमहल शाहजहां ने मुमताज़ की याद में बनवाया था. ताज एक मक़बरा है, जबकि गूजरी महल फिरोज़शाह तुग़लक ने गूजरी के रहने के लिए बनवाया था, जो महल ही है.
गूजरी महल की स्थापना के लिए बादशाह फ़िरोज़शाह तुग़लक ने क़िला बनवाया. यमुना नदी से हिसार तक नहर लाया और एक नगर बसाया. क़िले में आज भी दीवान-ए-आम, बारादरी और गूजरी महल मौजूद हैं. दीवान-ए-आम के पूर्वी हिस्से में स्थित कोठी फ़िरोज़शाह तुग़लक का महल बताई जाती है. इस इमारत का निचला हिस्सा अब भी महल-सा दिखता है. फ़िरोज़शाह तुग़लक के महल की बंगल में लाट की मस्जिद है. अस्सी फ़ीट लंबे और 29 फ़ीट चौड़े इस दीवान-ए-आम में सुल्तान कचहरी लगाता था. गूजरी महल के खंडहर इस बात की निशानदेही करते हैं कि कभी यह विशाल और भव्य इमारत रही होगी.
सुल्तान फ़िरोज़शाह तुग़लक और गूजरी की प्रेमगाथा बड़ी रोचक है. हिसार जनपद के ग्रामीण इस प्रेमकथा को इकतारे पर सुनते नहीं थकते. यह प्रेम कहानी लोकगीतों में मुखरित हुई है. फ़िरोज़शाह तुग़लक दिल्ली का सम्राट बनने से पहले शहज़ादा फ़िरोज़ मलिक के नाम से जाने जाते थे. शहज़ादा अकसर हिसार इलाक़े के जंगल में शिकार खेलने आते थे. उस वक़्त यहां गूजर जाति के लोग रहते थे. दुधारू पशु पालन ही उनका मुख्य व्यवसाय था. उस काल में हिसार क्षेत्र की भूमि रेतीली और ऊबड़-खाबड़ थी. चारों तरफ़ घना जंगल था. गूजरों की कच्ची बस्ती के समीप पीर का डेरा था. आने-जाने वाले यात्री और भूले-भटके मुसाफ़िरों की यह शरणस्थली थी. इस डेरे पर एक गूजरी दूध देने आती थी. डेरे के कुएं से ही आबादी के लोग पानी लेते थे. डेरा इस आबादी का सांस्कृतिक केंद्र था.
एक दिन शहज़ादा फ़िरोज़ शिकार खेलते-खेलते अपने घोड़े के साथ यहां आ पहुंचा. उसने गूजर कन्या को डेरे से बाहर निकलते देखा, तो उस पर मोहित हो गया. गूजर कन्या भी शहज़ादा फ़िरोज़ से प्रभावित हुए बिना न रह सकी. अब तो फ़िरोज़ का शिकार के बहाने डेरे पर आना एक सिलसिला बन गया. फ़िरोज़ ने गूजरी के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा, तो उस गूजर कन्या ने विवाह की मंज़ूरी तो दे दी, लेकिन दिल्ली जाने से यह कहकर इंकार कर दिया कि वह अपने बूढ़े माता-पिता को छोड़कर नहीं जा सकती. फ़िरोज़ ने गूजरी को यह कहकर मना लिया कि वह उसे दिल्ली नहीं ले जाएगा.
1309 में दयालपुल में जन्मा फ़िरोज़ 23 मार्च 1351 को दिल्ली का सम्राट बना. फ़िरोज़ की मां हिन्दू थी और पिता तुर्क मुसलमान था. सुल्तान फ़िरोज़शाह तुग़लक ने इस देश पर साढ़े 37 साल शासन किया. उसने लगभग पूरे उत्तर भारत में कलात्मक भवनों, क़िलों, शहरों और नहरों का जाल बिछाने में ख्याति हासिल की. उसने लोगों के लिए अनेक कल्याणकारी काम किए. उसके दरबार में साहित्यकार, कलाकार और विद्वान सम्मान पाते थे.
दिल्ली का सम्राट बनते ही फ़िरोज़शाह तुग़लक ने महल हिसार इलाक़े में महल बनवाने की योजना बनाई. महल क़िले में होना चाहिए, जहां सुविधा के सब सामान मौजूद हों. यह सोचकर उसने क़िला बनवाने का फ़ैसला किया. बादशाह ने ख़ुद ही करनाल में यमुना नदी से हिसार के क़िले तक नहरी मार्ग की घोड़े पर चढ़कर निशानदेही की थी. दूसरी नहर सतलुज नदी से हिमालय की उपत्यका से क़िले में लाई गई थी. तब जाकर कहीं अमीर उमराओं ने हिसार में बसना शुरू किया था.
किवदंती है कि गूजरी दिल्ली आई थी, लेकिन कुछ दिनों बाद अपने घर लौट आई. दिल्ली के कोटला फ़िरोज़शाह में गाईड एक भूल-भूलैया के पास गूजरी रानी के ठिकाने का भी ज़िक्र करते हैं. तभी हिसार के गूजरी महल में अद्भुत भूल-भूलैया आज भी देखी जा सकती है.
क़ाबिले-ग़ौर है कि हिसार को फ़िरोज़शाह तुग़लक के वक़्त से हिसार कहा जाने लगा, क्योंकि उसने यहां हिसार-ए-फ़िरोज़ा नामक क़िला बनवाया था. 'हिसार' फ़ारसी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है 'क़िला'. इससे पहले इस जगह को 'इसुयार' कहा जाता था. अब गूजरी महल खंडहर हो चुका है. इसके बारे में अब शायद यही कहा जा सकता है-
सुनने की फुर्सत हो तो आवाज़ है पत्थरों में
उजड़ी हुई बस्तियों में आबादियां बोलती हैं...
सरफ़राज़ ख़ान
अरावली की मनोरम पर्वत मालाओं के अंचल में स्थित सोहना अपने गर्म पानी के चश्मों के लिए प्राचीनकाल से ही प्रसिध्द है. दिल्ली से करीब 50 किलोमीटर दिल्ली-अलवर मार्ग पर हरियाणा में बसा यह नगर प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर होने के कारण तीर्थ यात्रियों व पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. दिल्ली, जयपुर, अलवर, पलवल व गुड़गांव से आने वाली सड़कों का मुख्य केंद्र होने के कारण यहां सालभर श्रध्दालुओं का जमघट लगा रहता है.
किवदंती है कि सोहना को महर्षि सोनक ने बनाया था. इसलिए उन्हीं के नाम पर स्थल का नाम सोहना पड़ा. कुछ विद्वानों का मानना है कि प्राचीनकाल में यहां की पहाड़ियों से सोना मिलता था. इस वजह से इस स्थल को सुवर्ण कहा जाता था, जो बाद में सोहना के नाम से जाना जाने लगा. वैसे बरसात के दिनों में पहाड़ी नालों की रेत में अकसर सोने के कण दिखाई देते हैं. इस सोने को लेकर एक और किस्स मशहूर है जिसके मुताबिक वर्ष 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में आख़िरी मुगल सम्राट बहादुरशाह ज़फ़र के परिजनों को दिल्ली छोड़कर जाना पड़ा. अंग्रेज़ फ़ौज से बचने के लिए उन्होंने सोहना इलाके के गांव में डेरा डाला और अपने ख़ज़ाने को पहाड़ियों की किसी सुरक्षित गुफ़ा में दबा दिया. बाद में अंग्रेजी सेना ने उनकी हत्या कर दी.
इस घटना के करीब चार दषक बाद वर्ष 1895 में के.एम. पॉप नामक अंग्रेज कर्नल ने उस खजाने की तलाश में लंबे समय तक पहाड़ियों की ख़ाक छानी. मगर जब उसे कोई कामयाबी नहीं मिली, तो उसने इलाक़े के कुछ लोगों को साथ लेकर नए सिरे से ख़ज़ाने की खोज शुरू की. उन्हें ख़ज़ाने वाली गुफ़ा भी मिल गई, लेकिन भूत-प्रेत के ख़ौफ़ से ग्रामीणों ने गुफा में जाने से इंकार कर दिया. इसके बावजूद कर्नल ने हार नहीं मानी और अकेले ही ख़ज़ाने तक जाने का फ़ैसला किया. गुफ़ा के अंदर जाने पर उन्हें अस्थि पंजर दिखाई दिए, लेकिन इसके बाद भी वह आगे बढ़ते रहे. अंधेरी गुफा की जहरीली गैस से उनका दम घुटने लगा और वह बाहर की ओर दौड़ पड़े. इस गैस का उनकी सेहत पर गहरा असर पड़ा. स्वास्थ्य लाभ होने पर वे दोबारा गुफ़ा में गए, लेकिन तब तक सारा ख़ज़ाना चोरी हो चुका था. प्राचीनकाल में यहां ठंडे पानी के चश्मे भी थे, जो प्राकृतिक आपदाओं या परिवर्तन की वजह से धरती के नीचे समा गए. इनके बारे में ख़ास बात यह है कि इन चश्मों का संबंध जितना प्राचीन कथा से जुड़ा है, उतना ही इनकी खोज का विषय भी विवादास्पद रहा है. कुछ लोगों के मुताबिक़ ये चश्मे करीब तीन सौ साल पहले खोजे गए, जबकि बुजुर्गों का कहना है कि इन पर्वत मालाओं के नीचे से होकर गुजरने वाले व्यापारी और तीर्थ यात्रियों ने इन चश्मों की खोज की थी.
अरावली पर्वत की शाखाएं यहां से अजमेर तक फैली हैं. इन पहाड़ियों में दस-दस मील की दूरी तक कोई न कोई कुंड या झरना मौजूद है. इन झरनों व चश्मों की आखिरी कड़ी अजमेर में 'पुष्कर' सरोवर के नाम से विख्यात है. इन चश्मों की खोज के बारे में कई दंत कथाएं प्रचलित हैं. कहा जाता है कि एक बार चतुर्भुज नामक एक बंजारा ऊंटों, भेड़ों और खच्चरों पर नमक डालकर सोहना इलाक़े से गुज़र रहा था. गर्मी का मौसम था. इसलिए प्यास से व्याकुल होने पर उसने अपने कुत्ते को पानी की तलाश के लिए भेजा. थोड़ी देर बाद कुत्ता वापस आया. उसके पैर पानी से भीगे हुए थे. यह देखकर बंजारा बहुत खुश हुआ और कुत्ते के साथ पानी के चश्मे की ओर गया. उसने देखा कि निर्जन स्थलों पर शीतल जल का चश्मा है. उसने सोचा कि दैवीय शक्ति के कारण ही वीरान चट्टानों में पानी का चश्मा है. इसलिए उसने देवी से अपने कारोबार में मुनाफ़ा होने की मन्नत मांगी और उसे बहुत लाभ हुआ.
लौटते समय उसने अपने गुरु के नाम पर साखिम जाति नाम के गुम्बद और कुंडों का निर्माण करवाया। बाद में लक्खी नामक बंजारे ने इन कुंडों का जीर्णोद्वार करवाया. साखिम जाति के गुम्बद पर लगा सोने का कलम क़रीब आठ दशक पुराना है. इसे केशावानंद जी ने इलाके के लोगों से एकत्रित घन से चढ़वाया था. आईने-अकबारी में भी यहां के गर्म पानी के चश्मों का ज़िक्र आता है. किवदंती है कि योग दर्शन के रचयिता महार्षि पतंजलि का इस स्थल पर अनेक बार आगमन हुआ. संत महात्मा ऐसे ही स्थलों के आसपास अपने आश्रम बनाते थे. आधुनिक समय (1872 ई.) में अंग्रेजों ने इन चश्मों का पता लगाया था. ये चश्मे शहर के मध्य स्थित एक सीधी चट्टान के तल में स्थित हैं. इन चश्मों की तीर्थ के रूप में माना जाता है.
मथुरा (उत्तर प्रदेश). क्या आपने कभी भूतों का मंदिर देखा या सुना है? अगर नहीं तो आज हम आपको बताएंगे कि भूतों ने भी एक मंदिर बनाया है.
आज से 2100 वर्ष पहले मथुरा से 10 -12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित वृंदावन में भूतों ने एक मंदिर बनाया था, जिसे गोविन्द देव जी का मंदिर कहा जाता है. यहां पर रहने वालों का कहना है कि इस मंदिर को भूतों ने बनाया है. तभी इसे तों के मंदिर के नाम से जाना जाता है. जब हमने इस मंदिर के पुजारी से बात की तो उन्होंने बताया कि यह मंदिर गोविन्द देव जी का है, लेकिन यह कहा जाता है कि इस मंदिर को आधी रात के समय भूत बना रहे थे. तभी सुबह के समय किसी महिला ने चक्की चला दी और उसकी आवाज़ सुनकर भूत मंदिर को अधूरा बना हुआ छोड़कर भाग गए. तब से ही ये मंदिर अधूरा ही है. बताया जाता है कि इस मंदिर में पहले गोविन्द देव जी की असली प्रतिमा थी, लेकिन अब वह असली प्रतिमा भी नहीं है. इसका कारण यह है कि जब औरंगज़ेब का शासन आया तो उस समय औरंगज़ेब हिन्दुओं के मंदिरों को ख़त्म करवा रहा था. उस समय औरंगज़ेब ने इस मंदिर को तुड़वाना शुरू किया. इस मंदिर के चार मंज़िल को वह तुड़वा चुका था और मंदिर की नक्काशियों में जड़े हुए जवाहरातों को वह निकालकर ले गया था. मंदिर की असली प्रतिमा को मंदिर के पुजारी औरंगज़ेब के डर के कारण जयपुर लेकर चले गए थे. फिर जयपुर के राजा ने जयपुर में ही गोविन्द देव का मंदिर बनवा कर उस असली प्रतिमा को स्थापित करवा दिया जो आज भी जयपुर के उस मंदिर में मौजूद है.
सुभाशिष के. चंदा
लहरदार पगडंडियां, घने जंगल और घाटियां और संकरी नदियां और सोतों के मनोरम दृश्य, अनोखी वनस्पतियां और वन्य जीवों के आसपास होने का अहसास, और अपनी शहरी जिंदगी की रेलमपेल से भागे हुए जंगल के अभयारण्यक। ऐसा ही है उनाकोटि का प्राकृतिक भंडार, जो इतिहास, पुरातत्व और धार्मिक खूबियों के रंग, गंध से पर्यटकों को अपनी ओर इशारे से बुलाता है। यह एक औसत ऊंचाई वाली पहाड़ी श्रृंखला है, जो उत्तरी त्रिपुरा के हरे-भरे शांत और शीतल वातावरण में स्थित है।
राज्य की राजधानी से 170 किलोमीटर की दूरी पर स्थित उनाकोटि की पहाड़ी पर हिन्दू देवी-देवताओं की चट्टानों पर उकेरी गई अनगिनत मूर्तियां और शिल्प मौजूद हैं। बड़ी-बड़ी चट्टानों पर ये विशाल नक्काशियों की तरह दिखते हैं, और ये शिल्प छोटे-बड़े आकार में और यहां-वहां चारों तरफ फैले हैं। पौराणिक कथाओं में इसके बारे में दिलचस्प कथा मिलती है, जिसके अनुसार यहां देवी-देवताओं की एक सभा हुई थी। भगवान शिव, बनारस जाते समय यहां रुके थे, तभी से इसका नाम उनाकोटि पड़ा है।
उनाकोटि में चट्टानों पर उकेरे गए नक्काशी के शिल्प और पत्थर की मूर्तियां हैं। इन शिल्पों का केंद्र शिव और गणेश हैं। 30 फुट ऊंचे शिव की विशालतम छवि खड़ी चट्टान पर उकेरी हुई है, जिसे ‘उनाकोटिस्वर काल भैरव’ कहा जाता है। इसके सिर को 10 फीट तक के लंबे बालों के रूप में उकेरा गया है। इसी के पास शेर पर सवार देवी दुर्गा का शिल्प चट्टान पर उकेरी हुई है, वहां दूसरी तरफ मकर पर सवार देवी गंगा का शिल्प भी है। यहां नंदी बैल की जमीन पर आधी उकेरे हुए शिल्प भी हैं।
शिव के शिल्पों से कुछ ही मीटर दूर भगवान गणेश की तीन शानदार मूर्तियां हैं। चार-भुजाओं वाले गणेश की दुर्लभ नक्काशी के एक तरफ तीन दांत वाले साराभुजा गणेश और चार दांत वाले अष्टभुजा गणेश की दो मूर्तियां स्थित हैं। इसके अलावा तीन आंखों वाला एक शिल्प भी है, जिसके बारे में माना जाता है कि वह सूर्य या विष्णु भगवान का है। चतुर्मुख शिवलिंग, नांदी, नरसिम्हा, श्रीराम, रावण, हनुमान, और अन्य अनेक देवी-देवताओं के शिल्प और मूर्तियों यहां हैं। एक किंवदंती है कि अभी भी वहां कोई चट्टानों को उकेर रहा है, इसीलिए इस उनाकोटि-बेल्कुम पहाड़ी को देवस्थल के रूप में जाना जाता है, आप कहीं से भी, किधर से भी गुजर जाइए आपको शिव या किसी देव की चट्टान पर उकेरी हुई मूर्ति या शिल्प मिलेगा। पहाडों से गिरते हुए सुंदर सोते उनाकोटि के तल में एक कुंड को भरते हैं, जिसे ‘’सीता कुंड’’ कहते हैं। इसमें स्नान करना पवित्र माना जाता है। हर साल यहां अप्रैल के महीने में ‘अशोकाष्टमी मेला’ लगता है, जिसमें हजारों श्रद्धालु आते हैं और ‘सीता कुंड’ में स्नान करते हैं।
इसे एक आदर्श पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए केंद्रीय पर्यटन मंत्री ने 2009-10 में उनाकोटि डेस्टिनेशन डेवलेपमेंट प्रोजेक्ट के तहत यहां 5 किलोमीटर के दायरे में पर्यटक सूचना केंद्र, कैफेटेरिया, सार्वजनिक सुविधाएं, प्राकृतिक दृष्यों के लिए व्यूप्वाइंट आदि के निर्माण के लिए 1.13 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। त्रिपुरा पर्यटन विकास के योजना अधिकारियों के अनुसार, यह योजना एएसआई को सौंप दी गई है, और जल्दी ही इस पर काम शुरू होने की संभावना है।
माना जाता है कि उनाकोटि पर भारतीय इतिहास के मध्यकाल के पाला-युग के शिव पंथ का प्रभाव है। इस पुरातात्विक महत्व के स्थल के आसपास तांत्रिक, शक्ति, और हठ योगी जैसे कई अन्य संप्रदायों का प्रभाव भी पाया जाता है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण (एएसआई) के अनुसार उनाकोटि का काल 8वीं या 9वीं शताब्दी का है। हालांकि, इसके शिल्पों के बारे में, उनके समय-काल के बारे अनेक मत हैं।
देखा जाए तो ऐतिहासिक रूप से और उनकोटि की कथाएं अभी भी एएसआई और ऐसी ही अन्य संस्थाओं से इस पर समन्वित अनुसंधान की मांग कर रही हैं, ताकि भारतीय सभ्यता के लुप्त अध्याय के रहस्य को उजागर किया जा सके।
(लेखक पीआईबी, अगरतला में मीडिया एवं संचार अधिकारी हैं)
सतपाल
दिल्ली जो एक शहर है, हर शक्स की पसंद
चर्चे इस शहर के हमेशा रहे बुलन्द।
किसी भी दौर में यह वीराना नहीं होता
शहर-ए-दिल्ली, कभी पुराना नही होता।
आज चर्चा है दिल्ली के सौ साल पूरे होने की मगर तथ्य पर गौर करें तो पता चलेगा कि यह सत्य नहीं हैं। दिल्ली का इतिहास कई हजार साल पुराना है। कहते है कि पांडवों की दिल्ली का नाम इन्द्रप्रस्थ था। इस बीच का कई सैकडों वर्ष का विवरण गुमनाम है मगर, सात बार उजड़ने और बसने की कहानी आज भी लोगों को याद है। इन सात शहरों के नाम और खंडहर तो अपने काल का हाल चाल सुना रहे हैं। दिल्ली हमेशा से देश की राजधानी रही । हर साम्राज्य ने दिल्ली को देश का दिल समझकर इसे राजधानी बनाना पसंद किया। मुगल साम्राज्य भी अपनी राजधानी आगरा और फतेहपुर सीकरी से लेकर दिल्ली आया और ख्वाबों के हसीन शहर शाहजहांनाबाद की तामीर कराई। यमुना नदी के किनारे बसा शहर समूचे संसार में मशहूर हुआ और कई विदेशी राजा इससे ईष्र्या करने लगे। अंग्रेजों को भी यहां के ईमानदार और मेहनती लोग और यहां का भूगोल और हरा-भरा इलाका पसंद आया और उन्होंने 1911 में अपने दरबार में अपने इण्डिया की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाने की घोषणा कर दी। उन्होंने यह घोषणा तब के तमाम राजा, महाराजाओं, नवाबों और बादशाहों की उपस्थिति में की ताकि हरेक आम और खास को इसकी जानकारी मिल जाए और राजधानी के इस बदलाव का संदेश देश के कोने-कोने में पहुंच जाए। इस तरह यह सौ साल फिर से दिल्ली को राजधानी बनाने का ऐलान करने से संबंधित है। मुगलों के कमजोर हो जाने और ईस्ट इण्डिया कम्पनी की राजधानी के रूप में कलकत्ता का महत्व बढ़ जाने के बाद अंग्रेजों ने यह जरूरी समझा कि देश की पुरातन, सनातन राजधानी यानि ऐतिहासिक शहर दिल्ली को राजधानी बनाया जाए ताकि वह एक ऐसे शहर से समूचे भारत पर लम्बे से लम्बे समय तक राज कर सकें, जहां से मुगल सल्तनत का हुक्म देश के कोने-कोने तक सम्मान और गर्व के साथ सुना जाता था।
कुछ लोग इसे नई दिल्ली के सौ साल होने का दावा कर रहे है। गौर किया जाए तो, पता चलेगा कि यह भी सत्य नहीं है। न तो 1911 में नई दिल्ली की नींव पड़ी और न ही इस साल नई दिल्ली का उद्घाटन किया गया। नई दिल्ली का उद्घाटन तो 1931 में हुआ जिसके बाद दिल्ली एक नगर से महानगर बनना शुरू हो गया।
यह सच है कि आज ज्यादातर दिल्ली का भाग नया है मगर जो शहर कभी दीवारों के बीच सटा हुआ था और मिली-जुली तहजीब का मरकज माना जाता था वह भी तो नया ही महसूस होता है, क्योंकि वहां का रहन-सहन पूरी तरह बदला तो नहीं मगर आधुनिकता के साथ घी और शक्कर की तरह मिल कर और भी समृद्ध हो गया है।
अंग्रेजों ने जब राजधानी दिल्ली बनाने की घोषणा की तो उन्होंने सिविल लाइन्स में राजधानी के लिए जरूरी इमारतें बनानी शुरू की और कश्मीरी गेट को मुख्य बाजार और रिज की दहलीज के चारों ओर सत्ता के गलियारे बनाने शुरू किए। लेकिन जब उन्हें यमुना जो कभी बारहमासी नदी हुआ करती थी, उसका रौद्र रूप दिखाई दिया तो वह भयभीत हो गए और इस इलाके को निचला क्षेत्र मानकर एक उंचे स्थान पर राजधानी बनाने की तलाश में निकल पड़े। मगर, दिल्ली की सबसे पुरानी चर्च कश्मीरी गेट और चांदनी चौक में अब भी विद्यमान हैं और किसी लिहाज से पुरानी नहीं लगती। इसी तरह पुराना सचिवालय तो अंग्रेजों की पहली संसद थी और इसी के सभागार में दिल्ली यूनिवर्सिटी की पहली कन्वोकेशन हुई थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी का वी0सी0 ऑफिस कभी वायसरॉय निवास था। कहां बदला है ये सब कुछ। पहले से कहीं ज्यादा रौनक और ताजगी है वहां।
अंग्रेजों ने जब नई दिल्ली का निर्माण शुरू किया तो न जाने कितनी इमारतें बनाई गई। लुटियन के नक्शे के हिसाब से खुला-खुला, हरा-भरा नया शहर यानी नई दिल्ली सामने आई। इसकी हर इमारत ऐतिहासिक है मगर इस्तेमाल की दृष्टि से नई भी है और सुविधा सम्पन्न भी। क्या नई दिल्ली की शान पुरानी हुई है? नहीं, कभी नहीं हो सकती। एक समय आया जब अंग्रेजों का बनाया कनॉट प्लेस व्यापार की दृष्टि से महत्व खोने लगा मगर जब मेट्रो का जादू चला तो यहां की रौनक लौट आई और व्यापारी भी फिर प्रसन्न होने लगे। यह साबित करता है कि दिल्ली कभी न तो बूढ़ी होगी और न ही पुरानी।
अगर हम तब और अब की ट्रांसपोर्ट की चर्चा करें तो आप महसूस करेंगे कि अंग्रेजों के जमाने के ट्रांसपोर्ट के छोड़े गए निशान पर आज हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट दौड़ रही है। अंग्रेजों ने 1903 में चांदनी चौक से ट्राम का सफर शुरू किया था। यह ट्राम 1963 तक चली और इसका किराया एक टका यानी आधा आना और एक आना हुआ करता था। आज उसी स्थान के नीचे चांदनी चौक, चावड़ी बाजार और सब्जी मण्डी, बर्फखाने में भूमिगत और एलिवेटिड मेट्रो दौड़ रही है। कभी अंग्रेजों ने रायसीना हिल्स तक निर्माण के लिए पत्थर पहुंचाने के मकसद से रेल लाइन बिछाई थी वहां जमीन के नीचे आज मेट्रो की दो लाइनें सेंट्रल सेक्रेट्रियट स्टेशन से निकल रही इतना ही नहीं अंग्रेजों ने 1911 में अपने दरबार तक जाने के लिए एक रेल लाइन बिछाई थी जो आजाद पुर तक दौड़ती थी। उसी लाइन के एक स्टेशन तीस हजारी की जगह पर ही आज दिल्ली मेट्रो का तीस हजारी स्टेशन है।
आज भी लोग कुतुब मीनार को दिल्ली की पहचान मानते हैं। यह बात और है कि कई किताबों में बहाई टेम्पल यानी लोटस टेम्पल को दिल्ली की नई पहचान मानकर दिखाया जाता है मगर कुतुब मीनार अपनी बुलंदी की वजह से हर काल में नई पहचान ही बना रहेगा। कभी यहां तक जाने के लिए लोग पुरानी दिल्ली से तांगों पर जाया करते थे। हरियाली के बीचों बीच संकरी सड़क से होकर तांगे में बैठे मुसाफिरों को एअर कंडीशन सवारी का आनन्द मिलता था और आज वहां तक जाने के लिए एअर कंडीशन मेट्रो है। कह सकते है कि वही दिल्ली, वही कुतुब मीनार, वही एअर कंडीशन सफर तो कौन कहता है कि दिल्ली पुरानी हुई है। दिल्ली का दिल एक ऐसे नौजवान की तरह धड़कता है जिसे हर दम आगे बढ़ने की ललक होती है। इसी तरह दिल्ली हर पल, संवरती, निखरती, बदलती, सुधरती दिखाई देती है तो कौन कहेगा कि यह शहर पुराना होता है।
इस शहर के हर दम नया रहने के तो ये कुछ संकेत है। अगर हजारों साल की इस दिल्ली के इतिहास में नएपन का मजा लेना हो तो दिल से दिल्ली वाला बनना होगा।
दिल्ली नहीं है शहर, एक मिजाज का नाम है
यह खास, इस कदर है कि इसका सलाम है
(लेखक दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के सूचना अधिकारी हैं)
समीर पुष्प
बीते युग की कहानी कहती है कि दिल्ली सात बार बसी और सात बार उजड़ी। गाथाओं के सृजन की शक्ति और इतिहास के बदलने के साथ अंग्रेजों की दिल्ली के गौरवशाली 100 वर्ष पूरे हो गये हैं। अनेक असाधारण घटनाओं की गवाह रही दिल्ली कुछेक दु:खद किन्तु यहां के लोगों की असाधारण प्रतिभा के परिणामस्वरूप अक्सर सफलता के हर्षोल्लास और विविध घटनाओं से परिपूर्ण रही है
एक जीवन्त महानगर के रूप में इसके कई किस्से है जो समय के साथ दब गयेकिन्तु उनकी तात्कालिकता अब भी भावपूर्ण है। एक समृद्ध इतिहास, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, सांस्कृतिक विविधता और धार्मिक एकता के अलावा दिल्ली के पास और भी बहुत कुछ है। दिल्ली एक ऐसी झलक पेश करती है, जिसमें जटिलताएं, विषमताएं, सुन्दरता और एक नगर की गतिशीलता है, जहां अतीत और वर्तमान का अस्तित्व एक साथ कायम है। यहां अनेक शासकों ने राज किया और जिससे इसके जीवन में कई सांस्कृतिक घटकों का समावेश हो गया। एक ओर जहां ऐतिहासिक इमारतें, प्राचीन काल की महिमा का प्रमाण हैं, वहीं दूसरी ओर लम्बे समय से पीडि़त यमुना नदी भी है जो वर्तमान की उपेक्षा की कहानी कहती है। दिल्ली का अस्तित्व बहुस्तरीय है और यह सबसे तेजी से विकसित होते महानगरों में शामिल है। 13वीं और 17वीं शताब्दी में बसे सात नगरों से निकलकर दिल्ली ने अपने नगरीय क्षेत्र का निरंतर विस्तार किया है। इसकी गगनचुम्बी इमारतें, आवासीय कॉलोनियां और तेजी से बढ़ते व्यावसायिक मॉल ये सभी बदलते समय के परिचायक हैं। उर्जा, बौद्धिकता और उल्लास की भावना से ओतप्रोत लोग दिल्ली की आत्मा हैं। करोड़ों लोग अपना आशियाना बसाने और अपनी आशाओं को पूरा करने के उद्देश्य से पूरी जीवन्तता और जोश के साथ यहां काम में जुटे रहते हैं। पिछले कई दशकों से दिल्ली विविध अवधारणाओं अभिनव परम्पराओं का प्रतिनिधित्व करती रही है। अपने आप को पुनर्जीवित करने की शक्ति और समय की कसौटी पर खरा उतरने की उर्जा दिल्ली को बेजोड़ बनाती है, जो इसकी जीवनचर्या में देखी जा सकती है।
भारत एक महान राष्ट्र है और इसकी राजधानी होने के कारण दिल्ली इस महानता में पुरानी और नई भागीदारी का एक प्रतीक है। आज की दिल्ली एक बहुआयामी, बहु-सांस्कृतिक और बहुविध प्रगतिशील है। यह निरंतर साथ मिलकर चलने की प्रवृति रखती है। बिना किसी हिचक के दिल्ली करोड़ो लोगों का घर और उनकी आशायें है। स्वतंत्रता के बाद दिल्ली में व्यापक सुधार हुए और विकसित राष्ट्र की राजधानियों के साथ-साथ इसका भी जोरदार विकास हुआ। अतीत में कुछ समय से दिल्ली सत्ता का स्थान नहीं था। हालांकि यहां का हरेक पत्थर और यहां की हरेक र्इंट हमारे कानों में इसके लम्बे और गौरवमय इतिहास की कहानी कहते है।
अरावली की क्षीण होती श्रेणियों और यमुना के बीच दिल्ली ने अपने युगों के इतिहास की भूलभुलैया को दफन कर रखा है। दिल्ली ने अपना नाम राजा ढिल्लु से लिया है। दिल्ली का शुरुआती ऐतिहासिक संदर्भ पहली शताब्दी पूर्व से शुरू होता है। इतिहास में दिल्ली की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसकी वजह इसकी भौगोलिक अवस्थिति हो सकती है। दिल्ली का मध्य एशिया, उत्तर-पश्चिमी सीमांत क्षेत्र और देश के बाकी क्षेत्र के साथ हमेशा सुविधाजनक संपर्क रहा है। प्रसिद्ध मौर्य शासक अशोक के समय का शिलालेख बताता है कि दिल्ली मौर्यों की उत्तरी राजमार्ग पर अवस्थित थी और यह उनकी राजधानी पाटलिपुत्र को तक्षशिला से जोड़ती थी। इसी रास्ते से बौद्ध भिक्षु तक्षशिला जाते थे। इसी मार्ग से मौर्यों के सैनिक भी तक्षशिला और सीमावर्ती विद्रोहियों से निपटने के लिए जाते थे। इस वजह से दिल्ली को सामरिक लिहाज से महत्वपूर्ण स्थान मिला।
दिल्ली की कहानी में कई शहरों के अस्तित्व की कहानी छुपी है। इसका वर्णन नीचे किया जा रहा है:
इन्द्रपस्थ 1450 ई. पू.
स्थल: पुराना किला।
अवशेष: पुरातात्विक साक्ष्य अब यह साबित करते हैं कि वास्तव में यही दिल्ली का सबसे पुराना नगर था। दिल्ली का कोई शख्स इंद्रप्रस्थ का अस्तित्व कभी नकार नहीं पाता। इसके पतन का कारण पता नहीं है।
लाल कोट या किला राय पिथौरा 1060 ई.
स्थल: कुतुब मीनार-महरौली परिसर
अवशेष: मूल लालकोट का बहुत थोड़ा हिस्सा शेष। राय पिथौर किले के 13 दरवाजों में से केवल 3 शेष हैं।
निर्माता: राजपूत तोमर। 12वीं शताब्दी। राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान ने इस पर कब्जा किया और इसका विस्तार किया।
सीरी 1304 ई.
स्थल: हौजखास और गुलमोहर पार्क।
अवशेष: कुछ हिस्से और दीवारें शेष। अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी के चारों ओर अन्य चीजों जैसे दरवाजा, कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद का दक्षिणी दरवाजा और वर्तमान के हौजखास में जलाशय आदि का निर्माण भी करवाया।
निर्माता: दिल्ली सल्तनत के अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी को उसके द्वारा किए गए व्यापारिक सुधारों के लिए जाना जाता है। इसलिए यह बहुत बड़ा कारोबारी केंद्र था।
तुगलकाबाद 1321.23 ई.
स्थल: कुतुब परिसर से 8 किलोमीटर दूर
अवशेष: दीवारों और कुछ भवनों के भग्नावशेष।
निर्माता: गयासुद्दीन तुगलक।
जहानपनाह 14वीं सदी के मध्य
स्थल: सीरी और कुतुबमीनार के मध्य।
अवशेष: रक्षात्मक प्राचीर के कुछ अवशेष।
निर्माता: मोहम्मद-बिन-तुगलक।
फिरोज़ाबाद 1354 ई.
स्थल: कोटला फिरोज़शाहअवशेष: अवशेषों में केवल अशोक स्तम्भ बचा हुआ है। अब वहां क्रिकेट स्टेडियम है जो फिरोजशाह कोटला मैदान के नाम से विख्यात है।निर्माता: फिरोजशाह तुगलक। यह सिकन्दर लोधी के आगरा चले जाने तक राजधानी रहा।
दिल्ली शेरशाही (शेरगढ़) 1534
स्थल: चिडि़याघर के सामने पुराना किले के आसपास।
अवशेष: उंचे द्वार, दीवारें, मस्जिद और एक बड़ी बावड़ी (कुंआ)। काबुली और लाल दरवाज़ा, द्वार और शेर मंडल।द्वारा निर्मित: वास्तव में इस दिल्ली का निर्माण दूसरे मुगल बादशाह हुमायुं द्वारा शुरू किया गया और शेरशाह सूरी ने इसे पूरा किया गया।
शाजहानाबाद 17वीं शताब्दी का मध्यकालस्थल: मौजूदा पुरानी दिल्ली
अवशेष: लालकिला, जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली के मुख्य बाजार जैसे चाँदनी चौक, दीवारों के लम्बे भाग और नगर के कई द्वार। पुरानी दिल्ली भीड़-भाड़ वाली रही होगी, लेकिन यह अभी भी अपना मध्ययुगीन सौंदर्य बनाये हुए है। लोग गर्मजोशी से स्वागत करने वाले हैं। मुगलवंश के पांचवें बादशाह शाहजहां अपनी राजधानी आगरा से यहां ले आए।
भारत की राजधानी न केवल अपनी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के लिए जानी जाती है, बल्कि उत्कृष्ट कला और शिल्पकला के लिए भी प्रसिद्ध है। वास्तव में दिल्ली की कलाएं और शिल्पकलाएं शाही जमाने से संरक्षित है। अपने समय के सांस्कृतिक केंद्र के रूप में दिल्ली ने सर्वोत्तम चित्रकारों, संगीतज्ञों और नर्तकों को आकर्षित किया। ऐसा इसलिए क्योंकि इस शहर की कोई अपनी विशिष्ट पहचान नहीं है। समय बीतने के साथ-साथ भारत के विभिन्न क्षेत्रों से लोग आए और यहां बस गए। इस प्रकार दिल्ली भांति-भांति के लोगों का केंद्र बन गई। धीरे-धीरे दिल्ली ने यहां रहने वाले हर तरह के लोगों की पहचानों को अपना लिया, जिसने इसे बहुरंगी पहचान वाला शहर बना दिया।
दिल्ली की सबसे बड़ी पहचान इसकी विविधता है। इसमें विभिन्न पृष्ठभूमियों जैसे धर्म, क्षेत्र, भाषा, जाति और वर्ग के लोग आकर बस गए, जिनकी अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संसाधनों और अवसरों तक मिलीजुली पहुंच है। दिल्ली हमेशा से विविध गतिविधियों का केंद्र रहा है, जिसने बड़े उतार-चढ़ाव देखे हैं। दिल्ली की हवा वर्तमान की गलतियों और अतीत की सुगंध से भरपूर है, जो नए भारत का मार्ग प्रशस्त करती है।
(समीर पुष्प एक स्वतंत्र लेखक हैं)
कुआलालंपुर (मलेशिया). पर्यटन को और बढ़ावा देने के लिए अब
मलेशिया सरकार ने भारतीय नागरिकों को वीजा फ्री ट्रांजिट सुविधा देने
का फ़ैसला किया है. एक जुलाई से इसे शुरू कर दिया जाएगा. मलेशिया के आव्रजन विभाग
के एक बयान के मुताबिक बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका के नागरिकों को भी यह
सुविधा दी जाएगी. सरकार को इस साल 6,50,000 सैलानियों के आने की उम्मीद है. मलेशिया
में अनेक दर्शनीय स्थल हैं.
स्टार न्यूज़ एजेंसी
नई दिल्ली. भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (एएसआई) आंध्र प्रदेश राज्य में पुरातत्वीय खुदाई के कार्य को सुदृढ़ करने के लिए कार्य कर रहा है।
पिछले तीन वर्षों के दौरान एएसआई ने आंध्र प्रदेश में खुदाई वैज्ञानिक निकासी के जो कार्य किए हैं उनमें प्राचीन बौध्द टीला, एलुरू, जिला कृष्णा, प्राचीन बौध्द टीला, कोट्टुरू, जिला विशाखापट्नम, बौध्द टीला, कोदावली, जिला पूर्वी गोदावरी, बौध्द टीला, घंटासाला, जिला कृष्णा, प्राचीन टीला, कांटामनेनिवरी, गुदेम, जिला पश्चिम गोदावरी और प्राचीन टीला, कोन्डापुर, जिला मेडक शामिल है।
नई दिल्ली. भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (एएसआई) आंध्र प्रदेश राज्य में पुरातत्वीय खुदाई के कार्य को सुदृढ़ करने के लिए कार्य कर रहा है।
पिछले तीन वर्षों के दौरान एएसआई ने आंध्र प्रदेश में खुदाई वैज्ञानिक निकासी के जो कार्य किए हैं उनमें प्राचीन बौध्द टीला, एलुरू, जिला कृष्णा, प्राचीन बौध्द टीला, कोट्टुरू, जिला विशाखापट्नम, बौध्द टीला, कोदावली, जिला पूर्वी गोदावरी, बौध्द टीला, घंटासाला, जिला कृष्णा, प्राचीन टीला, कांटामनेनिवरी, गुदेम, जिला पश्चिम गोदावरी और प्राचीन टीला, कोन्डापुर, जिला मेडक शामिल है।
फ़िरदौस ख़ान
देश में बाघों की लगातार घटती संख्या से चिंतित सरकार बाघ अभयारण्य पर विशेष ज़ोर दे रही है. ऐसा ही एक बांदीपुर बाघ अभयारण्य है, जो कर्नाटक राज्य के मैसूर ज़िले में स्थित है. भारत में 1973 में शुरू की गई बाघ परियोजना के तहत इसकी गिनती पहले नौ बाघ अभयारण्यों में है. बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क मैसूर के महाराजाओं द्वारा 1930 में स्थापित सर्वाधिक आकर्षक वन्य जीव केन्द्रों में से एक है. शिकार करने का उनका निजी पार्क था. वर्ष 1941 में इसका विस्तार करके उत्तर पश्चिम में राजीव गांधी राष्ट्रीय पार्क-नागरहोल के साथ, दक्षिण पश्चिम में केरल के वयनाड वन्य-जीव शरण स्थल के साथ और दक्षिण मे तमिलनाडु के मदुमलाई वन्यजीव शरणस्थल के साथ मिला दिया गया जो अब मिलकर नीलगिरि बायोस्फीयर शरणस्थल के नाम से जाना जाता है. यह भारत का पहला बायोस्फीयर शरणस्थल है. इस पार्क को इस बात का गर्व है कि यहां तब से बाघों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी होती रही है. यह चंदन के वृक्षों और दुलर्भ पेड़-पौधों के लिए भी प्रसिध्द है. यहां सबसे ऊंची शिखर गोपालस्वामी पहाड़ी है. बांदीपुर का तापमान 10 और 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है. इस पार्क में औसतन वर्षा 1200 एमएम होती है.
इस अभयारण्य के मुख्य बारहमासी नदियां नुगु, काबीनी और मोयर हैं. नुगु नदी इस अभयराण्य के बीचोबीच बहती है, जबकि मोयर नदी इस अभयारण्य और मधुमलाई वन्य जीव शरण स्थल की दक्षिणी सीमा है. काबीनी नदी इस अभयारण्य और नागरहोल के बीच सीमा का काम करती है और इस नदी पर बीचनहाली में एक बड़ा बांध बनाया गया है.
काबीनी जलाशय बड़ी और लम्बी विपत्ति के समय में सैंकड़ों हाथियों के लिए चरने का मैदान और जल की सुविधा उपलब्ध कराता है. यहां पर मौसमी नदियां भी है. इनके नाम हैं - बादली, चमनहाला, एदासनहत्तीहाल, हेबकला, वराचीं, चिप्पनकला और माबिनहल्ला. इस अभयराण्य में कुछ प्राकृतिक और कृत्रिम लवणलेह भी है और जंगली पशुओं द्वारा उनका नियमित रूप से प्रयोग किया जाता है.
बांदीपुर बाघ अभयारण्य, 1973 में तत्कालीन वेणुगोपाल वन्य जीव पार्क के अधिकांश वन क्षेत्र और बांदीपुर मंदिर को मिलाकर बनाया गया था और इसका नाम बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क रखा गया. 1931 में बांदीपुर अभयारण्य के वन में 90 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में एक शरणस्थल बनाया गया. वेणुगोपाल वन्य जीव पार्क 1941 में बनाया गया जो कि 800 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला है. इस पहाड़ी के शिखर पर स्थित मंदिर का नाम वेणुगोपाल देवता के नाम पर रखा गया. इस अभयारण्य में शामिल सभी वन आरक्षित वन हैं और स्वतंत्रता से पहले अधिसूचित किए गए हैं. बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क में बेशकीमती इमारती लकड़ी के अनेक किस्म के वृक्ष हैं. इसके अलावा जाने-माने फूलों और फलों के अनेक वृक्ष भी हैं.
बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क मे बड़ी संख्या में हाथी पाए जाते हैं. यहां स्तनधारी परभक्षियों की भी अच्छी आबादी है. मुख्य पशुओं में बाघ,चीता, हाथी, सम्बर, गौर, लकड़बघा, चित्तीदार हिरण, जंगली कुत्ते, कुरंग. उनमें बाघ, चार सीघों वाले कुरंग, गौर, हाथी, तेंदुआ, मगरमच्छ, सांप आदि संकटापन्न पशु हैं. अलग-अलग प्रकार की 85 तितलियां और 67 प्रकार की चीटियां भी यहां पाई जाती हैं.
देश में बाघों की लगातार घटती संख्या से चिंतित सरकार बाघ अभयारण्य पर विशेष ज़ोर दे रही है. ऐसा ही एक बांदीपुर बाघ अभयारण्य है, जो कर्नाटक राज्य के मैसूर ज़िले में स्थित है. भारत में 1973 में शुरू की गई बाघ परियोजना के तहत इसकी गिनती पहले नौ बाघ अभयारण्यों में है. बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क मैसूर के महाराजाओं द्वारा 1930 में स्थापित सर्वाधिक आकर्षक वन्य जीव केन्द्रों में से एक है. शिकार करने का उनका निजी पार्क था. वर्ष 1941 में इसका विस्तार करके उत्तर पश्चिम में राजीव गांधी राष्ट्रीय पार्क-नागरहोल के साथ, दक्षिण पश्चिम में केरल के वयनाड वन्य-जीव शरण स्थल के साथ और दक्षिण मे तमिलनाडु के मदुमलाई वन्यजीव शरणस्थल के साथ मिला दिया गया जो अब मिलकर नीलगिरि बायोस्फीयर शरणस्थल के नाम से जाना जाता है. यह भारत का पहला बायोस्फीयर शरणस्थल है. इस पार्क को इस बात का गर्व है कि यहां तब से बाघों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी होती रही है. यह चंदन के वृक्षों और दुलर्भ पेड़-पौधों के लिए भी प्रसिध्द है. यहां सबसे ऊंची शिखर गोपालस्वामी पहाड़ी है. बांदीपुर का तापमान 10 और 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है. इस पार्क में औसतन वर्षा 1200 एमएम होती है.
इस अभयारण्य के मुख्य बारहमासी नदियां नुगु, काबीनी और मोयर हैं. नुगु नदी इस अभयराण्य के बीचोबीच बहती है, जबकि मोयर नदी इस अभयारण्य और मधुमलाई वन्य जीव शरण स्थल की दक्षिणी सीमा है. काबीनी नदी इस अभयारण्य और नागरहोल के बीच सीमा का काम करती है और इस नदी पर बीचनहाली में एक बड़ा बांध बनाया गया है.
काबीनी जलाशय बड़ी और लम्बी विपत्ति के समय में सैंकड़ों हाथियों के लिए चरने का मैदान और जल की सुविधा उपलब्ध कराता है. यहां पर मौसमी नदियां भी है. इनके नाम हैं - बादली, चमनहाला, एदासनहत्तीहाल, हेबकला, वराचीं, चिप्पनकला और माबिनहल्ला. इस अभयराण्य में कुछ प्राकृतिक और कृत्रिम लवणलेह भी है और जंगली पशुओं द्वारा उनका नियमित रूप से प्रयोग किया जाता है.
बांदीपुर बाघ अभयारण्य, 1973 में तत्कालीन वेणुगोपाल वन्य जीव पार्क के अधिकांश वन क्षेत्र और बांदीपुर मंदिर को मिलाकर बनाया गया था और इसका नाम बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क रखा गया. 1931 में बांदीपुर अभयारण्य के वन में 90 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में एक शरणस्थल बनाया गया. वेणुगोपाल वन्य जीव पार्क 1941 में बनाया गया जो कि 800 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला है. इस पहाड़ी के शिखर पर स्थित मंदिर का नाम वेणुगोपाल देवता के नाम पर रखा गया. इस अभयारण्य में शामिल सभी वन आरक्षित वन हैं और स्वतंत्रता से पहले अधिसूचित किए गए हैं. बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क में बेशकीमती इमारती लकड़ी के अनेक किस्म के वृक्ष हैं. इसके अलावा जाने-माने फूलों और फलों के अनेक वृक्ष भी हैं.
बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क मे बड़ी संख्या में हाथी पाए जाते हैं. यहां स्तनधारी परभक्षियों की भी अच्छी आबादी है. मुख्य पशुओं में बाघ,चीता, हाथी, सम्बर, गौर, लकड़बघा, चित्तीदार हिरण, जंगली कुत्ते, कुरंग. उनमें बाघ, चार सीघों वाले कुरंग, गौर, हाथी, तेंदुआ, मगरमच्छ, सांप आदि संकटापन्न पशु हैं. अलग-अलग प्रकार की 85 तितलियां और 67 प्रकार की चीटियां भी यहां पाई जाती हैं.
स्टार न्यूज़ एजेंसी
बाल्मीकि बाघ अभयारण्य भारत का 18वां बाघ अभयारण्य और बिहार के पश्चिमी चम्पारन जिले के धुर उत्तरी भाग में स्थित बिहार का दूसरा बाघ अभयारण्य है। 1950 के प्रारंभिक वर्षों तक बाल्मीकि नगर का विस्तृत वन क्षेत्र बत्तीहा राज और रामनगर राज के स्वामित्व में था। 1989 में मुख्य क्षेत्र को राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया। बिहार सरकार ने 1978 में 464.60 वर्ग किलोमीटर को बाल्मीकि वन्य जीव शरण स्थल अधिसूचित किया था। बाद में 1990 में 419.18 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र इस शरण स्थल में जोड़ दिया गया । इस प्रकार बाल्मीकि वन्यजीव शरण स्थल कुल 880.78 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है।
बाल्मीकि भू-भाग फटा-फटा और असमतल क्षेत्र है। यहां अकसर अत्याधिक भू-वैज्ञानिक संरचनाएं बनती रहती हैं। परिणामस्वरूप यहां खड़ी घाटियां हैं , चाकू के किनारे जैसी पर्वत श्रेणियां और प्रपाती दिवारें हैं जो कि जमीन के फिसलन और भूमि के कटाव से बनती हैं।
यहां बहने वाली छोटी-छोटी नदियों का सारा पानी इकट्ठा होकर महान गंडक और मसान नदियों में जमा होता है। ये नदियां और नाले एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर अपने मार्ग बदलते रहते हैं। किनारों की कटाव संभावित रेतीली और कच्ची जमीन के कारण पंचवाद , मानोर, बापसा और कापन जैसी मौसमी नदियां एक स्थान पर कटाव और दूसरे स्थान पर लाई हुई उस मिट्टी के जमाव का विचित्र स्वरूप प्रस्तुत करती हैं।
वनस्पति
बाल्मीकि बाघ अभयारण्य में अनेक प्रकार के पेड़ पौधे हैं जैसे साल, असन, सेमल, रौर, केन , जामुन और पीपल आदि।
वन
इस शरण स्थल में मौजूद वनों के प्रमुख प्रकारों में भाबरदुन साल वन, शुष्क शिवालक साल वन, पश्चिमी मांगे आर्द्र मिश्रित पर्णपाती वन, पूर्वी आर्द्र कछारी घास स्थल आदि शामिल हैं।
बाल्मीकि बाघ अभयारण्य में अनेक प्रकार के पशु भी मिलते हैं । बाघ के अलावा वन्य जीवों में चीता, फिशिंग कैट, चितकबरा हिरण, चीतल , सांभर, भेडिया, जंगली कुत्ते, लंगूर आदि शामिल हैं।
बघवा- चिगैनी रेल सड़क संपर्क पुल के निर्माण के कारण कोहुआ और कोटारहैया नदियों के प्राकृतिक बहाव को रोक दिया गया और 1691 हेक्टेयर वन भूमि में पानी भर गया जिसके कारण इस अभयारण्य के मदनपुर खंड में 15000 वृक्ष नष्ट होने के कगार पर हैं । इस क्षेत्र में खनन गतिविधियों ने भी अभ्यारण्य को नुकसान पहुंचाया है।
पुरातत्व
इस क्षेत्र में पुरातत्व की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण स्थान हैं लौरिया नन्दन गढ में अशोक स्तंभ है जो पालिश शुदा रेत के पत्थर का एक खंड है जिसकी ऊंचाई 32, -9.5 है। आधार पर 35.5 का और शीर्ष पर 26.2 का व्यास है। यह स्तंभ 2000 वर्ष से अधिक पुराना है और उत्कृष्ट स्थिति में है।
फ़िरदौस ख़ान
बाल्मीकि बाघ अभयारण्य भारत का 18वां बाघ अभयारण्य और बिहार के पश्चिमी चम्पारन ज़िले के धुर उत्तरी भाग में स्थित बिहार का दूसरा बाघ अभयारण्य है. यह पर्यटन के लिए यह एक आकर्षण का केंद्र है. साल 1950 के शुरू तक बाल्मीकि नगर का विस्तृत वन क्षेत्र बत्तीहा राज और रामनगर राज के स्वामित्व में था. 1989 में मुख्य क्षेत्र को राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया. बिहार सरकार ने 1978 में 464.60 वर्ग किलोमीटर को बाल्मीकि वन्य जीव शरण स्थल अधिसूचित किया था. बाद में 1990 में 419.18 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र इस शरण स्थल में जोड़ दिया गया. इस प्रकार बाल्मीकि वन्यजीव शरण स्थल कुल 880.78 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है.
बाल्मीकि भू-भाग फटा-फटा और असमतल क्षेत्र है. यहां अकसर अत्याधिक भू-वैज्ञानिक संरचनाएं बनती रहती हैं. यहां खड़ी घाटियां हैं, चाकू के किनारे जैसी पर्वत श्रेणियां और प्रपाती दिवारें हैं जो कि जमीन के फिसलन और भूमि के कटाव से बनती हैं.
यहां बहने वाली छोटी-छोटी नदियों का सारा पानी इकट्ठा होकर महान गंडक और मसान नदियों में जमा होता है. ये नदियां और नाले एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर अपने मार्ग बदलते रहते हैं. किनारों की कटाव संभावित रेतीली और कच्ची जमीन के कारण पंचवाद, मानोर, बापसा और कापन जैसी मौसमी नदियां एक स्थान पर कटाव और दूसरे स्थान पर लाई हुई उस मिट्टी के जमाव का विचित्र स्वरूप प्रस्तुत करती हैं.
बाल्मीकि बाघ अभयारण्य भारत का 18वां बाघ अभयारण्य और बिहार के पश्चिमी चम्पारन ज़िले के धुर उत्तरी भाग में स्थित बिहार का दूसरा बाघ अभयारण्य है. यह पर्यटन के लिए यह एक आकर्षण का केंद्र है. साल 1950 के शुरू तक बाल्मीकि नगर का विस्तृत वन क्षेत्र बत्तीहा राज और रामनगर राज के स्वामित्व में था. 1989 में मुख्य क्षेत्र को राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया. बिहार सरकार ने 1978 में 464.60 वर्ग किलोमीटर को बाल्मीकि वन्य जीव शरण स्थल अधिसूचित किया था. बाद में 1990 में 419.18 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र इस शरण स्थल में जोड़ दिया गया. इस प्रकार बाल्मीकि वन्यजीव शरण स्थल कुल 880.78 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है.
बाल्मीकि भू-भाग फटा-फटा और असमतल क्षेत्र है. यहां अकसर अत्याधिक भू-वैज्ञानिक संरचनाएं बनती रहती हैं. यहां खड़ी घाटियां हैं, चाकू के किनारे जैसी पर्वत श्रेणियां और प्रपाती दिवारें हैं जो कि जमीन के फिसलन और भूमि के कटाव से बनती हैं.
यहां बहने वाली छोटी-छोटी नदियों का सारा पानी इकट्ठा होकर महान गंडक और मसान नदियों में जमा होता है. ये नदियां और नाले एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर अपने मार्ग बदलते रहते हैं. किनारों की कटाव संभावित रेतीली और कच्ची जमीन के कारण पंचवाद, मानोर, बापसा और कापन जैसी मौसमी नदियां एक स्थान पर कटाव और दूसरे स्थान पर लाई हुई उस मिट्टी के जमाव का विचित्र स्वरूप प्रस्तुत करती हैं.
स्टार न्यूज़ एजेंसी
नई दिल्ली. भारतीय रेल खान-पान और पर्यटन निगम आईआरसीटीसी ने
मांग के आधार पर महत्त्वपूर्ण बौध्द तीर्थ स्थलों की यात्रा के लिए मासिक पर्यटन
पैकेज शुरू करने की योजना बनाई है। इन तीर्थ स्थलों के नाम है: नागार्जुन
कोंडा, अजंता और एलोरा गुफाएं स्रावस्ती, सांची, कुशीनगर, राजगीर, बोध गया आदि।
रेल राज्य मंत्री के एच मुनियप्पा द्वारा आज लोक सभा में बताया
कि आईआरसीटीसी इस समय ओडिशा में बौध्द तीर्थ स्थलों की यात्रा के लिए दो रेल
यात्रा पैकेज चला रहा है। इन तीर्थ स्थलों के नाम हैं - धौलगिरि, खंडगिरि, उदयगिरि, ललितगिरि और रत्नगिरि। ये पैकेज नियमित रेल सेवाओं द्वारा उपलब्ध है।
स्टार न्यूज़ एजेंसी
नई दिल्ली. भारत में अधिक संख्या में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सरकार ने
पांच देशों के नागरिकों के लिए 'पहुंचने पर वीज़ा' जारी करने की योजना जनवरी 2010 में शुरू की है। इन देशों के नाम हैं फिनलैंड, जापान, लुक्जमबर्ग, न्यूजीलैंड और सिंगापुर। जनवरी-मार्च 2010 के दौरान इस योजना के अधीन इन देशों के नागरिकों के लिए कुल 1793 वीज़ा जारी किए गए।
इस योजना के अधीन आलोच्य अवधि के दौरान सिंगापुर के 642, फिनलैंड के 466, न्यूजीलैंड के 378, जापान के 298 और लुक्जमबर्ग के 9
कल्पना पालकीवाला
राजस्थान के जैसलमेर जिले के थार मरुस्थल में अवस्थित मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान न केवल राज्य का सबसे बड़ा उद्यान है बल्कि पूरे भारत में इसके बराबर का कोई राष्ट्रीय मरूउद्यान नहीं है। उद्यान का कुल क्षेत्र 3162 वर्ग किलोमीटर है। उद्यान का काफी बड़ा भाग लुप्त हो चुके नमक की झीलों की तलहटी और कंटीली झाड़ियों से परिपूर्ण है। इसके साथ ही रेत के टीलों की भी बहुतायत है। उद्यान का 20 प्रतिशत भाग रेत के टीलों से सजा हुआ है। उद्यान का प्रमुख क्षेत्र खड़ी चट्टानों, नमक की छोटी-छोटी झीलों की तलहटियों, पक्के रेतीले टीलों और बंजर भूमि से अटा पड़ा है।
थार की भंगुर पर्यावरणीय प्रणाली में अनेक प्रकार की अनूठी वनस्पतियों और पशुओं की प्रजातियों के साथ-साथ वन्यजीवों को पनाह मिली हुई है। मरुस्थलीय पर्यावरण प्रणाली का यह सर्वथा उपयुक्त उदाहरण है। इन कठिन परिस्थितियों में अनेक प्रकार के जीवों को फलते फूलते देखना अपने आप में एक सुखद आश्चर्य है। उद्यान की अद्भुत वनस्पतियों और पशुओं को देखने का सबसे उत्तम स्थान सुदाश्री वन चौकी है। भरतपुर पक्षी अभयारण्य के निकट स्थित होने के कारण यहां भी अनेक प्रकार के प्रवासी पक्षी आते रहते हैं। उद्यान में तीन प्रमुख झीलें हैं - राजबाग झील, मलिक तलाव झील और पदम तलाव। ये तीनों झीलें, इस राष्ट्रीय उद्यान के निवासियों के प्रमुख जल स्रोत हैं।
भंगुर पर्यावरणीय प्रणाली के बावजूद यहां अनेक प्रकार के पक्षी पाये जाते हैं। लुप्तप्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (सोन चिरैया) इस उद्यान में अच्छी खासी संख्या में मौजूद हैं। यह क्षेत्र मरुस्थल के प्रवासी एवं स्थानीय पक्षियों का सुरक्षित आश्रयस्थल बना हुआ है। यहां उकाब, बाज़, चील, लंबे पांव और चोंच वाले अनेक प्रकार के शिकारी पक्षियों के अलावा गिध्दों का दीदार आसानी से हो जाता है। विविध रंगरूप, पंखों और पंजों की बनावट वाले चील, उकाब, बाज़ और गिध्द यहां पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। शाही मरु तीतर छोटे-छोटे तलाबों और झीलों के आसपास देखे जा सकते हैं। बटेर, मधुमक्खी- भक्षी, लवा (भरत पक्षी) और इस तरह की अनेक प्रजातियां यहां सर्वत्र देखी जा सकती हैं, जबकि लंबी गर्दन वाले सारस और बगुले जाड़ों में ही दिखाई देते हैं। नीली दुम वाले और हरे मधुभक्षी पक्षियों के अलावा अनेक प्रकार के सामान्य और दुर्लभ तीतर-बटेर पक्षीप्रेमियों के आकर्षण का केन्द्र बने हुए हैं। इस उद्यान में शीतकाल में अनेक प्रवासी पक्षी भी अपना बसेरा बनाते नज़र आते हैं।
उद्यान की वनस्पतियों और पेड़-पौधों की प्रजातियों में धोक, रोंज, सलाई और ताड़ के वृक्ष प्रमुख हैं। वनस्पतियां बिखरी और छितरी हुई हैं । आक की झाड़ियों और सेवान घास से भरे छोटे-छोटे भूखंड भी यत्र-तत्र दिखाई देते हैं।
मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान में पशुओं और पौधों के जीवाश्मों के ढेर लगे हैं । कहते हैं कि ये जीवाश्म 18 करोड़ वर्ष पुराने हैं। डायनासोर के 60 लाख वर्ष पुराने जीवाश्म भी इस क्षेत्र में पाए जाते हैं ।
मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान (डेज़र्ट नेशनल पार्क) के वन्यजीवों में ब्लैक बक (काला हिरण), चिंकारा, रेगिस्तानी लोमड़ी, बंगाल लोमड़ी, भारतीय भेड़िया, रेगिस्तानी बिल्ली, खरगोश आदि प्रमुख हैं। सांप भी यहां खूब पाए जाते हैं। अनेक प्रकार की छिपकलियां, गिरगिट , रूसेल वाइपर, करैत जैसे जहरीले सांपों की अन्य कई प्रजातियां भी यहां पाई जाती हैं।
राजस्थान सरकार ने जैसलमेर जिले के इस उद्यान का 4 अगस्त, 1980 को जारी अपनी अधिसूचना क्रमांक एफ-3(1)(73) संशो. के जरिये इसे मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान अर्थात डेजर्ट नेशनल पार्क के रूप में अधिसूचित किया था। इससे पूर्व यह मरुभूमि वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता था। अपने पर्यावरणीय और वानस्पतिक, महत्व के कारण ही इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्रदान किया गया है, ताकि उद्यान में रहने वाले वन्यजीवों और इस राष्ट्रीय उद्यान के पर्यावरण का संरक्षण, प्रचार और विकास भलीभांति किया जा सके।


.jpg)