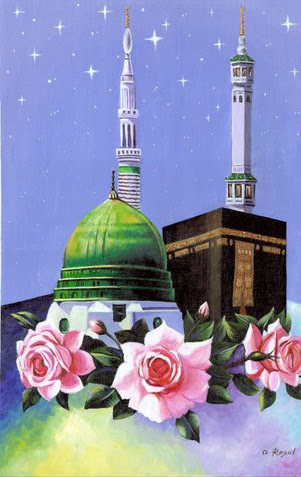डॉ. फ़िरदौस ख़ान
हर भाषा की अपनी अहमियत होती है। फिर भी मातृभाषा हमें सबसे प्यारी होती है, क्योंकि उसी ज़ुबान में हम बोलना सीखते हैं। बच्चा सबसे पहले मां ही बोलता है। इसलिए भी मां बोली हमें सबसे अज़ीज़ होती है। लेकिन देखने में आता है कि कुछ लोग जिस भाषा के सहारे ज़िन्दगी बसर करते हैं, यानी जिस भाषा में लोगों से संवाद क़ायम करते हैं, उसी को 'तुच्छ' समझते हैं। बार-बार अपनी मातृभाषा का अपमान करते हुए अंग्रेजी की तारीफ़ में क़सीदे पढ़ते हैं। हिन्दी के साथ ऐसा सबसे ज़्यादा हो रहा है। वे लोग जिनके पुरखे अंग्रेजी का 'ए' नहीं जानते थे, वे भी हिन्दी को गरियाते हुए मिल जाएंगे। हक़ीक़त में ऐसे लोगों को न तो ठीक से हिन्दी आती है और न ही अंग्रेजी। दरअसल, वह तो हिन्दी को गरिया कर अपनी 'कुंठा' का 'सार्वजनिक प्रदर्शन' करते रहते हैं।
अंग्रेजी भी अच्छी भाषा है। इंसान को अंग्रेजी ही नहीं, दूसरी देसी-विदेशी भाषाएं भी सीखनी चाहिए। इल्म हासिल करना तो अच्छी बात है, लेकिन अपनी मातृभाषा की क़ुर्बानी देकर किसी दूसरी भाषा को अपनाए जाने को किसी भी सूरत में जायज़ नहीं ठहराया जा सकता है। यह अफ़सोस की बात है कि हमारे देश में हिंदी और दूसरी क्षेत्रीय भाषाओं की लगातार अनदेखी की जा रही है। हालत यह है कि अब तो गांव-देहात में भी अंग्रेज़ी का चलन बढ़ने लगा है। पढ़े-लिखे लोग अपनी मातृभाषा में बात करना पसंद नहीं करते, उन्हें लगता है कि अगर वे ऐसा करेंगे तो गंवार कहलाएंगे। क्या अपनी संस्कृति की उपेक्षा करने को सभ्यता की निशानी माना जा सकता है, क़तई नहीं। हमें ये बात अच्छे से समझनी होगी कि जब तक हिन्दी भाषी लोग ख़ुद हिन्दी को सम्मान नहीं देंगे, तब तक हिन्दी को वो सम्मान नहीं मिल सकता, जो उसे मिलना चाहिए।
देश को आज़ाद हुए साढ़े सात दशक बीत चुके हैं। इसके बावजूद अभी तक हिन्दी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा हासिल नहीं हो पाया है। यह बात अलग है कि हर साल 14 सितम्बर को हिन्दी दिवस पर कार्यक्रमों का आयोजन कर रस्म अदायगी कर ली जाती है। हालत यह है कि कुछ लोग तो अंग्रेज़ी में भाषण देकर हिन्दी की दुर्दशा पर घड़ियाली आंसू बहाने से भी नहीं चूकते।
हमारे देश भारत में बहुत सी भाषायें और बोलियां हैं। इसलिए यहां यह कहावत बहुत प्रसिद्ध है- कोस-कोस पर पानी बदले, चार कोस पर वाणी। भारतीय संविधान में भारत की कोई राष्ट्र भाषा नहीं है। हालांकि केन्द्र सरकार ने 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में स्थान दिया है। इसमें केन्द्र सरकार या राज्य सरकार अपने राज्य के मुताबिक़ किसी भी भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में चुन सकती है। केन्द्र सरकार ने अपने काम के लिए हिन्दी और रोमन भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में जगह दी है। इसके अलावा राज्यों ने स्थानीय भाषा के मुताबिक़ आधिकारिक भाषाओं को चुना है। इन 22 आधिकारिक भाषाओं में असमी, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संतली, सिंधी, तमिल, तेलुगू, बोड़ो, डोगरी, बंगाली और गुजराती शामिल हैं।
ग़ौरतलब है कि संवैधानिक रूप से हिन्दी भारत की प्रथम राजभाषा है। यह देश की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। स्टैटिस्टा के मुताबिक़ दुनियाभर में हिन्दी भाषा तेज़ी से बढ़ रही है। साल 1900 से 2021 के दौरान इसकी रफ़्तार 175.52 फ़ीसदी रही, जो अंग्रेज़ी की रफ़्तार 380.71 फ़ीसदी के बाद सबसे ज़्यादा है। अंग्रेज़ी और मंदारिन भाषा के बाद हिन्दी दुनिया की तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। साल 1961 में ही हिन्दी दुनिया की तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा बन गई। उस वक़्त दुनियाभर में 42.7 करोड़ लोग हिन्दी बोलते थे। साल 2021 में यह तादाद बढ़कर 117 करोड़ हो गई। इनमें से 53 करोड़ लोगों की मातृभाषा हिन्दी है। हालत यह है कि हिन्दी अब शीर्ष 10 कारोबारी भाषाओं में शामिल है। इतना ही नहीं दुनियाभर के 10 सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले अख़बारों में शीर्ष-6 हिन्दी के अख़बार हैं। भारत के अलावा 260 से ज़्यादा विश्वविद्यालयों में हिन्दी पढ़ाई जा रही है। विदेशों में 28 हज़ार से ज़्यादा शिक्षण संस्थान हिन्दी भाषा सिखा रहे हैं। हिन्दी का व्याकरण सर्वाधिक वैज्ञानिक माना जाता है। हिन्दी का श्ब्द भंडार भी बहुत विस्तृत है। अंग्रेज़ी में जहां 10 हज़ार शब्द हैं, वहीं हिन्दी में इसकी तादाद अढ़ाई लाख बताई जाती है। हिन्दी मुख्यतः देवनागरी में लिखी जाती है, लेकिन अब इसे रोमन में भी लिखा जाने लगा है। मोबाइल संदेश और इंटरनेट से हिन्दी को काफ़ी बढ़ावा मिल रहा है। सोशल मीडिया पर भी हिन्दी का ख़ूब चलन है। गूगल पर हिन्दी के 10 लाख करोड़ से ज़्यादा पन्ने मौजूद हैं।
देश में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा होने के बाद भी हिन्दी राष्ट्रीय भाषा नहीं बन पाई है। हिन्दी हमारी राजभाषा है। राष्ट्रीय और आधिकारिक भाषा में काफ़ी फ़र्क़ है। जो भाषा किसी देश की जनता, उसकी संस्कृति और इतिहास को बयान करती है, उसे राष्ट्रीय या राष्ट्रभाषा भाषा कहते हैं। मगर जो भाषा कार्यालयों में उपयोग में लाई जाती है, उसे आधिकारिक भाषा कहा जाता है। इसके अलावा अंग्रेज़ी को भी आधिकारिक भाषा का दर्जा हासिल है।
संविधान के अनुचछेद-17 में इस बात का ज़िक्र है कि आधिकारिक भाषा को राष्ट्रीय भाषा नहीं माना जा सकता है। भारत के संविधान के मुताबिक़ देश की कोई भी अधिकृत राष्ट्रीय भाषा नहीं है। यहां 23 भाषाओं को आधिकारिक भाषा के तौर पर मंज़ूरी दी गई है। संविधान के अनुच्छेद 344 (1) और 351 के मुताबिक़ भारत में अंग्रेज़ी सहित 23 भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें आसामी, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू शामिल हैं। ख़ास बात यह भी है कि राष्ट्रीय भाषा तो आधिकारिक भाषा बन जाती है, लेकिन आधिकारिक भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाने के लिए क़ानूनी तौर पर मंज़ूरी लेना ज़रूरी है। संविधान में यह भी कहा गया है कि यह केंद्र का दायित्व है कि वह हिन्दी के विकास के लिए निरंतर प्रयास करे। विभिन्नताओं से भरे भारतीय परिवेश में हिन्दी को जनभावनाओं की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम बनाया जाए।
भारतीय संविधान के मुताबिक़ कोई भी भाषा, जिसे देश के सभी राज्यों द्वारा आधिकारिक भाषा के तौर पर अपनाया गया हो, उसे राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया जाता है। मगर हिन्दी इन मानकों को पूरा नहीं कर पा रही है, क्योंकि देश के सिर्फ़ 10 राज्यों ने ही इसे आधिकारिक भाषा के तौर पर अपनाया है, जिनमें बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश शामिल है। इन राज्यों में उर्दू को सह-राजभाषा का दर्जा दिया गया है। उर्दू जम्मू-कश्मीर की राजभाषा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में हिन्दी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है। संविधान के लिए अनुच्छेद 351 के तहत हिन्दी के विकास के लिए विशेष प्रावधान किया गया है।
ग़ौरतलब है कि देश में 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। देश में हिन्दी और अंग्रेज़ी सहित 18 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा हासिल है, जबकि यहां क़रीब 800 बोलियां बोली जाती हैं। दक्षिण भारत के राज्यों ने स्थानीय भाषाओं को ही अपनी आधिकारिक भाषा बनाया है। दक्षिण भारत के लोग अपनी भाषाओं के प्रति बेहद लगाव रखते हैं, इसके चलते वे हिन्दी का विरोध करने से भी नहीं चूकते। साल 1940-1950 के दौरान दक्षिण भारत में हिन्दी के ख़िलाफ़ कई अभियान शुरू किए गए थे। उनकी मांग थी कि हिन्दी को देश की राष्ट्रीय भाषा का दर्जा न दिया जाए।
संविधान सभा द्वारा 14 सितम्बर, 1949 को सर्वसम्मति से हिन्दी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया था। तब से केन्द्रीय सरकार के देश-विदेश स्थित समस्त कार्यालयों में प्रतिवर्ष 14 सितम्बर हिन्दी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसीलिए हर साल 14 सितम्बर को हिन्दी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 343 (1) के मुताबिक़ भारतीय संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपी देवनागरी होगी। साथ ही अंकों का रूप अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप यानी 1, 2, 3, 4 आदि होगा। संसद का काम हिन्दी और अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं में किया जा सकता है, मगर राज्यसभा या लोकसभा के अध्यक्ष विशेष परिस्थिति में सदन के किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकते हैं। संविधान के अनुच्छोद 120 के तहत किन प्रयोजनों के लिए केवल हिन्दी का इस्तेमाल किया जाना है, किनके लिए हिन्दी और अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं का इस्तेमाल ज़रूरी है और किन कार्यों के लिए अंग्रेज़ी भाषा का इस्तेमाल किया जाना है। यह राजभाषा अधिनियम-1963, राजभाषा अधिनियम-1976 और उनके तहत समय-समय पर राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय की ओर से जारी किए गए दिशा-निर्देशों द्वारा निर्धारित किया गया है।
पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव के कारण अंग्रेज़ी भाषा हिन्दी पर हावी होती जा रही है। अंग्रेज़ी को स्टेट्स सिंबल के तौर पर अपना लिया गया है। लोग अंग्रेज़ी बोलना शान समझते हैं, जबकि हिन्दी भाषी व्यक्ति को पिछड़ा समझा जाने लगा है। हैरानी की बात तो यह भी है कि देश की लगभग सभी बड़ी प्रतियोगी परीक्षाएं अंग्रेज़ी में होती हैं। इससे हिन्दी भाषी योग्य प्रतिभागी इसमें पिछड़ जाते हैं। अगर सरकार हिन्दी भाषा के विकास के लिए गंभीर है, तो इस भाषा को रोज़गार की भाषा बनाना होगा। आज अंग्रेज़ी रोज़गार की भाषा बन चुकी है। अंग्रेज़ी बोलने वाले लोगों को नौकरी आसानी से मिल जाती है। इसलिए लोग अंग्रेज़ी के पीछे भाग रहे हैं। आज छोटे क़स्बों तक में अंग्रेज़ी सिखाने की 'दुकानें' खुल गई हैं। अंग्रेज़ी भाषा नौकरी की गारंटी और योग्यता का 'प्रमाण' बन चुकी है। अंग्रेज़ी शासनकाल में अंग्रेज़ों ने अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए अंग्रेज़ियत को बढ़ावा दिया था, मगर आज़ाद देश में मैकाले की शिक्षा पध्दति को क्यों ढोया जा रहा है, यह समझ से परे है।
हिन्दी के विकास में हिन्दी साहित्य के अलावा हिन्दी पत्रकारिता का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसके अलावा हिन्दी सिनेमा ने भी हिन्दी के प्रचार-प्रसार को बढ़ावा दिया है। मगर अब सिनेमा की भाषा भी 'हिन्गलिश' होती जा रही है। छोटे पर्दे पर आने वाले धारावाहिकों में ही बिना वजह अंग्रेज़ी के वाक्य ठूंस दिए जाते हैं। हिन्दी सिनेमा में काम करके अपनी रोज़ी-रोटी कमाने वाले कलाकार भी हर जगह अंग्रेज़ी में ही बोलते नज़र आते हैं। आख़िर क्यों हिन्दी को इतनी हेय दृष्टि से देखा जाने लगा है? यह एक ज्वलंत प्रश्न है।
अधिकारियों का दावा है कि हिन्दी राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, जनभाषा के सोपानों को पार कर विश्व भाषा बनने की ओर अग्रसर है, मगर देश में हिन्दी की जो हालत है, वो जगज़ाहिर है। साल में एक दिन को ‘हिन्दी दिवस’ के तौर पर मना लेने से हिन्दी का भला होने वाला नहीं है। इसके लिए ज़रूरी है कि हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए ज़मीनी स्तर पर ईमानदारी से काम किया जाए।
रूस में अपनी मातृभाषा भूलना बहुत बड़ा शाप माना जाता है। एक महिला दूसरी महिला को कोसते हुए कहती है- अल्लाह, तुम्हारे बच्चों को उनकी मां की भाषा से वंचित कर दे। अल्लाह तुम्हारे बच्चों को उनसे महरूम कर दे, जो उन्हें उनकी ज़ुबान सिखा सकता हों। नहीं, अल्लाह तुम्हारे बच्चों को उससे महरूम करे, जिसे वे अपनी ज़ुबान सिखा सकते हों। मगर पहा़डों में तो किसी तरह के शाप के बिना भी उस आदमी की कोई इज्ज़त नहीं रहती, जो अपनी ज़ुबान की इज्ज़त नहीं करता। पहाड़ी मां विकृत भाषा में लिखी अपने बेटे की कविताएं नहीं पढ़ेगी। रूस के प्रसिद्ध लेखक रसूल हमज़ातोव ने अपनी किताब मेरा दाग़िस्तान में ऐसे कई क़िस्सों का ज़िक्र किया है, जो मातृभाषा से जुड़े हैं। कैस्पियन सागर के पास काकेशियाई पर्वतों की ऊंचाइयों पर बसे दाग़िस्तान के एक छोटे से गांव त्सादा में जन्मे रसूल हमज़ातोव को अपने गांव, अपने प्रदेश, अपने देश और उसकी संस्कृति से बेहद लगाव रहा है। मातृभाषा की अहमियत का ज़िक्र करते हुए ‘मेरा दाग़िस्तान’ में वह लिखते हैं, मेरे लिए विभिन्न जातियों की भाषाएं आकाश के सितारों के समान हैं। मैं नहीं चाहता कि सभी सितारे आधे आकाश को घेर लेने वाले अतिकाय सितारे में मिल जाएं। इसके लिए सूरज है, मगर सितारों को भी तो चमकते रहना चाहिए। हर व्यक्ति को अपना सितारा होना चाहिए। मैं अपने सितारे अपनी अवार मातृभाषा को प्यार करता हूं। मैं उन भूतत्वेत्ताओं पर विश्वास करता हूं, जो यह कहते हैं कि छोटे-से पहाड़ में भी बहुत-सा सोना हो सकता है।
एक बेहद दिलचस्प वाक़िये के बारे में वह लिखते हैं, किसी बड़े शहर मास्को या लेनिनग्राद में एक लाक घूम रहा था। अचानक उसे दाग़िस्तानी पोशाक पहने एक आदमी दिखाई दिया। उसे तो जैसे अपने वतन की हवा का झोंका-सा महसूस हुआ, बातचीत करने को मन ललक उठा। बस भागकर हमवतन के पास गया और लाक भाषा में उससे बात करने लगा। इस हमवतन ने उसकी बात नहीं समझी और सिर हिलाया। लाक ने कुमीक, फिर तात और लेज़गीन भाषा में बात करने की कोशिश की। लाक ने चाहे किसी भी ज़बान में बात करने की कोशिश क्यों न की, दाग़िस्तानी पोशाक में उसका हमवतन बातचीत को आगे न बढ़ा सका। चुनांचे रूसी भाषा का सहारा लेना पड़ा। तब पता चला कि लाक की अवार से मुलाक़ात हो गई थी। अवार अचानक ही सामने आ जाने वाले इस लाक को भला-बुरा कहने और शर्मिंदा करने लगा। तुम भी कैसे दाग़िस्तानी, कैसे हमवतन हो, अगर अवार भाषा ही नहीं जानते, तुम दाग़िस्तानी नहीं, मूर्ख ऊंट हो। इस मामले में मैं अपने अवार भाई के पक्ष में नहीं हूं। बेचारे लाक को भला-बुरा कहने का उसे कोई हक़ नहीं था। अवार भाषा की जानकारी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अहम बात यह है कि उसे अपनी मातृभाषा, लाक भाषा आनी चाहिए। वह तो दूसरी कई भाषाएं जानता था, जबकि अवार को वे भाषाएं नहीं आती थीं।
अबूतालिब एक बार मास्को में थे। सड़क पर उन्हें किसी राहगीर से कुछ पूछने की आवश्यकता हुई। शायद यही कि मंडी कहां है? संयोग से कोई अंग़्रेज़ ही उनके सामने आ गया। इसमें हैरानी की तो कोई बात नहीं। मास्को की सड़कों पर तो विदेशियों की कोई कमी नहीं है।
अंग्रेज़ अबूतालिब की बात न समझ पाया और पहले तो अंग्रेज़ी, फिर फ्रांसीसी, स्पेनी और शायद दूसरी भाषाओं में भी पूछताछ करने लगा। अबूतालिब ने शुरू में रूसी, फिर लाक, अवार, लेज़गीन, दार्ग़िन और कुमीक भाषाओं में अपनी बात को समझाने की कोशिश की। आख़िर एक-दूसरे को समझे बिना वे दोनों अपनी-अपनी राह चले गए। एक बहुत ही सुसंस्कृत दाग़िस्तानी ने जो अंग्रेज़ी भाषा के ढाई शब्द जानता था, बाद में अबूतालिब को उपदेश देते हुए यह कहा-देखो संस्कृति का क्या महत्व है। अगर तुम कुछ अधिक सुसंस्कृत होते तो अंग्रेज़ से बात कर पाते। समझे न? समझ रहा हूं। अबूतालिब ने जवाब दिया। मगर अंग्रेज़ को मुझसे अधिक सुसंस्कृत कैसे मान लिया जाए? वह भी तो उनमें से एक भी ज़ुबान नहीं जानता था, जिनमें मैंने उससे बात करने की कोशिश की?
रसूल हमज़ातोव लिखते हैं, एक बार पेरिस में एक दाग़िस्तानी चित्रकार से मेरी भेंट हुई। क्रांति के कुछ ही समय बाद वह पढ़ने के लिए इटली गया था, वहीं एक इतावली लड़की से उसने शादी कर ली और अपने घर नहीं लौटा। पहाड़ों के नियमों के अभ्यस्त इस दाग़िस्तानी के लिए अपने को नई मातृभूमि के अनुरूप ढालना मुश्किल था। वह देश-देश में घूमता रहा, उसने दूर-दराज़ के अजनबी मुल्कों की राजधानियां देखीं, मगर जहां भी गया, सभी जगह घर की याद उसे सताती रही। मैंने यह देखना चाहा कि रंगों के रूप में यह याद कैसे व्यक्त हुई है। इसलिए मैंने चित्रकार से अपने चित्र दिखाने का अनुरोध किया। एक चित्र का नाम ही था मातृभूमि की याद। चित्र में इतावली औरत (उसकी पत्नी) पुरानी अवार पोशाक में दिखाई गई थी। वह होत्सातल के मशहूर कारीगरों की नक़्क़ाशी वाली चांदी की गागर लिए एक पहाड़ी चश्मे के पास खड़ी थी। पहाड़ी ढाल पर पत्थरों के घरों वाला उदास-सा अवार गांव दिखाया गया था और गांव के ऊपर पहाड़ी चोटियां कुहासे में लिपटी हुई थीं। पहाड़ों के आंसू ही कुहासा है-चित्रकार ने कहा, वह जब ढालों को ढंक देता है, तो चट्टानों की झुर्रियों पर उजली बूंदें बहने लगती हैं। मैं कुहासा ही हूं। दूसरे चित्र में मैंने कंटीली जंगली झाड़ी में बैठा हुआ एक पक्षी देखा। झाड़ी नंगे पत्थरों के बीच उगी हुई थी। पक्षियों को गाता हुआ दिखाया गया था और पहाड़ी घर की खिड़की से एक उदास पहाडिन उसकी तरफ़ देख रही थी। चित्र में मेरी दिलचस्पी देखकर चित्रकार ने स्पष्ट किया-यह चित्र पुरानी अवार की किंवदंती के आधार पर बनाया गया है।
किस किंवदंती के आधार पर?
एक पक्षी को पकड़कर पिंजरे में बंद कर दिया गया। बंदी पक्षी दिन-रात एक ही रट लगाए रहता था-मातृभूमि, मेरी मातृभूमि, मातृभूमि… बिल्कुल वैसे ही, जैसे कि इन तमाम सालों के दौरान मैं भी यह रटता रहा हूं। पक्षी के मालिक ने सोचा, जाने कैसी है उसकी मातृभूमि, कहां है? अवश्य ही वह कोई फलता-फूलता हुआ बहुत ही सुन्दर देश होगा, जिसमें स्वार्गिक वृक्ष और स्वार्गिक पक्षी होंगे। तो मैं इस परिन्दे को आज़ाद कर देता हूं, और फिर देखूंगा कि वह किधर उड़कर जाता है। इस तरह वह मुझे उस अद्भुत देश का रास्ता दिखा देगा। उसने पिंजरा खोल दिया और पक्षी बाहर उड़ गया। दस एक क़दम की दूरी पर वह नंगे पत्थरों के बीच उगी जंगली झाड़ी में जा बैठा। इस झाड़ी की शाख़ाओं पर उसका घोंसला था। अपनी मातृभूमि को मैं भी अपने पिंजरे की खिड़की से ही देखता हूं। चित्रकार ने अपनी बात ख़त्म की।
तो आप लौटना क्यों नहीं चाहते?
देर हो चुकी है। कभी मैं अपनी मातृभूमि से जवान और जोशीला दिल लेकर आया था। अब मैं उसे सिर्फ़ बूढ़ी हड्डियां कैसे लौटा सकता हूं?
रसूल हमज़ातोव ने अपनी कविताओं में भी अपनी मातृभाषा का गुणगान किया है। अपनी एक कविता में वह कहते हैं-
मैंने तो अपनी भाषा को सदा हृदय से प्यार किया है
हमें भी अपनी मातृ भाषा के प्रति अपने दिल में यही जज़्बा पैदा करना होगा।
(लेखिका स्टार न्यूज़ एजेंसी में सम्पादक हैं)
जमशेद क़मर सिद्दीक़ी
मुसलमानों में एक नया 'बुद्धिजीवी' वर्ग पैदा हो गया है जिसे मुसलमानों की हर मकामी रवायत 'जहालत' लगती है। इनकी खुद की कुल तालीम बस इतनी है कि इन्होंने इर्तगुल गाज़ी के सारे सीज़न देखे हैं और मोहल्ले के लड़कों के साथ गश्त लगाई है। इन्हें लगता है कि ताज़िये के साथ निकलती भीड़, अलम उठाते हुए नौजवान, अशरे पर होने वाले मातम, मज़ारों पर होने वाली कव्वाली, मोहल्लों में होने वाली करतबबाज़ी - ये सब जहालत है। बस ये एक बड़े तालीमयाफ़्ता हैं, बाकी सब जाहिल।
असल बात ये है कि इन्हें मालूम ही नहीं कि ये मज़हब नहीं मआशरी अमल हैं। एक खित्ते का स्थानीयता का रंग है, लोकल हिस्ट्री का कनेक्शन है जो बाप दादा सदियों से करते आए हैं। उसका एक कॉनटेक्स्ट है। हिंदुस्तान सैकड़ों तहज़ीबों से मिलकर बना एक मुल्क है। यहां हर चार कोस पर मज़हब के साथ नई तरह की आंचलिकता जुड़ी है। आप एक ही रंग की तहज़ीब हर जगह नहीं पा सकते। अगर आप के लिहाज़ से सफेद कुर्ता पायजामे पर काली सदरी पहनकर मस्जिद तक जाना और लौट आने के अलावा सब कुछ 'जहालत' है तो जाहिल आप हैं। जिसे नहीं पता मज़हब और माशरत के बीच का फर्क। ये वो मुल्क है जहां समाज और मज़हब इतने गुंधे हुए हैं कि हर कल्चर एक दूसरे के थोड़े थोड़े रंग सजाए है। मुसलमानों की शादियों में दुल्हन हिंदू संस्कृति में शुभ माने जाने वाला लाल जोड़ा पहनती है और हिंदुओं की शादी में दूल्हा मुसलमानों के बीच मोहज़्ज़ब मानी जाने वाली शेरवानी। इसी देश में में उन ब्रह्मणों के वंशज मौजूद हैं जो कर्बला में इमाम हुसैन के साथ जंग लड़े और इसी देश में वो सूफी भी हैं जिन्होंने खुदा को अपना महबूब कह दिया और आज उनकी मज़ारों की लोग ज़ियारत करते हैं।
लखनऊ में किन्नरों का समाज भी अपना ताज़िया निकालता है। सफेद कपड़ों में किन्नर कर्बला की जंग को याद करते हुए गाते-बजाते निकलते हैं बीसियों साल से। छोट छोटे मुहल्लों के चौराहों पर लोग कर्बला में इमाम हुसैन को मिले दर्द को याद करते हुए करतबबाज़ी करते हैं, इन स्टंट के ज़रिये वो अपनी जान जोखिम में डालते हैं उस डर को महसूस करते हैं जो यज़ीद की भारी-भरकम फौज का सामना करने पहले एक बार लश्कर के दिल में आया होगा। ये उस ज़मीन की तहज़ीब हैं जिसने मज़हब को सिर्फ़ किताब से नहीं, हज़ारों सालों की तहज़ीब के रंग में जिया है।लेकिन अफ़सोस ये है कि आज तारिक मसूद को सुनकर नौजवान हुआ मुसलमान इसे फितना कहकर न सिर्फ खारिज करता है, उन्हें मिटाने पर भी आमादा है। इन्हें लगता है कि मज़हब महज़ एक क्लीन कट, मिनिमलिस्ट आइडिया है जिसमें लोकल कल्चर की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। इनकी समझ में धर्म का रिश्ता ज़मीन से नहीं, सिर्फ़ स्क्रीन से है। इनके इस्लाम का मरकज़ किताबें नहीं, क्लिपिंग्सौ हैं। ये सोचते हैं कि अगर कोई मज़ार पर चादर चढ़ा रहा है, या कोई बच्चा अलम को माथा टेक रहा है, तो वह जाहिल है।
हक़ीक़त ये है कि ये रस्में, ये रवायतें, ये लोक-तहज़ीब — ये सब मिलकर ही तो हिंदुस्तानी इस्लाम को मुकम्मल बनाती हैं। सिर्फ़ अरबी पहनावा, या टीवी वाले तुर्की किरदार देखकर किसी तहज़ीब को “शुद्ध” नहीं कहा जा सकता। क्योंकि इस मुल्क में इस्लाम सिर्फ़ मदीना से नहीं आया — वो यहां के खेतों, खलिहानों, बाज़ारों, फकीरों, दरवेशों, दस्तकारों और बाप-दादाओं की नसीहतों के ज़रिए फैला है।
जो लोग इन रवायतों को जहालत कहते हैं, उन्हें दरअसल अपने वजूद की जड़ों से डर लगता है। उन्हें हर वो चीज़ खटकती है जो इस्लाम को इस ज़मीन का बनाती है। ये दरअसल ‘सांस्कृतिक हीनभावना’ है — जो अपने भीतर की परंपराओं से भागती है, और बाहर की चमक को असली मान लेती है।
इसलिए याद रखिए मज़हब और माशरत का रिश्ता गहरा है। इसे अपनी पीढ़ियों और शिजरों की रौशनी में समझिये। ये हमारा लोकल कल्चर है जो हर दस मील पर बदलता है, इसका रंग, ज़ंबान अंदाज़ और तरीका सब बदलता है। ये अच्छी बुरी जैसी भी हैं हमारी जड़े हैं और जो इसे जहालत कहे वो खुद जाहिल है।
इनके बावजूद हम इस्लाम में विभाजन पाते हैं, जिन्हें कई लेखकों ने अलग-अलग संप्रदायों के रूप में वर्णित किया है। जिस अर्थ में 'संप्रदाय' शब्द का उपयोग अन्य धर्मों में किया जाता है, वह शायद इस्लाम पर लागू नहीं होता है। इसलिए, हम उचित अभिव्यक्ति के लिए अभिव्यक्ति के हल्के अर्थ पर विचार करते हुए "विचारधारा" शब्द का उपयोग करेंगे। विभाजन का निहितार्थ। हम कई कारणों से हल्की अभिव्यक्ति का उपयोग कर रहे हैं। सबसे
पहले, इस्लाम किसी भी अन्य धर्म के लिए अज्ञात भाईचारे का पालन करता है।
दूसरे, इस्लाम में विभाजन बहुत अधिक बुनियादी सिद्धांतों पर आधारित नहीं हैं। सख्त बुनियादी सिद्धांतों में लोगों के बीच अलग-अलग विभाजन हैं मुसलमान असहमत नहीं हैं। तीसरा, इस्लाम में विभाजन के कारण अन्य धर्मों से बहुत अलग हैं। अन्य धर्मों में संप्रदायों की उत्पत्ति व्यवस्था की अपूर्णता और मानवीय आवश्यकताओं के साथ इसकी असंगति के कारण हुई, जो मानव के गलत दृष्टिकोण से उत्पन्न हुई प्रकृति। लेकिन इस्लाम में विभाजन राजनीतिक विचारों और विदेशी प्रभावों के कारण उत्पन्न हुए।
अपने दृष्टिकोण के समर्थन में हम यहां कुछ महान प्राच्यविदों के लेखन को उद्धृत कर सकते हैं।
ए अली के शब्दों को उद्धृत करने के लिए, "ईसाई धर्म में जिन बुराइयों की हम निंदा करते हैं, वे व्यवस्था की अपूर्णता को जन्म देती हैं। और मानव आवश्यकताओं के साथ इसकी असंगति में, इस्लाम में, जिन बुराइयों का हमें वर्णन करना होगा, वे लालच से उत्पन्न हुई हैं।" सांसारिक उन्नति, और
व्यक्तियों और वर्गों की क्रांतिकारी प्रवृत्ति नैतिक कानून और व्यवस्था के प्रति असंतुलित है।" कुछ गैर-मुस्लिम आधुनिक लेखक भी इस तर्क का समर्थन करते हैं।
एच.ए.आर. गिब कहते हैं, "किसी भी महान धार्मिक समुदाय के पास कभी भी पूरी तरह से कैथोलिक भावना नहीं थी या वह इससे अधिक तैयार नहीं था। अपने सदस्यों को व्यापक स्वतंत्रता की अनुमति देने के लिए, केवल यह कि वे कम से कम बाहरी रूप से, विश्वास के न्यूनतम दायित्वों को स्वीकार करते हैं। यह कहना कठोर सत्य की सीमा से बहुत आगे जाना नहीं होगा, वास्तव में धार्मिक संप्रदायों के किसी भी समूह को रूढ़िवादी इस्लामी समुदाय से कभी भी बाहर नहीं रखा गया है, लेकिन जो लोग इस तरह के बहिष्कार की इच्छा रखते थे और जैसा कि यह था, उन्हें स्वयं बाहर रखा गया था। मौड रॉयडेन का कहना है: "मोहम्मद के धर्म ने मनुष्य के दिमाग में कल्पना किए गए पहले वास्तविक लोकतंत्र की घोषणा की। उनका ईश्वर इतनी उत्कृष्ट महानता वाला था कि उसके सामने सभी सांसारिक मतभेद शून्य थे और यहां तक कि रंग की गहरी और क्रूर दरार भी समाप्त हो गई थी। अन्य जगहों की तरह मुसलमानों में भी सामाजिक स्तर हैं, बुनियादी तौर पर (अर्थात, आध्यात्मिक रूप से) सभी आस्तिक समान हैं: और यह मौलिक आध्यात्मिक समानता कोई कल्पना नहीं है जैसा कि ईसाइयों के बीच है; यह स्वीकृत है और वास्तविक है। यह बहुत हद तक फ़ॉस का कारण बनता है
इस्लाम की आत्मा', पृष्ठ 290, 2. "मुहम्मदवाद" पृष्ठ 119
2. विभिन्न विचारधाराओं के उदय के कारण
जैसा कि पहले ही संकेत दिया जा चुका है, इस्लाम में विभिन्न विचारधाराओं का उदय मुख्यतः राजनीतिक विचारों और विदेशी प्रभावों के कारण हुआ। लेकिन सभी अलग-अलग स्कूलों का उदय एक ही कारण से नहीं हुआ। किसी में एक कारण प्रमुख था तो किसी में दूसरा। मामले को स्पष्ट रूप से समझने के लिए कारणों को नीचे अलग से गिनाया गया है:
(जे) नेतृत्व के लिए प्रतिद्वंद्विता या विभिन्न समूह
इस्लाम में कुछ विचारधाराओं के उदय का श्रेय राजनीतिक कारणों से दिया जा सकता है। इसका मुख्य कारण नेतृत्व के लिए विभिन्न समूहों की प्रतिद्वंद्विता थी। अरब के पुराने जनजातीय झगड़े, विशेष रूप से उमैयद और हाशिम के झगड़े, जो उमैया और हाशिम के समय से हैं, ने इस कारक को बहुत बढ़ा दिया है।
पैगंबर ने स्पष्ट रूप से अपने उत्तराधिकारी को नामित नहीं किया। उन्होंने कोई पुरुष मुद्दा नहीं छोड़ा. उनकी एकमात्र जीवित संतान उनकी सबसे छोटी बेटी बीबी फातिमा थी, जिसका विवाह उनके चचेरे भाई और पालक पुत्र हज़रत अली से हुआ था। ऐसे अवसर थे जिनसे संकेत मिलता था कि पैगंबर चाहते थे कि 'अली' उनके उत्तराधिकारी बनें। वहीं दूसरी ओर। उनकी आखिरी बीमारी के दौरान अबू बक्र को उनकी ओर से प्रार्थना का नेतृत्व करने के लिए कहा गया था। इसके अलावा, पैगंबर की शिक्षाओं ने मुसलमानों में लोकतंत्र और पुरुषों के समान अधिकारों की भावना का संचार किया। इस प्रकार मुसलमानों ने एक नेता का चयन करने के लिए चुनाव के सिद्धांत को अपनाया और अबू बक्र को खलीफा (उत्तराधिकारी) के रूप में चुना गया। इस पद्धति ने मामले को स्थायी रूप से निपटाने के बजाय बढ़ावा दिया
1. फ़िलिस्तीन की समस्या पृ. 37.
विभिन्न दलों का विकास हुआ और इस प्रकार चुनाव की प्रक्रिया पर विभिन्न सिद्धांत विकसित हुए। जैसा कि हमेशा होता है, जब कोई गंभीर प्रश्न लोकप्रिय निर्णय के लिए खुला रखा जाता है, तो मुहम्मद की मृत्यु के बाद कई परस्पर विरोधी दल उभरे, साहसपूर्वक हम मुसलमानों के बीच चार अलग-अलग समूहों को देखते हैं: मुहाजिर, अंतर, उमय्यद और शयनकक्ष. महाजिर (खनन प्रवासी, अरबी बहुवचन अफुबजिरन) उन शुरुआती विश्वासियों के लिए थे जो मक्का से मदीना चले गए थे, वे इस्लाम स्वीकार करने वाले पहले व्यक्ति थे, हाशिमिड्स, यानी। ई... वह परिवार जिसमें पैगंबर का जन्म हुआ था, और कुरैश जनजाति के अन्य परिवारों के कुछ सदस्य उस समूह के थे। अंतर (समर्थकों) ने मदीना मुसलमानों के समूह का गठन किया, जिन्होंने पैगंबर को मदीना बुलाया जब उनके मक्का में बुरे दिन थे। मुहाजिरों और अंसार को एक ही नाम सहाबा (साथी) से जाना जाता था। मुहाजिरों में एलिड्स या लेजिटिमिस्ट भी थे। वैकल्पिक सिद्धांतों के विपरीत, शासन करने का दैवीय अधिकार माना जाता है। उमय्यद, जिनके पास इस्लाम-पूर्व दिनों में सत्ता और धन की बागडोर थी, ने बाद में उत्तराधिकार पर अपना अधिकार जमा लिया। इन समूहों के अलावा, रेगिस्तान के बेडौइन भी थे। जिन्होंने बाद में समग्र रूप से क़ुरैशों के ख़िलाफ़ अपना दावा पेश किया।
जैसा कि पहले ही हाशिमिड्स और के बीच प्रतिद्वंद्विता का संकेत दिया गया है
उमय्यद के बीच लंबी खींचतान थी। का मूल कारण
प्रतिद्वंद्विता का वर्णन एस. अंसार अली ने पांचवें में इस प्रकार किया है
फ़िहर के वंशज सेंचुरी रॉसे ने स्वयं को स्वामी बना लिया
मेक का, और धीरे-धीरे पूरा हिजाज़... कोसे की मृत्यु लगभग 480 ए.सी. में हुई और उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र अबल 1, हिटी पी.के. "अरबों का इतिहास पृष्ठ 139-140
उद-दार. अब्द उद-दार की मृत्यु के बाद मक्का के शासन की सफलता को लेकर उनके पोते और उनके भाई अब्द मनाफ के बेटों के बीच विवाद छिड़ गया। इस विवाद को अधिकार के विभाजन द्वारा सुलझाया गया था, मेसेस की जल आपूर्ति का प्रशासन और करों को बढ़ाने का काम अब्द मनाफ के पुत्र अब्द उश-शम्स को सौंपा गया था; जबकि किआब्स, परिषद-कक्ष और सैन्य मानक की संरक्षकता अब्द-उद-दार के पोते को दी गई थी।
अब्द उश-शम्स ने अधिकार अपने भाई हाशिम को हस्तांतरित कर दिया, जो मेकोस का एक प्रमुख गुर्गा और पुत्रवत व्यक्ति था, जो अजनबियों के प्रति अपनी उदारता के लिए विख्यात था। हिशिम की मृत्यु लगभग 510 ई.पू. में हुई और उसके बाद उसका भाई मुत्तलिब आया, जिसका उपनाम हिशिम का उदार पुत्र था।
इस बीच अब्द उद-दार के पोते अमीर हो रहे थे। जनता के बीच हाशिम के परिवार की स्थिति से ईर्ष्या करते हुए, वे पूरी सत्ता पर कब्ज़ा करने और खुद को मक्का का शासक बनाने की कोशिश कर रहे थे। उनके पक्ष में अब्द उश-शम्स का महत्वाकांक्षी पुत्र ओम्नेया था। लेकिन इसके बावजूद, अब्दुल मुत्तलिब के उच्च चरित्र और सभी कोराई लोगों द्वारा उनके प्रति सम्मान ने उन्हें लगभग उनतालीस वर्षों तक मक्का पर शासन करने में सक्षम बनाया। उन्हें सरकार में बुजुर्गों द्वारा सहायता प्रदान की गई, जो दस प्रमुख परिवारों के मुखिया थे।" (2) कुरान की व्याख्या में मतभेद।
कुरान और हदीस की व्याख्या में मतभेद के कारण कुछ अलग-अलग विचारधाराएँ उत्पन्न हुईं। पैगंबर की मृत्यु के बाद. वहाँ व्याख्या की आवश्यकता उत्पन्न होती है। जरूरत पड़ी सबसे पहले धर्म को विभिन्न पक्षों से समझने की और दूसरी उसे नई परिस्थितियों के साथ ढालने की-
1. सार्केन्स का एक संक्षिप्त इतिहास। पृष्ठ 5-7
नृत्य और जीवन की नई आवश्यकताएँ। इन व्याख्याओं की प्रक्रिया में मतभेद उत्पन्न हुए और इनसे विभिन्न विचारधाराओं का जन्म हुआ। इस्लाम के शुरुआती दौर में मुसलमान अलग-अलग जगहों पर अपने धर्म का प्रचार-प्रसार करने में विशेष रूप से व्यस्त थे। इसके अलावा, जब पैगंबर जीवित थे तो उन्हें अपने मन में उठने वाली समस्याओं का तुरंत समाधान मिल जाता था। इसलिए पैगम्बर की मृत्यु के बाद उन्हें जीवन की नई समस्याओं को समझाने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा। इसके अलावा अन्य धर्मों के साथ उनके संपर्क ने स्थिति को और अधिक गंभीर बना दिया। अधिकांश नए जीते गए स्थानों में इस्लाम को लंबे समय से स्थापित धार्मिक विचारों का विरोध करना पड़ा। इस प्रकार दूसरों से अपनी श्रेष्ठता को उचित ठहराने के लिए विभिन्न पक्षों से धर्म के अधीन खड़े होने की आवश्यकता उत्पन्न हुई। फिर, विभिन्न देशों में इस्लाम के विस्तार के साथ और समय बीतने के साथ नई परिस्थितियाँ और नई आवश्यकताएँ आईं। ऐसे में नई-नई व्याख्याओं की आवश्यकता बढ़ती गई।
(3) ज्ञान के विभिन्न स्रोतों पर विशेष जोर कुछ विचारधाराओं का उदय ज्ञान के विभिन्न स्रोतों पर दिए गए विशेष तनाव के कारण हुआ। अल-कुरान में ज्ञान के तीन स्रोतों का उल्लेख है-एजी (कारण), नागल (परंपरा) और कश्फ अंतर्ज्ञान)। इस्लाम के व्यापक दर्शन को तीन सूत्रों को एक साथ लेकर ही खड़ा किया जा सकता है। लेकिन लाइम के दौरान कुछ लोगों ने एक स्रोत पर जोर दिया और दूसरों की उपेक्षा की। इस प्रकार हम पाते हैं कि सोम: पैट ने 'अग्ल' और सोम: नग्ल पर विशेष जोर दिया, जबकि अन्य लोगों ने कशफ को ज्ञान का एकमात्र वास्तविक स्रोत माना।
4) धर्म को तर्कसंगत बनाने के प्रयास धर्म को तर्कसंगत बनाने और एक बौद्धिक प्रणाली के निर्माण के प्रयासों के कारण कुछ विचारधाराएँ उत्पन्न हुईं
जिस पर उसे खड़ा किया जा सके। इस्लाम के शुरुआती दिनों में, मुसलमान विभिन्न देशों में अपने विश्वास के प्रचार-प्रसार में विशेष रूप से व्यस्त थे। ऐसे में उनके पास आस्था के बारे में गहराई से सोचने का व्यावहारिक रूप से कोई समय नहीं था। लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता गया, उन्होंने आस्था के बारे में गंभीरता से सोचना शुरू कर दिया और एक बौद्धिक प्रणाली बनाने की कोशिश की। इसमें यूनानी दर्शन का प्रभाव प्रबल रूप से महसूस किया गया: (5) विदेशी विचारों का परिचय
इस्लाम में कुछ विभिन्न विद्यालयों के उदय का श्रेय विदेशी धार्मिक विचारों और अन्य विचारों को दिया जा सकता है। इस्लाम का इतिहास दर्शाता है कि खिलाफत की शुरुआत से ही इसने इस धर्म को स्वीकार करने वाले विभिन्न देशों में प्रचलित रीति-रिवाजों के प्रति सहिष्णुता के साथ काम किया। इस सहिष्णु रवैये ने मुसलमानों को विदेशी शिष्टाचार, रीति-रिवाजों और धार्मिक विचारों को अपनाने में बहुत मदद की। पैगंबर की मृत्यु के बाद बहुत ही कम समय में मुसलमानों ने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया-इस्लाम पूरे अरब, एशिया, उत्तरी अफ्रीका और फारस के पास फैल गया। इस्लाम को विभिन्न लोगों द्वारा स्वीकार किया गया जिनमें बहुत कम या कुछ भी समानता नहीं थी। प्रत्येक वेश्या को लंबे समय से स्थापित धर्मों का सामना करना पड़ा और इस तरह कई विदेशी धार्मिक विचारों को आत्मसात करना पड़ा जिसने मुस्लिम जीवन को सभी पहलुओं में प्रभावित किया। इनका आकार दो तरह से हुआ - मुसलमानों के बीच मतभेद, अमूर्त विषयों तक सीमित और विदेशी लोगों द्वारा इस्लाम में अपने धार्मिक विचारों को पढ़ने के प्रयासों में। (6) कुछ मुस्लिम पंडितों की विशिष्टता
रूढ़िवादी लोगों (अर्थात्, जो हदीस को मजबूती से मानते थे) के बीच विभिन्न विचारधाराओं के उदय का मुख्य कारण था
1. सी.एफ. शिबली नुमानी, 'इल्मु एल-कलाम। पृष्ठ 14-15.
मुस्लिम सिवंतों की विशिष्टता के लिए। सोम: मुस्लिम विद्वान हदीस की खोज और परीक्षण में इतने व्यस्त थे कि उनके पास दूसरों के साथ समस्याओं पर चर्चा करने के लिए व्यावहारिक रूप से समय नहीं था। इनमें से अधिकांश विद्वान विशेष स्थानों से प्राप्त हदीसों पर विशेष जोर देते थे और उन्हें अंतिम मानते थे। आगे। इनमें से प्रत्येक विद्वान के आसपास छात्रों का एक समूह था और इन छात्रों ने श्रीमान के शब्दों को सत्य के अंतिम शब्द के रूप में लिया। इस प्रकार कुछ विभिन्न विचारधाराओं का उदय हुआ
3. विभिन्न विद्यालयों का वर्गीकरण
चूंकि इस्लाम में विभिन्न विचारधाराओं के बीच कोई सख्त विभाजन नहीं है, इसलिए किसी भी प्रकार के विभाजन में कुछ अंतर विभाजन शामिल होगा। शाहरस्तानी, इस विषय पर शुरुआती लेखकों में से एक। विभिन्न विद्यालयों को कई सिद्धांतों के अनुसार वर्गीकृत करता है। इसमें बहुत अधिक क्रॉस-विभाजन शामिल है। क्रॉस-डिवीजन को कम करने के लिए, हम डिवीजनों को दूसरे तरीके से वर्गीकृत कर सकते हैं।
सबसे पहले इस्लाम में विभिन्न विचारधाराओं को तीन समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है - राजनीतिक। धार्मिक और दार्शनिक. निःसंदेह, इन विभाजनों को मजबूत नहीं कहा जा सकता। जो विद्यालय प्रारंभ में केवल राजनीतिक था, उसने बाद में परिस्थितियों के अनुसार अपना एक धर्मशास्त्र और अपना विशिष्ट दर्शन भी तैयार किया। वह स्कूल जो शुरू में केवल धार्मिक प्रतीत हो सकता है, अगर जांच की जाए तो नीचे राजनीतिक कारण दिखाई दे सकता है। दार्शनिक विद्यालयों के अपने धार्मिक विचार और राजनीतिक झुकाव भी थे। तो विभिन्न विद्यालयों का हमारा वर्गीकरण राजनीतिक, धर्मशास्त्रीय और में है
दार्शनिक बल्कि मनमाना है। मुख्य राजनीतिक स्कूल सुन्नी, शिया और हैं। सुन्नियों को मुक़ल्लिद और ग़ैर में विभाजित किया जा सकता है
मुक़ल्लिद. मुक़ल्लिड्स को चार प्रमुख स्कूलों हिनाउ, शफी', मिलिकी और हनबली में विभाजित किया गया है, इन्हें कभी-कभी ऑर्थोडॉक्स स्कूल के रूप में जाना जाता है। सुनाइयों को परंपरावादी कहा जा सकता है। लेकिन ऐसे उत्कृष्ट परंपरावादी भी हैं, जो स्वयं को अहल-ए-हदीस या सलाफ़ी कहते हैं।
धार्मिक विद्यालय मुरजी, कादरिया, जबरिया और सिफतिया हैं। ये स्कूल पहली शताब्दी के अंतिम भाग और दूसरी शताब्दी हिजरी के पहले भाग के दौरान उभरे। कादरिया और जबरिया ने इच्छा की स्वतंत्रता के प्रश्न पर चर्चा की। मुर्जिया ने आस्था के स्वरूप पर चर्चा की। सिफतिया ने ईश्वरीय गुणों की प्रकृति पर चर्चा की।
दार्शनिक विद्यालय मुताज़िला, मुताकल्लिम, सूफ़ी और हुकमी या फ़लासिफ़ा हैं, मुर्तज़िलवाद पहली शताब्दी ए, एच के अंतिम भाग में शुरू हुआ था और मुताकल्लिम आंदोलन 300 ए.एच. में अल- द्वारा शुरू किया गया था। अशरी। सूफीवाद व्यावहारिक रूप से इस्लाम जितना ही पुराना है, फिर भी इसे यह विशिष्ट नाम दूसरी शताब्दी हिजरी के अंत तक मिला। बगदाद में अब्बासिड्स और स्पेन में मुवाहिदों के स्वर्ण युग के दौरान फलासिफा फला-फूला।
4. शबरातानी का विभिन्न विद्यालयों का वर्गीकरण
अपनी प्रसिद्ध पुस्तक किताबु एल-मिलाल वा'एन-निहाल शाहरस्तानी में मुसलमानों के बीच विभिन्न स्कूलों को चार मुख्य सिद्धांतों और कुछ उप-सिद्धांतों के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। ये हैं
1) अल्लाह के धत (तौहीद) और सिफत के विषय में 2) क़दर (फ़रमान) और अदल (न्याय) के विषय में
3) वा'द (वादा) और हुक्म (निर्णय) के संबंध में
4) सैम (परंपरा) और 'एक्यूएल कारण' के संबंध में
हम शाहरस्तानी के लेखन से नीचे उद्धृत करते हैं: "पहला सिद्धांत गुणों (सिफ़ात) से संबंधित है
एकता (तौहीद). इसमें शाश्वत गुण का प्रश्न शामिल है
संबंध (सिफ़तु एल-अज़ल्ल), कुछ लोगों द्वारा पुष्टि की गई और दूसरों द्वारा अस्वीकार की गई और सार के गुणों (रिफतु ध-दिहान) और कार्रवाई के गुणों (रिफ़तुर फ़ि'') की व्याख्या की गई। इसमें यह प्रश्न भी शामिल है कि परमपिता परमेश्वर में क्या आवश्यक है और उसके लिए क्या संभव है और क्या असंभव है। इसमें अशरिया, कार्कमिया, मुजस्सिमस/एंथ्रोपोमोर्फिस्ट) और मुर्तज़िला के बीच केंद्रशासितता शामिल है।
दूसरा सिद्धांत कॉनकारस डिक्री (क़दर) और न्याय ('एडीटी) यह नियति (क़द्ज़ा) और डिक्री (क़दर, बल (जबर) और अधिग्रहण (कुस्ब), अच्छाई और बुराई की इच्छा, और के प्रश्न को गले लगाता है। आदेशित और ज्ञात, कुछ लोगों द्वारा पुष्टि की गई और दूसरों द्वारा खंडन किया गया। इसमें कादरिया, नज्जरिया, जबरिया, अशरिया और कर्रिमिया के बीच विवाद शामिल हैं।
तीसरा सिद्धांत वादा (डब्ल्यू) और निर्णय (हुक्म) से संबंधित है। इसमें विश्वास (ईमान) और पश्चाताप (फौबा), धमकी (वाल्ड) और स्थगित करना (एफआरजेए") के सवाल को शामिल किया गया है, चे को अविश्वासी घोषित किया गया है (तकफिर) और एक भटके हुए व्यक्ति (तदालिल) का नेतृत्व किया गया है, जिसका दूसरों द्वारा अपमान किया गया है और दूसरों द्वारा इनकार किया गया है। इसमें शामिल है मुर्जिया, वारिदियिस, मुताज़िला, अशरिया और कररामियेस के बीच विवाद।
चौथा सिद्धांत परंपरा (सैम) और कारण (एजी), और भविष्यवाणी मिशन (रिसेल) और नेतृत्व (इमामत) पर विचार करता है। इसमें किसी कार्य को अच्छे (तहसीन) या बुरे (तकबिक) के रूप में निर्धारित करने, फ़ायदेमंद होने (फ़ेकफ़) के निर्धारण, पैगम्बर को पाप (इस्मा) से बचाने के प्रश्नों को शामिल किया गया है। इसमें कुछ के अनुसार क़ानून (मास) द्वारा और कुछ के अनुसार समझौते (एमए) द्वारा इमामत की स्थिति के प्रश्न को भी शामिल किया गया है
दूसरों के लिए, और यह उन लोगों के दृष्टिकोण में कैसे स्थानांतरित होता है जो कहते हैं कि यह क़ानून द्वारा है, और यह उन लोगों के दृष्टिकोण में कैसे तय होता है जो कहते हैं कि यह समझौते के द्वारा है। इसमें शियाओं, खरिजियों, मुताज़िलों, कर्रमिया और अशरियाओं के बीच के विवाद शामिल हैं।"
फ़िरदौस ख़ान
हाल में ‘हिन्दू’ अख़बार में राज्यसभा सदस्य और कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी का एक लेख शाया हुआ है. इस लेख में उन्होंने लोकसभा चुनाव के बाद पैदा हुए सियासी हालात का ज़िक्र किया है. सियासी गलियारे में सोनिया गांधी के इस लेख को बहुत ही गंभीरता से लिया जा रहा है. कांग्रेस भले ही लोकसभा चुनाव में उतना करिश्मा नहीं कर पाई है, जिसकी उससे उम्मीद की जा रही थी. लेकिन 99 सीट जीतकर वह विपक्ष नेता का पद ज़रूर हासिल कर पाई है. इससे कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दलों में उत्साह का माहौल है. कार्यकर्ता जोश से भरे हुए हैं. उन्हें उम्मीद है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो उन्हें कामयाबी ज़रूर मिलेगी.
सोनिया गांधी ने लिखा है- “अभी 4 जून 2024 को आए चुनावी नतीजों में हमारे देश के मतदाताओं ने स्पष्ट और मज़बूती के साथ अपना फ़ैसला सुनाया है. यह एक ऐसे प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत, राजनीतिक और नैतिक हार का संकेत है, जिसने चुनाव प्रचार के दौरान ख़ुद को दैवीय दर्जा दे दिया था. इस फ़ैसले ने न केवल ऐसे दावों-दिखावों को नकार दिया है, बल्कि विभाजनकारी, कलह पूर्ण और नफ़रत की राजनीति को स्पष्ट रूप से ख़ारिज करते हुए नरेंद्र मोदी के शासन की प्रकृति और शैली दोनों का परित्याग किया है. फिर भी प्रधानमंत्री के हाव-भाव वैसे ही नज़र आते हैं जैसे कि कुछ नहीं बदला है. वे आम सहमति के महत्व का उपदेश तो देते हैं, लेकिन टकराव को ही अहमियत देते हैं. चुनावी नतीजों या जनादेश से उन्हें कोई सबक़ मिला है, इसका कोई संकेत नहीं मिलता कि देश के करोड़ों मतदाताओं ने उन्हें कोई संदेश दिया है.”
18वीं लोकसभा के पहले कुछ दिन दुखद रूप से निराशाजनक रहे. ऐसी कोई भी उम्मीद या अपेक्षा कि हमें कोई बदला हुआ रवैया देखने को मिलेगा, वह धराशायी हो गई. आपसी सम्मान और सामंजस्य की नई भावना, या सौहार्द की बात तो दूर, इस बाबत कोई कदम उठाने की उम्मीद भी ग़लत ही साबित हुई.
मैं पाठकों को याद दिलाना चाहती हूं कि जब स्पीकर पद पर प्रधानमंत्री के दूतों ने इंडिया जनबंधन के लोगों से सहमति की बात की थी तो गठबंधन के दलों ने प्रधानमंत्री को क्या कहा था. साफ़ और सीधे शब्दों में कहा गया था कि “हम सरकार का समर्थन करेंगे, लेकिन परम्परा और प्रथा के मुताबिक़ डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को दिया जाना उचित होगा.” यह एक तार्किक आग्रह था जिसे उस शासन ने ठुकरा दिया जिसने 17वीं लोकसभा में लोकसभा उपाध्यक्ष के संवैधानिक पद को ख़ाली ही छोड़ दिया था.
इसके अलावा प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी द्वारा आश्चर्यजनक रूप से फिर से उछाला गया. यहां तक कि लोकसभा अध्यक्ष ने भी इसका ज़िक्र किया, जिनकी स्थिति निष्पक्षता के अलावा किसी भी सार्वजनिक राजनीतिक के रुख़ या झुकाव से अलग होनी चाहिए. यह प्रयास संविधान, उसके मूलभूत सिद्धांतों और मूल्यों, और उसके द्वारा बनाई गई और सशक्त की गई संस्थाओं पर हमले से ध्यान हटाने का तरीक़ा था जो कि संसद के सुचारू कामकाज के लिए क़तई अच्छा नहीं है.
दरअसल यह ऐतिहासिक तथ्य है कि मार्च 1977 में देश के लोगों ने इमरजेंसी पर स्पष्ट जनादेश दिया था जिसे निस्संकोच और सदाशयता से स्वीकार किया गया था. यह भी तथ्य और इतिहास में दर्ज है कि तीन साल बाद ही उस पार्टी की सत्ता में वापसी हुई थी, जिसे देश ने ख़ारिज कर दिया था, वह भी ऐसे बहुमत के साथ जिसे श्री मोदी और उनकी पार्टी कभी हासिल नहीं कर पाए.
हमें आगे की ओर देखना होगा. संसद की सुरक्षा में हुई निंदनीय चूक पर चर्चा की वैध मांग कर रहे 146 सांसदों का बेहद अटपटा और अभूतपूर्व निलंबन स्पष्ट रूप से यह सुनिश्चित करने का एक तरीक़ा था कि बिना किसी चर्चा के तीन ऐसे आपराधिक न्याय क़ानून पारित किए जा सकें जिनके दूरगामी परिणाम होंगे. कई क़ानूनी विशेषज्ञों और अन्य लोगों ने इन क़ानूनों के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त की है. क्या इन क़ानूनों को तब तक लागू होने से नहीं टाला जा सकता है जब तक कि इनकी स्थापित संसदीय प्रक्रियाओं द्वारा जांच नहीं हो जाती, ख़ासतौर से जबकि 2024 के चुनावी नतीजे स्पष्ट संदेश देते हैं. इसी तरह वन संरक्षण और जैव विविधता संरक्षण क़ानूनों को भी बीते साल उस दौरान ज़बरदस्ती पास करा दिया गया जब संसद में हंगामा हो रहा था. ग्रेटर निकोबार प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया गया जिससे कि पर्यावरण, पारिस्थिकीय और मानविकी आपदा की आशंका है. क्या इसकी भी समीक्षा नहीं होनी चाहिए जिससे कि प्रधानमंत्री जो सहमति का दावा करते हैं, वह अर्थपूर्ण साबित हो सकता और क़ानूनों को संसद में पूरी चर्चा के बाद ही पास कराया जाता?
लाखों युवाओं के जीवन पर क़हर ढाने वाले नीट घोटाले पर शिक्षा मंत्री की त्वरित और पहली प्रतिक्रिया तो यही थी कि जो कुछ हुआ है इसका खंडन करते हुए उसकी गंभीरता को ही नकार दिया जाए. प्रधानमंत्री जो ख़ुद ‘परीक्षा पे चर्चा’ करते रहे हैं, पेपर लीक के पूरे मामले पर संदिग्ध रूप से ख़ामोश हैं जिसने देश के तमाम परिवारों को परेशान करके रख दिया है. एक कथित ‘उच्चाधिकार वाली समिति’ तो बना दी गई है, लेकिन असली मुद्दा यह है कि एनसीईआरटी, यूजीसी और विश्वविद्यालयों जैसी शैक्षणिक संस्थाओं की व्यवसायिकता को बीते दस वर्षों में काफ़ी नुक़सान पहुंचाया गया है.
इस बीच देश के अल्पसंख्यकों के ख़िलाफ़ हिंसा और उत्पीड़न की घटनाओं में फिर से वृद्धि हो गई है. भाजपा शासित राज्यों में मात्र आरोपों पर ही क़ानूनी प्रक्रियाओं का उल्लंघन करते ए अल्पसंख्यकों के घरों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें सामूहिक सजा दी जा रही है. चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री ने लोगों पर साम्प्रदायिक अपशब्दों और ख़ालिस झूठ के ज़रिये जो हमले किए थे, उसके बाद जो कुछ हो रहा है, वह सब आश्चर्यजनक नहीं है. उन्होंने इस डर से भड़काऊ बयानों को और बढ़ावा दिया क्योंकि चुनाव उनके हाथ से निकल रहा था, इस तरह उन्होंने अपने पद की गरिमा और मर्यादा का पूरी तरह से अनदेखा किया.
फ़रवरी 2022 में भाजपा और उसके सहयोगी दलों को मणिपुर के विधानसभा चुनाव में साफ़ बहुमत मिला था. फिर भी तीन महीने के अंदर ही मणिपुर जल उठा, या कहें कि इसे जलने दिया गया. सैकड़ों लोगों की जान गई और हज़ारों लोग बेघर हो गए. इस बेहद संवेदनशील राज्य में सामाजिक तानाबाना तहस-नहस हो गया. लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री को न तो राज्य का दौरा करने या वहां के नेताओं से मिलने का वक़्त मिला. और इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उनकी पार्टी वहां दोनों लोकसभा सीटें हार गई, लेकिन इससे मणिपुर के विविधतापूर्ण समाज में व्याप्त संकट के प्रति उनके असंवेदनशील रवैये पर कोई असर नहीं पड़ता दिखता.
प्रधानमंत्री ने चालीस दिनों से ज़्यादा समय तक चले चुनाव प्रचार अभियान के दौरान ख़ुद बेहद कमतर साबित किया. उनके शब्दों ने हमारे सामाजिक ताने-बाने और उस पद की गरिमा को बहुत नुक़सान पहुंचाया है जिस पर वे गर्व करते है. उन्हें आत्मचिंतन करना चाहिए और यह पहचानना चाहिए कि 400 से ज़्यादा संसदीय सीटों के लिए उनके आह्वान को अस्वीकार करके, हमारे करोड़ों लोगों ने - जिनसे वे सबका साथ, सबका विकास का वादा करते हैं - एक शक्तिशाली संदेश दिया है कि अब बहुत हो चुका.
इंडिया गठबंधन के दलों ने साफ़ कर दिया है कि वे टकराव वाला रवैया नहीं अपनाना चाहते. विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सहयोग की पेशकश की है. गठबंधन के घटक दलों के नेताओं ने स्पष्ट कर दिया है कि वे संसद में रचनात्मक सहयोग देना चाहते हैं और संसद की कार्यवाही के संचालन में निष्पक्षता चाहते हैं. हमें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री और उनकी सरकार इस पर सकारात्मक रुख़ अपनाएगी. लेकिन शुरुआती लक्षण अच्छे नहीं हैं, फिर भी विपक्ष में हम इस बात को लेकर कटिबद्ध हैं कि संसद में संतुलन बना रहे ताकि देश के उन करोड़ों लोगों की आवाज़ और चिंताओं का प्रतिनिधित्व हो सके जिन्होंने हमें इस सदन में अपने प्रतिनिधि के रूप में भेजा है. हम उम्मीद करते हैं कि सत्ता पक्षा हमारे लोकतांत्रिक दायित्वों को पूरा करने में आगे आएगा.”
बहरहाल सोनिया गांधी पूरे जोश के साथ मैदान में डटी हुई हैं. वे हर पल अपने बेटे राहुल गांधी और पार्टी के साथ खड़ी नज़र आती हैं. जिस उम्र में लोग सिर्फ़ आराम करना चाहते हैं, उस उम्र में भी वे देश की अवाम के बारे में सोच रही हैं, उनके हक़ के लिए लड़ रही हैं. उनका यही जज़्बा कार्यकर्ताओं में में उत्साह बनाए रखता है.
फ़िरदौस ख़ान
देश और समाज में आज महिला सशक्तीकरण की ख़ूब बातें हो रही हैं. आख़िर क्या है महिला सशक्तिकरण. दरअसल, महिला को सशक्त बनाने को ही महिला सशक्तीकरण कहा जाता है. महिलाओं का जीवन के हर क्षेत्र में सशक्त होना ही महिला सशक्तीकरण है. महिलाओं को धन के मामले में आत्मनिर्भर होना होगा. इससे उनमें आत्म-सम्मान और आत्मविश्वास पैदा होगा. इसके लिए उन्हें शिक्षित करना होगा. शिक्षित महिलाएं ही आने वाली पीढ़ी की बच्चियों और महिलाओं को बेहतर परिवेश दे पाएंगी. यह शिक्षा का ही असर है कि जिस देश में, जिस समाज में लोग बेटियों की बजाय बेटों को ज़्यादा तरजीह देते रहे हैं, वहां अब लोग बेटियों को परिवार में ज़रूरी मानने लगे हैं, उनकी चाहत करने लगे हैं. एक सर्वे के मुताबिक़ बेटियों को लेकर समाज का नज़रिया बदलने लगा है.
नेशनल फ़ैमिली एंड हेल्थ सर्वे की एक रिपोर्ट के मुताबिक़ 15 से 49 साल की 79 फ़ीसद महिलाएं और 15 से 54 साल के 78 फ़ीसद पुरुष चाहते हैं कि उनके परिवार में कम से कम एक बेटी ज़रूर होनी चाहिए. बेटी चाहने वालों में मुस्लिम, दलित और आदिवासी सबसे आगे हैं. राज्यों की बात करें, तो इसमें उत्तर प्रदेश और बिहार आगे हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि ग़रीबी रेखा से नीचे आने वाले तबक़े और निम्न मध्वर्गीय परिवारों की 86 फ़ीसद महिलाएं और 85 फ़ीसद पुरुष बेटी के जन्म पर ख़ुशी मनाते हैं. मुस्लिम, दलित और आदिवासी तबक़ों के लोगों का मानना है कि परिवार में बेटी का होना बहुत ज़रूरी है.
इस सर्वे की ख़ास बात यह भी है कि साल 2005-06 के सर्वे के मुक़ाबले इस बार गांवों की महिलाओं ने परिवार में बेटियों को ख़ासी तरजीह दी है. पुराने सर्वे में 74 फ़ीसद शहरी महिलाओं ने बेटियों को तरजीह दी थी, जबकि 65 फ़ीसद ग्रामीण महिलाओं ने बेटी की ख़्वाहिश ज़ाहिर की थी. लेकिन इस बार ग्रामीण इलाक़ों की 81 फ़ीसद महिलाओं ने बेटी को तरजीह दी है, जबकि शहरी इलाक़ों की 75 फ़ीसद महिलाओं ने बेटी की चाहत जताई है. ग्रामीण इलाक़ों के 80 फ़ीसद पुरुष परिवार में बेटी चाहते हैं, जबकि शहरी इलाक़ों के 75 फ़ीसद पुरुषों ने ही घर में बेटी को ज़रूरी माना है.
परिवार में बेटी को तरजीह देने के मामले में शिक्षा का असर देखने को मिला है, यानी बारहवीं पास 85 फ़ीसद महिलाएं बेटी को ज़रूरी मानती हैं, जबकि इससे कम शिक्षित 72 फ़ीसद महिलाओं ने परिवार में बेटी की पैदाइश को ज़रूरी माना है. इस मामले में पुरुषों की सोच महिलाओं से एकदम विपरीत है यानी सिर्फ़ 74 फ़ीसद शिक्षित पुरुष ही बेटियों की चाहत रखते हैं, जबकि 83 फ़ीसद कम शिक्षित पुरुषों ने बेटियों को अपनी पहली पसंद क़रार दिया है.
रिपोर्ट के मुताबिक़ 79 फ़ीसद बौद्ध और 79 फ़ीसद हिन्दू महिलाओं का मानना है कि घर में कम से कम एक बेटी तो होनी ही चाहिए. जातीय समुदाय का ज़िक्र करें, तो 81 फ़ीसद दलित और 81 फ़ीसद आदिवासी और 80 अन्य पिछड़ा वर्ग के परिवारों की महिलाओं ने बेटी को ज़रूरी माना है. इसी तरह 84 फ़ीसद आदिवासी पुरुष और 79 फ़ीसद दलित पुरुष भी बेटी चाहते हैं.
ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ पुरुष की बेटों की चाहत रखते हैं. समाज में ऐसी महिलाओं की कोई कमी नहीं है, जो ख़ुद महिला होने के बावजूद बेटी को पसंद नहीं करतीं और बेटियों को बोझ समझती हैं. सर्वे के मुताबिक़ 19 फ़ीसद महिलाएं ऐसी भी हैं, जो बेटा चाहती हैं. इसके विपरीत 3.5 फ़ीसद ऐसी महिलाएं भी सामने आईं, जिन्हें सिर्फ़ बेटियां चाहिए. हालांकि बिहार की 37 फ़ीसद महिलाएं और उत्तर प्रदेश की 31 फ़ीसद महिलाएं बेटों को बेटियों से ज़्यादा अच्छा समझती हैं.
साल 2011 की जनगणना के आंकड़े भी यह साबित करते हैं कि मुसलमानों में बेटियों का लिंगानुपात अन्य समुदायों के मुक़ाबले में बेहतर है. मुस्लिम समुदाय में कुल लिंग अनुपात 950:1000 है, जबकि हिन्दू समुदाय में लिंगानुपात 925:1000 है. हालांकि इस मामले में ईसाई समुदाय सबसे आगे है. ईसाइयों में लिंगानुपात 1009 :1000 है. औसत राष्ट्रीय लिंग अनुपात 933:1000 है.
इस्लाम ने बेटियों को दिया इज्ज़त का मुक़ाम
तक़रीबन 81 फ़ीसद मुसलमान परिवारों ने घर में बेटियों का होना बेहद ज़रूरी माना है. दरअसल, मुस्लिम समाज में बेटियों को चाहने की मज़हबी वजह भी है. क़ाबिले-ग़ौर है कि अरब देशों में पहले लोग अपनी बेटियों को पैदा होते ही ज़िन्दा दफ़ना दिया करते थे, लेकिन अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मद ने इस घृणित और क्रूर प्रथा को ख़त्म करवाकर बेटियों को इज़्ज़त का मुक़ाम दिया. उन्होंने मुसलमानों से अपनी बेटियों की अच्छी तरह से परवरिश करने को कहा. एक हदीस के मुताबिक़ अल्लाह के रसूल हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया- "जिसकी तीन बेटियां या तीन बहनें, या दो बेटियां या दो बहनें हैं, जिन्हें उसने अच्छी तरह रखा और उनके बारे में अल्लाह से डरता रहा, तो वह जन्नत में दाख़िल होगा." (सहीह इब्ने हिब्बान 2/190 हदीस संख्या 446)
इस्लाम में वंश चलाने के लिए बेटों को ज़रूरी नहीं माना जाता. अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वंश उनकी प्यारी बेटी सैयदना फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से चला. जब तमाम लोग अल्लाह के रसूल हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आते, तो सबसे पहले यह कहते- “या रसूल अल्लाह ! मेरे मां-बाप आप पर क़ुर्बान.” फिर उसके बाद ही वे अपनी कोई फ़रियाद करते. लेकिन जब अल्लाह के रसूल हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी से कोई बात करते, तो सबसे पहले यह इरशाद फ़रमाते- “फ़ातिमा ! तुझ पर मेरे मां-बाप क़ुर्बान.” रसूल अल्लाह ने अपनी बेटी को इतना बुलंद मर्तबा दिया. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया की हर बेटी को आदर-सम्मान दिया. इस्लाम के मुताबिक़ रोज़े-महशर में हर शख़्स अपनी मां के नाम के साथ पुकारा जाएगा. उस वक़्त उसे उसकी मां के नाम से ही पहचाना जाएगा. ऐसा इसलिए है कि इस दुनिया में उन औरतों की कमी नहीं है, जिनके साथ ज़बरदस्ती की गई या जिन्हें जिस्म फ़रोशी के ग़लीज़ धंधे में धकेल दिया गया. रोज़े महशर में ऐसी मांओं के बच्चों को शर्मिंदगी से बचा लिया गया है.
इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि बेटियां हर घर की रौनक़ होती हैं. बेटियां अपने माता-पिता के दिल के क़रीब होती हैं. बेटियां दूर होकर भी अपने माबाप से दूर नहीं होतीं. बहरहाल, यह एक अच्छी ख़बर है कि बेटियों के प्रति समाज का नज़रिया बदलने लगा है.
(लेखिका स्टार न्यूज़ एजेंसी में सम्पादक हैं)
अमूमन इनमें से सबने यही कहा था कि वे झाड़ू को वोट देंगे. वजह पूछने पर यही जवाब मिला कि केजरीवाल ने बहुत काम किया है.
क्या काम क्या है? इसका उनके पास कोई जवाब नहीं था.
आज आम आदमी पार्टी के जीते हुए पार्षदों का जुलूस पूरे हर्षोल्लास से निकला, तो इन लोगों में ख़ुशी की लहर दौड़ गई. हालत यह थी कि लोग एक-दूसरे को फ़ोन पर मुबारकबाद दे रहे थे. गलियों में बच्चे भी ख़ुशी से चीख़-चीख़कर कह रहे थे- "केजरीवाल जीत गया."
अब केजरीवाल को लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि
अवाम को भाजपा का विकल्प मिल गया है.
कट्टर कांग्रेसी कैसे 'आप' समर्थक हो गए? क्या इस पर कांग्रेस ग़ौर करेगी?
’लौह महिला’ के नाम से मशहूर इंदिरा गांधी न सिर्फ़ भारतीय राजनीति पर छाई रहीं, बल्कि विश्व राजनीति के क्षितिज पर भी सूरज की तरह चमकीं. उनकी ज़िन्दगी संघर्ष, चुनौतियों और कामयाबी का एक ऐसा सफ़रनामा है, जो अदम्य साहस का इतिहास बयां करता है. अपने कार्यकाल में उन्होंने अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों का सामना किया और हर मोर्चे पर कामयाबी का परचम लहराया. मामला चाहे कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी कलह का हो, अलगाववाद का हो, पाकिस्तान के साथ जंग का हो, बांग्लादेश की आज़ादी का हो, या फिर इसी तरह का कोई और बड़ा मुद्दा हो. हर मामले में उन्होंने अपनी सूझबूझ और साहस का परिचय दिया. बैंकों के राष्ट्रीयकरण, प्रीवी पर्स का ख़ात्मा, प्रथम पोखरण परमाणु विस्फोट, प्रथम हरित क्रांति जैसे कार्यों के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा. गुटनिरपेक्ष आंदोलन की अगुवाई और बांग्लादेश की आज़ादी भी उनके साहसिक कार्यों में शामिल है.
देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का जन्म 19 नवंबर 1917 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में हुआ था. उनका पूरा नाम इंदिरा प्रियदर्शिनी गांधी था. उनके पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री थे और माता कमला नेहरू थीं. उन्होंने शुरुआती तालीम इलाहाबाद के स्कूल में ही ली. इसके बाद उन्होंने गुरु रबींद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन स्थित विश्व भारती विश्वविद्यालय में दाख़िला लिया. कहते हैं, रबीन्द्रनाथ टैगोर ने ही उन्हें ’प्रियदर्शिनी’ नाम दिया था. इसके बाद वे इंग्लैंड चली गईं और ऑक्सफ़ोर्ड विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा में बैठीं,लेकिन नाकाम हुईं. इसके बाद उन्होंने ब्रिस्टल के बैडमिंटन स्कूल में कुछ महीने बिताए. फिर साल 1937 में इम्तिहान में कामयाब होने के बाद उन्होंने ऑक्सफ़ोर्ड के सोमरविल कॉलेज में दाख़िला ले लिया. उस दौरान उनकी मुलाक़ात फ़िरोज़ गांधी से हुई, जिन्हें वे इलाहाबाद से जानती थीं. फ़िरोज़ गांधी उन दिनों लंदन स्कूल ऑफ़ इकॉनॉमिक्स में पढ़ रहे थे. उनकी जान-पहचान मुहब्बत में बदल गई और फिर 16 मार्च 1942 को उन्होंने इलाहाबाद के आनंद भवन में फिरोज़ से विवाह कर लिया. उनके दो बेटे संजय और राजीव हुए. राजीव गांधी बाद में देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री बने.
बचपन से ही इंदिरा गांधी को सियासी माहौल मिला था, जिसका उनके किरदार और उनकी ज़िन्दगी पर गहरा असर पड़ा. साल 1941 में ऑक्सफ़ोर्ड से स्वदेश वापसी के बाद वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गईं. उन्होंने युवाओं के लिए वानर सेना बनाई. वानर सेना विरोध प्रदर्शन और झंडा जुलूस निकालने के साथ-साथ कांग्रेस नेताओं की भी ख़ूब मदद करती थी, मसलन संवेदनशील प्रकाशनों और प्रतिबंधित सामग्रियों को गंतव्य तक पहुंचाने का काम करती थी. आज़ादी की लड़ाई में इसके काम को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता. 1930 की दहाई के शुरू का वाक़िया है, जब इंदिरा गांधी ने पुलिस की निगरानी में रह रहे अपने पिता के घर से एक अहम दस्तावेज़ को अपनी किताबों के बस्ते में छुपाकर गंतव्य तक पहुंचाया था. इस दहाई के आख़िर में ऑक्सफ़ोर्ड विश्वविद्यालय में अपनी पढ़ाई के दौरान वे लंदन में आज़ादी के समर्थक दल भारतीय लीग की सदस्य बनीं और विदेश में रहकर भी स्वदेश के लिए काम करती रहीं. सितम्बर 1942 में उन्हें ब्रिटिश हुकूमत द्वारा गिरफ़्तार कर लिया गया. आख़िर तक़रीबन 243 दिन जेल में गुज़ारने के बाद उन्हें 13 मई 1943 को रिहा किया गया. साल 1947 के देश के बंटवारे के दौरान उन्होंने शरणार्थी शिविरों को संगठित किया और पाकिस्तान से आए लाखों शरणार्थियों के लिए भोजन और चिकित्सा का इंतज़ाम किया. उनके इस कार्य को ख़ूब सराहा गया और इससे उन्हें एक नई पहचान मिली.
1950 की दहाई में इंदिरा गांधी अपने पिता यानी देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के निजी सहायक के तौर पर काम कर रही थीं. साल 1959 वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गईं. पार्टी के लिए उन्होंने सराहनीय काम किया. 27 मई, 1964 को उनके पिता का देहांत हो गया. इसके बाद वे राज्यसभा सदस्य के रूप में चुनी गईं और प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल में सूचना और प्रसारण मंत्री बनीं. साल 1965 की भारत-पाकिस्तान जंग के दौरान वे सेना की हौसला अफ़ज़ाई के लिए श्रीनगर सीमा के इलाक़े में गईं. सेना की चेतावनी के बावजूद उन्होंने दिल्ली आना मंज़ूर नहीं किया और सेना का मनोबल बढ़ाती रहीं. उस दौरान लालबहादुर शास्त्री ताशक़ंद गए हुए थे, जहां सोवियत मध्यस्थता में पाकिस्तान के अयूब ख़ान के साथ शांति समझौते पर दस्तख़त करने के कुछ घंटों बाद ही उनका निधन हो गया.
इसके बाद 19 जनवरी, 1966 को इंदिरा गांधी देश की तीसरी प्रधानमंत्री बनीं. उस वक़्त कांग्रेस दो गुटों में बंट चुकी थी. समाजवादी ख़ेमा इंदिरा गांधी के साथ खड़ा था, जबकि दूसरा रूढ़िवादी गुट मोरारजी देसाई का समर्थक था. मोरारजी देसाई इंदिरा गांधी को ’गूंगी गुड़िया’ कहा करते थे, क्योंकि वे बहुत कम बोलती थीं. साल 1967 के चुनाव में 545 सीटों वाली लोकसभा में कांग्रेस को 297 सीटें मिलीं. उन्हें प्रधानमंत्री चुन लिया गया और वे 24 मार्च, 1977 अपने पद पर बनी रहीं. क़ाबिले-ग़ौर है कि वे 1967 में प्रधानमंत्री पद के लिए चुने जाने के बाद आख़िर तक प्रधानमंत्री बनी रहीं, लेकिन 1977 से 1980 के बीच उन्हें हुकूमत से बेदख़ल रहना पड़ा. उन्होंने मोरारजी देसाई को देश का उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री बनाया. साल 1969 में मोरारजी देसाई के साथ अनेक मुद्दों पर मतभेद हुए और आख़िरकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बंट गई. उन्होंने समाजवादी और साम्यवादी दलों के समर्थन से हुकूमत की. इसके कुछ वक़्त बाद फिर से देश को जंग का सामना करना पड़ा. साल 1971 में जंग के दौरान उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति को नई दिशा दी. नतीजतन, जंग में भारत ने शानदार जीत हासिल की. इस दौरान बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी मिली. दरअसल, बांग्लादेश को आज़ाद कराने में इंदिरा गांधी ने बेहद अहम किरदार निभाया था. कहते हैं कि इस जीत के बाद जब संसद सत्र शुरू हुआ, तो विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने भाषण मे इंदिरा गांधी को ‘दुर्गा’ कहकर संबोधित किया था.
इंदिरा गांधी ने 26 जून, 1975 को देश में आपातकाल लागू किया. इसकी वजह से उनकी पार्टी 1977 के आम चुनाव में पहली बार हार गई. उन्हें अक्टूबर 1977 और दिसम्बर 1978 में जेल तक जाना पड़ा. लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और जद्दोजहद करती रहीं. फिर 1980 में उन्होंने हुकूमत में वापसी की. कांग्रेस को शानदार कामयाबी मिली और 22 राज्यों में से 15 राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी. 14 जनवरी, 1980 को वे फिर से देश की प्रधानमंत्री बनीं और अपनी ज़िन्दगी के आख़िर तक हुकूमत की. उन दिनों पंजाब में आतंकवाद चरम पर था. उन्होंने पंजाब में अलगाववादियों के ख़िलाफ़ मुहिम शुरू कर दी. इसकी वजह से अलगाववादी उनकी जान के दुश्मन बन गए और 31 अक्टूबर, 1984 को दिल्ली में उनके अंगरक्षकों ने ही उनका क़त्ल कर दिया. उनकी आकस्मिक मौत से देश शोक में डूब गया.
श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से श्रीमती इंदिरा गांधी की तुलना करते हुए कहा था कि अपने पिता के विपरीत श्रीमती इंदिरा गांधी संसद से दूर-दूर रहती थीं. आरंभ में तो वह इतनी चुप रहती थीं कि उन्हें ’गूंगी गुड़िया’ तक कह दिया गया था, किंतु यह उनके साथ अन्याय था. वह कम बोलने में विश्वास करती थीं. सबकी बातें सुनने के बाद अपना मत स्थिर करती थीं और सबसे अंत में प्रकट करती थीं. वह सदन में आकर समय गंवाने की बजाय अपने कमरे में बैठकर सत्ता की चाबियां घुमाती थीं. उन्होंने चौदह वर्ष तक शासन कर विश्व को चमत्कृत कर दिया और विरोधियों को कई बार पछाड़ा. इंदिरा जी के साथ संसद में कई बार काफी नोक-झोंक होती रहती थी, किंतु राजनीति के मतभेदों को उन्होंने व्यक्तिगत संबंधों में बाधक नहीं बनने दिया. उनकी निर्मम त्रासद और क्रूर हत्या ने एक ऐसे व्यक्तित्व को हमारे बीच से उठा लिया, जिन्हें योग्य पिता की योग्य पुत्री के नाते ही नहीं, अपनी निजी योग्यता, कुशलता, निर्णय क्षमता तथा कठोरता के कारण याद किया जाएगा.
दरअसल, सियासत की इस महान और कामयाब शख़्सियत को अपनी निजी ज़िन्दगी में कई ग़म मिले थे. साल 1936 में उनकी मां कमला नेहरू तपेदिक से एक लम्बे अरसे तक जूझने के बाद उन्हें अकेला छोड़ गईं. उस वक़्त उनकी उम्र महज़ 18 साल थी. फिर शादीशुदा ज़िन्दगी में भी उन्हें दुख मिले.शादी के बाद उनकी शुरुआती ज़िन्दगी ठीक रही, लेकिन बाद में वे अपने पिता के घर आ नई दिल्ली आ गईं. देश के पहले आम चुनाव 1951 में वे अपने पिता और पति दोनों के लिए चुनाव प्रचार कर रही थीं. चुनाव जीतने के बाद फ़िरोज़ गांधी ने अपने लिए अलग घर चुना. फिर साल 1958 में उप-निर्वाचन के कुछ वक़्त बाद फिरोज़ गांधी को दिल का दौरा पड़ा. इस दौरान इंदिरा गांधी ने उनकी ख़ूब ख़िदमत की. उनके रिश्ते बेहतर होने लगे, लेकिन 8 सितम्बर1960 को जब इंदिरा गांधे अपने पिता के साथ एक विदेश दौरे पर गई थीं, तब फिरोज़ की मौत हो गई. उन्होंने ख़ुद को पार्टी और देश के काम में मसरूफ़ कर लिया. उन्होंने संजय गांधी को अपना सियासी वारिस चुना, लेकिन 23 जून, 1980 को एक उड़ान हादसे में उनकी मौत हो गई. इसके बाद वे अपने छोटे बेटे राजीव गांधी को सियासत में लेकर आईं. राजीव गांधी पायलट की नौकरी में ख़ुश थे और सियासत में आना नहीं चाहते थे, लेकिन मां को वे इंकार न कर सके और न चाहते हुए भी उन्हें सियासत में क़दम रखना पड़ा.
इंदिरा गांधी ख़ाली वक़्त में अपने परिजनों के लिए स्वेटर बुना करती थीं. उन्हें संगीत और किताबों से भी ख़ास लगाव था. पाकिस्तानी गायक मेहंदी हसन की ग़ज़लें भी अकसर सुनती थीं. सोने से पहले वे आध्यात्मिक किताबें पढ़ती थीं. भारत रत्न से सम्मानित इंदिरा गांधी ने कहा था- जीवन का महत्व तभी है, जब वह किसी महान ध्येय के लिए समर्पित हो. यह समर्पण ज्ञान और न्याययुक्त हो. शहादत कुछ ख़त्म नहीं करती, वो महज़ शुरुआत है. अगर मैं एक हिंसक मौत मरती हूं, जैसा कि कुछ लोग डर रहे हैं और कुछ षड़यंत्र कर रहे हैं, तो मुझे पता है कि हिंसा हत्यारों के विचार और कर्म में होगी, मेरे मरने में नहीं. लोग अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं, लेकिन अधिकारों को याद रखते हैं. अपने आप को खोजने का सबसे अच्छा तरीक़ा यह है कि आप अपने आप को दूसरों की सेवा में खो दें. संतोष प्राप्ति में नहीं, बल्कि प्रयास में होता है पूरा प्रयास पूर्ण विजय है. प्रश्न करने का अधिकार मानव प्रगति का आधार है. देशों के बीच के शांति, व्यक्तियों के बीच प्यार की ठोस बुनियाद पर टिकी होती है
उन्होंने यह भी कहा था, जब मैं सूर्यास्त पर आश्चर्य या चांद की ख़ूबसूरती की प्रशंसा कर रही होती हूं, उस समय मेरी आत्मा इन्हें बनाने वाले की पूजा कर रही होती है.
ये बरहक़ है कि जो पैदा हुआ है वह उम्र के मुख़्तलिफ़ मरहलों से गुज़रता है. पहले वह बच्चा होता है, फिर वह अपनी जवानी को पहुंचता है और इसके बाद रफ़्ता-रफ़्ता ज़ईफ़ी की तरफ़ बढ़ता है.
ख़ुशनसीब हैं वे लोग जो बूढ़े होते हैं, क्योंकि मौत के ज़ालिम पंजे किसी को पैदा होते ही अपनी गिरफ़्त में ले लेते हैं, तो किसी को बचपन में उनके अपनों से छीन लेते हैं. कितने ही लोग भरी जवानी में मौत की आग़ोश में समा जाते हैं.
क्या बूढ़ा होना कोई गुनाह है? क्या चेहरे की झुर्रियां शर्म की बात है? क्या दाढ़ी सफ़ेद होना नदामत की बात है?
ख़ूबसूरत लोग हमेशा ख़ूबसूरत नहीं रहते, लेकिन अच्छे लोग हमेशा ख़ूबसूरत होते हैं. हमारे नज़दीक राहुल गांधी दुनिया के सबसे ख़ूबसूरत इंसान हैं और हमेशा रहेंगे.
लाल बिहारी लाल
आज भारत में हिन्दी बोलने,लिखने तथा ब्यवहारिक प्रयोग करने वालों की संख्या लगभग 70 प्रतिशत है फिर भी आज दुख इस बात का है कि सरकारी दफ्तरों में और न्यायालयों में अंग्रैजी का बोलबाला है। खुशी की बात ये है कि इलाहाबाद न्यायालय के कुछ जज हिदी में केस की सुनवाई के लिए तैयार हो गये है, पर यह नकाफी है।
सितंबर माह आते ही हर साल हिन्दी दिवस और पखवाड़ा मनाने की चहल पहल हर सरकारी दफ्तरों में शुरु हो जाती है औऱ हिन्दी दिवस के नाम पर करोड़ो रुपये पानी की तरह बहा दिया जाता है। चाहे वो राज्य की सरकारें हो या केन्द्र सरकार हो। हिन्दी को हमारे नेता राष्ट्रभाषा बनाने चाहते थे। गांधी जी ने सन् 1918 में हिन्दी साहित्य सम्मेलन में हिन्दी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने को कहा था और ये भी कहा कहा था कि हिन्दी ही एक ऐसी भाषा, है जिसे जनभाषा बनाया जा सकता है। 14 सितंबर 1949 को हिन्दी को भारतीय संविधान में जगह दी गई पर दक्षिण भारतीय एवं अन्य कई नेताओं के विरोध के कारण राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के अनुरोध पर सन 1953 में 14 सिंतबर से हिंदी को राजभाषा का दर्जा दे दिया गया। परन्तु सन 1956-57 में जब आन्ध्र प्रदेश को भाषायी आधार पर देश का पहला राज्य बनाया गया तभी से हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने की धार कुंद पड़ गई और इतनी कुंद हुई कि आज तक इसकी धार तेज नहीं हो सकी। औऱ राष्ट्रभाषा की बात राजभाषा की ओर उन्मुख हो कर रह गई है।
आज हिन्दी हर सरकारी दफ्तरो में महज सितंबर माह की शोभा बन कर रह गई है। हिन्दी को ब्यवहार में न कोई कर्मचारी अपनाना चाहता है और नाहीं कोई अधिकारी जब तक कि उसका गला इसके प्रयोग में न फंसा हो। हिन्दी के दशा एवं दिशा देने के लिए उच्चस्तर पर कुछ प्रयास भी हुए। इसके लिए कुछ फांट भी आये और इसके दोषों को सुधारा भी गया औऱ आज सारी दुनिया में अंग्रैजी की भांति हिन्दी के भी सर्वब्यापी फांट यूनीकोड आ गया है जो हर लिहाज से काफी सरल ,सुगम एवं प्रयोग करने में आसान भी है। सरकार हिंदी के उत्थान हेतु कई नियम एवं अधिनियम बना चुकी है परन्तु अंग्रैजी हटाने के लिए सबसे बड़ी बाधा राज्य सरकारें है क्योकिं नियम में स्पष्ट वर्णन है कि जब तक भारत के समस्त राज्य अपने –अपने विधान सभाओं में एक विधेयक इसे हटाने के लिए पारित कर केन्द्र सरकार के पास नहीं भेज देती तब तक संसद कोई भी कानून इस विषय पर नहीं बना सकती है। ऐसे में अगर एक भी राज्य ऐसा नहीं करती है तो कुछ भी नहीं हो सकता है। नागालैण्ड एक छोटा –सा राज्य है जहां की सरकारी भाषा अंग्रेजी है। तो भला वो क्यों चाहेगा कि उसकी सता समाप्त हो। दूसरी ओर तामिलनाडू की सरकार एंव राजनीतिज्ञ भी हिन्दी के घोर विरोधी है औऱ नहीं चाहते की उन पर हिन्दी थोपी जाये जबकि वहां की अधिकांश जनता आसानी से हिन्दी बोलती एवं समझती है। आज भारत के राजनीतिज्ञों ने हिन्दी को कुर्सी से इस तरह जोड़ दिया है कि अब इसको राष्ट्रभाषा बनाने के सपने धूमिल हो गया हैं।आज हिन्दी विश्व पटल पर तो फैली है लेकिन भारत में ही उपेक्षित है । विदेशों में बाजारीकरण के कारण काफी लोकप्रिय हो गई है। कई देशों ने इसे स्वीकार किया है। कई विदेशी कंपनिया भी आज अपने उत्पादों के विज्ञापन हिन्दी में देने लगी है। इंटरनेट की कई सोशल सर्विस देने वाली साइटें मसलन-ट्वीटर ,फेसबूक,गूगल, वाट्स अप, टेलीग्राम आदि पर भी हिन्दी की उपलब्धता आसानी से देखी जा सकती है। हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए 10 जनवरी 1975 को नागपुर में प्रथम विश्व हिन्दी सम्मेलन आयोजित की गई थी। तब से लेकर अब तक देश दुनिया में 10 विश्व हिन्दी सम्मेलन इसके प्रचार-प्रसार के लिए आयोजित की जा चुकी है। हर साल 10 जनवरी को विश्व हिन्दी दिवस भी मनाते है। हिन्दी आज विश्व में लगभग 137 देशों में बोली जाती है।विश्व के प्रमूख 16 भाषाओं में 5 भारतीय भाषाएं शामिल है।
2001 की जनगणना के अनुसार भारत में हिंदी बोलने वाले 41.03 प्रतिशत थे। आज भारत में हिन्दी बोलने,लिखने तथा ब्यवहारिक प्रयोग करने वालों की संख्या लगभग 70 प्रतिशत है फिर भी आज दुख इस बात का है कि सरकारी दफ्तरों में और न्यायालयों में अंग्रैजी का बोलबाला है । खुशी की बात ये है कि इलाहाबाद न्यायालय के कुछ जज हिदी में केस की सुनवाई के लिए तैयार हो गये है पर यह नकाफी है। इसलिए आज अपने ही देश में हिन्दी बे-हाल होते जा रही है। अतः आज जरुरी है कि सरकारी दफ्तरों में हिंदी का प्रयोग बढ़ाया जाये और इसे जन-जन की भाषा बनायी जाये तभी कुछ इसका सार्वांगिन विकास हो सकता है।
लेखक लाल बिहारी लाल का परिचय
हिन्दी एवं भोजपुरी साहित्य के समर्पित क़लमकार लाल बिहारी लाल वरिष्ठ पत्रकार भी हैं. वह साहित्य टीवी के सम्पादक हैं. उनके सम्पादन में कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं. उनकी रचनाएं क्रांति बिहार के दो विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में शामिल हैं.कुमार कृष्णन
महात्मा गांधी के सपनों के भारत में एक सपना राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को प्रतिष्ठित करने का भी था। उन्होंने कहा था कि राष्ट्रभाषा के बिना कोई भी राष्ट्र गूँगा हो जाता है। हिन्दी को राष्ट्रीय पहचान दिलाने में एक राजनीतिक शख्सियत के रूप में उनका महत्वपूर्ण योगदान है।
महात्मा गांधी की मातृभाषा गुजराती थी और उन्हें अंग्रेजी भाषा का उच्चकोटि का ज्ञान था किंतु सभी भारतीय भाषाओं के प्रति उनके मन में विशिष्ट सम्मान भावना थी। प्रत्येक व्यक्ति अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करे, उसमें कार्य करे किंतु देश में सर्वाधिक बोली जाने वाली हिन्दी भाषा भी वह सीखे, यह उनकी हार्दिक इच्छा थी।
गांधी जी प्रांतीय भाषाओं के पक्षधर थे, वहां की शिक्षा का माध्यम भी प्रांतीय भाषाओं को बनाना चाहते थे। हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाने के संदर्भ में उनका दृष्टिकोण स्पष्ट था कि-‘‘ सारे देश के लोग हिन्दी का इतना ज्ञान प्राप्त कर लें तकि देश का राजकाज उसमें चलाया जा सके और सभी भारतवासी एक सामान्य भाषा में संवाद कायम कर सकें।‘‘ वे अकेले राजनीतिक व्यक्ति थे, जिन्होंने भारत की भाषा समस्या, राष्ट्रभाषा पर इतना ध्यान दिया। आधुनिक हिन्दी साहित्य के सुप्रसिद्ध आलोचक, निबंधकार, विचारक एवं कवि रामविलास शर्मा का यह कथन- ‘‘ सत्य अहिंसा, स्वराज, सर्वोदय- किसी भी अन्य विषय पर आज उनके लिये उपादेय नहीं है, जितने भाषा समस्या पर। अंग्रेजी, भारतीय भाषाओं, राष्ट्रभाषा हिन्दी और हिन्दी- उर्दू की समस्या पर उन्होंने जितनी बातें कही हैं, वे बहुत ही मूल्यवान है। किसी भी राजनीतिक नेता ने इन समस्याओं पर इतनी गहराई से नहीं सोचा, किसी भी पार्टी और उसके नेताओं ने भाषा समस्या के सैद्धांतिक समाधान को नित्य प्रतिदिन की कार्रवाई में इस तरह अमलीजामा पहनाया, जैसे गांधी ने। उनकी नीति के मूल सूत्र छोड़ देने से यह समस्या दिन प्रतिदिन उलझती जा रही है।’’
गांधीजी अपनी मां, मातृभूमि और मातृभाषा से अटूट स्नेह रखते थे। सन् 1906 ई. में उन्होंने अपनी एक प्रार्थना में कहा था-
''भारत की जनता से एक रूप होने की शक्ति और उत्कण्ठा दे। हमें त्याग, भक्ति और नम्रता की मूर्ति बना जिससे हम भारत देश को ज्यादा समझें, ज्यादा चाहें। हिन्दी एक ही है। उसका कोई हिस्सा नहीं है हिन्दी के अतिरिक्त दूसरा कुछ भी मुझे इस दुनिया में प्यारा नहीं है।''
इस प्रार्थना से उनका राष्ट्र-प्रेम और राष्ट्रीय एकता के प्रति उनका अनुराग पूर्णरूपेण परिलक्षित होता है। गांधी भाषा को माता मानते थे तथा हिन्दी का सबल समर्थन करते थे। उन्होंने हिन्द स्वराज (सन् 1909 ई.) में अपनी भाषा-नीति की घोषणा इस प्रकार की थी-
‘‘सारे हिन्दुस्तान के लिए जो भाषा चाहिए, वह तो हिन्दी ही होना चाहिए। उसे उर्दू या नागरी लिपि में लिखने की छूट होना चाहिये। हिन्दू-मुसलमानों के संबंध ठीक रहें, इसलिए हिन्दुस्तानियों को इन दोनों लिपियों को जान लेना जरूरी है। ऐसा होने से हम आपस के व्यवहार में अंग्रेजी को निकाल सकेंगे।’’
महात्मा गाँधी ने भारत आकर अपना पहला महत्वपूर्ण भाषण 6 फरवरी 1916 को बनारस में दिया था। उस दिन भारत के वायसराय लार्ड हार्डिंग वहाँ बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने आए थे। महामना मदनमोहन मालवीय के विशेष निमंत्रण पर महात्मा गाँधी भी इस समारोह में शामिल हुए थे। समारोह की अध्यक्षता महाराज दरभंगा कर रहे थे। मंच पर लार्डहार्डिंग के साथ श्रीमती एनी बेसेंट और मालवीयजी भी थे। समारोह में बड़ी संख्या में देश के राजा-महाराजा भी शामिल हुए थे। ये लोग देश के कोने-कोने से तीस विशेष रेलगाड़ियों से आए थे। मालवीयजी के आग्रह पर जब महात्मा गाँधी बोलने खड़े हुए हुए तो उनके अप्रत्याशित भाषण से सभी अवाक और स्तब्ध रह गए थे।
सर्वप्रथम उन्होंने समारोह की कार्रवाई एक विदेशी भाषा अँगरेजी में चलाए जाने पर आपत्ति की और दुख जताया। फिर उन्होंने काशी विश्वविद्यालय मंदिर की गलियों में व्याप्त गंदगी की आलोचना की। इसके बाद उन्होंने मंच पर और सामने विराजमान रत्नजड़ित आभूषणों से दमकते राजाओं-महाराजाओं की उपस्थिति को बेशकीमती जेवरों की भड़कीली नुमाइश बताते हुए उन्हें देश के असंख्य दरिद्रों की दारुण स्थिति का ध्यान दिलाया। उन्होंने जोड़ा कि जब तक देश का अभिजात वर्ग इन मूल्यवान आभूषणों को उतारकर उसे देशवासियों की अमानत समझते हुए पास नहीं रखेगा, तब तक भारत की मुक्ति संभव नहीं होगी। फिर उन्होंने 1916 के कांग्रेस अधिवेषन में अपना भाषण हिन्दी में दिया।
महात्मा गांधी भारतीय स्वतंत्रता-संग्राम में जनसंपर्क हेतु हिन्दी को ही सर्वाधिक उपयुक्त भाषा समझते थे।
इसके बाद 15 अक्टूबर 1917 को भागलपुर केे कटहलबाड़ी क्षेत्र में बिहारी छात्रों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। देशरत्न डाॅ राजेन्द्र प्रसाद के निर्देश पर बिहारी छात्रों के संगठन का काम लालूचक के श्री कृष्ण मिश्र को सौंपा गया था। बिहारी छात्रों के सम्मेेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। अपने संबोधन में महात्मा गांधी ने कहा था-‘ मुझे अध्यक्ष का पद देकर और हिन्दी में व्याख्यान देना और सम्मेेेेलन का काम हिन्दी में चलाने की अनुमति देकर आप बिद्यार्थियों ने मेरे प्रति अपने प्रेेम का परिचय दिया है। इस सम्मेलन का काम इस प्रांत की भाषा में ही और वही राष्ट्रभाषा भी है- करने का निश्चय दुराण्वेषी से किया है।’ इस सम्मेलन में सरोजनी नायडू का भाषण अंग्रेजी से हिन्दी अनुदित होकर छपा था। यह सम्मेलन आगे चलकर भारत की राजनीति, विषेषकर स्वतंत्रता संग्राम में राजनीति का कॅानवास बना, जिससे घर-घर में स्वतंत्रता संग्राम का शंखनाद करना मुमकिन हो सका। वही प्रसिद्ध गांधीवादी काका कालेलकर ने इस सम्मेलन के भाषण कोे राष्ट्रीय महत्व प्रदान कर राष्ट्रभाषा हिन्दी की बुनियाद डाली थी। बाद में इसी कटहलबाड़ी परिसर में मारबाड़ी पाठषाला की स्थापना हुुई।
सन् 1917 ई. में कलकत्ता (कोलकाता) में कांग्रेस अधिवेशन के अवसर पर राष्ट्रभाषा प्रचार संबंध कांफ्रेन्स में तिलक ने अपना भाषण अंग्रेजी में दिया था। जिसे सुनने के बाद गांधीजी ने कहा था-
‘‘बस इसलिए मैं कहता हूं कि हिन्दी सीखनें की आवश्यकता है। मैं ऐसा कोई कारण नहीं समझता कि हम अपने देशवासियों के साथ अपनी भाषा में बात न करें। वास्तव में अपने लोगों के दिलों तक तो हम अपनी भाषा के द्वारा ही पहुंच सकते हैं।’’
महात्मा गांधी किसी भाषा के विरोधी नहीं थे। अधिक से अधिक भाषाओं को सीखना वह उचित समझते थे। प्रत्येक भाषा के ज्ञान को वह महत्वपूर्ण मानते थे किंतु उन्होंने निज मातृभाषा और हिन्दी का सदैव सबल समर्थन किया। एक अवसर पर उन्होंने कहा था-
‘‘भारत के युवक और युवतियां अंग्रेजी और दुनिया की दूसरी भाषाएं खूब पढ़े मगर मैं हरगिज यह नहीं चाहूंगा कि कोई भी हिन्दुस्तानी अपनी मातृभाषा को भूल जाय या उसकी उपेक्षा करे या उसे देखकर शरमाये अथवा यह महसूस करे कि अपनी मातृभाषा के जरिए वह ऊंचे से ऊंचा चिन्तन नहीं कर सकता।’’
गांधीजी शिक्षा के माध्यम के लिए मातृभाषा को ही सर्वोत्तम मानते थे। उनका स्पष्ट मत था कि शिक्षा का माध्यम तो प्रत्येक दशा में मातृभाषा ही होनी चाहिए।
1918 में वाइसराय की सभा में में जब रंगरूटों की भर्ती के सिलसिले में गांधी गये तो उन्होंने हिन्दी- हिन्दूस्तानी में बोलने की इजाजत मांगी। इस घटना का उल्लेख करते हुए उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है-‘‘ हिन्दुस्तानी में बोलने के लिये मुझे बहुतों ने धन्यवाद दिया। वे कहते थे कि वाइसराय की सभा में हिन्दुस्तानी में बोलने का यह पहला उदाहरण था।पहले उदाहरण की बात सुनकर मैं शरमाया। अपने ही देश में , देश से संबध रखनेवाले काम की सभा में, देश की भाषा का वहिष्कार कितने दुख की बात है।’’
उनकी इच्छा थी कि भारत के प्रत्येक प्रदेश में शिक्षा का माध्यम उस-उस प्रदेश की भाषा को होना चाहिए। उनका कथन था-
‘‘राष्ट्र के वालक अपनी मातृभाषा में नहीं, अन्य भाषा में शिक्षा पाते हैं, वे आत्महत्या करते हैं। इससे उनका जन्मसिद्ध अधिकार छीन जाता है। विदेशी भाषा से बच्चों पर बेजा जोर पड़ता है और उनकी सारी मौलिकता नष्ट हो जाती है। इसलिए किसी विदेशी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना मैं राष्ट्र का बड़ा दुर्भाग्य मानता हूं।’’
इसके बाद गांधी जी ने कांग्रेस के अंदर प्रवेष कर उसकी कार्रवाईयों में हिन्दी को स्थान दिलाने के प्रयास शुरू किये। राष्ट्रीय नेताओं लोकमान्य वाल गंगाधर तिलक से हिन्दी सीखने का आग्रह, रवीन्द्रनाथ ठाकुर से हिन्दी सीखने का आग्रह महत्वपूर्ण है। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने काठियावाड़ में अपना भाषण हिन्दी में दिया।
इसी प्रकार एक अन्य अवसर पर उन्होंने अपना विचार इस प्रकार प्रकट किया था-
‘‘यदि हिन्दी अंग्रेजी का स्थान ले ले तो कम से कम मुझे तो अच्छा ही लगेगा। अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, लेकिन वह राष्ट्रभाषा नहीं हो सकती। अगर हिन्दुस्तान को सचमुच हमें एक राष्ट्र बनाना कोई माने या न माने राष्ट्रभाषा तो हिन्दी ही बन सकती है।’’
महात्मा गांधी ने भाषा के प्रश्न को स्वराज्य से जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि यदि स्वराज्य देश के करोड़ो भूखे, अनपढ,दलितों के लिए होना है तो जन-सामान्य की भाषा हिन्दी को राष्ट्रीय भाषा बनाना होगा।
मार्च 1918 में इंदौर में सम्पन्न हुए हिंदी साहित्य सम्मेलन के अधिवेशन के सभापति बनाए गये। सभापति के रूप में उन्होंने अपने भाषण में जोरदार शब्दों में कहा, जैसे अंग्रेज अपनी मादरी जबान अंग्रेजी में ही बोलते और सर्वथा उसे ही व्यवहार में लाते हें, वैसे ही मैं आपस प्रार्थना करता हूं कि— 'आप हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा बनने का गौरव प्रदान करें। हिंदी सब समझते हैं। इसे राष्ट्रभाषा बनाकर हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। इसी भाषण में उन्होंने हिंदी के क्षेत्र-विस्तार की आवश्यकता की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा, साहित्य का प्रदेश भाषा की भूमि जानने पर हो निश्चित हो सकता है। यदि हिंदी भाषा की भूमि सिर्फ उत्तर प्रांत की होगी, तो साहित्य का प्रदेश संकुचित रहेगा। यदि हिंदी भाषा राष्ट्रीय भाषा होगी, तो साहित्य का विस्तार भी राष्ट्रीय होगा। जैसे भाषक वैसी भाषा। भाषा-सागर में स्नान करने के लिए पूर्व-पश्चिम, दक्षिण-उत्तर से पुनीत महात्मा आएंगे, तो सागर का महत्व स्नान करने वालों के अनुरूप होना चाहिए।''
उपर्युक्त वक्तव्य से जाहिर है कि उत्तर प्रांत में हिंदी भाषा एवं साहित्य का जो उत्थान हो रहा था, उससे गांधी जी अवगत थे, लेकिन संतुष्ट नहीं, क्योंकि उनकी समझ में हिंदी का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक सबके लिए होना चाहिए- उसे एक सागर की तरह व्यापक होना चाहिए, न कि नदी की तरह संकुचित। इसी बात को बाद में उनके परम शिष्य विनोबा भावे ने इस प्रकार कहा, हिंदी को नदी नहीं, समुद्र बनना होगा।अर्थात् उत्तरी प्रांत में उभरा हिंदी नवजागरण एक उफनती नदी जैसा था, तो उसे राष्ट्रव्यापी सागर में परिणत करने का प्रयास गांधी जी के द्वारा हुआ, यह मानने में कोई अतिवाद नहीं है। इस तथ्य को ध्यान में रखने में हिंदी-भाषी प्रदेश के आधार पर हिंदी जाति की बात करना असंगत प्रतीत होता है। वस्तुतः गुजराती या बंगला या मराठी की तर्ज पर हिंदी को किसी प्रदेश विशेष की जाति की भाषा कहना, उसके कद को छोटा करना होगा।
इंदौर साहित्य-सम्मेलन के अवसर पर गांधी जी ने हिंदी के प्रचार के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य का आरंभ कराया जिसका संबंध दक्षिण भारत में हिंदी के प्रचार से था। उन्होंने अपने उसी भाषण में यह कहा कि- सबसे कष्टदायी मामला द्रविड़ भाषाओं के लिए है। वहां तो कुछ प्रयत्न भी नहीं हुआ है। हिंदी भाषा सिखाने वाले शिक्षकों को तैयार करना चाहिए। ऐसे शिक्षकों की बड़ी ही कमी है। इस कथन से स्पष्ट है कि दक्षिण भारत में हिंदी के प्रचार को लेकर तब तक कोई विशेष कार्य नहीं हुआ था। दक्षिण भारतीयों के बीच हिंदी का कैसे प्रचार हो, यह गांधी जी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण समस्या थी।
भारतीय राजनेताओं में गांधीजी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने द्रविड़ प्रदेश में राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने के लिए हिंदी को विधिवत् सिखाया जाना आवश्यक समझा और उसके लिए उन्होंने ठोस योजना प्रस्तुत की, जिसके अंतर्गत पुरुषोत्तम दास टंडन, वेंकटेश नारायण तिवारी, शिव प्रसाद गुप्ता सरीखे हिंदी-सेवियों को लेकर दक्षिण भारत हिन्द प्रचार सभा का गठन किया। इंदौर साहित्य-सम्मेलन के समापन के तुरंत बाद गांधी जी ने अखबारों के लिए एक पत्र जारी किया जिसमें उन्होंने दक्षिण वालों को हिंदी सीखने के लिए उत्साहित करते हुए कहा था, यदि हमें स्वराज्य का आदर्श पूरा करना है तो हमें एक ऐसी भाषा की जरूरत पड़ेगी ही, जिसे देश की विशाल जनता आसानी से समझ और सीख सके। ऐसी भाषा तो सदा से हिंदी हो रही है। मुझे मद्रास प्रांत की जनता की देशभक्ति, आत्मत्याग और बुद्धिमत्ता पर काफी भरोसा है। मैं जानता हूं कि जो भी लोग राष्ट्र की सेवा करना चाहेंगे या अन्य प्रांतों के साथ सम्पर्क चाहेंगे, उनको त्याग करना ही पड़ेगा, यदि हिंदी सीखने को त्याग ही माना जाय।
इंदौर हिंदी सम्मेलन के अवसर पर गांधी जी द्वारा व्यक्त विचारों पर गौर करें, तो मानना पडेगा कि हिंदी के संबंध में कुछ विशिष्ट बातें पहली बार राष्ट्र के सामने आयीं। हिंदी समस्त भारतवर्ष की सम्पर्क-भाषा बने, यह भारतीय नवजागरण के कई बौद्धिकों द्वारा प्रतिपादित किया जा चुका था, लेकिन यह कैसे संभव हो सके, इस संबंध में कोई सुनिश्चित योजना उनके द्वारा नहीं प्रस्तुत की जा सकी थी।
गाँधी जी ने 20 अक्टूबर 1917 ई. को गुजरात के द्वितीय शिक्षा सम्मेलन में दिए गए अपने भाषण में राष्ट्रभाषा के कुछ विशेष लक्षण बताए थे, वे निम्न हैं।
1. वह भाषा सरकारी नौकरों के लिए आसान होनी चाहिए।
2. उस भाषा के द्वारा भारत का आपसी धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक कामकाज शक्य होना चाहिए।
3. उस भाषा को भारत के ज्यादातर लोग बोलते हों।
4. वह भाषा राष्ट्र के लिए आसान होनी चहिए।
5. उस भाषा का विचार करते समय क्षणिक या अस्थायी स्थिति पर जोर न दिया जाये।
अंग्रेजी भाषा में इनमें एक भी लक्षण नहीं है। यह माने बिना काम चल नहीं सकता।हिन्दी भाषा में ये सारे लक्षण मौजूद हैं। हिन्दी भाषा मैं उसे कहता हूॅं जिसे उत्तर में हिन्दू और मुसलमान बोलते हैं और देवनागरी या फारसी में लिखते हैं।
20 अक्टूबर के बाद 11 नवम्बर, 1917 को बिहार के मुजफ्फरपुर शहर में भाषण करते हुए उन्होंने कहा, मैं कहता आया हूं कि राष्ट्रीय भाषा एक होनी चाहिए और वह हिंदी होनी चाहिए। हमारा कर्तव्य यह है कि हम अपना राष्ट्रीय कार्य हिंदी भाषा में करें। हमारे बीच हमें अपने कानों में हिंदी के ही शब्द सुनाई दें, अंग्रेजी के नहीं। इतना ही नहीं, हमारी धारा सभाओं में जो वाद-विवाद होता है, वह भी हिंदी में होना चाहिए। ऐसी स्थिति लाने के लिए मैं जीवन-भर प्रयत्न करूंगा।
इस दृष्टि से गांधी जी पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने हिंदी के राष्ट्रव्यापी प्रचार-प्रसार के लिए सुविचारित योजना प्रस्तुत की और हिंदी प्रचार के कार्य को मिशनरी स्वरूप प्रदान किया। धर्म के प्रचार को लेकर तो मानव-इतिहास में बहुतेरे मिशनरी, आत्मत्यागी महात्मा लोग होते आये है, लेकिन किसी भाषा के प्रचार के लिए मिशन की तरह, आत्मत्याग के रूप में काम करने का आह्वान करने वाले गांधी जी कदाचित् प्रथम व्यक्ति थे, जिन्होंने यह आह्वान हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए किया।
13 दिसम्बर, 1920 को कलकत्ता में भाषण करते हुए गांधीजी ने कहा, यह निश्चित है कि सारे देश में जहां-कहीं देश के विभिन्न हिस्सों के लोगों की मिली-जुली सभाएं और बैठकें होंगी, उनमें अभिव्यक्ति का राष्ट्रीय माध्यम हिंदी ही होगी। 22 जनवरी, 1921 को जारी किए, अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा, जो बात मैं जोर देकर आपसे कहना चाहता हूं वह यह कि आप सबकी एक सामान्य भाषा होनी चाहिए, सभी भारतीयों की एक सामान्य भाषा होनी चाहिए, ताकि वे भारत में जिस हिस्से में भी जायें, वहां के लोगों से बातचीत कर सकें। इसके लिए आपको हिंदी को अपनाना चाहिए। 23 मार्च 1921 को विजयनगरम में राष्ट्रभाषा हिंदी के महत्व को बताते हुए उन्होंने कहा, हिंदी पढ़ना इसलिए जरूरी है कि उससे देश में भाईचारे की भावना पनपती है। हिंदी को देश की राष्ट्रभाषा बना देना चाहिए। हिंदी आम जनता की भाषा होनी चाहिए। आप चाहते हैं कि हमारा राष्ट्र एक ओर संगठित हो, इसलिए आपकी प्रान्तीयता के अभियान को छोड़ देना चाहिए। हिंदी तीन ही महीनों में सीखी जा सकती है।
हिंदी के सवाल को गांधी जी केवल भावनात्मक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं मानते थे, अपितु उसे एक राष्ट्रीय आवश्यकता के रूप में भी देखने पर जोर देते थे। 10 नवम्बर, 1921 के ‘यंग इण्डिया’ में उन्होंने लिखा हिंदी के भावनात्मक अथवा राष्ट्रीय महत्व की बात छोड़ दें तो भी यह दिन प्रतिदिन अधिकाधिक आवश्यक मालूम होता जा रहा है कि तमाम राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं को हिंदी सीख लेनी चाहिए और राष्ट्र की तमाम कार्यवाही हिंदी में ही की जानी चाहिए। इस प्रकार असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने पूरे देश में हिंदी का राष्ट्रभाषा के रूप में प्रचार काफी जोरदार ढंग से किया और उसे राष्ट्रीय एकता, अखण्डता, स्वाभिमान का पर्याय-सा बना दिया।
उन्होंने अपने पुत्र देवदास गांधी को हिन्दी-प्रचार के लिए दक्षिण भारत भेजा था। दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा की स्थापना उन्हीं की परिकल्पना का परिणाम है। उन्होंने वर्धा में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना हिन्दी के प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से ही की थी तथा जन-नेताओं को भी हिन्दी में कार्य करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया था। उनकी प्रेरणा के ही परिणाम स्वरूप हिन्दीतर भाषा-भाषाी प्रदेशों के स्वतंत्रता संग्राम के ने हिन्दी को सीख लिया था और उसे व्यापक जन-सम्पर्क का माध्यम बनाया था।
महात्मा गांधी ने सभी भारतीय भाषाओं का समादर और हिन्दी के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए 17 मई 1942 तथा 9 अगस्त 1946 को कहा था-
महान प्रांतीय भाषाओं को उनके स्थान से च्युत करने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय भाषा की इमारत प्रांतीय भाषाओं की नींव पर ही खड़ी की जानी है। दोनों का लक्ष्य एक-दूसरे की जगह लेना नहीं, बल्कि एक-दूसरे की कमी को पूरा करना है।
महात्मा गांधी के विचार, महान् भारतीय नेताओं की भावना और हिन्दी-भाषा-भाषी जनता की विशाल संख्या को दृष्टिगत रखते हुए पर्याप्त चिंतन-मनन के उपरांत भारतीय संविधान निर्माताओं ने हिन्दी को भारतीय संविधान में राजभाषा की प्रतिष्ठा प्रदान की थी। 16 जून, 1920 के ‘यंग इंडिया’ में उन्होंने लिखा, मुझे पक्का विश्वास है कि किसी दिन हमारे द्रविड भाई-बहन गंभीर भाव से हिंदी का अध्ययन करने लगेंगे। आज अंग्रेजी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए वे जितनी मेहनत करते हैं, उसका आठवां हिस्सा भी हिंदी सीखने में करें, तो बाकी हिंदुस्तान जो आज उनके लिए बंद किताब की तरह है, उससे वे परिचित होंगे और हमारे साथ उनका ऐसा तादात्म्य स्थापित हो जायेगा जैसा पहले कभी न था।
हिंदी के प्रचार को लेकर गांधी जी का ध्यान देश के दक्षिणी छोर की तरफ जितना था, उतना ही पूर्वी छोर की तरफ भी था। मार्च, 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को जरूर स्थगित कर दिया, लेकिन राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के प्रचार का उनका कार्य जारी रहा। 24 मार्च, 1925 को हिंदी प्रचार कार्यालय, मद्रास में बोलते हुए गांधीजी ने कहा, मेरी राय में भारत में सच्ची राष्ट्रीयता के विकास के लिए हिंदी का प्रचार एक जरूरी बात है, विशेष रूप से इसलिए कि हमें उस राष्ट्रीयता को आम जनता के अनुरूप सॉचे में ढालना है। और सचमुच सच्ची राष्ट्रीयता के विकास के लिए गांधी जी जीवन-पर्यंत हिंदी के प्रचार-कार्य में लगे रहे। राष्ट्रभाषा के दायरे से मेहनतकश वर्ग बाहर न रहे, इसका भी गांधी जी ने पूरा ध्यान रखा। 21 दिसम्बर, 1933 को पैराम्बूर की मजदूर सभा में बोलते हुए गांधी जी ने कहा, साथी मजूदरों, यदि आप सारे भारत के मजदूरों के दुःख-सुख को बांटना चाहते हैं, उनके साथ तादात्म्य स्थापित करना चाहते हैं, तो आपको हिंदी सीख लेनी चाहिए, जब तक आप ऐसा नहीं करते, तब तक उत्तर और दक्षिण भारत में कोई मेल नहीं हो सकता।
जब भारत को स्वतंत्रता मिली ही थी। देश-विदेश के विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं के पत्रकार इस महत्वपूर्ण घटना के प्रकाशन हेतु भारतीय नेताओं के वक्तव्य, संदेश आदि के लिए आ रहे थे। ऐसे माहौल में एक विदेशी पत्रकार महात्मा गांधी से मिला। उसने बापू से अपना संदेश देने को कहा। किंतु वह इस बात पर अड़ रहा था कि बापू अपना संदेश अंग्रेजी में दें। गांधीजी इसके लिए सहमत नहीं हो रहे थे। मगर पत्रकार था कि लगातार जिद कर रहा था। उसका कहना था कि संदेश भारतीयों के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए है, इसलिए वह अंग्रेजी में ही बात कहें। उन दिनों बापू हिंदी का राष्ट्रभाषा के रूप में प्रचार भी कर रहे थे। थोड़ी देर तक वह शांत बने रहे, मगर अंततः पत्रकार की बात पर महात्मा गांधी ने उसे दो टूक उत्तर देते हुए कहा- दुनिया से कह दो कि गांधी अंग्रेजी नहीं जानता।
गांधी के अभियान का हश्र यह हुआ कि उत्तर प्रदेश, बिहार और अन्य क्षेत्रों के साहित्यकार जनपदीय भाषा को भूलकर राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी के विकास में अपनी कलम चलायी। प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, भवानी प्रसाद मिश्र, विष्णु प्रभाकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि ने हिन्दी को राष्ट्रीय धर्म के रूप में अपनाया। बिहार में भी आचार्य शिवपूजन सहाय, राधिकारमण सिंह, रामवृक्ष वेनीपुरी, लक्ष्मी नारायण सुधांशु, नार्गाजुन, फणीश्वर नाथ रेणु आदि ने भी अपनी क्षेत्रीय वोलियों के मोह से उपर उठकर हिन्दी के विकास में योगदान देना अपना राष्ट्रीय धर्म समझा।








.jpg)


.jpg)