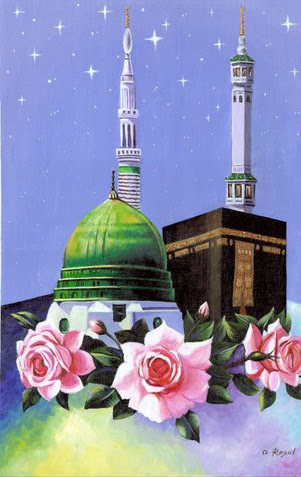फ़िरदौस ख़ान
खुम्बी यानी मशरूम बहुत स्वादिष्ट और पौष्टिक खाद्य पदार्थ है. यह एक प्रकार की कवक है. इसे खुम्ब और कुकुरमुत्ता भी कहा जाता है. अमूमन बरसात के मौसम में यह उग जाती है. दुनिया में दो हज़ार से ज़्यादा क़िस्मों की खुम्बी पाई जाती हैं. मगर इनमें से बहुत कम यानी तक़रीबन 250 क़िस्म की खुम्बी ही खाने के लायक़ होती हैं. बाक़ी खुम्बी ज़हरीली होती हैं, जो सेहत के लिए नुक़सानदेह हैं. चीन खुम्बी की कई प्रजातियों की खेती बहुत पहले से होती रही है. लेकिन दुनिया में सबसे पहले 1650 में फ़्रांस में श्वेत बटन खुम्बी की बाक़ायदा खेती शुरू हुई थी. भारत में तक़रीबन पांच दशक पहले खुम्बी की खेती की तरफ़ ध्यान दिया गया. हालांकि फ़िलहाल दुनिया में तक़रीबन 40 क़िस्म की खुम्बी की खेती की जा रही है, जिनमें श्वेत बटन मशरूम, ग्रीष्मकालीन श्वेत बटन मशरूम, ब्लैक ईयर मशरूम, शिटाके मशरूम, काबुल ढींगरी, ढींगरी मशरूम, पराली मशरूम और दूधिया मशरूम आदि शामिल हैं. श्वेत बटन मशरूम विश्व में सर्वाधिक उगाई जाने वाली खुम्बी है. औषधीय गुणों की उपलब्धता के कारण इसका औषधीय महत्व भी है. शिटाके मशरूम विश्व खुम्बी उत्पादन में दूसरे स्थान पर है. इसे खुम्बी का राजा भी कहा जाता है. ढिंगरी मशरूम विश्व में उगाए जानी वाली खुम्बियों में तीसरे स्थान पर है. एक अनुमान के मुताबिक़ दुनियाभर के एक सौ से भी ज़्यादा देशों में 50 लाख टन से ज़्यादा खुम्बी का सालाना उत्पादन किया जाता है, जबकि भारत में हर साल तक़रीबन 40 हज़ार टन श्वेत बटन मशरूम का उत्पादन किया जाता है. यहां से हर साल हज़ारों टन खुम्बी का निर्यात किया जा रहा है.
ग़ौरतलब है कि विश्व बाज़ार में खुम्बी की बढ़ती मांग को देखते हुए भारत में भी इसे प्रोत्साहन मिला. हिमाचल प्रदेश के चम्बाघाट में स्थित हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय में खुम्बी पर शोध कार्य शुरू किया गया. 23 अक्टूबर 1982 को छठी पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय मशरूम अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र सोलन में स्थापित करने का फ़ैसला किया गया. अगले ही साल 8 जून 1983 को इसका निर्माण कार्य शुरू हो गया. फिर 21 जून 1986 को तत्कालीन केंद्रीय कृषि मंत्री जीएस ढिल्लो ने इसका उदघाटन किया. सोलन से ही अखिल भारतीय समन्वित मशरूम अनुसंधान परियोजना शुरू की गई. इसके केंद्र लुधियाना, पंत नगर, फ़ैज़ाबाद, रायपुर, उदयपुर, कोयंबटूर, पुणे और गोआ काम कर रहे हैं. कृषि वैज्ञानिकों के शोध के बाद वैज्ञानिक तरीक़े से इसकी खेती की जा रही है. अन्य फ़सलों की तरह इसे ख़ास तरह की ज़मीन की ज़रूरत नहीं होती. इसकी खेती कमरों, छप्परों और गमलों में भी की जा सकती है. इसलिए खुम्बी की खेती भूमिहीन, सीमांत किसानों और महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रही है.
खुम्बी की खेती दो तरह से की जाती है. पहली सीजनल और दूसरी नियंत्रित वातावरण में. खुम्बी को विभिन्न फ़सली चक्रों में साल भर उगाया जा सकता है, जैसे मैदानी इलाक़ों और कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों पर सर्दियों के मौसम में श्वेत बटन मशरूम, गर्मियों में ग्रीष्मकालीन श्वेत बटन मशरूम व ढींगरी और बारिश के मौसम में पराली मशरूम व दूधिया मशरूम की खेती की जा सकती है. मैदानी इलाकों में नवम्बर से फ़रवरी तक श्वेत बटन मशरूम उगाया जा सकता है. इसी तरह सितम्बर से नवम्बर और फ़रवरी से अप्रैल तक ग्रीष्मकालीन श्वेत बटन मशरूम की खेती की जा सकती है. सितम्बर से मई तक ढींगरी मशरूम उगाया जा सकता है. जुलाई से सितम्बर तक पराली मशरूम की खेती की जा सकती है. दूधिया मशरूम फ़रवरी से अप्रैल और जुलाई से सितम्बर तक उगाया जा सकता है. मध्यम उंचाई वाले पहाड़ी इलाक़ों में सितम्बर से मार्च तक श्वेत बटन मशरूम की खेती की जा सकती है. इसी तरह जुलाई से अगस्त और मार्च से मई तक ग्रीष्मकालीन श्वेत बटन मशरूम उगाया जा सकता है. अक्टूबर से फ़रवरी तक शिटाके मशरूम और अप्रैल से जून तक दूधिया मशरूम की खेती की जा सकती है. ढिंगरी मशरूम को पूरे साल उगाया जा सकता है. ज़्यादा उंचाई वाले पहाड़ी इलाक़ों में मार्च से नवम्बर तक श्वेत बटन मशरूम की खेती की जा सकती है. इसी तरह मई से अगस्त तक ढिंगरी मशरूम और दिसम्बर से अप्रैल तक शिटाके मशरूम उगाया जा सकता है.
कृषि विशेषज्ञ के मुताबिक़ खुम्बी की अच्छी पैदावार लेने के लिए उन्नत क़िस्म के बीज और कुशल प्रबंधन की ज़रूरत होती है. खुम्बी उत्पादन के लिए सही कमरे का इस्तेमाल किया जाना चाहिए. कमरा हमेशा पूर्व-पश्चिम दिशा में होना चाहिए. इससे ताज़ी हवा और तापमान सही बना रहता है. कमरों का इंतज़ाम ऐसा होना चाहिए कि इनकी दूषित हवा दूसरे कमरे में न जाए. कमरे में बिजली के पंखों और पानी का इंतज़ाम होना चाहिए. कमरों का आकार 35 गुणा 25 गुणा 12 हो, तो बेहतर है, क्योंकि इसमें पांच शेल्फ़ों में 18 से 20 टन कम्पोस्ट ली जा सकेगी. खुम्बी उत्पादन के लिए उन्हीं पदार्थों से कंपोस्ट तैयार करनी चाहिए, जो आसानी से उपलब्ध होने के साथ-साथ सस्ते भी हों. कंपोस्ट पक्के फ़र्श पर ही बनानी चाहिए. कम्पोस्ट बनाने से पहले फ़र्श पर दो फ़ीसद फ़ारमेलिन के घोल डाल देना चाहिए, ताकि रोगों और कीटों से बचाव हो सके. कम्पोस्ट बनाते वक़्त पानी की मात्रा शुरू में ही इतनी हो, जिससे जिप्सम मिलाने के बाद कम्पोस्ट में पानी न डालना पड़े, क्योंकि बाद में पानी डालने पर चिकनापन आ जाता है, जिससे खुम्बी का जाला फैलने में परेशानी आती है.
कम्पोस्ट बनाते वक़्त बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है. कम्पोस्ट का ढेर बनाते वक़्त उसकी चौड़ाई और ऊंचाई पांच फ़ुट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. पलटाई इस तरह करनी चाहिए कि नीचे की खाद ऊपर और ऊपर की नीचे आ जाए, ताकि रासायनिक क्रियाएं सुचारू रूप से हो सकें. ढेर बनाते वक़्त कम्पोस्ट में नाइट्रोजन की मात्रा 1.5 से 1.75 फ़ीसद होनी चाहिए, जबकि खाद में इसकी दर 2. 6 फ़ीसद से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. तैयार कम्पोस्ट का पीएच मान 7.2 से 7.8 होना चाहिए और इसमें अमोनिया गैस की गंध न हो. तैयार कम्पोस्ट का रंग गहरा भूरा होना चाहिए. उसमें चिपचिपापन नहीं होना चाहिए और नमी की मात्रा 68 से 72 फ़ीसद होनी चाहिए. तैयार कम्पोस्ट में खुम्बी का बीज मिलाने से पहले नमी और अमोनिया की जांच ज़रूर करें. ज़्यादा पानी और अमोनिया दोनों ही खुम्बी के बीज के लिए नुक़सानदेह हैं. इन्हें कम करने के लिए तीन-चार दिन के अंतराल पर पलटाई करते हुए खाद को खुला छोड़ देना चाहिए. खुम्बी का बीज मिलाने के लिए कम्पोस्ट की तह छह इंच रखनी चाहिए, जबकि थैलों में सिर्फ़ तीन चौथाई खाद डालनी चाहिए. पीली फफूंद की रोकथाम के लिए प्रति 10 क्विंटल कम्पोस्ट में 1.5 लीटर फ़ारमोलिन और 75 ग्राम बाविस्टीन 50 लीटर पानी में घोल कर छिड़कें और दो दिन के लिए ढक दें.
खुम्बी का अच्छा उत्पादन लेने के लिए हमेशा अच्छी क़िस्म का ताज़ा बीज इस्तेमाल करना चाहिए. ध्यान रहे कि अनाज के दाने पर खुम्बी के फफूंद का जाला सफ़ेद और रेशम जैसा होना चाहिए. खुम्बी का बीज स्पॊन बनाने के लिए गेहूं का इस्तेमाल किया जाता है. गेहूं को ठंडे पानी में कई बार धोकर तब तक उबाला जाता है, जब तक उसके दाने नरम नहीं हो जाते. बस दाने फटने नहीं चाहिए. इसके बाद गेहूं के दानों को छाया में सुखा लिया जाता है. अब इनमें कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम सल्फ़ेट मिलाते हैं. बीज आपस में चिपकने नहीं चाहिए. इन दानों को बोतलों या प्लास्टिक के थैलों में भर लिया जाता है. बोतलों के मुंह पर रूई लगाकर और थैलियों के मुंह को डोरी से बांधकर बंद कर दिया जाता है. अब इन बोतलों और थैलों को निवेशन कक्ष में रख दिया जाता है. इन्हें 28 से 30 डिग्री सेल्सियस पर तीन हफ़्ते तक रखा जाता है. इस दौरान खुम्बी का जाल फैल जाता है. कम्पोस्ट में हमेशा खुम्बी का बीज 5.0 से 7.5 फ़ीसद की दर से मिलाना चाहिए. कम्पोस्ट में बीज मिलाने के बाद फ़ौरन रैकों और थैलियों को दो फ़ीसद फ़ारमेलिन से उपचारित काग़ज़ से ढक दें. बिजाई के बाद खुम्बी भवन में 0.1 फ़ीसद मैलाथियान या 0.5 फ़ीसद नुवान का छिड़काव करें, ताकि कीटों के संक्रमण से बचा जा सके. खुम्बी का जाल फैलने के लिए खुम्बी भवन का तापमान 24 से 26 डिग्री सैल्सियस और नमी की मात्रा 90 फ़ीसद के आसपास होनी चाहिए. शुरू में खुम्बी का जाला कम्पोस्ट में तेज़ी से फैलने के लिए खुम्बी भवन में कार्बन डाई ऒक्साइड की मात्रा ज़्यादा रखने के लिए सभी खिड़कियां, रौशनदान और दरवाज़े बंद रखने चाहिए. कम्पोस्ट में जाला फैलने के वक़्त खुम्बी भवन का तापमान 27 डिग्री सैल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए.
केसिंग मिश्रण को भी अच्छी तरह से तैयार करना चाहिए. केसिंग मिश्रण को 5 फ़ीसद फ़ारमेलिन से निर्जीवीकरण करने के बाद ही इस्तेमाल करना चाहिए. केसिंग मिश्रण का पीएच मान 7 फ़ीसद से 7.5 के बीच होना चाहिए. इसमें पानी सोखने की क्षमता तक़रीबन 60 फ़ीसद होनी चाहिए. कम्पोस्ट में पूरी तरह से जाला फैलने के बाद केसिंग मिश्रण को साफ़ पानी से गीला करने के बाद समानांतर मात्रा में कम्पोस्ट के ऊपर ढक देना चाहिए. ध्यान रहे सतह की मोटाई 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. केसिंग के बाद 0.15 फ़ीसद डाईथेन एम-45 या 0.1 फ़ीसद बावस्टिन और 0.1 फ़ीसद मैलाथियान 50 ईसी का छिड़काव करना चाहिए. केसिंग के 8 से 10 दिन बाद कमरों में नमी की मात्रा 90 से 95 फ़ीसद और तापमान 24 से 26 डिग्री सैल्सियस के बीच होना चाहिए. कार्बन डाई ऒक्साइड की ज़्यादा मात्रा बनाए रखने के लिए कमरे के दरवाज़े, खिड़कियां और रौशनदान बंद रखने चाहिए. केसिंग के 8 से 10 दिन बाद जब छोटे-छोटे पिन हैड निकलने लगें, तो कमरे की खिड़कियां, रौशनदान और दरवाज़े खोल दें, ताकि ताज़ी हवा अंदर आ सके और कार्बन डाई ऒक्साइड की मात्रा घट जाए. ऐसे में कमरे का तापमान 16 से 18 डिग्री सैल्सियस और नमी की मात्रा 80 से 90 फ़ीसद होनी चाहिए.
खुम्बी के उत्पादन के बाद बची कंपोस्ट का एक अति उत्तम ऑर्गेनिक खाद के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है. बहुत से किसान अपनी पारंपरिक फ़सलों के अलावा खुम्बी उत्पादन करके अतिरिक्त आमदनी अर्जित कर रहे हैं. बेकार पड़ी बंजर भूमि में भी खुम्बी की खेती की जा सकती है. कच्चे कमरे बनाकर भी इसकी खेती की जा सकती है. खुम्बी की कई क़िस्में 15 से 20 दिनों में ही उगनी शुरू हो जाती हैं, जबकि कुछ क़िस्मों को उगने में ढाई महीने तक का वक़्त लग जाता है. ग्रामीण महिलाएं भी खुम्बी का उत्पादन करके आत्मनिर्भर बन रही हैं. बेरोज़गारों के लिए खुम्बी आमदनी का बेहतर ज़रिया है. उत्तर भारत के मैदानी इलाक़ों में सर्दी के महीनों में बटन खुम्ब और गर्मियों में धान पुआल खुम्ब की खेती की जा सकती है. उत्तर भारत में सफ़ेद बटन मशरूम सबसे ज़्यादा उगाई जाती है. नियंत्रित वातावरण में बटन मशरूम की खेती सालभर की जा सकती है. इस दौरान मशरूम की चार से पांच फ़सलें मिल जाएंगी. खुम्बी की सीजनल खेती में लागत कम होने की वजह से यह ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो रही है.
खुम्बी स्वास्थ्यवर्धक और औषधीय गुणों से भरपूर है. इसमें एमीनो एसिड, खनिज, लवण, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन बी-12 जैसे पौष्टिक तत्व होते हैं. इससे बहुत-सी दवाएं और टॊनिक बनाए जाते हैं. यह खाने में स्वादिष्ट है. इससे तरह-तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जाते हैं. बाज़ार में इसकी मांग बढ़ रही है. चूंकि खुम्बी एक महंगी सब्ज़ी है, इसलिए यह पंच सितारा होटलों में पौष्टिक आहार के रूप में परोसी जाती है. विशेष समारोहों में भी खुम्बी पौष्टिक और महंगे भोजन की जगह ले रही है.
पिछले तीन दशकों में खुम्बी उत्पादन में क्रांति आई है. खुम्बी की बढ़ती मांग का ही नतीजा है कि आज पारंपरिक खेतीबाड़ी करने वाले किसान भी खुम्बी उत्पादन में दिलचस्पी दिखा रहे हैं. हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब और तमिलनाडु आदि राज्यों में खुम्बी का उत्पादन फलफूल रहा है. हर साल खुम्बी उत्पादन में इज़ाफ़ा हो रहा है और यह बढ़ोतरी देश ही नहीं, बल्कि विश्व स्तर पर देखी जा रही है. खुम्बी उत्पादन को स्वरोज़गार के तौर पर अपनाया जा सकता है. सरकार ने स्वरोजगार योजनाओं में खुम्बी उत्पादन को भी शामिल किया है. सरकार खुम्बी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी जानकारी के अलावा क़र्ज़ भी मुहैया करवा रही है. इस क्षेत्र में अब निजी बैंक भी सक्रिय हो रहे है, जिसका सीधा फ़ायदा उत्पादकों को मिल रहा है. बेरोज़गार युवा प्रशिक्षण हासिल करते खुम्बी की खेती कर रहे हैं.
जब से दुनिया शुरू हुई है, तभी से इंसान और क़ुदरत के बीच गहरा रिश्ता रहा है. पेड़ों से पेट भरने के लिए फल-सब्ज़ियां और अनाज मिला. तन ढकने के लिए कपड़ा मिला. घर के लिए लकड़ी मिली. इनसे जीवनदायिनी ऒक्सीज़न भी मिलती है, जिसके बिना कोई एक पल भी ज़िन्दा नहीं रह सकता. इनसे औषधियां मिलती हैं. पेड़ इंसान की ज़रूरत हैं, उसके जीवन का आधार हैं. अमूमन सभी मज़हबों में पर्यावरण संरक्षण पर ज़ोर दिया गया है. भारतीय समाज में आदिकाल से ही पर्यावरण संरक्षण को महत्व दिया गया है. भारतीय संस्कृति में पेड़-पौधों को पूजा जाता है. विभिन्न वृक्षों में विभिन्न देवताओं का वास माना जाता है. पीपल, विष्णु और कृष्ण का, वट का वृक्ष ब्रह्मा, विष्णु और कुबेर का माना जाता है, जबकि तुलसी का पौधा लक्ष्मी और विष्णु, सोम चंद्रमा का, बेल शिव का, अशोक इंद्र का, आम लक्ष्मी का, कदंब कृष्ण का, नीम शीतला और मंसा का, पलाश ब्रह्मा और गंधर्व का, गूलर विष्णू रूद्र का और तमाल कृष्ण का माना जाता है. इसके अलावा अनेक पौधे ऐसे हैं, जो पूजा-पाठ में काम आते हैं, जिनमें महुआ और सेमल आदि शामिल हैं. वराह पुराण में वृक्षों का महत्व बताते हुए कहा गया है- जो व्यक्ति एक पीपल, एक नीम, एक बड़, दस फूल वाले पौधे या बेलें, दो अनार दो नारंगी और पांच आम के वृक्ष लगाता है, वह नरक में नहीं जाएगा.
यह हैरत और अफ़सोस की ही बात है कि जिस देश में, समाज में पेड़-पौधों को पूजने की प्रथा रही है, अब उसी देश में, उसी समाज में पेड़ कम हो रहे हैं. बदलते दौर के साथ लोगों का प्रकृति से रिश्ता टूटने लगा. बढ़ती आबादी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वृक्षो को काटा जा रहा है. नतीजतन जंगल ख़त्म हो रहे हैं. देश में वन क्षेत्रफल 19.2 फ़ीसद है, जो बहुत ही कम है. इससे पर्यावरण के सामने संकट खड़ा हो गया है. घटते वन क्षेत्र को राष्ट्रीय लक्ष्य 33.3 फ़ीसद के स्तर पर लाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाने होंगे. साथ ही ख़ुशनुमा बात यह भी है कि अब जनमानस में पर्यावरण के प्रति जागरुकता आ रही है. लोग अब पेड़-पौधों की अहमियत को समझने लगे हैं. महिलाएं भी इस पुनीत कार्य में बढ़ चढ़कर शिरकत कर रही हैं.
बिहार के पूर्वी चंपारण ज़िले के गांव मझार की किरण ने अपने विवाह से पहले एक हज़ार पौधे लगाए. उन्होंने विवाह की मेहंदी लगाने के बाद अगले दिन सुबह से ही गड्डे खोदे और उनमें पौधे लगाए. इस मुहिम में मझार और इसके आसपास के गांवों के लोगों ख़ासकरलड़कियों और महिलाओं ने भी मदद की. किरण का कहना है कि वे पौधारोपण के ज़रिये अपने विवाह को यादगार बनाना चाहती थीं. आज इस तरह जंगल ख़त्म हो रहे हैं, पेड़ सूख रहे हैं, इसे देखते हुए पौधारोपण बहुत ज़रूरी है. पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, तो हम भी सुरक्षित रहेंगे. किरण के पिता जितेंद्र सिंह अपनी बेटी के इस काम से बहुत ख़ुश हैं. वे कहते हैं कि लोगों को इससे प्रेरणा मिलेगी.
इस बार ईद-उल-फ़ित्र के मौक़े पर ईद की नमाज़ के बाद जगह-जगह पौधारोपण किया गया. ईदी के तौर पर एक-दूसरे को पौधे भी दिए गए. तक़रीर में इमाम साहब ने कहा कि इस्लाम में पर्यावरण संरक्षण को बहुत मह्त्व दिया गया है. क़ुरान कहता है- जल और थल में बिगाड़ फैल गया ख़ुद लोगों की ही हाथों की कमाई के कारण, ताकि वह उन्हें उनकी कुछ करतूतों का मज़ा चखाए, शायद वे बाज़ आ जाएं. पैग़म्बर मुहम्मद सल्ल. ने फ़रमाया- अगर क़यामत आ रही हो और तुम में से किसी के हाथ में कोई पौधा हो, तो उसे ही लगा ही दो और नतीजे की फ़िक्र मत करो. पैग़म्बर मुहम्मद सल्ल. ने फ़रमाया-जिसने अपनी ज़रूरत से ज़्यादा पानी को रोका और दूसरे लोगों को पानी से वंचित रखा, तो अल्लाह फ़ैसले के दिन उस शख़्स से अपना फ़ज़लो-करम रोक लेगा. पैग़म्बर मुहम्मद सल्ल. ने फ़रमाया- जो शख़्स कोई पौधा लगाता है या खेतीबाड़ी करता है. फिर उसमें से कोई परिंदा, इंसान या अन्य कोई प्राणी खाता है, तो यह सब पौधा लगाने वाले की नेकी में गिना जाएगा. पैग़म्बर मुहम्मद सल्ल. ने फ़रमाया- जो भी खजूर का पेड़ लगाएगा, उस खजूर से जितने फल निकलेंगे, अल्लाह उसे उतनी ही नेकी देगा. पैग़म्बर मुहम्मद सल्ल. ने फ़रमाया- जिस घर में खजूर का पेड़ हो, वह भुखमरी से परेशान नहीं हो सकता. ईसाई भी पर्यावरण संरक्षण को महत्व देते हैं. वे मानते हैं- पर्यावरण का संरक्षण ही हमारा जीवन है, चाहे हम विश्वास करें या न करें, पर्यावरणीय संकट हमारे जीवन के सभी क्षेत्र, हमारे सामाजिक स्वास्थ्य, हमारे संबंध, हमारे आचरण, अर्थव्यवस्था, राजनीति, हमारी संस्कृति और हमारे भविष्य को प्रभावित करता है. प्रकृति का संरक्षण ही हमारी प्राणमयी ऊर्जा है.
किसानों का पर्यावरण से गहरा नाता रहा है. वे बढ़ते पर्यावरण असंतुलन पर चिंता ज़ाहिर करते हुए जहां जैविक खेती को अपना रहे हैं, वहीं कृषि वानिकी पर भी ख़ासा ध्यान दे रहे हैं. दरअसल कृषि वानिकी को अपनाकर कुछ हद तक पर्यावरण संतुलन को बेहतर बनाया जा सकता है. फ़सलों के साथ वृक्ष लगाने को कृषि वानिकी के नाम से जाना जाता है. खेतों की मेढ़ों पर वृक्ष लगाए जाते हैं. इसके अलावा गांव की शामिलात भूमि, परती भूमि और ऐसी भूमि, जिस पर कृषि नहीं की जा रही हैं, वहां भी उपयोगी वृक्ष लगाकर पर्यावरण को हरा-भरा बनाया जा रहा है. पशुओं के बड़े-बड़े बाड़ों के चारों ओर भी वृक्ष लगाए जा रहे हैं. कृषि वानिकी के तहत ऐसे वृक्ष लगाने चाहिए, जो ईंधन के लिए लकड़ी और खाने के लिए फल दे सकें. जिनसे पशुओं के लिए चारा और खेती के औज़ारों के लिए अच्छी लकड़ी भी मिल सके. इस बात का भी ख़्याल रखना चाहिए कि वृक्ष ऐसे हों, जल्दी उगें और उनका झाड़ भी अच्छा बन सके. बबूल, शीशम, नीम, रोहिड़ा, ढाक, बांस, महुआ, जामुन, कटहल, इमली, शहतूत, अर्जुन, खेजड़ी, अशोक, पोपलर, सागौन और देसी फलों आदि के वृक्ष लगाए जा सकते हैं.
बहुत-सी सरकारी और ग़ैर सरकारी संस्थाएं पौधारोपण की मुहिम चलाकर इस पुनीत कार्य में हिस्सेदार बन रही हैं. लोग अब अपने किसी ख़ास दिन को यादगार बनाने के लिए पौधे लगा रहे हैं. कोई पौधारोपण कर अपना जन्मदिन मना रहा है, तो कोई अपनी शादी की सालगिरह पर पौधा रोप रहा है. इतना ही नहीं, लोग अपने प्रिय नेता और अभिनेता के जन्मदिन और बरसी पर भी पौधारोपण कर वातावरण को हराभरा बनाने के काम में लगे हैं.
बेशक पौधे लगाना नेक काम है. लेकिन सिर्फ़ पौधा लगाना ही काफ़ी नहीं है. पौधे की समुचित देखभाल भी की जानी चाहिए, ताकि वे वृक्ष बन सके.
आओ पौधे लगाएं, अपनी धरा हो हरा बनाएं.
आज जब सब्ज़ियों के दाम आसमान छू रहे हैं और थाली में सब्ज़ियां कम होने लगी हैं. ऐसे में अगर घर में ही ऐसी सब्ज़ी का इंतज़ाम हो जाए, जो खाने में स्वादिष्ट हो और सेहत के लिए भी अच्छी हों, तो फिर क्या कहने. जी हां, हम बात कर रहे हैं सहजन की. गांव-देहात और छोटे-छोटे क़स्बों और शहरों में घरों के आंगन में सहजन के वृक्ष लगे मिल जाते हैं. बिहार की वैजयंती कहती हैं कि सहजन में ख़ूब फलियां लगती हैं. वह इसकी सब्ज़ी बनाती हैं, जिसे सभी ख़ूब चाव से खाते हैं. इसके फूलों की सब्ज़ी की भी घर में बार-बार मांग होती है. वह सहजन का अचार भी बनाती हैं. अपनी मां से उन्होंने यह सब सीखा है. उनके घर में एक गाय है. अपनी गाय को वह सहजन के पत्ते खिलाती हैं. गाय पहले से ज़्यादा दूध देने लगी हैं. इतना ही नहीं, वह सब्ज़ी वालों को फलियां बेच देती हैं. वह बताती हैं कि एक सब्ज़ी वाला उनसे अकसर वृक्ष से सहजन की फलियां तोड़ कर ले जाता है. इससे चार पैसे उनके पास आ जाते हैं. उन्होंने अपने आंगन में चार और पौधे लगाए हैं, जो कुछ वक़्त बाद उनकी आमदनी का ज़रिया बन जाएंगे.
जो लोग सहजन के पौष्टिक तत्वों से वाक़िफ़ हैं, वे हमेशा सहजन की मांग करते हैं. बाज़ार में सहजन की फलियां 100 रुपये किलो तक बिकती हैं. हिसार के सब्ज़ी बाज़ार में सहजन की फलियां कम ही आती हैं. इसलिए ये ऊंची क़ीमत पर मिलती हैं. बहुत-से ऐसे घर हैं, जिनके आंगन में सहजन के वृक्ष खड़े हैं, वे वहीं से पैसे देकर सहजन की फलियां तोड़ लेते हैं और उन ग्राहकों को बेच देते हैं, जो उनसे सहजन मंगाते हैं. सहजन के बहुत से ग्राहक बंध गए हैं. इनमें उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के लोग भी शामिल हैं.
सहजन बहुत उपयोगी वृक्ष है. इसे विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग नामों से जाना जाता है, जैसे बंगाल में सजिना, महाराष्ट्र में शेगटा, आंध्र प्रदेश में मुनग और हिंदी भाषी इलाक़ों में इसे सहजना, सुजना, सैजन और मुनगा आदि नामों से भी जाना जाता है. अंग्रेज़ी में इसे ड्रमस्टिक कहा जाता है. इसका वनस्पति वैज्ञानिक नाम मोरिंगा ओलिफेरा है. सहजन का वृक्ष मध्यम आकार का होता है. इसकी ऊंचाई दस मीटर तक होती है, लेकिन बढ़ने पर इसे छांट दिया जाता है, ताकि इसकी फलियां, फूल और पत्तियां आसानी से तोड़ी जा सकें. यह किसी भी तरह की ज़मीन पर उगाया जा सकता है. नर्सरी में इसकी पौध बीज या क़लम से तैयार की जा सकती है. पौधारोपण फ़रवरी-मार्च या बरसात के मौसम में करना चाहिए. इसे खेत की मेढ़ पर लगाया जा सकता है. इसे तीन से चार फ़ुट की दूरी पर लगाना चाहिए. यह बहुत तेज़ी से बढ़ता है. इसके पौधारोपण के आठ माह बाद ही इसमें फलियां लग जाती हैं. उत्तर भारत में इसमें एक बार फलियां लगती हैं, जबकि दक्षिण भारत में यह सालभर फलियों से लदा रहता है. हालांकि कृषि वैज्ञानिकों ने उत्तर भारत के लिए साल में दो बार फलियां देने वाली क़िस्म तैयार कर ली है और अब यही क़िस्म उगाई जा रही है. दक्षिण भारत के लोग इसके फूल, पत्ती और फलियों का इस्तेमाल विभिन्न प्रकार के व्यंजनों में करते हैं. उत्तर भारत में भी इन्हें ख़ूब चाव से खाया जाता है. इसकी फलियों से सब्ज़ी, सूप और अचार भी बनाया जाता है. इसके फूलों की भी सब्ज़ी बनाई जाती है. इसकी पत्तियों की चटनी और सूप बनाया जाता है.
गांव-देहात में इसे जादू का वृक्ष कहा जाता है. गांव-देहात के बुज़ुर्ग इसे स्वर्ग का वृक्ष भी कहते हैं. सहजन में औषधीय गुण पाए जाते हैं. इसके सभी हिस्से पोषक तत्वों से भरपूर हैं, इसलिए इसके सभी हिस्सों को इस्तेमाल किया जाता है. आयुर्वेद में इसे तीन सौ रोगों का उपचार बताया गया है. इसमें अनेक पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे कैलोरी, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, रेशा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फ़ास्फ़ोरस, पोटैशियम, कॊपर, सल्फ़र, ऒक्जेलिक एसिड, विटामिन ए-बीटासीरोटीन, विटामिन बी- कॊरिन, विटामिन बी1 थाइमिन, विटामिन बी2 राइबोफ़्लुविन, विटामिन बी3 निकोटिनिक एसिड, विटामिन सी एस्कार्बिक एसिड, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन के, ज़िंक, अर्जिनिन, हिस्टिडिन, लाइसिन, ट्रिप्टोफन,फ़िनॊयलेनेलिन, मीथिओनिन, थ्रिओनिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, वैलिन, ओमेगा आदि. एक अध्ययन के मुताबिक़ सहजन की पत्तियों में विटामिन सी संतरे से सात गुना होता है. इसी तरह इसकी पत्तियों में विटामिन ए गाजर से चार गुना, कैल्शियम दूध से चार गुना, पोटैशियम केले से तीन गुना और प्रोटीन दही से दोगुना होता है. सहजन के बीज से तेल निकाला जाता है, जो दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों में इस्तेमाल किया जाता है. इसकी छाल पत्ती, गोंद, जड़ आदि से आयुर्वेदिक दवाएं तैयार की जाती हैं. कहा जाता है कि इसके सेवन से सेहत अच्छी रहती है और बुढ़ापा भी दूर भागता है. आंखों की रौशनी भी अच्छी रहती है. इसके पोषक तत्वों को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने दक्षिण अफ़्रीका के कई देशों में कुपोषित लोगों के आहार में इसे शामिल करने की सलाह दी है. डब्ल्यूएचओ ने कुपोषण और भूख की समस्या से लड़ने के लिए इसे बेहतर माना है. फ़िलीपींस और सेनेगल में कुपोषण उन्मूलन कार्यक्रम के तहत बच्चों के आहार में सहजन को शामिल किया गया है. इसके बेहतर नतीजे सामने आए हैं. फ़िलीपींस, मैक्सिको, श्रीलंका, मलेशिया आदि देशों में सहजन की काफ़ी मांग है. बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बुज़ुर्गों के लिए यह वरदान है. इसकी पत्तियां पशुओं के लिए पौष्टिक आहार हैं. इसे चारे के लिए भी उगाया जाता है. चारे के लिए इसकी पौध छह इंच की दूरी पर लगाई जाती है. बरसीम की तरह इसकी कटाई 75 दिन के अंतराल पर करनी चाहिए. स्वीडिश यूनिवर्सिटी ऒफ़ एग्रीकल्चरल साइंस उपासला द्वारा निकारगुआ में किए गए एक अध्ययन के मुताबिक़ गायों को चारे के साथ सहजन की पत्तियां खिलाने से उनके दूध में 50 फ़ीसद बढ़ोतरी हुई है. सहजन के बीजों से पानी को शुद्ध किया जा सकता है. इसके बीजों को पीस कर पानी में मिलाया जाता है, जिससे पानी शुद्ध हो जाता है.
सहजन की खेती किसानों के लिए फ़ायदेमंद है. किसान सहजन की खेती कर आर्थिक रूप से समृद्ध बन सकते हैं. एक वृक्ष से आठ क्विंटल फलियां प्राप्त की जा सकती हैं. यह वृक्ष दस साल तक उपज देता है. इसे खेतों की मेढ़ों पर लगाया जा सकता है. पशुओं के बड़े-बड़े बाड़ों के चारों तरफ़ भी सजहन के वृक्ष लगाए जा सकते हैं. बिहार में किसान सहजन की खेती कर रहे हैं. यहां सहजन की खेती व्यवसायिक रूप ले चुकी है. बिहार सरकार ने सहजन की खेती के लिए महादलित परिवारों को पौधे मुहैया कराने की योजना बनाई है. इस योजना का मक़सद महादलित और ग़रीब परिवारों को स्वस्थ करना और उन्हें आमदनी का ज़रिया मुहैया कराना है. राज्य में समेकित जलछाजन प्रबंधन कार्यक्रम के तहत सहजन के पौधे वितरित किए जाते हैं. यहां स्कूलों और आंगनबाड़ी भवनों के परिसरों में सहजन बोया जा रहा है. कृषि विभाग के प्रोत्साहन की वजह से यहां के किसान सहजन उगा रहे हैं. किसानों का कहना है कि वे सहजन की क़लम खेत में लगाते हैं. मार्च-अप्रैल में वृक्ष फलियों से लद जाते हैं. उत्पादन वृक्ष के अनुसार होता है. एक वृक्ष से एक से पांच क्विंटल तक फलियां मिल जाती हैं. इसमें लागत भी ज़्यादा नहीं आती. वे अन्य सब्ज़ियों के साथ सहजन की खेती करते हैं. इससे उन्हें दोहरा फ़ायदा हो जाता है. इसके साथ ही पशुओं के लिए अच्छा चारा भी मिल जाता है, जो उनके लिए पौष्टिक आहार है. छत्तीसगढ़ में किसान पारम्परिक धान की खेती के साथ सहजन उगा रहे हैं. उनका कहना है कि वे इसकी फलियां शहर की मंडियों में बेजते हैं. पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और झारखंड आदि राज्यों में सहजन की ख़ासी मांग है. सहजन की फलियां 40 से 100 रुपये प्रति किलो बिकती हैं. सहजन के फ़ायदों को देखते हुए अनेक राज्य इसे प्रोत्साहित कर रहे हैं. इसे किचन गार्डन के तौर पर प्रोत्साहित किया जा रहा. स्थानीय जलवायु के अनुकूल इसकी नई क़िस्में तैयार की जा रही हैं.
आदिवासी इलाक़ों में भूमिहीन लोग बेकार पड़ी ज़मीन पर सहजन के वृक्ष उगाकर आमदनी हासिल कर रहे हैं. उनका कहना है कि ख़ाली ज़मीन पर जो भी वृक्ष उगाता है, वृक्ष के फल पर अधिकार भी उसी का होता है. इससे जहां बेकार पड़ी ज़मीन आमदनी का ज़रिया बन गई है, वहीं वृक्षों से पर्यावरण भी हराभरा बना रहता है. वृक्ष फल और छाया देने के साथ-साथ बाढ़ को रोकते हैं, भूमि कटाव को रोकते हैं.
कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि सहजन की विदेशों में बहुत मांग है, लेकिन जागरुकता की कमी की वजह से यहां के लोगों को इसके बारे में उतनी जानकारी नहीं है, जितनी होनी चाहिए. ऐसे में सहजन की खेती को बढ़ावा दिया जाना चाहिए. पारम्परिक खेती के साथ भी सहजन उगाया जा सकता है. इसमें कोई विशेष लागत भी नहीं आती. सहजन कृषि वानिकी और सामाजिक वानिकी का भी अहम हिस्सा बन सकता है. बस ज़रूरत है जागरुकता की.
गेहूं की फ़सल पककर तैयार हो चुकी है. कई जगह कटाई का काम भी शुरू हो गया है. किसानों को फ़सल की कटाई से लेकर फ़सल को बाज़ार तक ले जाने में काफ़ी सावधानियां बरतने की ज़रूरत होती है. गेहूं की फ़सल की कटाई के दौरान जान और माल के नु़क़सान के अनेक मामले सामने आते रहते हैं. गेहूं की थ्रेशिंग करते वक़्त मशीन की चपेट में आने से हाथ कट जाते हैं. इसी तरह आगज़नी से खेतों में खड़ी या खलिहान में एकत्रित फ़सलें का जलकर राख हो जाती हैं. ऐसे में किसानों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है. फ़सल की भरपाई, तो देर-सवेर पूरी हो भी सकती है, लेकिन अगर हाथ कट गया, तो उसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती. गेहूं की फ़सल को बीज से लेकर भंडारण तक सही देखभाल की ज़रूरत होती है, ऐसा न करने पर जहां उत्पादन प्रभावित होता है, वहीं अनाज ख़राब हो जाता है.
कृषि विशेषज्ञों के मुताबिक़ किसानों को गेहूं की कटाई और कढ़ाई में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, ताकि जान और माल का नुक़सान न हो. फ़सल की कटाई से पहले यह देख लेना चाहिए कि फ़सल पक चुकी है या नहीं. फ़सल की जांच करना बहुत आसान है. गेहूं की बाली से दाने निकाल कर उसे चबाएं. अगर दाने सख़्त हों और आवाज़ के साथ टूटें, तो समझ लें कि फ़सल तैयार है, इसे काटा जा सकता है. अगर गेहूं के दाने नरम हों, तो फ़सल को कुछ और दिनों के लिए खेत में पकने के लिए छोड़ देना चाहिए. गेहूं की बाली को तोड़कर भी फ़सल के पकने का अंदाज़ा लगाया जा सकता है. अगर फ़सल पक चुकी होगी, तो उसकी बाली आसानी से टूट जाएगी, जबकि अधपकी फ़सल की बाली मुड़ जाएगी, लेकिन टूटेगी नहीं.
गेहूं की कटी हुई फ़सल को एक जगह खलिहान में इकट्ठा करने की बजाय अलग-अलग खेतों में सुखाना चाहिए. ऐसा करने से फ़सल जल्दी सूखेगी. अगर फ़सल को एक ही खलिहान में एकत्रित करके गेहूं निकालना हो, तो खलिहान को सुरक्षित जगह पर बनाना चाहिए. खलिहान के पास पानी और रेत का पूरा इंतज़ाम किया जाना चाहिए, ताकि आग लगने पर फ़ौरन उस पर क़ाबू पाया जा सके. फ़सल की कटाई और गेहूं निकालते वक़्त किसी भी तरह का धूम्रपान नहीं करना चाहिए. फ़सल को अच्छी तरह सुखाकर ही गेहूं निकालना चाहिए. कंबाइन से काटी गई फ़सल के अनाज को अच्छी तरह साफ़ करके सुखा लें. उसके बाद ही थ्रेशर मशीन से गेहूं निकालें. थ्रेशिंग दिन में ही करनी चाहिए. दिन ढलने पर थ्रेशिंग करने पर दुर्घटना की आशंका बनी रहती है. थ्रेशर के पतनाले का दो तिहाई हिस्सा कवर करके थ्रेशिंग करनी चाहिए, ताकि हाथ को संभावित दुर्घटना से बचाया जा सके. थ्रेशिंग करते वक़्त ढीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए. महिलाओं को चाहिए कि वे थ्रेशिंग करते वक़्त साड़ी का पल्लू या चुनरी वग़ैरह को अच्छी तरह से लपेट लें. ऐसा करने से वे संभावित दुर्घटना से बची रहेंगी. गेहूं कटाई और बालियों से गेहूं निकालते वक़्त मुंह पर मलमल का कपड़ा बांध लेना चाहिए, ताकि हवा में मौजूद अवशेष सांस के साथ फेफड़ों के अंदर न जाएं. जिन लोगों को श्वास संबंधी कोई भी बीमारी है, उन्हें इन कामों से और उन जगहों से दूर ही रहना चाहिए, जहां गेहूं निकालने का काम हो रहा हो.
थ्रेशिंग समतल जगह पर ही करनी चाहिए, ताकि उसमें ज़्यादा कंपन न हो. हवा के रुख़ का ख़्याल रखना भी ज़रूरी है. अगर थ्रेशर से गहराई का काम करने के लिए ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो धुंआ निकलने वाली नली के ऊपर चिंगारी रोधक यंत्र लगा देना चाहिए, ताकि चिंगारी न निकले. खलिहान के आसपास भी किसी तरह की आग या चिंगारी का काम नहीं किया जाना चाहिए. ट्रैक्टर को फ़सल के ढेर से कुछ दूरी पर रखें, ताकि कोई चिंगारी निकले भी, तो वह फ़सल के ढेर तक न पहुंच पाए. अकसर एक छोटी सी चिंगारी पूरी फ़सल को जलाकर राख कर देती है.
अकसर यह देखा जाता है कि फ़सल कटाई के बाद खतों में बचे अवशेषों को आग लगाकर जला दिया जाता है. इससे मिट्टी में मौजूद मित्र कीट यानी फ़ायदेमंद जीवाणु मर जाते हैं और मिट्टी के पोषक तत्व भी नष्ट हो जाते हैं. इससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है. सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के साथ कार्बन की मात्रा घट जाती है. सूक्ष्म जीवाणु मिट्टी के अंदर पौधे को भोजन मुहैया कराते हैं. इनके नष्ट होने से पौधों को संतुलित आहार नहीं मिल पाता, जिससे उत्पादन पर असर पड़ता है. मिट्टी में कार्बन की मात्रा 6 से 8 फ़ीसद होनी चाहिए, जो अब घटकर महज़ दो फ़ीसद ही रह गई है.
अगर फ़सलों के अवशेषों को हल चलाकर मिट्टी में मिला दिया जाए, तो इससे मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा में बढ़ोतरी होगी. इससे मिट्टी की जलग्रहण क्षमता और पोषक तत्वों की उपलब्धता में वृद्धि होती है. कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि गेहूं की फ़सल की कटाई के बाद खेत में बची फ़सल की पराती को जलाना नहीं चाहिए. डिस्क हैरो या रोटावेटर से जुताई के बाद आठ किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ खेत में डालकर हल्की सिंचाई कर देना चाहिए. इससे अवशेष पूरी तरह सड़कर उर्वरक का काम करेंगे. इससे मिट्टी में जीवांश और कार्बन की मात्रा बढ़ जाएगी. इतना ही नहीं, फ़सलों के अवशेषों को जलाने से आसपास की फ़सलों को ख़तरा पैदा हो जाता है. इसकी चिंगारियां आसपास के खेतों में खड़ी फ़सल या खलिहानों में एकत्रित फ़सल को अपनी चपेट में ले लेती हैं, जिससे फ़सल जलकर राख हो जाती है. इसके अलावा धुएं से पर्यावरण भी प्रदूषित होता है. खेत में फ़सलों के अवशेष जलाना क़ानूनन अपराध भी है, जिसके लिए दोषी को सज़ा देने का प्रावधान है.
फ़सल के अवशेष जला देने से पशुओं के समक्ष चारे का संकट खड़ा हो जाता है. किसान इन अवशेषों के भूसे का इस्तेमाल पशु चारे के तौर पर भी कर सकते हैं. गेहूं के अवशेष की बाज़ार में काफ़ी मांग हैं. खुम्बी उत्पादन और बिना मिट्टी की खेती में इनका इस्तेमाल होता है. इन्हें जलाने की बजाय किसान इन्हें बेचकर कुछ रक़म हासिल कर सकते हैं.
गेहूं को साफ़ करके और सुखाकर ही भंडार गृह में भंडारण करना चाहिए. अगर गेहूं में दस फ़ीसद से ज़्यादा नमी है, तो उसे धूप में सुखा लेना चाहिए. इसके बाद गेहूं को छाया में कुछ वक़्त के लिए छोड़ देना चाहिए, ताकि धूप की गरमाहट से गेहूं में जो भाप बनी है, वह उड़ जाए. ख़्याल रखें कि भंडार गृह साफ़-सुथरा, खुला और हवादार हो. इसमें सूरज की रौशनी आती हो और नमी बिल्कुल भी न हो, वरना अनाज ख़राब हो जाएगा. जिस जगह गेहूं का भंडारण करना हो, एक लीटर पानी में दस मिलीलीटर मैलाथियान मिलाकर उसकी दीवारों और फ़र्श को अच्छी तरह से साफ़ करना चाहिए. फिर इसे कुछ दिन के लिए छोड़ देना चाहिए.
गेहूं को सीधा फ़र्श पर नहीं रखा जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर ज़मीन की नमी से अनाज ख़राब हो सकता है. पहले फ़र्श पर ईंटे रखनी चाहिए और फिर उन पर लकड़ी के तख़्ते रखने चाहिए. तख़्तों पर नीम की सूखी पत्तियां बिछा देनी चाहिए, ताकि गेहूं को कीड़ा न लगे. अब इन तख़्तों पर गेहूं की बोरियां रखी जानी चाहिए. इससे गेहूं की बोरियां ज़मीन की नमी से बची रहेंगी. अनाज को अगर बोरियों में भरा जाना हो, तो बोरियों को कीटनाशी दवाओं से उपचारित कर लेना चाहिए. बोरियां भी साफ़-सुथरी और सूखी होनी चाहिए. अगर बोरियों में नमी हो, तो उसे पहले धूप में अच्छी तरह से सुखा लें, फिर उनमें गेहूं भरें. बोरियों को सही तरीक़े से क़तार में रखना चाहिए, ताकि बोरियों को उठाने में आसानी रहे और उनकी गिनती में भी कोई दिक़्क़त न हो.
गेहूं बाज़ार में ले जाने से पहले गेहूं की अच्छी तरह से जांच कर लेनी चाहिए कि उनमें ज़्यादा नमी न हो. गेहूं में नमी की मात्रा 12 फ़ीसद से कम ही होनी चाहिए. नमी की मात्रा ज़्यादा होने पर ख़रीद एजेंसियां गेहूं नहीं ख़रीदतीं. किसानों को मंडी में भी अपनी फ़सल की देखभाल करनी चाहिए. अनाज को शेड के नीचे रखना चाहिए. अगर शेड न हो, तो प्लास्टिक शीट साथ लेकर जानी चाहिए, ताकि फ़सल को आंधी और बारिश से बचाया जा सके. अनाज को तुलवाकर मंडी में लेकर जाना चाहिए. मंडी में अनाज की तुलवाई अपने सामने करवानी चाहिए. अनाज की बिक्री की पक्की रसीद ज़रूर लेनी चाहिए. किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ी होने पर फ़ौरन संबंधित अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए.
बहरहाल, किसान फ़सल की बिजाई से लेकर बाज़ार तक सावधानी बरत कर न सिर्फ़ ज़्यादा उत्पादन पा सकते हैं, बल्कि फ़सल की अच्छी क़ीमत भी हासिल कर सकते हैं.
फ़िरदौस ख़ान
राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं, जो अपना वादा ज़रूर निभाते हैं. अब तेलंगाना में भी उनकी पार्टी कांग्रेस ने किसानों से किया अपना वादा पूरी ईमानदारी से निभाया है. राहुल गांधी ने तेलंगाना में किसानों को राहत देने का वादा किया था.
तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने किसानों का दो लाख रुपये तक क़र्ज़ माफ़ करने का ऐलान किया है. राज्य के मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि 12 दिसम्बर 2018 से 9 दिसम्बर 2023 के बीच जिन किसानों ने दो लाख रुपये तक का क़र्ज़ लिया है, उन्हें एकमुश्त माफ़ कर दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि पात्रता शर्तों सहित ऋण माफ़ी का विवरण जल्द ही एक सरकारी आदेश में घोषित किया जाएगा. क़र्ज़ माफ़ी से राज्य के ख़ज़ाने पर तक़रीबन 31 हज़ार करोड़ रुपये का भार पड़ेगा. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार दो लाख रुपये के कृषि ऋण माफ़ी के अपने चुनावी वादे को पूरा कर रही है.
कांग्रेस नेता व सांसद राहुल गांधी ने तेलंगाना के किसान परिवारों को बधाई देते हुए कहा है कि कांग्रेस सरकार ने आपके 2 लाख रुपये तक के सभी ऋण माफ़ कर ‘किसान न्याय’ के संकल्प को पूरा करने की दिशा में ऐतिहासिक क़दम बढ़ाया है- जो 40 लाख से ज़्यादा किसान परिवारों को क़र्ज़ मुक्त बनाएगा.
जो कहा, कर के दिखाया- यही नियत है और आदत भी.
कांग्रेस सरकार का मतलब है- राज्य का ख़ज़ाना किसानों और मज़दूरों समेत वंचित समाज को मज़बूत बनाने में ख़र्च होने की गारंटी, जिसका उदाहरण है तेलंगाना सरकार का यह फ़ैसला.
हमारा वादा है- कांग्रेस जहां भी सरकार में होगी, हिंदुस्तान का धन ‘हिंदुस्तानियों’ पर ख़र्च करेगी, ‘पूंजीपतियों’ पर नहीं.
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने लिखा कि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी ने किसानों का क़र्ज़ माफ़ करने का वादा किया था. उस वादे को पूरा करते हुए हमारी तेलंगाना सरकार ने फ़ैसला लिया है कि किसानों के क़र्ज़ माफ़ किए जाएंगे. इससे क़र्ज़ में डूबे 40 लाख किसानों को राहत मिलेगी.
कांग्रेस मानती है कि देश का सारा धन देश की जनता का है और उसे जनता की भलाई में ही ख़र्च होना चाहिए. हमने राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी किसानों का क़र्ज़ माफ़ किया था. जब केंद्र में हमारी सरकार थी तो देश भर के किसानों का 72 हज़ार करोड़ रुपये का क़र्ज़ माफ़ किया गया था.
कांग्रेस पार्टी किसानों, मज़दूरों, आदिवासियों, दलितों, वंचितों और मध्य वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है.
फ़िरदौस ख़ान
कहते हैं कि दुआएं तक़दीर बदल दिया करती हैं. अगर किसी दुरवेश की दुआ से ज़मीन के एक टुकड़े की हालत ही बदल जाए, तो वैज्ञानिक भी हैरान रह जाते हैं. वे इस बात के क़ायल हो जाते हैं कि क़ुदरत के करिश्मे को न कोई समझ पाया है और न कभी समझ सकता है. आज हम एक ऐसे ही करिश्मे की बात कर रहे हैं, जो नूह जिले के एक गांव में हुआ था और आज भी बरक़रार है.
देश की राजधानी दिल्ली के समीपवर्ती राज्य हरियाणा के नूह ज़िले का मढ़ी एक ऐसा गांव हैं, जहां फ़सल अन्य इलाक़ों के मुक़ाबले बहुत पहले पहले पक जाती है. जब आसपास और दूर-दराज़ के गांवों के खेतों में फ़सलें लहलहा रही होती हैं, तब इस गांव के किसान अपनी फ़सल काटकर घर ले जा चुके होते हैं. इस गांव के बाशिन्दे जैकम ख़ान का कहना है कि उन्होंने बुज़ुर्गों से सुना है कि किसी ज़माने में यहां भी आसपास के इलाक़ों की तरह ही अपने वक़्त पर फ़सल पका करती थी. एक बार की बात है कि यहां एक दरवेश आए और वे एक पेड़ के नीचे बैठ गए. वे वहां घंटों तक इबादत करते रहे. गांव के लोगों ने उन्हें देखा, तो वे उनके पास गए और उन्हें पीने के लिए पानी और खाने के लिए भोजन दिया. वह दरवेश कहीं दूर से आए थे और भूखे और प्यासे भी थे. गांववालों की मेहमान नवाज़ी से वह बहुत ख़ुश हुए. उन्होंने गांववालों को दुआ देते हुए कहा कि मालिक तुम्हें औरों से पहले रिज़्क़ देगा. कुछ वक़्त बाद वे दुरवेश गांव से चले गए. उनके जाने के कुछ माह बाद किसानों ने देखा कि उनकी फ़सल आसपास के गांवों की फ़सल से पहले पककर तैयार हो गई. इस बात की चर्चा दूर-दूर तलक होने लगी. पहले तो सबने इसे कोई इत्तेफ़ाक़ समझा, लेकिन जब लगातार फ़सल अन्य गांवों की फ़सल से पहले पकने लगी, तो लोग सोचने पर मजबूर हो गए. उन्हें दरवेश की दुआ याद आई कि उन्होंने कहा था कि मालिक तुम्हें औरों से पहले रिज़्क़ देगा. वे मान गए कि यह दरवेश की दुआ का ही असर है, जो उन्हें औरों से पहले रिज़्क़ यानी फ़सल मिल पाती है.
इस गांव की एक ख़ास बात यह भी है कि मढ़ी महामारी से महफ़ूज़ रहता है. जब कभी कोई महामारी फैलती है, तो भले ही आसपास के गांव उसकी चपेट में आ जाएं, लेकिन मढ़ी सुरक्षित रहता है. यहां के लोग कम बीमार पड़ते हैं. इसे भी गांववाले दुरवेश की दुआओं का ही असर मानते हैं. सूबे ख़ान कहते हैं कि मढ़ी ही नहीं, पूरे मेवात इलाक़े के लोग सादगी पसंद हैं. वे फ़क़ीरों और साधु-संतों का मान-सम्मान करने वाले हैं. यहां कोई फ़कीर, साधु-संत या कोई मुसाफ़िर आ जाए, तो गांववाले उसे भोजन करवाते हैं, उसे पानी पिलाते हैं, उसका आदर-सत्कार करते हैं. गांववाले कहते हैं कि मेहमान नवाज़ी करना तो हमारा फ़र्ज़ है. अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मौक़ों पर मेहमान का स्वागत करने, उसकी ख़िदमत करने और उसका ख़्याल रखने का हुक्म दिया है. गांववाले अपनी इस परम्परा को क़ायम रखे हुए हैं और वे अपने बच्चों को भी इसकी तालीम देते हैं.
कुछ लोग कहते हैं कि फ़सल को पर्याप्त सिंचाई जल न मिल पाने की वजह से मढ़ी में फ़सल जल्द पककर तैयार हो जाती है. लेकिन जब उनसे यह पूछा जाता है कि मढ़ी के आसपास के दर्जनों गांवों की यही हालत है. वहां भी फ़सलों की पर्याप्त सिंचाई नहीं हो पाती और उन्हें भी बहुत कम पानी मिल पाता है. फिर एक जैसी हालत में वहां की फ़सलें जल्द पककर तैयार क्यों नहीं होती? इस सवाल का उन लोगों के पास कोई जवाब नहीं होता, सिवाय इसके कि यह बात उनकी समझ से परे है.
गांववाले बताते हैं कि दूर-दूर से कृषि वैज्ञानिक उनके गांव में आए और उन्होंने हालात का जायज़ा लिया, लेकिन बिना किसी नतीजे पर पहुंचे वापस लौट गए.
जल संकट
गांव बाई के सरपंच आबिद बताते हैं कि इलाक़े के मढ़ी सहित तक़रीबन 66 गांवों में अब तक सिंचाई का नहरी पानी नहीं पहुंच पाया है. इसलिए इस इलाक़े के किसान सिंचाई के लिए बारिश के पानी पर निर्भर हैं. इस वजह से यहां साल में एक ही फ़सल हो पाती है. इस इलाक़े में भूजल-स्तर बहुत गहरा है. यहां का पानी बहुत खारा होने की वजह से पीने के लायक़ भी नहीं है. ऐसे में फ़सल कहां से हो. यहां के किसान अनाज में गेहूं और जौ की फ़सल उगाते हैं. दलहन में मसूर और तिलहन में सरसों की खेती की जाती है.
क़ाबिले-ग़ौर है कि 1507 वर्ग किलोमीटर में फैले मेवात यानी नूह इलाक़े का भू-जल स्तर बहुत नीचे है. इतना ही नहीं, यहां के ज़्यादातर इलाक़े का पानी बहुत खारा और फ़्लोराइडयुक्त है, जिससे यह पीने लायक़ बिल्कुल भी नहीं है. सिर्फ़ अरावली पहाड़ों की तलहटी में बसे गांवों का पानी ही पीने के लायक़ है. एक सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक़ मेवात में जल संकट की हालत बहुत गंभीर हैं. यहां के 443 गांवों में से महज़ 57 गांव ही ऐसे हैं, जहां का भू-जल पीने लायक़ है. इलाक़े के 104 गांवों का पानी बहुत ज़्यादा खारा है. यहां के 31 गांवों के पानी में फ़्लोराइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है, जो सेहत के लिए बहुत नुक़सानदेह है. इलाक़े के 52 गांवों का पानी खारा भी है और उसमें फ़्लोराइड भी बहुत ही ज़्यादा है.
स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक़ पानी में फ़्लोराइड की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से यह धीमे ज़हर का काम करता है. इस पानी के सेवन से गुर्दों में पथरी हो जाती है. इससे हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं. शरीर में दर्द रहने लगता है और ज़रा सी चोट से हड्डी टूट भी सकती है. इसके अलावा फ़्लोराइडयुक्त पानी के सेवन से त्वचा संबंधी बीमारियां भी हो जाती हैं.
हालांकि मेवात के तक़रीबन अढ़ाई सौ गांवों में रेनीवेल परियोजना के तहत पेयजल की आपूर्ति की जा रही है. यह पानी यमुना के किनारे बड़े बोरवेल के बूस्टिंग स्टेशनों के ज़रिये गांवों में पहुंचाया जा रहा है.
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर 2004 को तत्कालीन मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला ने इस योजना की आधारशिला रखी थी. इसका मक़सद यमुना किनारे रेनीवेल बनाकर मेवात में पानी पहुंचाना था. यह परियोजना 2019 की आबादी को ध्यान में रखकर बनाई गई थी. इसके तहत प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 55 लीटर स्वच्छ पेयजल देने का प्रावधान किया गया था, लेकिन बढ़ती आबादी की लगातार बढ़ती पानी की मांग की वजह से यहां जल संकट बना रहता है.
(लेखिका स्टार न्यूज़ एजेंसी में सम्पादक हैं)
फ़िरदौस ख़ान
न हींग लगे, न फिटकरी और रंग चौखा. यह कहावत सनाय की खेती पर पूरी तरह से लागू होती है, क्योंकि सनाय की खेती में लागत बहुत कम आती है और आमदनी ख़ूब होती है. सबसे बड़ी बात, इसे न तो उपजाऊ ज़मीन की ज़रूरत होती है, न ज़्यादा सिंचाई जल की, न ज़्यादा खाद की और न ही ज़्यादा कीटनाशकों की. इसे किसी ख़ास देखभाल की भी ज़रूरत नहीं होती. तो हुआ न फ़ायदा का सौदा. इसके फ़ायदों को देखते हुए किसान सनाय की खेती करने लगे हैं. बहुत से किसानों ने सनाय की खेती करके बंजर ज़मीन को हराभरा बना दिया है. ऐसे ही एक व्यक्ति हैं राजस्थान के जोधपुर के नारायणदास प्रजापति. उन्होंने बंजर ज़मीन पर सनाय की खेती की और इतनी कामयाबी हासिल कर ली कि आज उनका उद्योग भी है. उन्होंने अरब देशों से सनाय के बीज मंगवाकर इसकी खेती शुरू की थी. अब वह कई देशों में सनाय की पत्तियों का निर्यात करते हैं. शुरू में उन्हें अपनी फ़सल बेचने में परेशानी काफ़ी हुई. फिर उन्होंने ऐसे व्यापारियों को ढूंढा, जो सनाय की पत्तियां ख़रीदते हैं. जब एक बार व्यापारियों से उनका संपर्क हो गया, तो फिर उन्हें फ़सल बेचने में कोई दिक़्क़त नहीं हुई. इसके बाद उन्होंने अपना उद्योग स्थापित कर लिया. उन्होंने एक प्रशिक्षण केंद्र भी खोला, जहां किसानों को सनाय की खेती की जानकारी दी जाती है. उन्होंने सनाय पर आधारित एक संग्रहालय भी बनाया हुआ है. उनके परिवार के सदस्य भी उनका हाथ बटा रहे हैं. उनके यहां से प्रशिक्षण पाकर बहुत से किसान सनाय की खेती करने लगे हैं.
सनाय औषधीय पौधा है. इसे स्वर्णमुखी, सोनामुखी और सुनामुखी भी कहा जाता है. यह झाड़ीनुमा पौधा है. इसकी ऊंचाई 120 सेंटीमीटर तक होती है. भारत में यह अरब देश से आया और सबसे पहले तमिलनाडु में इसकी खेती शुरू हुई. इसके बाद देश के अन्य राज्यों में भी इसकी खेती शुरू हो गई. नतीजतन, आज भारत सनाय की खेती के मामले में दुनियाभर में पहले स्थान पर है. यह बहुवर्षीय पौधा है. एक बार बिजाई के बाद यह पांच साल तक उपज देता है. सनाय की ख़ासियत यह है कि यह बंजर ज़मीन में भी उगाया जा सकता है. रेतीली और दोमट भूमि इसके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर है. लवणीय भूमि इसके लिए ठीक नहीं होती. जिस भूमि में बरसात का पानी थोड़ा भी रुकता है, उसमें सनाय नहीं उगाना चाहिए, क्योंकि वहां यह पनप नहीं पाता. इसकी जड़ें गल जाती हैं, जिससे पौधा सूख जाता है. इसे ज़्यादा सिंचाई की ज़रूरत नहीं होती. इसलिए यह बहुत कम वर्षा वाले इलाक़ों में भी उगाया जा सकता है. किसानों को इसकी सिंचाई पर ज़्यादा पैसे ख़र्च नहीं करने पड़ते. पौधे के बढ़ने पर इसकी जड़ें ज़मीन से पानी सोख लेती हैं. यह पौधा चार डिग्री से 50 डिग्री सैल्सियस तापमान में भी ख़ूब फलता-फूलता है. देश के शुष्क और बंजर इलाक़ों में इसकी खेती की जा सकती है.
कृषि विशेषज्ञों के मुताबिक़ सनाय की बिजाई के लिए 15 जुलाई से 15 सितंबर का वक़्त अच्छा माना जाता है. इसकी बिजाई के लिए किसी ख़ास तैयारी की ज़रूरत नहीं होती. खेत में एक-दो जुताई करना ही काफ़ी है. इसकी बिजाई एक फ़ुट की दूरी पर करनी चाहिए. सनाय की एक ख़ासियत यह भी है कि इसमें किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं लगती. हालांकि बरसात के मौसम में कभी-कभार इसके पत्तों पर काले धब्बे आ जाते हैं, लेकिन धूप निकलने पर ये धब्बे ख़ुद-ब-ख़ुद दूर हो जाते हैं. इसलिए फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है. सनाय को किसी भी तरह की ज़्यादा खाद और रसायनों की ज़रूरत नहीं होती. कीट-पतंगे और पशु-पक्षी भी इसे कोई नुक़सान नहीं पहुंचाते. इसलिए इसे किसी विशेष देखभाल की ज़रूरत नहीं होती. बिजाई के तक़रीबन सौ दिन बाद इसकी पत्तियां काटी जा सकती हैं. पौधों को ज़मीन से पांच इंच ऊपर काटना चाहिए, ताकि फिर से पौधे में पत्तियां उग सकें. कटाई वक़्त पर कर लेनी चाहिए. दूसरी कटाई 70 दिन बाद की जा सकती है, जबकि तीसरी कटाई 60 दिन में की जा सकती है. दोबारा बिजाई के लिए इसके बीज प्राप्त करने के लिए स्वस्थ पौधों को छोड़ देना चाहिए. इनकी कटाई नहीं करनी चाहिए. इससे इनमें फलियां लग जाएंगी. पकने पर फलियां भूरे रंग की हो जाती हैं. इन फलियों को धूप में सुखाकर इनके बीज निकाल लेने चाहिए. यही बीज बाद में नई फ़सल उगाने में काम आएंगे.
पत्तियों को सुखाते वक़्त ध्यान रखना चाहिए कि इनका रंग हरा रहे. ताकि बाज़ार में इनकी अच्छी क़ीमत मिल सके. टहनियों की छोटी-छोटी ढेरियां बनाकर इन्हें छाया में सुखाना चाहिए. इनके सूख जाने पर इन्हें किसी तिरपाल पर झाड़ देना चाहिए, जिससे पत्तियां टहनी से अलग हो जाएं. फिर इन्हें बोरियों में भर देना चाहिए. अब सनाय बिक्री के लिए तैयार है. सनाय औषधीय पौधा है, इसलिए बाज़ार में इसकी ख़ासी मांग है. सनाय की पत्तियों का इस्तेमाल आयुर्वेदिक, यूनानी और एलोपैथिक दवाओं के निर्माण में किया जाता है. इससे पेट संबंधी दवाएं बनाई जाती हैं. बड़े स्तर पर खेती करने पर दवा निर्माता खेत से ही सनाय की पत्तियां ख़रीद लेते हैं, जिससे किसानों को बिक्री के लिए बाज़ार जाना नहीं पड़ता. सनाय अमेरिका, जापान, आस्ट्रेलिया, जर्मनी, चीन सहित कई देशों में निर्यात किया जाता है. इससे भारत को हर साल तीस करोड़ रुपये से ज़्यादा की विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है.
बहरहाल, जिन लोगों को कृषि की ज़्यादा जानकारी नहीं है, वे भी सनाय की खेती करके मुनाफ़ा हासिल कर सकते हैं.
सर्दियों के मौसम में किसानों को सबसे ज्यादा जिस चीज़ का डर सताता है, वह है पाला. हर साल पाले से उत्तर भारत में फलों और सब्जियों की फसलें प्रभावित होती हैं. इससे पैदावार घट जाती है. अमूमन पाला दिसंबर और जनवरी में पड़ता है, लेकिन कभी-कभार यह फ़रवरी के पहले पखवाड़े तक भी क़हर बरपाता है.
चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिकों के मुताबिक़ तापमान गिरने से जब भूमि की ऊष्मा बाहर निकलती है और भूमि के समीप वायुमंडल का तापमान एक डिग्री से नीचे हो तो ऐसे में ओस की बूंदे जम जाती हैं, जिसे पाला कहा जाता है. जब आसमान साफ हो, हवा न चल रही हो और तापमान गिरकर 0.5 डिग्री से. तक पहुंच जाए तो पाला गिरने की संभावना बढ़ जाती है. पाला दो प्रकार का होता है, काला पाला और सफेद पाला. जब भूमि के समीप तापमान 0.5 डिग्री से कम हो जाए और पानी की बूंदे न जमें तो इसे काला पाला कहते हैं. इस अवस्था में हवा बेहद शुष्क हो जाती है और पानी की बूंदे नहीं बन पातीं. जब पाला ओस की बूंदों के रूप में होता है तो उसे सफेद पाला कहते हैं. सफ़ेद पाला ही फ़सलों को सबसे ज्यादा नुक़सान पहुंचाता है. सफेद पाला ज्यादा देर तक रहने से पौधे नष्ट हो जाते हैं. पाले के कारण पौधों की कोशिकाओं व ऊतकों में मौजूद कोशिका द्रव्य जमकर बर्फ़ बन जाता है. इससे कोशिका का द्रव्य आयतन बढ़ने से कोशिका भित्ति फट जाती है. कोशिकाओं में निर्जलीकरण होने लगता है, जिससे पौधों की जैविक क्रियाएं प्रभावित होती हैं और पौधा मर जाता है. पाला फलों में आम, पपीते व केले और सब्जियों में आलू, मटर, सरसों व अन्य कोमल पत्तियों वाली सब्ज़ियों को ज्यादा प्रभावित करता है.
फलों को पाले से बचाने के लिए कई तरीक़े अपनाए जा सकते हैं. जिस रात पाला पड़ने की संभावना हो, उस वक्त सूखी पत्तियां या उपले या पुआल आदि जलाकर बाग में धुंआ कर दें. इससे आसपास के वातावरण का तापमान बढ़ जाएगा और पाले से नुकसान नहीं होगा. धुंआ पाले को नीचे आने से भी रोकता है. फसल को पाले से बचान के लिए 10 से 15 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करते रहना चाहिए. सिंचाई करने से भूमि के तापमान के साथ पौधों के तापमान में भी बढ़ोतरी होती है, जो पाले के असर को कम कर देती है. बाग में सूखी पत्तियां और घास-फूंस फैलाना देने और पेड़ों के तनों पर गोबर का लेप कर देने से भी पाले से बचाव किया जा सकता है. छोटे पौधों और नर्सरियों को पाले से बचाने उन्हें प्लास्टिक शीट से ढक देना चाहिए. इससे तापमान बढ़ जाता है. इसके अलावा सरकंडों और धान की पुआल की टाटियां बनाकर भी पौधों की पाले से रक्षा की जा सकती है. वायुरोधी टाटियां उत्तर-पश्चिम की तरफ़ बांधें. छोटे फलदार पौधों के थांवलों के चारों तरफ़ पूर्वी भाग छोड़कर टाटियां लगाकर सुरक्षा करें.
सभी प्रकार के पौधों पर गंधक के तेज़ाब का 0.1 प्रतिशत घोल का छिड़काव करना चाहिए. इससे न केवल पाले से बचाव होता है, बल्कि पौधों में लौह तत्व की जैविक व रासायनिक सक्रियता भी बढ़ जाती है. यह पौधों को रोगों से बचान व फसल को जल्दी पकाने का भी काम करता है. इस छिड़काव का असर एक पखवाड़े तक रहता है. इसी तरह सब्जियों की फसल को पाले से बचाने के लिए भी कई तरीके अपनाए जा सकते हैं. सबसे महत्वपूर्ण बात, बिजाई के वक्त ऐसे किस्मों को चुना जाना चाहिए, जो पालारोधी हों. फसल की सिंचाई करते रहना चाहिए. खेत में घासफूंस बिछाकर भी तापमान को कम होने से रोका जा सकता है.
दुनिया भर में आबादी लगातार बढ़ रही है. आबादी को रहने के लिए घर भी चाहिए और पेट भरने के लिए अनाज भी. बसावट के लिए जंगल काटे जा रहे हैं, खेतों की जगह बस्तियां बसाई जा रही हैं. ऐसे में लगातार छोटे होते खेत आबादी का पेट कैसे भर पाएंगे. इंसान को ज़िन्दा रहने के लिए हवा और पानी के अलावा भोजन भी चाहिए. ज़रा सोचिए, जब कृषि भूमि कम हो जाएगी, तब अनाज, फल और सब्ज़ियां कहां से आएंगी. ऐसी हालत में खेतीबाड़ी की ऐसी तकनीक की ज़रूरत होगी, जिससे बिना मिट्टी के भी फ़सलें उगाई जा सकें. काफ़ी अरसे से कृषि वैज्ञानिक ऐसी तकनीक की खोज में जुटे हैं, जिनके ज़रिये उन हालात में भी फ़सलें उगाई जा सकें, जब कृषि योग्य ज़रूरी चीज़ें उपलब्ध न हों. कृषि वैज्ञानिकों की मेहनत का ही नतीजा है कि आज ऐसी कई तकनीक मौजूद हैं, जिनके ज़रिये कम पानी और बंजर ज़मीन में भी फ़सलें लहलहा रही हैं. इतना ही नहीं, अब तो बिना मिट्टी के भी फ़सलें उगाई जा रही हैं. अमेरिका, ऒस्ट्रेलिया, चीन, जापान, इज़राइल, थाइलैंड, कोरिया, इंडोनेशिया और मलेशिया आदि देशों में बिना मिट्टी के सब्ज़ियां उगाई जा रही हैं. इन देशों की देखादेखी और देश भी इस तकनीक को अपना रहे हैं. इस तकनीक के ज़रिये टमाटर, गोभी, बैंगन, भिंडी, करेला, मिर्च, ककड़ी, शिमला मिर्च, खीरा और पालक व अन्य़ पत्तेदार सब्ज़ियों की खेती की जा रही है.
बिना मिट्टी वाली खेती में मिट्टी की जगह ठोस पदार्थ के रूप में बालू, बजरी, धान की भूसी, कंकड़, लकड़ी का चूरा, पौधों का वेस्ट जैसे नारियल का जट्टा, जूट आदि का इस्तेमाल किया जाता है. जूट और नारियल के जट्टे में पानी सोखने की क्षमता ज़्यादा होती है. यह भुरभुरा होता है, जिससे जड़ों को हवा मिलती रहती है. बिना मिट्टी के खेती करने की तकनीक को हाइड्रोपोनिक्स यानी जलकृषि कहा जाता है. जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है, इसमें मिट्टी का इस्तेमाल नहीं किया जाता. मिट्टी की जगह पानी ही खेती की बुनियाद होता है. पौधों को पानी से भरे एक बर्तन में उगाया जाता है. पौधों को बढ़ने के लिए जिन पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, उन्हें पानी में मिला दिया जाता है. पोषक तत्वों और ऑक्सीज़न को पौधों की जड़ों तक पहुंचाने के लिए एक पतली नली का इस्तेमाल किया जाता है. जलकृषि दो तरीक़ों से की जाती है. पहली है घोल विधि और दूसरी माध्यम विधि. घोल विधि के तहत पौधों को पानी से भरे एक बर्तन में रखा जाता है और फिर पोषक तत्वों का घोल प्रवाहित किया जाता है. पौधों की जड़ों तक ऑक्सीज़न और पोषक तत्वों को पहुंचाया जाता है. घोल विधि तीन तरह की है- स्थैतिक घोल विधि, सतत बहाव विधि और एयरोपोनिक्स. स्थैतिक घोल विधि में पौधों को पानी से भरे बर्तन में रखा जाता है और फिर पोषक तत्वों के घोल को धीरे-धीरे नली से प्रवाहित किया जाता है. जब पौधे कम हों, तो यह विधि इस्तेमाल में लाई जाती है. ऐसा होने से जड़ों को ऑक्सीज़न भी मिलती रहती है. सतत बहाव घोल विधि के तहत पोषक तत्वों के घोल को लगातार जड़ों की तरफ़ प्रवाहित किया जाता है. जब बड़े से बर्तन में ज़्यादा पौधे उगाने हों, तो इसका इस्तेमाल करते हैं. इन्हें डीप वाटर विधि भी कहा जाता है. अमूमन एक हफ़्ते बाद जब घोल निर्धारित स्तर से कम हो जाता है, तो पानी और पोषक तत्वों को इसमें मिला दिया जाता है. एयरोपोनिक्स यानी बिना मिट्टी के हवा और नमी वाले वातावरण में फलों, सब्ज़ियों और फूलों की फ़सल उगाना. इस तकनीक के तहत पौधों को प्लास्टिक के पैनल के ऊपर बने छेदों में टिकाया जाता है और उनकी जड़ें हवा में लटका दी जाती हैं. सबसे नीचे पानी का टैंक रखा जाता है, जिसमें घुलने वाले पोषक तत्व डाल दिए जाते हैं. टैंक में लगे पंप के ज़रिये पौधों की हवा में लटकी जड़ों पर पानी का छिड़काव किया जाता है. पानी में मिले पोषक तत्वों से ख़ुराक और हवा से ऑक्सीज़न मिलने की वजह पौधे बड़ी तेज़ी से बढ़ते हैं और काफ़ी कम वक़्त में भरपूर पैदावार देते हैं. कमरे में होने वाली इस खेती में रौशनी के लिए एलईडी बल्ब इस्तेमाल किए जाते हैं.
वर्टिकल फ़ार्मिंग भी एक बेहतर विकल्प है. इसमें मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती. वर्टिकल फ़ार्म एक बहुमंज़िला ‘ग्रीन हाउस’ है. इस विधि के तहत कमरों में एक बहु-सतही ढांचा खड़ा किया जाता है, जो कमरे की ऊंचाई के बराबर हिसाब से बनाया जाता है. इसकी दीवारें कांच की होती हैं, जिससे सूरज की रौशनी अंदर तक आती है. वर्टिकल यानी खड़े ढांचे के सबसे निचले ख़ाने में पानी से भरा टैंक रख दिया जाता है. उसमें मछलियां डाली जाती हैं. मछलियों की वजह से पानी में नाइट्रेट की अच्छी ख़ासी मात्रा होती है, जो पौधों के जल्दी बढ़ने में मददगार है. टैंक के ऊपरी ख़ानों में पौधों के छोटे-छोटे बर्तन रख दिए जाते हैं. टैंक से पंप के ज़रिये इस बर्तन तक पानी पहुंचाया जाता है.
जलकृषि में ऐसे पोषक तत्वों का इस्तेमाल किया जाता है, जो पानी में घुलनशील होते हैं. इनका रूप अकार्बनिक और आयनिक होता है. कैल्सियम, मैग्निशियम और पोटैशियम प्राथमिक घुलनशील तत्व हैं. वहीं प्रमुख घोल के रूप में नाइट्रेट, सल्फ़ेट और डिहाइड्रोजन फ़ॊस्फ़ेट इस्तेमाल में लाए जाते हैं. पोटेशियम नाइट्रेट, कैल्सियम नाइट्रेट, पोटेशियम फ़ॊस्फ़ेट और मैग्निशियम सल्फ़ेट रसायनों का भी इस्तेमाल किया जाता है. इसके अलावा आयरन, मैगनीज़, कॉपर, ज़िंक, बोरोन, क्लोरीन और निकल का भी इस्तेमाल होता है. इस तकनीक की ख़ासियत यह है कि इसमें मिट्टी के बिना और कम पानी के इस्तेमाल से सब्ज़ियां उगाई जाती हैं. इसमें मिट्टी का इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए इसके ज़रिये छत पर भी खेती की जा सकती है. इस तकनीक की खेती में मेहनत कम लगती है. फ़सल की बुआई के लिए खेतों में जुताई करने और सिंचाई की भी ज़रूरत नहीं है. खरपतवान निकालने की मेहनत से भी आज़ादी है. इसमें पानी भी बहुत कम लगता है. मिसाल के तौर पर मिट्टी वाले खेत में एक किलो सब्ज़ी उगाने में जितने पानी की ज़रूरत होती है, उतने ही पानी में जलकृषि के ज़रिये सौ किलो से ज़्यादा सब्ज़ियां उगाई जा सकती हैं. इसमें खरपतवार नहीं उगते और फ़सल पर नुक़सानदेह कीटों का भी कोई प्रकोप नहीं होता. ऐसे में कीटनाशकों के छिड़काव की मेहनत और ख़र्च दोनों बच जाते हैं. कीटनाशकों का इस्तेमाल न होने की वजह से सब्ज़ियां पौष्टिक तत्वों से भरपूर होती हैं और लम्बे वक़्त तक ताज़ी रहती हैं. ये सब्ज़ियां ऒर्गेनिक सब्ज़ियों जैसी ही होती हैं और इनकी गुणवत्ता भी मिट्टी में उगने वाली फ़सल की तुलना में बेहतर साबित हुई है. ग़ौरतलब है कि सामान्य खेती में कीटनाशकों और रसायनों के अंधाधुंध इस्तेमाल ने फ़सलों को ज़हरीला बना दिया है. अनाज ही नहीं, दलहन, फल और सब्ज़ियां भी ज़हरीली हो चुकी हैं. इनका सीधा असर सेहत पर पड़ रहा है.
इसके अलावा एक और विधि से बहुत कम पानी और कम मिट्टी में भी सब्ज़ियां उगाई जाती हैं. इस विधि का नाम है ट्रे कल्टीवेशन यानी ट्रे में फ़सल उगाना. इसके तहत ट्रे में हरी जाली बिछाई जाती है. फिर उसमें जूट बिछा दिया जाता है. इसके बाद केंचुए की खाद डाली जाती है. फिर इसमें बीज बो दिए जाते हैं. समय-समय पर इसमें पोषक तत्वों का छिड़काव किया जाता है. फिर से ट्रे को जाली से ढक दिया जाता है. जाली से ढकी होने की वजह से पौधे कीट-पतंगों से सुरक्षित रहते हैं. राजस्थान में किसान इस तकनीक को अपना रहे हैं. राज्स्थान में इस तकनीक से खेती हो रही है.
देश के कई हिस्सों में अब बिना मिट्टी के खेती हो रही है. हरियाणा के पानीपत ज़िले के जोशी गांव के किसान अनुज भी बिना मिट्टी के खेती कर रहे हैं. उन्होंने ऒस्ट्रेलिया में बिना मिट्टी वाली खेती देखी और इसका प्रशिक्षण लिया. फिर स्वदेश लौटने पर उन्होंने इस नई तकनीक से खेती शुरू की. वह 15 एकड़ से भी ज़्यादा भूमि पर मिट्टी रहित जैविक खेती कर रहे है. इस प्रगतिशील किसान का कहना है कि उनके गांव की मिट्टी में खरपतवार बहुत है, जिससे उत्पादन होता है. इसी वजह से उन्होंने मिट्टी रहित खेती की इस तकनीक को अपनाया. उन्होंने बताया कि इस खेती में मिट्टी की जगह नारियल के अवशेष का इस्तेमाल होता है और इसे छोटी-छोटी थैलियों में डालकर पॊली हाऊस में सब्ज़ी के पौधे उगाए जाते हैं. नारियल के इस अवशेष को खेती के लिए लगातार तीन साल तक इस्तेमाल किया जा सकता है. उन्होंने बताया कि इस तकनीक से लगातार सात महीनों तक सब्ज़ियों की पैदावार होती है. वह हर तीन साल बाद केरल से नारियल के अवशेष मंगवाते हैं. इसका एक बैग तक़रीबन 5 किलो का होता है, जिसकी क़ीमत 30 रुपये है. उन्होंने बताया कि वह टमाटर, शिमला मिर्च, गोभी, मटर और खीरा आदि सब्ज़ियां उगाते हैं. सब्ज़ियों को बेचने के लिए उन्हें बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती. व्यापारी ख़ुद उनके फ़ार्म से सब्ज़ियां ख़रीद कर ले जाते हैं. उन्हें सब्ज़ियों की अच्छी क़ीमत मिलती है.
छत्तीसगढ़ के रायपुर में रहने वाले अनिमेष तिवारी अपने घर की छत पर सब्ज़ियां उगाते हैं. वह गोभी, बैंगन, शिमला मिर्च और चाइनीज़ कैबिज, ब्रोकोली आदि की खेती करते हैं. उन्होंने छत पर एक स्टैंड पर प्लास्टिक के मोटे पाइप रखे हुए हैं, जिनमें थोड़ी-थोड़ी दूरी पर ख़ास आकार में छेद किए गए हैं. वह जालीदार बर्तन में नारियल की भूसी डालते हैं. फिर इसी भूसी में सब्ज़ियों के बीज बो देते हैं. इन बर्तनों में पानी डाला जाता है. जब बीज से छोटे पौधे निकलने लगते हैं, तो बर्तन को प्लास्टिक के पाइप में बने छेद पर फिट कर दिया जाता है. इससे उन्हें काफ़ी मुनाफ़ा हो रहा है.
इस तकनीक के ज़रिये अब चारा भी उगाया जाएगा. कम पानी वाले शुष्क इलाक़ों में उगने वाली सेवण घास की पौध भी इस तकनीक से तैयार की जा चुकी है. राजस्थान के वेटरनरी विश्वविद्यालय के पशुधन चारा संसाधन प्रबंधन एवं तकनीक केंद्र के वैज्ञानिकों ने सेवण के बीजों को बिना मिट्टी के धूप, पानी और पोषक तत्वों का इस्तेमाल करके नियंत्रित तापक्रम पर सात दिन की अवधि में सेवण की पौध तैयार की थी. वैज्ञानिकों का कहना है कि इस तकनीक से तैयार हुई पौध से चारागाह में सेवण घास को पनपाने और हल्के-फुल्के बीजों की बिजाई में आने वाली मुश्किलों से छुटकारा मिल जाएगा. ग़ौरतलब है कि सेवण घास रेगिस्तानी इलाक़ों के पालतू पशुओं गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट और वन्य पशुओं का पौष्टिक आहार है. सेवण का पौधा एक बार पनपने के बाद बूझे का स्वरूप ले लेता है, जो बहुत लंबे वक़्त तक शुष्क क्षेत्र में पौष्टिक एवं स्वादिष्ट चारे का उत्पादन देने में सक्षम होता है. सेवण के बीज परिपक्व होते ही झड़ कर तेज़ हवा और आंधी में उड़ जाते हैं.
जलकृषि के ज़रिये लगातार पैदावार ली जा सकती है और किसी भी मौसम में सब्ज़ियां उगाई जा सकती हैं. इसमें खेती के आधुनिक उपकरणों की भी कोई ज़रूरत नहीं होती. इस तकनीक की एक बड़ी ख़ासियत यह भी है कि फ़सलें प्राकृतिक आपदाओं जैसे ओलावृष्टि, बेमौसमी बारिश और सूखे से भी बची रहती हैं. किसानों को बिना मिट्टी के खेती की यह तकनीक बहुत पसंद आ रही है. मिट्टी पारंपरिक खेती के मु़क़ाबले इसमें लागत बहुत कम आती है, जबकि मुनाफ़ा ज़्यादा होता है. कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि जिन किसानों की ज़मीन बंजर है, वे जलकृषि को अपनाकर फ़सलें उगा सकते हैं. कृषि विभाग के अधिकारी किसानों को बिना मिट्टी के खेती करने का प्रशिक्षण दे रहे हैं. हरियाणा के किसानों ने तक़रीबन 1800 एकड़ बंजर ज़मीन में पॊली हाउस बनाए हुए हैं.
जलकृषि वक़्त की ज़रूरत है. दुनिया की आबादी तक़रीबन आठ अरब है, जो लगातार बढ़ ही रही है. अगले एक-दो दशक में आबादी बढ़कर नौ अरब होने की संभावना है. आने वाले दो दशकों में खाद्यान्न उत्पादन में 50 फ़ीसद बढ़ोतरी होने पर ही लोगों को भोजन मिल पाएगा. फ़िलहाल दुनिया भर में तक़रीबन 25000 लाख टन खाद्यान्न की पैदावार हो रही है, जो भविष्य़ की बढ़ी आबादी के लिए बहुत कम रहेगी. लगातार जलवायु परिवर्तन, बंजर होती ज़मीन, घटती कृषि भूमि, जल संकट को देखते हुए कृषि के नये तरीक़े अपनाकर ही आबादी के लिए खाद्यान्न जुटाया जा सकेगा.
वर्टिकल फ़ार्मिंग के ज़रिये भी किसान कम जगह में सब्ज़ियां उगा सकते हैं. कम जगह, कम लागत, कम मेहनत में अच्छी पैदावार मुनाफ़े का सौदा है. आज़माकर ज़रूर देखें.
रबी की फ़सल कट रही है. ख़रीफ़ की फ़सल की बुआई से पहले किसान खेतों को ख़ाली रखने की बजाय मूंग की फ़सल उगा कर अतिरिक्त आमदनी हासिल कर रहे हैं. फ़सल चक्र अपनाने से उत्पादन के साथ-साथ भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहती है. धान आधारित क्षेत्रों के लिए धान-गेहूं-मूंग या धान-मूंग-धान, मालवा निमाड़ क्षेत्र के लिए मूंग-गेहूं-मूंग, कपास-मूंग-कपास फ़सल चक्र अपनाया जाता है. मूंग की फ़सल भारत की लोकप्रिय दलहनी फ़सल है और इसकी खेती विभिन्न प्रकार की जलवायु में की जाती है. यह फ़सल सभी प्रकार की भूमि में उगाई जा सकती है, लेकिन अच्छे जल निकास वाली बलुई और दोमट मिट्टी इसके लिए उपयुक्त रहती है. मूंग ख़रीफ़, रबी और जायद तीनों मौसम में उगाई जाती है. दक्षिण भारत में मूंग रबी मौसम में उगाई जाती है, जबकि उत्तर भारत में ख़रीफ़ और जायद मौसम में उगाई जाती है. उत्तर भारत में किसान रबी और ख़रीफ़ मौसम के बीच मूंग की खेती कर रहे हैं. पहले किसान रबी की फ़सल काटने के बाद और ख़रीफ़ की फ़सल की बुआई से पहले बीच के वक़्त में साठी धान की फ़सल उगाते थे. साठी धान में पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती है और लगातार घटते भू-जलस्तर को देखते हुए अनेक स्थानों पर साठी धान उगाने पर पाबंदी लगा दी गई है. ऐसे में कृषि विशेषज्ञ किसानों को मूंग की फ़सल उगाने की सलाह दे रहे हैं. उनका कहना है कि गर्मी में ज़्यादा तापमान होने पर भी मूंग की फ़सल में इसे सहन करने की शक्ति होती है. कम अवधि की फ़सल होने की वजह से यह आसानी से बहु फ़सली प्रणाली में भी ली जा सकती है. उन्नत जातियों और उत्पादन की नई तकनीकी तथा सदस्य पद्धतियों को अपनाकर इसकी पैदावार बढ़ाई जा सकती है. गर्मी में मूंग की खेती से कई फ़ायदे होते हैं. इस मौसम में मूंग पर रोग और कीटों का प्रकोप कम होता है और अन्य फ़सलों के मुक़ाबले सिंचाई की ज़रूरत भी कम होती है. धान के मुक़ाबले किसानों को मूंग की फ़सल से ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है. इसलिए अब किसानों का रुझान मूंग की तरफ़ बढ़ रहा है. मूंग की फ़सल 65 से 70 दिन में पककर तैयार हो जाती है और किसान 400 से 480 किलो प्रति हेक्टेयर उपज हासिल कर सकते हैं.
कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि दलहनी फ़सल होने के कारण यह तक़रीबन 20 से 22 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हैक्टेयर स्थिर करके मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाती है. मूंग की फ़सल खेत में काफ़ी मात्रा में कार्बनिक पदार्थ छोड़ती है, जिससे किसानों को अतिरिक्त लाभ मिल जाता है. जायद और रबी के लिए मूंग की अलग-अलग क़िस्में होती हैं. कृषि विशेषज्ञों के मुताबिक़ जायद के लिए मूंग की दो अच्छी क़िस्में हैं. पहली पूसा-9531. इस क़िस्म का पौधा सीधा बढ़ने वाला छोटा क़द का होता है, दाना मध्यम, चमकीला हरा, पीला मोजेक वायरस प्रतरोधी है. दूसरी क़िस्म है पूसा-105. इस क़िस्म का दाना गहरा हरा, मध्यम आकार का, पीला मोजेक वायरस प्रतरोधी होने के साथ-साथ पावडरी मल्डयू और मायक्रोफोमीना ब्लाईट रोगों के प्रति सहनशील है. मूंग की बुआई करते वक़्त किसान ध्यान रखें कि कतारों के बीच 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए. मूंग की फ़सल की बुआई के लिए 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की ज़रूरत होती है. मूंग की बिजाई के बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर तीन-चार बार सिंचाई करनी चाहिए. पहली नींदाई बुवाई के 20 से 25 दिन के भीतर और दूसरी 40 से 45 दिन में करना चाहिए. दो-तीन बार कोल्पा चलाकर खेत को नींदा रहित रखा जा सकता है. खरपतवार नियंत्रण के लिए नींदा नाशक दवाओं जैसे बासालीन या पेंडामेथलीन का इस्तेमाल भी किया जा सकता है. बासालीन 800 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से 250 से 300 लीटर पानी में बोनी पूर्व छिड़काव करना चाहिए. मूंग की फ़सल की शुरुआत में तनामक्खी, फलीबीटल, हरी इल्ली, सफ़ेद मक्खी, माहों, जैसिड, थ्रिप्स आदि का प्रकोप होता है. इनकी रोकथाम के लिए इंडोसल्फान 35 ईसी 400 से 500 मिलीलीटर और क्वीनालफॉस 25 ईसी 600 मिलीलीटर प्रति एकड़ या मिथाइल डिमेटान 25 ईसी 200 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए. ज़रूरत पड़ने पर 15 दिन बाद दोबारा छिड़काव करना चाहिए. पुष्पावस्था में फली छेदक, नीली तितली का प्रकोप होता है. क्वलीनालफॉस 25 ईसी का 600 मिलीलीटर या मिथाइल डिमेटान 25 ईसी का 200 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करने से इनकी रोकथाम हो सकती है. कई इलाको़ में कम्बल कीड़े का भारी प्रकोप होता है. इसकी रोकथाम के लिए पेराथियान चूर्ण दो फ़ीसद, 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से भुरकाव करना चाहिए. फ़सल को मेक्रोफोमिना रोग से बचाने के लिए 0.5 फ़ीसद कार्बेंडाजिम या फायटोलान या डायथेन जेड-78, 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए. कोफोमिना और सरकोस्पोरा फफूंद द्वारा पत्तियों के निचले भाग कत्थई भूरे रंग के विभिन्न आकार के धब्बे पर बन जाते हैं. इसी तरह भभूतिया रोग या बुकनी रोग से बचाव के लिए घुलनशील गंधक 0.15 फ़ीसद या कार्बेंडाजिम 0.1 फ़ीसद के 15 दिन के अंतराल पर तीन बार छिड़काव करना चाहिए. इस रोग की वजह से 30 से 40 दिन की फ़सल में पत्तियों पर सफ़ेद चूर्ण दिखाई देता है. पीला मोजेक वायरस रोग के कारण पत्तियां और फलियां पीली पड़ जाती है और उपज पर प्रतिकूल असर होता है. यह सफ़ेद मक्खी द्वारा फैलने वाला विषाणु जनित रोग है. इसकी रोकथाम के लिए मोनोक्रोटोफॉस 36 ईसी 300 मिलीलीटर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करना चाहिए. प्रभावित पौधों को उखाड़कर नष्ट कर देना चाहिए. इस रोग से बचने के लिए पीला मोजेक वायरस निरोधक क़िस्मों को उगाना चाहिए. जब फलियां काली होकर पकने लगें, तब उन्हें तोड़ना चाहिए. फिर इन फलियों को सुखा लें और गहाई करें.
दलहनी फ़सलों के बाज़ार में अच्छे दाम मिल जाते हैं.
क़ाबिले-ग़ौर है कि सरकार ने दलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए तिलहन, दलहन और मक्का प्रौद्योगिकी मिशन के तहत राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना (एनपीडीपी) शुरू की है. इसके तहत दलहन की फ़सलों को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को बीज, खाद आदि कृषि विभाग की ओर से मुफ़्त दिए जाते हैं. किसान इस योजना का लाभ भी उठा सकते हैं.
ग्रामीण इलाक़ों में रहने वाली 70 फ़ीसद से ज़्यादा आबादी सहित देश का आर्थिक विकास कृषि क्षेत्र की हालत पर निर्भर करता है. किसानों के लिए यह भी बेहद ज़रूरी है कि ख़ून-पसीने से सींची गई फ़सल की उन्हें सही क़ीमत मिले. इसके लिए सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं, जिनका फ़ायदा किसानों को मिल भी रहा है. भूमंडलीकरण और आर्थिक उदारीकरण के दौर में कृषि विपणन क्षेत्र में भी ख़ासा बदलाव देखा गया है. किसानों के उत्पादों को नये वैश्विक बाज़ार पहुंचाने के लिए देश की आंतरकि कृषि विपणन प्रणाली का एकीकरण और सशक्तिकरण किया जा रहा है. विभिन्न अध्ययनों की मानें, तो किसान अपने उत्पादों को ग्रामीण और अविनियमित थोक बाज़ारों के मुक़ाबले विनिमित बाजारों (कृषि उत्पाद बाजार समितियां यानी एपीएमसीए) में बेचकर ज़्यादा मुनाफ़ा हासिल करते हैं. विपणन और निरीक्षण निदेशालय (डीएमआई) देश में बाज़ार मूल्यों संबंधी सूचना के प्रभावी आदान-प्रदान के लिए काम कर रहा है.
ग़ौरतलब है कि कृषि विपणन निदेशालय किसानों के लिए विपणन सुविधाएं मुहैया कराने का काम करता है, ताकि उन्हें उनके उत्पादन की वाजिब क़ीमत मिल सके. कारोबार में कदाचार को ख़त्म करने के लिए बाज़ार को नियम के अधीन रखा गया है और इसलिए यह नियमित बाज़ार के रूप में जाना जाता है. मानकीकरण और कृषि उपज की ग्रेडिंग भी शुरू गई है. इस तरह किसानों को गुणवत्ता वाले उत्पादन का अच्छा मुनाफ़ा मिलता है. बाज़ार आसूचना का कार्य बाज़ार व्यवहार को एकत्रित करना है, जो विपणन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एक शर्त के रूप में विचार में लाया जाता है. एगमार्क के तहत ग्रेडिंग, निदेशालय का एक महत्वपूर्ण कार्य है. दरअसल, बाज़ार और बाज़ार कार्यप्रणाली के विनियमन के तहत किसानों को उनकी फ़सल के लाभकारी मूल्य के लिए विपणन सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं.
कृषि उत्पादकों के हितों की रक्षा करने के लिए कृषि उत्पाद मार्केट समितियों की स्थापना की गई है. ये बाज़ार दिल्ली कृषि विपणन निर्माण (विनियमन) अधिनियम, 1998 के प्रावधान के तहत स्थापित किए गए हैं. दिल्ली कृषि विपणन बोर्ड अधीक्षण और विनियमित बाज़ार समिति के नियंत्रण के लिए कार्य कर रहा है. बाद में यह सीधे निदेशालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आ गया है. दिल्ली में अनेक विनियमित बाज़ार काम कर रहे हैं, जिनमें नज़फ़गढ़ का खाद्य अनाज बाज़ार, नरेला में खाद्य अनाज बाज़ार, शाहदरा और ग़ाज़ीपुर का खाद्यान्न, फल और सब्ज़ी बाज़ार, मंगोलपुरी इंडस्टियल एरिया, फ़ेज़-दो का चारा बाज़ार, आज़ादपुर का फल और सब्ज़ी बाज़ार, ग़ाज़ीपुर की मछली, मुर्ग़ा और अंडे की मार्केट, बाग़ दीवार का खोया व मावा बाज़ार, महरौली का फूल बाज़ार और केशोपुर का फल और सब्ज़ी बाज़ार शामिल हैं.
एगमार्क के तहत ग्रेडिंग का संवर्धन किया जाता है. यह योजना उत्पादकों के लिए, ग्रेडिंग सुविधाएं मुहैया करती है, ताकि वे पूर्व परीक्षत गुणवत्तायुक्त उत्पादों के बाज़ारीकरण द्वारा अनुकूल प्रतिलाभ सुनिश्चित कर सकें. ग्रेडिंग एग्रीकल्चर प्रोडयूस ग्रेडिंग और मार्केटिंग अधिनियम-1986 के तहत की जाती है. ग्रेडिंग के लिए ग्रेड मानक निर्धारित करना, रासायनिक परीक्षण के लिए पहली ज़रूरत है. इस अधिनियम के मुताबिक़ उत्पादकों के पास उत्पाद के परीक्षण के लिए अपनी प्रयोगशाला होनी चाहिए. वैकल्पिक रूप से वे राज्य सरकारों द्वारा ग्रेडिंग/ परीक्षण के लिए राज्य ग्रेडिंग प्रयोगशाला द्वारा स्थापित सेवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं. इस निदेशालय में राज्य ग्रेडिंग प्रयोगशाला कार्यान्वित है. फ़िलहाल विभाग के ज़रिये ग्रेडिंग के लिए तक़रीबन 70 निर्माता संलग्न हैं. मौजूदा वक़्त में मसाले, बेसन, दालें, गेहूं का आटा, शहद, आमचूर पाउडर, हींग और वनस्पति तेल को राज्य ग्रेडिंग प्रयोगशाला में वर्गीकृत किया गया है. मई 2007 के बाद ग्रेडिंग, फलों और सब्ज़ियों का मानकीकरण भी शुरू हो गया, जिसके लिए नई माइक्रोबायोलॉजी एवं इंस्ट्रूमेंटेशन लैब्स अधिकृत हुई.
बाज़ार आसूचना के लिए समन्वित योजना के तहत बाज़ार का सर्वेक्षण, बाज़ार के नियमन और विपणन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए, सही फ़ैसले की ज़रूरत है. बाज़ार के व्यवहार का नियमित अध्ययन यानी आगमन, मूल्य अध्ययन इत्यादि, नीति आदि बनाने के लिए ज़रूरी है. इसके तहत ऐसी गतिविधियों चल रही हैं, जहां विभिन्न बाज़ारों से बाज़ार की जानकारी को दैनिक और साप्ताहिक आधार पर इकट्ठा किया जा रहा है. इसके बाद इन सूचनाओं का विश्लेषण किया जाता है और विभिन्न प्रमुख एजेंसियों को विभिन्न मंत्रालयों के लिए ज़रूरी चीज़ों की दैनिक दरों को दिया जाता है. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के विभिन्न बाज़ारों में विभिन्न वस्तुओं का व्यवहार का चित्रण मासिक बुलेटिन भी प्रकाशित किया गया है. थोकयुक्त एक साप्ताहिक रिपोर्ट और बड़ी संख्या में विभिन्न अनियंत्रित बाज़ार की ज़रूरी चीज़ों का खुदरा मूल्य भी तैयार किया जाता है और केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को भेजा जाता है.
पिछले दिनों प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने कृषि-तकनीक मूलभूत सुविधा कोष (एटीआईएफ) के ज़रिये राष्ट्रीय कृषि विपणन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय क्षेत्र परियोजना को अपनी मंज़ूरी दी है. कृषि एवं सहकारिता विभाग (डीएसी) इसे पूरे देश में चयनित विनियमित बाजारों में तैनाती योग्य आम इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के निर्माण द्वारा लघु किसानों को कृषि व्यवसाय संघ (एसएफएसी) के माध्यम से स्थापित करेगा. इसके तहत साल 2015-16 से साल 2017-18 की परियोजना के लिए 200 करोड़ रुपये की धनराशि निर्धारित की गई है. इसमें डीएसी की ओर से राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के लिए निःशुल्क सॉफ्टवेयर की आपूर्ति का प्रावधान शामिल है. साथ ही, इसमें डीएसी द्वारा 30 लाख प्रति मंडी (निजी मंडियों के अलावा) तक के लिए केंद्र सरकार की ओर से संबंधित हार्डवेयर व बुनियादी ढांचे की लागत में रियायत देने का प्रावधान भी शामिल है.
इसका लक्ष्य देशभर में चयनित 585 विनियमित बाजारों को कवर करना है. साल 2015-16 में 250 मंडी, 2016-17 में 200 मंडी और 2017-18 में 135 मंडियों को कवर करने का लक्ष्य रखा गया है. किसान और व्यापारी देश भर में पारदर्शी तरीक़े से उचित दामों पर कृषि-पदार्थों की ख़रीद/बिक्री कर सकें, इसके लिए 585 विनियमित बाज़ारों को आम ई-मंच के साथ एकीकृत किया जाएगा. इसके अलावा इसकी पहुंच बढ़ाने के लिए निजी बाज़ारों को भी इस तरह से ई-मंच के इस्तेमाल की इजाज़त दी जाएगी. यह योजना अखिल भारतीय स्तर पर लागू होगी. योजना के तहत राज्यवार आवंटन का विकल्प मौजूद नहीं है. हालांकि इच्छुक राज्य को ज़रूरी कृषि-विपणन सुधारों को इस्तेमाल में लाने के लिए पूर्व अपेक्षित मांगों को पूरा करने की ज़रूरत होगी.
एसएफ़एसी कृषि मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ई-बाज़ार का विकास करने के लिए अगुआ एजेंसी होगी और यह खुली बोली (ओपन बिडिंग) के माध्यम से सेवा प्रदाता का चयन करेगी. एक उपयुक्त आम ई-बाज़ार मंच की स्थापना की जाएगी, जो राज्य/संघ प्रशासित केंद्रों में ई-मंच से जुड़ने को इच्छुक चयनित 585 विनियमित थोक बाज़ार में तैनाती योग्य होगा. एसएफ़एसी 2015-16, 2016-17 और 2017-18 की अवधि के दौरान राष्ट्रीय ई-प्लेटफॉर्म को तीन चरणों में लागू करेगी. डीएसी राज्यों के लिए सॉफ्टवेयर और इसके अनुकूलन पर हो रहे ख़र्च को पूरा करेगी और इसे राज्य और संघ शासित प्रदेशों को निःशुल्क उपलब्ध करवाएगी. डीएसी ई-विपणन मंच की स्थापना के लिए, 585 विनियमित बाज़ारों में, संबंधित उपकरण/बुनियादी ढांचे के लिए प्रति मंडी 30 लाख रुपये तक की अंतिम सीमा में एक बार तय की गई लागत के रूप में अनुदान भी देगी. बड़ी और निजी मंडियों को भी मूल्य निर्धारण के लिए ई-मंच के इस्तेमाल की इजाज़त होगी. हालांकि उन्हें उपकरण/बुनियादी ढांचे के लिए किसी भी तरह के धन से मदद नहीं की जाएगी.
ई-मंच के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों को पूरे राज्य में वैध एकल लाइसेंस, बाज़ार शुल्क का एकल बिंदु लेवी मूल्य और मूल्य निर्धारण के लिए एक साधन के रूप में इलेक्ट्रॉनिक नीलामी के प्रावधान के रूप में ये तीन पूर्व सुधारों को अपनाने की ज़रूरत होगी. परियोजना के तहत सहयोग पाने के लिए केवल वही राज्य और केंद्रशासित प्रदेश योग्य होंगे, जो इन तीन पूर्व अपेक्षित मांगों को पूरा करेंगे. ई-विपणन मंच का उद्देश्य कृषि विपणन क्षेत्र में सुधारों को बढ़ावा देना होना चाहिए और देशभर में कृषि-पदार्थों के मुक्त प्रवाह को बढ़ावा देने के अलावा किसानों की संतुष्टि को बढ़ाना भी होना चाहिए, क्योंकि इससे किसान के उत्पादन के विपणन की संभावनाएं काफ़ी बढ़ेंगी. उसकी विपणन संबंधी सूचनाओं तक बेहतर पहुंच होगी और उनके पास अपने उत्पादों की बेहतर क़ीमत पाने के लिए ज़्यादा कुशल पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी विपणन का मंच होगा, जो पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के ज़रिये राज्य के भीतर और बाहर भी बड़ी संख्या में ख़रीददारों तक उनकी पहुंच बनाएगा. इससे किसानों की गोदाम आधारित बिक्री के ज़रिये बाज़ार तक पहुंच में भी बढ़ोतरी होगी और इस तरह मंडी तक अपने उत्पादों को भेजने की ज़रूरत नहीं रहेगी.
क़ाबिले-ग़ौर है कि कृषि-तकनीक मूलभूत सुविधा कोष और राष्ट्रीय विपणन को स्थापित करने के लिए क्रमशः साल 2014 और 2015 में लगातार किए गए बजट की घोषणाओं के बाद, डीएसी ने कृषि-तकनीक मूलभूत सुविधा कोष (एटीआईएफ़) की मदद से राष्ट्रीय कृषि बाज़ार के संवर्धन के लिए एक योजना तैयार की है. देशभर में ई-मंच के ज़रिये कृषि बाज़ारों के एकीकरण को मौजूदा कृषि बाज़ार व्यवस्था द्वारा पेश की गई चुनौतियों, ख़ासकर बहु-विपणन क्षेत्र में राज्य का विखंडन जिसमें प्रत्येक को अलग अलग एपीएमसी द्वारा व्यवस्थित किया जाता है, मंडी शुल्क के विविध स्तर, विभिन्न एपीएमसीज में व्यापार के लिए बहु लाइसेंस प्रणाली की ज़रूरत, बुनियादी ढांचे की बुरी हालत और तकनीक, सूचना विषमता का कम इस्तेमाल, कीमत निर्धारण की अपारदर्शी प्रक्रिया, बाज़ार परिवर्तन का उच्च स्तर, गति नियंत्रण का कम इस्तेमाल आदि समस्याओं को हल करने के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण क़दम के रूप में देखा जा रहा है. यहां राज्य और देश के स्तर पर बाज़ार को एकीकृत करने, स्पष्ट तौर पर किसानों को बेहतर मूल्य प्रदान करने के लिए, आपूर्ति श्रृंखला को बेहतर बनाने के लिए, बर्बादी को रोकने के लिए और राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत बाज़ार की स्थापना के लिए आम ई-मंच के प्रावधान की ज़रूरत है.
राष्ट्रीय कृषि बाज़ार (एनएएम) के ज़रिये भी कृषि उत्पादों के विपणन को बढ़ावा दिया जा रहा है. केन्द्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह के मुताबिक़ राष्ट्रीय कृषि बाज़ार एक राष्ट्रीय स्तर का इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है, जिसे भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा विकसित किया जा रहा है. इसका उद्देश्य देश के विभिन्न राज्यों में स्थित कृषि उपज मंडी श्रृंखला को इंटरनेट के माध्यम से जोड़कर एकीकृत राष्ट्रीय कृषि उपज बाज़ार बनाना है. राष्ट्रीय कृषि बाज़ार के पीछे स्थानीय कृषि उपज मंडी रहेगी. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय कृषि बाज़ार को समानांतर कृषि विपणन व्यवस्था के रूप में विकसित नहीं किया जा रहा है. राष्ट्रीय कृषि बाज़ार से जुड़कर कोई भी कृषि उपज मंडी पहले की भांति काम करती रहेगी. राष्ट्रीय कृषि बाज़ार से जुड़कर कोई भी कृषि उपज मंडी राष्ट्रीय व्यापार नेटवर्क में भाग ले सकती है. किसान जब स्थानीय स्तर पर अपने उत्पाद बेचने के लिए मंडी में लाते हैं, तो उन्हें स्थानीय व्यापारियों के साथ-साथ इंटरनेट के माध्यम से देश के अन्य राज्यों में स्थित व्यापारियों को भी अपने माल बेचने का विकल्प व व्यवस्था होगी. जहां बेहतर भाव मिलेंगे, किसान वहां बेचने के लिए स्वतंत्र होंगे.
कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय बाज़ार का लक्ष्य है कि पूरा देश एक मंडी क्षेत्र बने, जिसमें किसी भी स्थान से दूसरे स्थान के लिए कृषि उत्पाद की आवाजाही तथा विपणन आसानी से व कम समय में हो. इसका सीधा लाभ कृषकों, व्यापरियों तथा ग्राहकों को मिलेगा, क्योंकि बड़े पैमाने पर कृषि उत्पाद का व्यापार किसानों को बेहतर दाम देगा, वहीं व्यापारियों को भी अधिक अवसर मिलेंगे. यह सब करते वक़्त स्थानीय कृषि उपज मंडी के हित को कोई नुक़सान नहीं पहुंचेगा, क्योंकि पूरा व्यापार उसके माध्यम से ही होगा. इसके साथ कृषि उपज मंडी के कर्मचारी व व्यापारी प्रशिक्षण, आधारभूत संरचना आदि के लिए वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे कृषि उपज मंडी इस व्यवस्था को प्रभावशाली रूप से चलाने के लिए सक्षम हो.
कृषि मंत्री का यह भी कहना है कृषि उपज मंडी के राष्ट्रीय बाज़ार नेटवर्क से जुड़ने से पूर्व उस राज्य की मंडी अधिनियम में तीन प्रावधान होने ज़रूरी हैं. पहला राज्य मंडी अधिनियम में इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का प्रावधान होना चाहिए. दूसरा, राज्य मंडी अधिनियम में भारत के अन्य राज्यों के व्यापारियों को लाइसेंस देने का प्रावधान होना चाहिए, जिससे वे किसी भी मंडी में राष्ट्रीय कृषि बाज़ार के माध्यम से कृषि व्यापार प्रक्रिया में भाग ले सकें. तीसरा, मंडी अधिनियम में यह प्रावधान भी होना चाहिए कि केवल एक लाइसेंस लेकर व्यापारी प्रदेश की सभी मंडी में व्यापार कर सकता है और मंडी शुल्क एक स्थान पर अदा किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय कृषि बाज़ार को एक ऐसी व्यवस्था के रूप में विकसित किया जा रहा है, ताकि इससे जुड़े हर वर्ग को लाभ मिले. किसान को राष्ट्रीय कृषि बाज़ार के माध्यम से कृषि उत्पाद के विक्रय में अधिक दाम मिलने की संभावना है. स्थानीय व्यापारियों को अपने ही प्रदेश के अन्य भागों में तथा अन्य राज्यों में कृषि उत्पाद बेचने के मौक़े मिलेंगे. थोक व्यापारियों को, चावल, दाल, दलहन, मिल संचालकों को सीधे राष्ट्रीय कृषि बाज़ार के माध्यमों से दूर स्थित मंडी से कृषि उत्पाद ख़रीदने का मौक़ा मिलेगा. ग्राहकों को कृषि उपज आसानी से उपलब्ध होगा और मूल्य भी स्थिर रहेगा. बड़े पैमाने पर ख़रीदारी होने से गुणवत्ता तथा उत्पाद ख़राब होने का अनुपात भी कम होगा. देश की सभी मंडियों के धीरे-धीरे राष्ट्रीय कृषि बाज़ार नेटवर्क से जुड़ने से भारत में पहली बार एक राष्ट्रीय कृषि उपज बाज़ार विकसित होगा. नतीजतन देश में ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत के कृषि उत्पादों के विक्रय की सुविधा होगी.
कृषि विभाग द्वारा जगह-जगह प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन कर किसानों को उनके कृषि उत्पाद से प्रोडेक्ट बनाने और उनकी मार्केटिंग के गुर सिखाए जाते हैं. इस दौरान विशेषज्ञ किसानों को आलू के चिप्स बनाने, अपने घर पशुओं के दूध से विभिन्न क़िस्म की मिठाइयां और पनीर आदि बनाने के तरीक़े बताते हैं. वहीं कृषि उत्पाद का भंडारण से लेकर उसके बिक्री तक उसका सुरक्षित रखरखाव कैसे किया जाए, इसकी जानकारी भी दी जाती है. विशेषज्ञ किसानों को बताते हैं कि अच्छी क़ीमत हासिल करने के लिए वे समूह बनाकर सोसाइटी एक्ट तथा कंपनी एक्ट के तहत अपने उत्पाद की मार्केटिंग करें.
किसान दिन-रात मेहनत करते फ़सल उगाते हैं. उन्हें अपनी फ़सल की सही क़ीमत हासिल करने के लिए जागरूक होना होगा. अगर वो बिचौलिये के चक्कर में न पड़कर ख़ुद अपनी उपज बाज़ार में ले जाकर बेचेंगे, तो उन्हें ज़्यादा मुनाफ़ा होगा. इसके लिए इन्हें जागरूक होना होगा.
वृक्ष जीवन का आधार हैं. इनसे जीवनदायिनी ऒक्सीज़न मिलती है. फल-फूल मिलते हैं, औषधियां मिलती हैं, छाया मिलती, लकड़ी मिलती है. इस सबके बावजूद बढ़ती आबादी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वृक्षो को काटा जा रहा है. घटते वन क्षेत्र को राष्ट्रीय लक्ष्य 33.3 फ़ीसद के स्तर पर लाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाने होंगे. देश में वन क्षेत्रफल 19.2 फ़ीसद है. जंगल ख़त्म हो रहे हैं. इससे पर्यावरण के सामने संकट खड़ा हो गया है. इसलिए वन क्षेत्र को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है. कृषि वानिकी को अपनाकर कुछ हद तक पर्यावरण संतुलन को बेहतर बनाया जा सकता है. फ़सलों के साथ वृक्ष लगाने को कृषि वानिकी कहा जाता है.
खेतों की मेढ़ों के अलावा गांव की शामिलात भूमि, परती भूमि और ऐसी भूमि, जिस पर कृषि नहीं की जा रही हैं, वहां भी उपयोगी वृक्ष लगाकर पर्यावरण को हरा-भरा बनाया जा सकता है. पशुओं के बड़े-बड़े बाड़ों के चारों ओर भी वृक्ष लगाए जा सकते हैं. कृषि वानिकी के तहत ऐसे वृक्ष लगाने चाहिए, जो ईंधन के लिए लकड़ी और खाने के लिए फल दे सकें. जिनसे पशुओं के लिए चारा और खेती के औज़ारों के लिए अच्छी लकड़ी भी मिल सके. इस बात का भी ख़्याल रखना चाहिए कि वृक्ष ऐसे हों, जल्दी उगें और उनका झाड़ भी अच्छा बन सके. बबूल, शीशम, नीम, रोहिड़ा, ढाक, बांस, महुआ, जामुन, कटहल, इमली, शहतूत, अर्जुन, खेजड़ी, अशोक, पोपलर, सागौन और देसी फलों आदि के वृक्ष लगाए जा सकते हैं.
बबूल रेतीले, ऊबड़-खाबड़ और कम पानी वाले क्षेत्रों में उगाया जा सकता है. इसका झाड़ काफ़ी फैलता है. बबूल की हरी पतली टहनियां दातुन के काम आती हैं. बबूल की दातुन दांतों को स्वच्छ और स्वस्थ रखती है. बबूल की लकड़ी बहुत मज़बूत होती है. उसमें घुन नहीं लगता. बबूल की लकड़ी का कोयला भी अच्छा होता है. भारत में दो तरह के बबूल ज़्यादा पाए और उगाये जाते हैं. एक देसी बबूल, जो देर से होता है और दूसरा विलायती बबूल. बबूल लगाकर पानी के कटाव को रोका जा सकता है. बबूल उगाकर बढ़ते रेगिस्तान को रोका जा सकता है. इसकी लकड़ी से किश्तियां, रेल स्लीपर, खिड़की-दरवाज़े, फ़र्नीचर और खेती में काम आने वाले कई तरह के औज़ार आदि बनाए जाते हैं. इससे ईंधन के लिए भी काफ़ी लकड़ी मिल जाती है. इसकी पत्तियों और बीजों को चारे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है. बकरियों और भेड़ों का यह मुख्य भोजन है.
शीशम भी बहुत उपयोगी वृक्ष है. यह बहुत जल्दी बढ़ता है. इसका झाड़ बहुत बड़ा होता है. इसकी लकड़ी, पत्तियां, जड़ें सभी काम में आती हैं. इसकी लकड़ी भारी और मज़बूत होती है. इससे खिड़की-दरवाज़े, फ़र्नीचर आदि बनाया जाता है. शीशम की लकड़ी से खेतीबाड़ी में इस्तेमाल होने वाले औज़ार भी बनाए जाते हैं. इसकी पत्तियां पशुओं के चारे के काम आती हैं. इसकी पत्तियों में प्रोटीन होता है. जड़ें ज़मीन को उपजाऊ बनाती हैं. भूमि कटाव को रोकते हैं.
नीम सदाबहार वृक्ष है. इसे जीवनदायिनी वृक्ष माना जाता है. यह काफ़ी भिन्नता वाली मिट्टी में उग जाता है. किसी भी प्रकार के पानी में जीवित रहता है. यह बहुत ज़्यादा तापमान को बर्दाश्त कर लेता है. पतझड़ में इसकी पत्तियां झड़ जाती हैं. यह घने झाड़ वाला वृक्ष है. इसकी छाया आराम देती है. इसके फूल सफ़ेद और सुगंधित होते हैं. इसका फल चिकना गोलाकार से अंडाकार होता है, जिसे निंबोली कहते हैं. फल का छिलका पतला, गूदा रेशेदार, सफ़ेद पीले रंग का और स्वाद में कड़वा-मीठा होता है. यह औषधीय गुणों से भरपूर है. यह वातावरण को शुद्ध करता है. अनेक बीमारियों के इलाज में इसका इस्तेमाल होता है. इसके बीज खाद के रूप में प्रयोग किए जाते हैं. इसमें काफ़ी मात्रा में नाइट्रोजन और कीटनाशक तत्व पाए जाते हैं. इसकी लकड़ी मज़बूत होती है. इसका इस्तेमाल मकान, ठेले और फ़र्नीचर बनाने के लिए होता है. घरों में इसे लगाना अच्छा माना जाता है. सड़कों के किनारे छाया के लिए नीम के वृक्ष लगाए जाते हैं.
रोहिड़ा सदाबहार वृक्ष है. इसे रोहिरा, रोही, रोहिटका आदि नामों से भी जाना जाता है. यह रेतीली मिट्टी में उगने वाला वृक्ष है. इसमें सूखा सहन करने की विलक्षण क्षमता होती है. यह कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी उगता है और अपना विकास करता है. इसे रेत के स्थायी टीलों पर सरलता से उगाया जा सकता है, जहां तापमान बहुत कम और बहुत ज़्यादा हो. इसकी जड़ें मिट्टी की ऊपरी सतह पर फैल जाती हैं. इससे मिट्टी का कटाव रुक जाता है.यह हवा के बहाव को भी नियंत्रित करता है. इसकी शाख़ाएं झुकी हुई और तना मुड़ा हुआ होता है. इसे खेतों के बीच भी उगाया जा सकता है. इसकी लकड़ी मज़बूत, सख़्त, सलेटी और पीले रंग की होती है. इसकी लकड़ी से फ़र्नीचर, खेती के औज़ार और खिलौने आदि बनाए जाते हैं. इसकी लकड़ी पर आसानी से नक़्क़ाशी हो जाती है. इसलिए इससे सजावटी सामान भी बनाया जाता है. इसकी शाख़ाएं ईंधन के काम आती हैं. इसमें औषधीय गुण पाए जाते हैं. इससे विभिन्न प्रकार के रोगों की देसी और आयुर्वेदिक औषधियां तैयार की जाती हैं. रोहिड़ा वृक्ष के तने की छाल में निकोटिन नामक पदार्थ पाया जाता है. यह लीवर संबंधी रोगों में विशेष रूप से गुणकारी है. लिव-52 नामक औषधि बनाने के लिए इसी का इस्तेनाल किया जाता है. रोहिड़ा का फूल बहुत ख़ूबसूरत होता है. इस पर सर्दियों के मौसम में फूल आते हैं. इसके फूल पीले, नारंगी और लाल रंग के होते हैं, जो घंटी के समान होते हैं.
पलाश को पलास, परसा, ढाक, टेसू, किंशुक और केसू भी कहा जाता है. इसके फूल बहुत आकर्षक होते हैं. इसके आकर्षक फूलों के कारण इसे ’जंगल की आग’ भी कहा जाता है. प्राचीन काल ही से इसके फूलों से होली के रंग भी बनाए जाते हैं. यह अनुपजाऊ भूमि में भी उग जाते हैं. इसका झाड़ भी बहुत फैलता है. पलाश के पत्ते पत्तल और दोने आदि के बनाने के काम आते हैं. इनके पत्तों से बीड़ियां भी बनाई जाती हैं. फूल और बीज औषधीय गुणों से भरपूर हैं. इसकी छाल से रेशा निकलता है, जिसे जहाज़ के पटरों की दरारों में भरा जाता है, ताकि अंदर पानी न आ सके. जड़ की छाल से निकलने वाले रेशे से रस्सियां बटी जाती हैं. इससे दरी और काग़ज़ भी बनाया जाता है. इसकी पतली डालियों को उबालकर एक प्रकार का कत्था तैयार किया जाता है. मोटी डालियों और तनों को जलाकर कोयला तैयार किया जाता है. इसकी छाल से गोंद निकलता है.
बांस भी बहुत उपयोगी वृक्ष है. इसकी लकड़ी बहुत उपयोगी मानी जाती है और छोटी-छोटी घरेलू वस्तुओं से लेकर मकान बनाने तक के काम आती है.
इसकी लकड़ी से कई तरह का सजावटी सामान बनाया जाता है. इससे काग़ज़ भी बनाया जाता है. बांस की खपच्चियों को तरह-तरह की चटाइयां, कुर्सी, मेज़, चारपाई, मछली पकड़ने का कांटा, डलियां और अन्य कई प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती हैं. प्राचीन काल में बांस की कांटेदार झाड़ियों से क़िलों की रक्षा की जाती थी. इससे कई तरह के बाजे, जैसे बांसुरी और वॉयलिन आदि भे बनाए जाते हैं. दवा में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है. बांस का प्ररोह खाया जाता है. इसका अचार और मुरब्बा भी बनता है. बांस के पेड़ तालाबों और पोखरों के पास लगाए जा सकते हैं. बांस पर सूखे या बारिश का ज़्यादा असर नहीं पड़ता. बांस अन्य वृक्षों के मुक़ाबले 30 फ़ीसद ज़्यादा ऑक्सीजन छोड़ता. यह पीपल के वृक्ष की तरह दिन में कार्बन डाईऑक्साइड खींचता है और रात में ऑक्सीजन छोड़ता है.
महुआ तेज़ी से बढ़ने वाला वृक्ष है. यह हर तरह की ज़मीन में उग जाता है. इसका पेड़ ऊंचा और छतनार होता है और डालियां चारों तरफ़ फैलती हैं. अमूमन यह सालभर हरा-भरा रहता है. यह भी बहु उपयोगी वृक्ष है. इसके बीज, फूल और लकड़ी कई काम आती है. इसका फल परवल के आकार का होता है, जिसे कलेंदी कहते हैं. इसे छीलकर, उबालकर और बीज निकालकर तरकारी भी बनाई जाता है. इसके बीच में एक बीज होता है, जिससे तेल निकलता है. इसके पके फलों का गूदा खाने में मीठा होता है. इसके बीजों से त्वचा की देखभाल की चीज़ें, साबुन और डिटर्जेंट आदि का निर्माण किया जाता है. इसका तेल ईंधन के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है. तेल निकालने के बाद बचे इसके खल का इस्तेमाल पशुओं के खाने और उर्वरक के रूप में किया जाता है. औषधीय गुणों के लिए दवाओं में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है. महुए के फूल में चीनी का अंश होता है, जिसे इंसान ही नहीं बल्कि पशु-पक्षी भी ख़ूब पसंद करते हैं. इसके रस में पूड़ी भी पकाई जाती है. इसे पीसकर आटे में मिलाकर रोटियां बनाई जाती हैं, जिन्हें महुअरी कहा जाता है. हरे और सूखे महुए लोग भूनकर भी खाते हैं. इसे पशुओं को भी खिलाया जाता है. इससे पशुओं का दूध ज़्यादा और गाढ़ा होता है. आदिवासी इसे पवित्र मानते हैं.
जामुन भी उपयोगी वृक्ष है. इसे जामुन, राजमन, काला जामुन, जमाली, ब्लैकबेरी आदि नामों से जाना जाता है. इससे खाने के लिए लज़ीज़ फल तो मिलते ही हैं, साथ ही इसकी पत्तियां और छाल भी औषधियों के तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं. जामुन के फल में ग्लूकोज़ और फ्रक्टोज़ पाए जाते हैं. फल में खनिजों की तादाद ज़्यादा होती है. अन्य फलों के मुक़ाबले यह कम कैलोरी प्रदान करता है. एक मध्यम आकार का जामुन 3-4 कैलोरी देता है. फल के बीज में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और कैल्शियम की अधिकता होती है. यह लौह का बड़ा स्रोत है. प्रति 100 ग्राम में एक से दो मिलीग्राम आयरन होता है. इसमें विटामिन बी, कैरोटिन, मैग्नीशियम और फाइबर होते हैं. जामुन को मधुमेह के बेहतर उपचार के तौर पर जाना जाता है. यकृत यानी लीवर से संबंधित बीमारियों समेत कई रोगों के बचाव में भी जामुन बेहद उपयोगी साबित होता है. जहां बाढ़ ज़्यादा आती हो, वहां इसे लगाना चाहिए. इससे भूमि कटाव रुकता है.
कटहल एक फलदार वृक्ष है. वृक्ष पर लगने वाले फलों में इसका फल दुनिया में सबसे बड़ा होता है. फल के बाहरी सतह पर छोटे-छोटे कांटे होते हैं.
इसकी सब्ज़ी और अचार बनाया जाता है. इसका फल बहुत पौष्टिक माना जाता है. इसकी जड़, छाल और पत्ते औषधि के रूप में काम आता है. कटहल में कई पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं, जैसे विटामिन ए, सी, थाइमिन, पोटैशियम, कैल्शियम, राइबोफ्लेविन, आयरन, नियासिन और जिंक आदि. इसमें फ़ाइबर पाया जाता है. इसमें बिल्कुल भी कैलोरी नहीं होती है.
इमली का वृक्ष ऊंचा और घने झाड़ वाला होता है. इन्हें सड़कों के किनारे भी लगाया जाता है. इससे छाया के साथ-साथ इमली भी मिलती है. इसमें कैरोटीन, विटामिन सी और बी पाया जाता है. इसके फल खट्टे होते हैं. इसलिए खटाई के तौर पर विभिन्न प्रकार के व्यंजनों में इसका इस्तेमाल किया जाता है. इमली की पत्तियों का प्रयोग हर्बल चाय बनाने में किया जाता है. कई तरह की बीमारियों में भी यह कारगर है.
शहतूत एक बहुवर्षीय वृक्ष है. यह 15 सालों तक उच्च गुणवत्ता की पत्तियां देता है. शहतूत में ऐसे कई फ़ायदेमंद गुण पाए जाते हैं, जो कई बीमारियों में वरदान साबित हो सकते हैं. शहतूत में उम्र को रोकने वाला गुण होता है. यह त्वचा को युवा बना देता है और झुर्रियों को चेहरे से ग़ायब कर देता है.
अर्जुन एक औषधीय वृक्ष है. इसे घवल, ककुभ और नदीसर्ज भी कहते हैं, क्योंकि यह नदी नालों के किनारे काफ़ी पाया जाता है. इसकी छाल पेड़ से उतार लेने पर फिर उग आती है. इसके फल कमरख़ों जैसे आकार के होते हैं. इनमें हल्की-सी सुगंध होती है और स्वाद कसैला होता है. इसकी छाल औषधियों में काम आती है. होम्योपैथी में अर्जुन एक प्रचलित औषधि है.
खेजडी को संस्कृत में शमी वृक्ष कहा गया है. शमी का शाब्दिक अर्थ है शमन करने वाला. इसे जांट, जांटी, जंड, समी, सुमरा आदि नामों से जाना जाता है. इसकी सबसे बड़ी ख़ासियत यह है कि ये तेज़ गर्मियों के दिनों में भी हरा-भरा रहता है. इसकी छाया में पशु-पक्षी ही नहीं, इंसान भी आराम पाते हैं. जब खाने को कुछ नहीं होता है, तब यह चारा देता है, जिसे लूंग कहा जाता है. इसका फूल मींझर कहलाता है. इसके फल को सांगरी कहते हैं, जिसकी सब्ज़ी बनाई जाती है. यह फल सूखने पर खोखा कहलाता है, जो सूखा मेवा है. इसकी लकड़ी मज़बूत होती है. इससे फ़र्नीचर बनाया जाता है. इसकी जड़ से हल बनाया जाता है. इसकी लकड़ी ईंधन के रूप में भी इस्तेमाल की जाती है.
अशोक का वृक्ष घना और छायादार हाता है. इसके पत्ते शुरू में तांबे जैसे रंग के होते हैं, इसलिए इसे ताम्र पल्लव भी कहते हैं. इसके नारंगी रंग के फूल बसंत ऋतु में आते हैं, जो बाद में लाल रंग के हो जाते हैं. सुनहरी लाल रंग के फूलों वाला होने से इसे हेमपुष्पा भी कहा जाता है. यह औषधीय वृक्ष है. इसकी छाल में हीमैटाक्सिलिन, टेनिन, केटोस्टेरॉल, ग्लाइकोसाइड, सैपोनिन, कार्बनिक कैल्शियम और लौह के यौगिक पाए गए हैं.
पोपलर एक उपयोगी वृक्ष है. यह 15 से 50 मीटर ऊंचा होता है. यह जल्द बढ़ने वाला वृक्ष है. सर्दी के मौसम में पत्ते न होने की वजह से इसे खाद्यान्न, सब्ज़ियों, मसालों, तिलहनों और दलहन वाली फ़सलों को आसानी से उगाया जा सकता है.यह बाग़ों के किनारे और पानी की नालियों के साथ-साथ लगाए जाते हैं. इसकी लकड़ी प्लाई बनाने के काम आती है. इससे खेल-कूद का सामान भी बनाया जाता है. पोपलर सूर्य उष्णता, हवा के कुम्भालाने वाले प्रभाव से फ़सलों की रक्षा और मिट्टी का कटाव रोकने में भी मदद करता है. उपजाऊ मिट्टी और उच्च जल स्तर वृक्षारोपण को ऊपर उठाने के लिए काफ़ी अनुकूल पाया गया है.
सागौन सालभर हरा-भरा रहने वाला वृक्ष है. यह 80 से 100 फुट ऊंचा होता है. इसका वृक्ष काष्ठीय होता है. इसकी लकड़ी हल्की, मज़बूत और लंबे वक़्त तक चलने वाली होती है. इसके पत्ते काफ़ी बड़े होते हैं. यह बहुमूल्य इमारती लकड़ी देता है. इसकी लकड़ी बहुत कम सिकुड़ती है. इस पर पॉलिश जल्द चढ़ जाती है, जिससे यह बहुत आकर्षक हो जाती है. इसकी लकड़ी जहाज़ों, नावों, बोगियों, खिड़कियों, चौखटों, रेल के डिब्बों और फ़र्नीचर के निर्माण में इस्तेमाल की जाती है.
इनके अलावा सिरस, कचनार, शहतूत और बेरी आदि वृक्ष लगाकर भी कृषि वानिकी को बढ़ावा दिया जा सकता है. ये वृक्ष पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. वृक्षों के पत्तों से चारा मिलता है. कचनार और शहतूत की पत्तियों के चारे में घास के मुक़ाबले ज़्यादा वसा, प्रोटीन, चूना आदि ज़रूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं. गांवों में ऐसे वृक्ष लगाने चाहिए, जिनसे पशुओं के लिए चारा मिल सके. इमारती लकड़ी और ईंधन के रूप में इस्तेमाल होने वाली लकड़ी की बढ़ती ज़रूरतों को कृषि वानिकी से पूरा किया जा सकता है. ऐसे में जंगल भी सुरक्षित रहेंगे. खेतों के आसपास पेड़ लगाने से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले कार्बन डाई ऑक्साइड से छुटकारा पाने में काफी मदद मिलेगी. कृषि वानिकी शोधकर्ताओं ने देश के विभिन्न जलवायु क्षेत्रों के लिए उपयुक्त वृक्षों की पहचान की है, ताकि वे अच्छे से फलफूल सकें. उनका मानना है कि स्थानीय जलवायु के मुताबिक़ अनुकूलित वृक्ष और झाड़ियां कृषि वानिकी के लिए सबसे सुरक्षित हैं. कई पौधों की प्रजातियां जैव विविधता की रक्षा करने, मृदा स्वास्थ्य में सुधार, लकड़ी और ईंधन लकड़ी मुहैया कराने, कार्बन डाई ऑक्साइड को कम करने आदि फ़ायदों को ध्यान में रखकर तय की गई हैं.
देश में प्रति हेक्टेयर औसत लकड़ी का उत्पादन विश्च के औसत से कम है. लकड़ी की मांग आपूर्ति से बहुत ज़्यादा है. इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए सालाना 400 करोड़ रुपए की लकड़ी बाहर से मंगवानी पड़ती है. देश की खाद्यान्नों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ज़मीन पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है. इसकी वजह से भूमि के पोषक तत्व कम हो रहे हैं. मिट्टी के जल भंडारण की क्षमता भी कम हो रही है और भू-जल स्तर में भी गिरावट आ रही है. एक किलो धान पैदा करने के लिए 5000 लीटर पानी की ज़रूरत होती है. इसी तरह एक किलो गेहूं पैदा करने के लिए 1500 लीटर पानी का इस्तेमाल होता है, जबकि एक किलो लकड़ी पैदा करने में 500 लीटर पानी ख़र्च होता है. घटते वन क्षेत्र को बढ़ाने और लकड़ी की मांग को पूरा करने के लिए कृषि वानिकी को अपनाना चाहिए. कृषि वानिकी के ज़रिये एक ही भूखंड पर एक साथ कई तरह की उपयोगी चीज़ें हासिल की जा सकती हैं, जैसे खाद्यान्न, फल-फूल, सब्ज़ियां, दूध, शहद, ईंधन, रेशा, चारा और खाद आदि. भूमि में नमी बनाकर रखी जा सकती है. भूमि कटाव को रोका जा सकता है. वृक्ष रेगिस्तान के बढ़ाव को रोकते हैं. हर साल रेगिस्तान का क्षेत्रफल बढ़ रहा है. रेगिस्तान में वृक्ष लगा देने से वे वहीं रुक जाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते.
बेरोज़गार युवकों को कृषि वानिकी की मुहिम में शामिल करके जहां उन्हें रोज़गार मुहैया कराया जा सकता है, वहीं इससे पर्यावरण भी स्वच्छ बनेगा. प्रशिक्षण शिविर लगाकर युवाओं को इसके बारे में जानकारी दी जा सकती है. इसके लिए ग्रामीणों ख़ासकर किसानों और पशु पालकों को भी जागरूक किया जाना चाहिए. दरअसल कृषि वानिकी आज के वक़्त की बहुत बड़ी ज़रूरत है. इसके ज़रिये जहां पर्यावरण को स्वच्छ रखा जा सकत है, वहीं वृक्षों से लाभ भी अर्जित किया जा सकता है.