फ़िरदौस ख़ान
भारत एक कृषि प्रधान देश है. इसलिए प्राचीनकाल से ही यहां तालाबों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है. तालाब उपयोगी होने के साथ-साथ भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग भी रहे हैं. भारत में जल देवता को पूज्य मानते हुए तालाबों की पूजा-अर्चना की जाती रही है. आज भी गांव-देहात में मंगल कार्यों के मौक़ों पर महिलाएं इकट्ठी होकर तालाबों को पूजती हैं. पुराने ज़माने में जहां लोग प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग करते हुए उनका संरक्षण भी किया करते थे, वहीं आज के दौर में इन्हीं प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग करके विनाशकारी माहौल पैदा किया जा रहा है. प्राकृतिक संसाधनों के अति दोहन की वजह से ही आज जल, जंगल और ज़मीन पर ख़तरे के बादल छाये हुए हैं. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी प्राकृतिक संसाधनों की उपयोगिता को जानते और समझते थे, तभी उन्होंने कहा था कि क़ुदरत सभी की ज़रूरतों को पूरा कर सकती है, लेकिन एक व्यक्ति का भी लालच पूरा नहीं कर सकती. लेकिन आज व्यक्ति के लालच की वजह से कहीं सूखे, तो कहीं बाढ़ के हालात बन गए हैं.
राजकमल प्रकाशन द्वारा प्रकाशित पुस्तक मेवात का जोहड़ में मेवात के जोह़डों पर रौशनी डाली गई है. इसके साथ ही मेवात में आज़ादी के आंदोलन और विभाजन, मेवात को लेकर महात्मा गांधी के सपने, मेवात में रचनात्मकता को चुनौतियों और मेवात के इतिहास के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है.
हरियाणा के फिरोजपुर झिरका, नूंह, पलवल, सोता, फ़रीदाबाद, गुड़गांव, राजस्थान के रामगढ़, किशनगढ़, खैरपल, तिजारा, कुम्हेर, डीग, पहा़डी और उत्तर प्रदेश के आगरा और मथुरा के यमुना तट के हिस्से को मेवात इलाक़ा कहा जाता है. बक़ौल लेखक राजेन्द्र सिंह, महात्मा गांधी का मेवात में जोहड़ पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा अपने जीते जी मेवात के लिए किए गए समर्पण की दास्तान है. महात्मा गांधी ने मेवात को बचाने-बसाने के लिए 19 दिसंबर, 1947 को सोहना (हरियाणा) और नोगांवा (राजस्थान) के बीच घासेडा गांव में जाकर राजस्थान के अलवर-भरतपुर से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़-मथुरा-आगरा बाग़पत से आए और हरियाणा के मेवों की सभा में जाकर उन्हें यहीं बसे रहने को कहा. जब ये लोग अच्छे से अपनी जगह बसे रहे तो पाकिस्तान गए बहुत से मेव वापस आकर मेवात में बसे. उन्होंने अपनी पुरानी धरती मेवात में वापस जाने की मांग की. बापू के विश्वास से उजड़ता मेवात बच गया. जो उजड़े थे, वे वापस आकर बस गए. यह मेवों का मेवात बन गया. भारत की राजधानी ख़ासकर राष्ट्रपति भवन मेवों के गांव उजाड़ कर अंग्रेजों ने बनाया था. जिन्हें आज मेव कहते हैं, वे मीणा, राजपूत, गुर्जर, अहीर, त्यागी, जाट थे, जो धर्म परिवर्तन कर मुसलमान बन गए थे. ये अरावली पहाड़ियों की कंदराओं, चोटियों पर छुपकर रहना पसंद करते थे. पहाड़ियों में अपने घर बनाकर रहते थे. झोपड़ी को चारों तरफ़ से घेरकर पेड़ों के झुरमुट में रहना इन्हें पसंद था. इनका जीवन जंगल, जंगली जानवरों के शिकार पर चलता था.
इसलिए अरावली पर्वत मालाओं में इनके लिए अनुकूल थीं. मेवाती में इसे काला पहाड़ कहते हैं. इस पहाड़ी क्षेत्र के बहुत से गांव जोहड़ से पानीदार बने हुए थे. जोहड़ ही इनका सबकुछ है.
हमारे पूर्वज जानते थे कि तालाबों से जंगल और ज़मीन का पोषण होता है. भूमि के कटाव एवं नदियों के तल में मिट्टी के जमाव को रोकने में भी तालाब मददगार होते हैं. इसलिए वे वर्षा के जल को उसी स्थान पर रोक लेते थे. उनकी जल के प्रति एक विशेष प्रकार की चेतना और उपयोग करने की समझ थी. इस चेतना के कारण ही गांव के संगठन की सूझबूझ से गांव के सारे पानी को विधिवत उपयोग में लेने के लिए तालाब नाए जाते थे. इन तालाबों से अकाल के समय भी पानी मिल जाता था. इनके निर्माण, रखरखाव, मरम्मत आदि के कामों से गांव के संगठन को मज़बूत बनाने में मदद मिलती थी. मेवात आज भी तालाबों को खरा मानता है. उन्हें बनाता-संभालता है. उनके घरेलू सभी काम तालाब से पूरे होते हैं, और सभी ग्रामवासी मिलकर मेहनत करके जोहड़ बनाते थे.
तालाबों के रखरखाव के लिए गांव के लोग सर्वसम्मति से कुछ नियम भी बनाते थे, जिसे गंवई दस्तूर कहा जाता था. ये दस्तूर गंवई बही में भी लिखे जाते थे या मौखिक परंपरा के ज़रिये पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलते जाते थे. गांव में आने वाले बाहरी व्यक्ति को भी इन गंवई दस्तूर का पालन करना प़डता था. अलवर ज़िले के गांवों के गंवई दस्तूर के मुताबिक़, तालाब की आगोर में कोई जूता लेकर प्रवेश नहीं करता था. शौचादि के हाथ अलग से पानी लेकर आगोर के बाहर ही धोये जाते थे. आगोर में किसी गांव सभा की अनुमति के बिना मिट्टी खोदना मना होता था. हर साल जेष्ठ माह में पूरा गांव ही मिलका आगोर से मिट्टी निकालता था. आगोर से ही नहीं, बल्कि तालाब के जलग्रहण क्षेत्र तक में शौचादि के लिए जाना मना था. किसी प्रकार गंदगी फैलाने वाले को तालाब की स़फाई करके प्रायश्चित करने का सुझाव दिया जाता था. प्रायश्चित के लिए तालाब की पाल पर पे़ड लगाने तथा उसके ब़डा होने तक उसकी देखभाल करने की परंपरा थी. तालाब के जलग्रहण क्षेत्र से मिट्टी कटकर नहीं आए और तालाब में जमा नहीं हो, इसकी व्यवस्था तालाब बनाते समय ही कर दी जाती थी. इससे लंबे समय तक तालाब उथले नहीं हो पाते थे. जब तालाब की मरम्मत करने की ज़रूरत होती थी, पूरा गांव मिल-बैठकर, तय करके इस काम को करता था. तालाब से निकलने वाली मिट्टी खेतों में डालने या कुम्हारों के काम आती थी. तालाब को गांव की सार्वजनिक संपत्ति माना जाता था. गांव के लोग जब किसी दूसरे गांव को जाते थे, तो सबसे पहले वह तालाब को अपने गांव की संपत्ति में गिनाया करते थे. गांव का जैसा तालाब होता था, वैसा ही उस गांव को माना जाता था. गांव का तालाब अच्छा है तो उस गांव को समृद्ध, संगठित, शक्तिशाली माना जाता था. यह भी कि वह गांव अपने महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम है, यह मान लिया जाता था. यह परंपरा 1860 तक चली. इसके बाद अंग्रेजों ने इन परंपराओं को ख़त्म करने के लिए कई योजनाएं बनाईं. अंग्रेजों की नीतियों ने रंग दिखाना शुरू किया और ग्राम समाज के टूट जाने के कारण तालाबों का निर्माण, रखरखाव और मरम्मत बंद हो गई. तालाबों के साथ-साथ गांव के संगठन भी बिखरने लगे. इसके बावजूद आज भी मेवात का सामुदायिक संगठन देश के दूसरे हिस्सों से इस मामले में काफ़ी अच्छा है.
बड़े बांध बनाने पर भारत सरकार 2008 तक अरबों-खरबों रुपये ख़र्च कर चुकी है. इन योजनाओं से दो करोड़ हैक्टेयर ज़मीन सिंचित होने का सरकारी दावा किया गया था, लेकिन हक़ीक़त में आज कितनी ज़मीन की सिंचाई ये योजनाएं कर रही हैं, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता. देश में तालाबों की उपेक्षा करने की भूल आज भी की जा रही है. 1950 में देश के कुल सिंचित क्षेत्र की 17 फ़ीसद सिंचाई तालाबों से की जाती थी. तालाबों में पाए गए शिलालेख इसका प्रमाण हैं. पिछले बरसों के भयंकर अकाल ने एक फिर तालाबों की याद दिलाई है. इसलिए गत वर्षों में छोटे-बड़े दस हज़ार से ज़्यादा तालाब, जोहड़, बांध बनाए गए या उनकी मरम्मत कराई गई है. इन पर तक़रीबन 15 करोड़ रुपये ख़र्च हुए. मिसाल के तौर पर गोपालपुर गांव को ही लें, जहां 1986 में सिंचाई और पीने के पानी वाले कुएं सूख गए थे. ज़मीन में कुछ पैदा ही नहीं हो रहा था. तभी इस गांव के तालाबों के निर्माण का काम शुरू किया गया और 1987 के जून तक तीन बड़े तालाब बनाए गए. गांव वाले इन्हें बांध कहते हैं. इनके निर्माण कार्य में दस हज़ार रुपये की क़ीमत का गेहूं दिया गया. जुलाई 1987 में इस इलाक़े में कुल 13 सेंटीमीटर वर्षा हुई. यह सारी वर्षा एक साथ ही 48 घंटे के अंदर हो चुकी थी. इनके पानी से ज़मीन पुन: सजल हुई और गांव के आसपास के 20 कुओं का जलस्तर बढ़कर ऊपर आ गया. वर्षा का पानी अपने साथ जंगल और पहाड़ियों से पत्ते आदि बहाकर ले आया था, जो तालाबों की तली में बैठ गया. बड़े तालाब खेतों की ज़मीन पर बने हुए थे. इसलिए नवंबर तक तालाबों का पानी तो नीचे की ज़मीन की सिंचाई करने के काम में ले लिया गया और तालाब के पेटे में गेहूं की फ़सल बो दी गई. एक फ़सल में केवल इन तालाबों की ज़मीन से ही तीन सौ क्विंटल अनाज पैदा हुआ, जिसकी क़ीमत तक़रीबन पौन लाख होती है. इसके अलावा तालाब में पूरे साल पानी भरा रहा. इसे पशुओं के पीने के काम में लिया गया और तालाब के चारों तरफ़ उगी घास पशुओं के चारे के रूप में इस्तेमाल की गई. इसके साथ ही वातावरण भी हराभरा रहा.
हमारे देश में ऐसी अनगिनत मिसालें मिल जाएंगी, जब लोगों ने ख़ुद पहल करते इस तरह के बेहतरीन कामों को अंजाम दिया है. बहरहाल, यह किताब मेवात के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मुहैया कराती है. चूंकि किताब के लेखक राजेन्द्र सिंह अपने विद्यार्थी जीवन से ही संपूर्ण क्रांति आंदोलन से जुड़े रहे हैं और आजकल गंगा नदी की अविरलता और निर्मलता के लिए संघर्षरत हैं. उन्होंने जल संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है. फ़िलहाल वह भारत सरकार के नदी जोड़ योजना के पर्यावरण विशेषज्ञ समिति एवं योजना आयोग के अंतर मंत्रालय समूह और राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण के सदस्य हैं. इस किताब में उनके कार्यों की झलक भी साफ़ दिखाई पड़ती है. यह कहना ग़लत न होगा कि यह किताब जल संरक्षण के प्रति पाठकों को जागरूक करती नज़र आती है.
समीक्ष्य कृति : मेवात का जोहड़
लेखक : राजेन्द्र सिंह
प्रकाशक : राजकमल प्रकाशन
क़ीमत : 400 रुपये





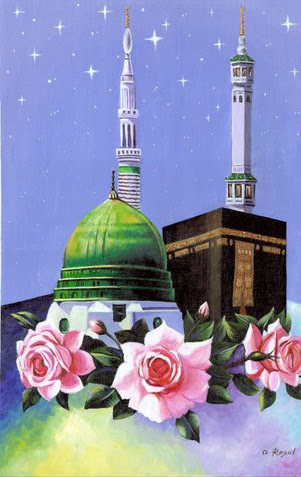

















.jpg)



