फ़िरदौस ख़ान
देश में बढ़ती आबादी की वजह से कृषि भूमि लगातार कम हो रही है. ऐसे में जहां खाद्यान्न संकट का ख़तरा पैदा हो गया है, वहीं खेत छोटे होने से किसानों की आमदनी भी कम हुई है. ज़मीन और पानी के साधन सीमित हैं. कृषि भूमि भी बंजर होने लगी है. पानी का जल स्तर भी लगातार नीचे जा रहा है. इसलिए आबादी को अपनी ज़रूरतें सीमित साधनों से ही पूरी करनी होंगी. उसके लिए उपलब्ध ज़मीन, पानी और तकनीकों का ज़्यादा से ज़्यादा समुचित इस्तेमाल करना होगा. मौजूदा खाद्यान्न की ज़रूरत को देखते हुए देश में दूसरी हरित क्रांति पर ख़ासा ज़ोर दिया जा रहा है. देश की खाद्यान्न उत्पादकता को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने साल 2010-11 से सात पूर्वी राज्यों असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, उत्तर प्रदेश (पूर्वी) और पश्चिम बंगाल में राष्टीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के तहत एक कार्यक्रम शुरू किया. इसे ‘पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाना’ नाम दिया गया. इसका मक़सद विभिन्न कृषि जलवायु उप-क्षेत्रों की प्रमुख बाधाओं का समाधान करते हुए चावल उत्पादन को बढ़ाना है. यह कार्यक्रम 105 ज़िलों में शुरू किया गया. चावल की पैदावार के लिए 96 और गेहूं के लिए 29 ज़िले चुने गए. इनमें असम के 13 ज़िले, बिहार के 23, छत्तीसगढ़ के 8, झारखंड के 17, ओडिशा के 15, पूर्वी उत्तर प्रदेश के 13 और पश्चिम बंगाल के 16 ज़िले शामिल हैं. दूसरी हरित क्रांति लाने का कार्यक्रम कामयाब रहा और पूर्वी भारत में 2011-12 के ख़रीफ़ मौसम में 70 लाख टन ज़्यादा धान का उत्पादन हुआ, जो देश के कुल धान उत्पादन के आधे से भी ज़्यादा था. इस कार्यक्रम की बदौलत इस इलाक़े में धान और गेहूं की पैदावार के अच्छे नतीजे सामने आए हैं.
कृषि मंत्रालय के कृषि एवं सहकारिता विभाग के मुताबिक़ खाद्यान्न की बढ़ती हुई ज़रूरत को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) अगस्त 2007 में शुरू की गई थी. इसका मक़सद राज्यों को कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना है. ऐसा करते वक़्त उन्हें कृषिगत जलवायु परिस्थितियों, प्राकृतिक संसाधन मामलों और प्रौद्योगिकी को ध्यान में रखना होता है और पशुधन, मुर्ग़ी पालन और मत्स्य पालन को पूर्णता समन्वित करना होता है. इसमें योजनाओं के आयोजन और कार्यान्वयन में राज्यों को अधिक लचीलापन और स्वायत्ता दी जाती है. यह कृषि क्षेत्र में राज्यों का निवेश बढ़ाने का प्रमुख उपाय बन गया है. इसमें अब जिंस विशेष के कई उपाय जैसे भारत के पूर्वी क्षेत्र में हरित क्रांति लाना, तिलहन और दलहन के लिए विशेष पहल, चारा उत्पादन को बढ़ाना, सब्ज़ियां पैदा करने के समूह तैयार करना, पौष्टिक अनाज, ऑयल पाम विकास, प्रोटीन पूरक, वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम और ज़ाफ़रानी मिशन शामिल है. इसके अलावा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफ़एसएम) का मक़सद चावल, गेहूं और दालों का क्रमश: 10, 8 और 2 मिलियन टन अतिरिक्त उत्पादन करना है. राष्ट्रीय बाग़वानी मिशन (एनएचएम) का लक्ष्य सभी हितधारकों की सक्रिय भागीदारी से सामूहिक दृष्टिकोण के ज़रिये अग्र और मंद संयोजन सुनिश्चित करके बाग़वानी क्षेत्र का संपूर्ण विकास करना है. इससे बाग़वानी क्षेत्र का बड़े पैमाने पर कायाकल्प हुआ है. उत्तर-पूर्वी और हिमालयायी राज्यों के लिए बाग़वानी मिशन ने बाग़वानी के विभिन्न उत्पादों के उत्पादन में अच्छी ख़ासी बढ़ोतरी हुई है. इसके लिए एफ़एसी गठित किए गए, किसानों से फ़ीडबैक लिया गया और किसानों के ज्ञानवर्धन के लिए यात्राओं का आयोजन आदि करके राज्य विस्तार कार्यक्रमों को समर्थन दिया गया. इस योजना के अधीन देश में 28 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के 604 ग्रामीण ज़िलों में जिला स्तरीय कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसियां गठित की गई हैं.
दूरदर्शन और आकाशवाणी किसानों को कृषि संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने में उल्लेखनीय योगदान कर रहे हैं. इसके अलावा यह मंच विभिन्न योजनाओं के अधीन उपलब्ध सहायता के बारे में जानकारी पैदा करने के लिए प्रचार अभियानों की भी सुविधा देता है. इसके अलावा कृषि क्लीनिक, कृषि व्यापार केंद्र और किसान कॉल केंद्र अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम है. ये किसानों को अदायगी आधार पर विस्तार सेवाएं करा रहे हैं. इसके लिए वे आर्थिक रूप से किफ़ायती स्व-रोज़गार कार्य चलाते हैं और देशव्यापी 11 अंकों वाली एक टोल फ़्री संख्या 1800-180-1551 के ज़रिये किसानों को कृषि संबंधी जानकारी उपलब्ध कराते हैं. इन किसान कॉल केंद्रों में आधुनिक तकनीकों को इस्तेमाल में लाया गया है. इन केंद्रों से लाभ उठाने वाले किसानों की तादाद दिनोदिन बढ़ रही है. कृषि के विकास के बारे में किसानों को जानकारी देने के लिए पूर्वोत्तर सहित देश के पांच ज़ोनों में डीएसी की सहायता से राज्य कृषि विश्वविद्यालय/आईसीएआर संस्थान प्रदर्शनियां और मेले आयोजित करते हैं. विस्तार निदेशालय की सहायता के लिए केंद्रीय संस्थाओं के समर्थन की एक योजना है. इसके तहत कृषि संबंधी सभी गतिविधियों को एक राष्ट्रीय संस्था और 4 विस्तार शिक्षा संस्थानों द्वारा चलाया जा रहा है. सरकार के ये कार्यक्रम अनाज, दलहन, तिलहन, फलों, सब्ज़ियों और मसालों का रिकॉर्ड उत्पादन प्राप्त करने में काफ़ी मददगार साबित हुए हैं. भूमि के विस्तार की सीमाओं, बढ़ती जनसंख्या और खेतीहर ज़मीन की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में गिरावट को देखते हुए उत्पादन में दीर्घकालिक विकास का मुख्य स्रोत विभिन्न निवेशों का सही इस्तेमाल करना है.
ग़ौरतलब है कि देश में हरित क्रांति की शुरुआत साल 1966-67 में हुई थी. इसकी शुरुआत दो चरणों में की गई थी, पहला चरण 1966-67 से 1980-81 और दूसरा चरण 1980-81 से 1996-97 रहा. हरित क्रांति से अभिप्राय देश के सिंचित और असिंचित कृषि क्षेत्रों में ज़्यादा उपज वाले संकर और बौने बीजों के इस्तेमाल के ज़रिये तेज़ी से कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी करना है. हरित क्रांति की विशेषताओं में अधिक उपज देने वाली क़िस्में, उन्नत बीज, रासायनिक खाद, गहन कृषि ज़िला कार्यक्रम, लघु सिंचाई, कृषि शिक्षा, पौध संरक्षण, फसल चक्र, भू-संरक्षण और ऋण आदि के लिए किसानों को बैंकों की सुविधाएं मुहैया कराना शामिल है. रबी, ख़रीफ़ और जायद की फ़सलों पर हरित क्रांति का अच्छा असर देखने को मिला. किसानों को थोड़े पैसे ज़्यादा ख़र्च करने के बाद अच्छी आमदनी हासिल होने लगी. हरित क्रांति की वजह से हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के खेत सोना उगलने लगे. साठ के दशक में हरियाणा और पंजाब में गेहूं के उत्पादन में 40 से 50 फ़ीसद तक बढ़ोतरी दर्ज की गई. जिस वक़्त हरित क्रांति का नारा बुलंद हुआ उस वक़्त देश भुखमरी के दौर से गुज़र रहा था और देश को अनाज की सख़्त ज़रूरत थी. इसलिए सभी का ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा अनाज पैदा करने में था, लेकिन जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता गया रासायनिक उर्वरकों और अत्यधिक विषैले कीटनाशकों के अंधाधुंध इस्तेमाल की वजह से सोना उगलने वाली धरती बंजर होने लगी. उपजाऊ शक्ति के लगातार ह्रास से भूमि के बंजर होने की समस्या ने किसानों के सामने एक नई चुनौती पैदा कर दी है. सूखा, बाढ, लवणीयता, कीटनाशकों के अंधाधुंध इस्तेमाल और अत्यधिक दोहन के कारण भू-जल स्तर में लगातार गिरावट आने से उपजाऊ भूमि बंजर हो रही है. एक रिपोर्ट के मुताबिक़ 90 के दशक तक मिट्टी की उपजाऊ शक्ति सही थी, लेकिन उसके बाद मिट्टी से जिंक, आयरन और मैगनीज़ जैसे पोषक तत्वों की कमी होने लगी. राज्य के दस ज़िलों की मिट्टी का पीएच लेवल सामान्य स्तर पर नहीं है.
आज़ादी के बाद सिंचाई के परंपरागत तरीक़ों की बजाय आधुनिक सिंचाई प्रणालियों को अपनाया गया, जिससे भूमि की उत्पादकता में कमी आई है. भूमि के बंजर होने व अन्य कारणों से प्रति व्यक्ति कृषि भूमि क्षेत्र में कमी हो रही है. लेकिन सवाल यह है कि जब सोना उगलने वाली धरती ही बंजर हो जाएगी, तो अनाज कैसे पैदा होगा. इसलिए भूमि की उर्वरक शक्ति को बचाए रखना बेहद ज़रूरी है, वरना कृषि के विकास की तमाम योजनाएं धरी रह जाएंगी. पहली हरित क्रांति की बुनियाद गेहूं और चावल का ज़्यादा उत्पादन था और इसके लिए अच्छी क़िस्में और रासायनिक खाद और कीटनाशकों का जमकर इस्तेमाल किया गया. उसके नतीजे भी देख लिए. दूसरी हरित क्रांति में अनाज गेहूं, चावल, मक्का के साथ दलहनी, तिलहनी और गन्ना जैसी फ़सलों की अच्छी क़िस्मों पर ध्यान देना होगा. साथ ही इस बात का भे ख़्याल रखना होगा कि रासायनिक खादों और कीटनाशकों का समुचित इस्तेमाल किया जाए. मुख्य फ़सलों में अच्छी गुणवत्ता और ज़्यादा उत्पादन वाली क़िस्मों के विकास के लिए पारंपरिक तकनीकों के साथ-साथ जैव प्रौद्योगिकी का भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करना होगा. जैविक कृषि को बढ़ावा देना होगा. हालांकि भारत में जैविक खेती योग्य क्षेत्र पिछले एक दशक में तक़रीबन 17 गुना बढ़ गया है. यह क्षेत्र साल 2003-04 में 42 हज़ार हेक्टेयर था, जो साल 2013-14 में बढ़कर 7.23 लाख हेहेक्टेयर हो गया. केन्द्र सरकार ने साल 2001 में जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीओपी) लागू किया. इस हेक्टेयर कार्यक्रम में प्रमाणन एजेंसियों के लिए मान्यता कार्यक्रम, जैव उत्पादन के मानक, जैविक खेती को बढ़ावा देना इत्यादि शामिल हैं. कई राज्यों जैसे उत्तराखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, केरल, नागालैंड, मिज़ोरम और सिक्किम जैविक खेती को बढ़ावा देते रहे हैं.
ग़ौरतलब है कि जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए नाबार्ड योजना चला रही है. इसके तहत वाणिज्यिक जैव खाद उत्पादन इकाई की स्थापना के लिए 20 लाख रुपये तक की राशि 25 फ़ीसद सब्सिडी पर दी जाती है. इसके अलावा वर्मी कल्चर हैचरी यूनिट के लिए डेढ़ लाख रुपये और ख़राब हुए फल-सब्ज़ियों व कूड़े-कर्कट से खाद बनाने की इकाई के लिए 40 लाख रुपये तक का क़र्ज़ विभिन्न बैंकों के ज़रिये दिया जाता है. इस पर भी 25 फ़ीसद सब्सिडी है. सरकारी स्तर पर समय-समय पर प्रशिक्षण शिविर लगाकर किसानों को जैविक खेती के बारे में ज़रूरी जानकारी दी जाती है. शिविर में जहां एक तरफ़ मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने के देसी तरीक़ों के बारे में जानकारी दी जाती है, वहीं बीज पड़ताल, उपचार, कीट और खरपतवार नियंत्रण आदि मुद्दों पर चर्चा होती है. जैविक खेती कर रहे किसानों ने अन्य किसानों के साथ अपने अनुभव भी साझा करते हैं. कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि जैविक उत्पाद और रासायनिक उत्पाद की गुणवत्ता में काफ़ी फ़र्क़ होता है. सही तरीक़े से तैयार गोबर की खाद प्रचलित कुरडी की खाद से हल्की होती है. किसान के लिए इससे आसान और सस्ता उत्पादन बढ़ाने का कोई और तरीक़ा नहीं हो सकता है. बशर्ते किसान गोबर की खाद बनाने के अपने तरीक़े में सुधार करें.
कृषि मंत्रालय का कृषि और सहकारिता विभाग (डीएसी), खेतिहर किसानों के लाभ के लिए नित नये कार्यक्रम तैयार करके देश में कृषि क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने की दिशा में सक्रिय भूमिका निभा रहा है. किसानों कृषि की अत्याधुनिक तकनीकों के साथ पारंपरिक विधियों को अपनाकर जहां कृषि लागत को कम किया, वहीं बाग़वानी, कृषि वानिकी, मछली पालन, मधुमक्खी पालन और पशुपालन को अपनाकर एक-दूसरे के ज़रिये लाभ को बढ़ाया. साथ ही डीप इरीगेशन, ऑर्गेनिक फ़ार्मिंग, रोग व कीट नियंत्रण, मृदा संरक्षण, उन्नत कृषि, फ़सल चक्र, ज़ीरो टिलेज, कार्बनिक खाद, उन्नत बीजों का इस्तेमाल, कृषि यंत्रों का बेहतर उपयोग कर उन्होंने सराहनीय कृषि प्रदर्शन किया है. किसानों में खेतीबाड़ी की नित नई तकनीकों के प्रति जागरूकता बढ़ रही है.
बहरहाल, पुरानी बातों से सबक़ लेते हुए कृषि की अत्याधुनिक तकनीकों के साथ फ़ायदेमंद पारंपरिक विधियों के इस्तेमाल से दूसरी हरित क्रांति के सपने को साकार किया जा सकता है. भारत में जैविक संसाधन प्रचुर मात्रा में मौजूद हैं. विभिन्न फ़सलों में जैविक उत्पादन की तकनीक विकसित करके ज़्यादा उपज ली जा सकती है. इससे जहां खाद्यान्न का संकट हल होगा, वहीं किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी.
देश में बढ़ती आबादी की वजह से कृषि भूमि लगातार कम हो रही है. ऐसे में जहां खाद्यान्न संकट का ख़तरा पैदा हो गया है, वहीं खेत छोटे होने से किसानों की आमदनी भी कम हुई है. ज़मीन और पानी के साधन सीमित हैं. कृषि भूमि भी बंजर होने लगी है. पानी का जल स्तर भी लगातार नीचे जा रहा है. इसलिए आबादी को अपनी ज़रूरतें सीमित साधनों से ही पूरी करनी होंगी. उसके लिए उपलब्ध ज़मीन, पानी और तकनीकों का ज़्यादा से ज़्यादा समुचित इस्तेमाल करना होगा. मौजूदा खाद्यान्न की ज़रूरत को देखते हुए देश में दूसरी हरित क्रांति पर ख़ासा ज़ोर दिया जा रहा है. देश की खाद्यान्न उत्पादकता को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने साल 2010-11 से सात पूर्वी राज्यों असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, उत्तर प्रदेश (पूर्वी) और पश्चिम बंगाल में राष्टीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के तहत एक कार्यक्रम शुरू किया. इसे ‘पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाना’ नाम दिया गया. इसका मक़सद विभिन्न कृषि जलवायु उप-क्षेत्रों की प्रमुख बाधाओं का समाधान करते हुए चावल उत्पादन को बढ़ाना है. यह कार्यक्रम 105 ज़िलों में शुरू किया गया. चावल की पैदावार के लिए 96 और गेहूं के लिए 29 ज़िले चुने गए. इनमें असम के 13 ज़िले, बिहार के 23, छत्तीसगढ़ के 8, झारखंड के 17, ओडिशा के 15, पूर्वी उत्तर प्रदेश के 13 और पश्चिम बंगाल के 16 ज़िले शामिल हैं. दूसरी हरित क्रांति लाने का कार्यक्रम कामयाब रहा और पूर्वी भारत में 2011-12 के ख़रीफ़ मौसम में 70 लाख टन ज़्यादा धान का उत्पादन हुआ, जो देश के कुल धान उत्पादन के आधे से भी ज़्यादा था. इस कार्यक्रम की बदौलत इस इलाक़े में धान और गेहूं की पैदावार के अच्छे नतीजे सामने आए हैं.
कृषि मंत्रालय के कृषि एवं सहकारिता विभाग के मुताबिक़ खाद्यान्न की बढ़ती हुई ज़रूरत को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) अगस्त 2007 में शुरू की गई थी. इसका मक़सद राज्यों को कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना है. ऐसा करते वक़्त उन्हें कृषिगत जलवायु परिस्थितियों, प्राकृतिक संसाधन मामलों और प्रौद्योगिकी को ध्यान में रखना होता है और पशुधन, मुर्ग़ी पालन और मत्स्य पालन को पूर्णता समन्वित करना होता है. इसमें योजनाओं के आयोजन और कार्यान्वयन में राज्यों को अधिक लचीलापन और स्वायत्ता दी जाती है. यह कृषि क्षेत्र में राज्यों का निवेश बढ़ाने का प्रमुख उपाय बन गया है. इसमें अब जिंस विशेष के कई उपाय जैसे भारत के पूर्वी क्षेत्र में हरित क्रांति लाना, तिलहन और दलहन के लिए विशेष पहल, चारा उत्पादन को बढ़ाना, सब्ज़ियां पैदा करने के समूह तैयार करना, पौष्टिक अनाज, ऑयल पाम विकास, प्रोटीन पूरक, वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम और ज़ाफ़रानी मिशन शामिल है. इसके अलावा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफ़एसएम) का मक़सद चावल, गेहूं और दालों का क्रमश: 10, 8 और 2 मिलियन टन अतिरिक्त उत्पादन करना है. राष्ट्रीय बाग़वानी मिशन (एनएचएम) का लक्ष्य सभी हितधारकों की सक्रिय भागीदारी से सामूहिक दृष्टिकोण के ज़रिये अग्र और मंद संयोजन सुनिश्चित करके बाग़वानी क्षेत्र का संपूर्ण विकास करना है. इससे बाग़वानी क्षेत्र का बड़े पैमाने पर कायाकल्प हुआ है. उत्तर-पूर्वी और हिमालयायी राज्यों के लिए बाग़वानी मिशन ने बाग़वानी के विभिन्न उत्पादों के उत्पादन में अच्छी ख़ासी बढ़ोतरी हुई है. इसके लिए एफ़एसी गठित किए गए, किसानों से फ़ीडबैक लिया गया और किसानों के ज्ञानवर्धन के लिए यात्राओं का आयोजन आदि करके राज्य विस्तार कार्यक्रमों को समर्थन दिया गया. इस योजना के अधीन देश में 28 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के 604 ग्रामीण ज़िलों में जिला स्तरीय कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसियां गठित की गई हैं.
दूरदर्शन और आकाशवाणी किसानों को कृषि संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने में उल्लेखनीय योगदान कर रहे हैं. इसके अलावा यह मंच विभिन्न योजनाओं के अधीन उपलब्ध सहायता के बारे में जानकारी पैदा करने के लिए प्रचार अभियानों की भी सुविधा देता है. इसके अलावा कृषि क्लीनिक, कृषि व्यापार केंद्र और किसान कॉल केंद्र अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम है. ये किसानों को अदायगी आधार पर विस्तार सेवाएं करा रहे हैं. इसके लिए वे आर्थिक रूप से किफ़ायती स्व-रोज़गार कार्य चलाते हैं और देशव्यापी 11 अंकों वाली एक टोल फ़्री संख्या 1800-180-1551 के ज़रिये किसानों को कृषि संबंधी जानकारी उपलब्ध कराते हैं. इन किसान कॉल केंद्रों में आधुनिक तकनीकों को इस्तेमाल में लाया गया है. इन केंद्रों से लाभ उठाने वाले किसानों की तादाद दिनोदिन बढ़ रही है. कृषि के विकास के बारे में किसानों को जानकारी देने के लिए पूर्वोत्तर सहित देश के पांच ज़ोनों में डीएसी की सहायता से राज्य कृषि विश्वविद्यालय/आईसीएआर संस्थान प्रदर्शनियां और मेले आयोजित करते हैं. विस्तार निदेशालय की सहायता के लिए केंद्रीय संस्थाओं के समर्थन की एक योजना है. इसके तहत कृषि संबंधी सभी गतिविधियों को एक राष्ट्रीय संस्था और 4 विस्तार शिक्षा संस्थानों द्वारा चलाया जा रहा है. सरकार के ये कार्यक्रम अनाज, दलहन, तिलहन, फलों, सब्ज़ियों और मसालों का रिकॉर्ड उत्पादन प्राप्त करने में काफ़ी मददगार साबित हुए हैं. भूमि के विस्तार की सीमाओं, बढ़ती जनसंख्या और खेतीहर ज़मीन की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में गिरावट को देखते हुए उत्पादन में दीर्घकालिक विकास का मुख्य स्रोत विभिन्न निवेशों का सही इस्तेमाल करना है.
ग़ौरतलब है कि देश में हरित क्रांति की शुरुआत साल 1966-67 में हुई थी. इसकी शुरुआत दो चरणों में की गई थी, पहला चरण 1966-67 से 1980-81 और दूसरा चरण 1980-81 से 1996-97 रहा. हरित क्रांति से अभिप्राय देश के सिंचित और असिंचित कृषि क्षेत्रों में ज़्यादा उपज वाले संकर और बौने बीजों के इस्तेमाल के ज़रिये तेज़ी से कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी करना है. हरित क्रांति की विशेषताओं में अधिक उपज देने वाली क़िस्में, उन्नत बीज, रासायनिक खाद, गहन कृषि ज़िला कार्यक्रम, लघु सिंचाई, कृषि शिक्षा, पौध संरक्षण, फसल चक्र, भू-संरक्षण और ऋण आदि के लिए किसानों को बैंकों की सुविधाएं मुहैया कराना शामिल है. रबी, ख़रीफ़ और जायद की फ़सलों पर हरित क्रांति का अच्छा असर देखने को मिला. किसानों को थोड़े पैसे ज़्यादा ख़र्च करने के बाद अच्छी आमदनी हासिल होने लगी. हरित क्रांति की वजह से हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के खेत सोना उगलने लगे. साठ के दशक में हरियाणा और पंजाब में गेहूं के उत्पादन में 40 से 50 फ़ीसद तक बढ़ोतरी दर्ज की गई. जिस वक़्त हरित क्रांति का नारा बुलंद हुआ उस वक़्त देश भुखमरी के दौर से गुज़र रहा था और देश को अनाज की सख़्त ज़रूरत थी. इसलिए सभी का ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा अनाज पैदा करने में था, लेकिन जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता गया रासायनिक उर्वरकों और अत्यधिक विषैले कीटनाशकों के अंधाधुंध इस्तेमाल की वजह से सोना उगलने वाली धरती बंजर होने लगी. उपजाऊ शक्ति के लगातार ह्रास से भूमि के बंजर होने की समस्या ने किसानों के सामने एक नई चुनौती पैदा कर दी है. सूखा, बाढ, लवणीयता, कीटनाशकों के अंधाधुंध इस्तेमाल और अत्यधिक दोहन के कारण भू-जल स्तर में लगातार गिरावट आने से उपजाऊ भूमि बंजर हो रही है. एक रिपोर्ट के मुताबिक़ 90 के दशक तक मिट्टी की उपजाऊ शक्ति सही थी, लेकिन उसके बाद मिट्टी से जिंक, आयरन और मैगनीज़ जैसे पोषक तत्वों की कमी होने लगी. राज्य के दस ज़िलों की मिट्टी का पीएच लेवल सामान्य स्तर पर नहीं है.
आज़ादी के बाद सिंचाई के परंपरागत तरीक़ों की बजाय आधुनिक सिंचाई प्रणालियों को अपनाया गया, जिससे भूमि की उत्पादकता में कमी आई है. भूमि के बंजर होने व अन्य कारणों से प्रति व्यक्ति कृषि भूमि क्षेत्र में कमी हो रही है. लेकिन सवाल यह है कि जब सोना उगलने वाली धरती ही बंजर हो जाएगी, तो अनाज कैसे पैदा होगा. इसलिए भूमि की उर्वरक शक्ति को बचाए रखना बेहद ज़रूरी है, वरना कृषि के विकास की तमाम योजनाएं धरी रह जाएंगी. पहली हरित क्रांति की बुनियाद गेहूं और चावल का ज़्यादा उत्पादन था और इसके लिए अच्छी क़िस्में और रासायनिक खाद और कीटनाशकों का जमकर इस्तेमाल किया गया. उसके नतीजे भी देख लिए. दूसरी हरित क्रांति में अनाज गेहूं, चावल, मक्का के साथ दलहनी, तिलहनी और गन्ना जैसी फ़सलों की अच्छी क़िस्मों पर ध्यान देना होगा. साथ ही इस बात का भे ख़्याल रखना होगा कि रासायनिक खादों और कीटनाशकों का समुचित इस्तेमाल किया जाए. मुख्य फ़सलों में अच्छी गुणवत्ता और ज़्यादा उत्पादन वाली क़िस्मों के विकास के लिए पारंपरिक तकनीकों के साथ-साथ जैव प्रौद्योगिकी का भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करना होगा. जैविक कृषि को बढ़ावा देना होगा. हालांकि भारत में जैविक खेती योग्य क्षेत्र पिछले एक दशक में तक़रीबन 17 गुना बढ़ गया है. यह क्षेत्र साल 2003-04 में 42 हज़ार हेक्टेयर था, जो साल 2013-14 में बढ़कर 7.23 लाख हेहेक्टेयर हो गया. केन्द्र सरकार ने साल 2001 में जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीओपी) लागू किया. इस हेक्टेयर कार्यक्रम में प्रमाणन एजेंसियों के लिए मान्यता कार्यक्रम, जैव उत्पादन के मानक, जैविक खेती को बढ़ावा देना इत्यादि शामिल हैं. कई राज्यों जैसे उत्तराखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, केरल, नागालैंड, मिज़ोरम और सिक्किम जैविक खेती को बढ़ावा देते रहे हैं.
ग़ौरतलब है कि जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए नाबार्ड योजना चला रही है. इसके तहत वाणिज्यिक जैव खाद उत्पादन इकाई की स्थापना के लिए 20 लाख रुपये तक की राशि 25 फ़ीसद सब्सिडी पर दी जाती है. इसके अलावा वर्मी कल्चर हैचरी यूनिट के लिए डेढ़ लाख रुपये और ख़राब हुए फल-सब्ज़ियों व कूड़े-कर्कट से खाद बनाने की इकाई के लिए 40 लाख रुपये तक का क़र्ज़ विभिन्न बैंकों के ज़रिये दिया जाता है. इस पर भी 25 फ़ीसद सब्सिडी है. सरकारी स्तर पर समय-समय पर प्रशिक्षण शिविर लगाकर किसानों को जैविक खेती के बारे में ज़रूरी जानकारी दी जाती है. शिविर में जहां एक तरफ़ मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने के देसी तरीक़ों के बारे में जानकारी दी जाती है, वहीं बीज पड़ताल, उपचार, कीट और खरपतवार नियंत्रण आदि मुद्दों पर चर्चा होती है. जैविक खेती कर रहे किसानों ने अन्य किसानों के साथ अपने अनुभव भी साझा करते हैं. कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि जैविक उत्पाद और रासायनिक उत्पाद की गुणवत्ता में काफ़ी फ़र्क़ होता है. सही तरीक़े से तैयार गोबर की खाद प्रचलित कुरडी की खाद से हल्की होती है. किसान के लिए इससे आसान और सस्ता उत्पादन बढ़ाने का कोई और तरीक़ा नहीं हो सकता है. बशर्ते किसान गोबर की खाद बनाने के अपने तरीक़े में सुधार करें.
कृषि मंत्रालय का कृषि और सहकारिता विभाग (डीएसी), खेतिहर किसानों के लाभ के लिए नित नये कार्यक्रम तैयार करके देश में कृषि क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने की दिशा में सक्रिय भूमिका निभा रहा है. किसानों कृषि की अत्याधुनिक तकनीकों के साथ पारंपरिक विधियों को अपनाकर जहां कृषि लागत को कम किया, वहीं बाग़वानी, कृषि वानिकी, मछली पालन, मधुमक्खी पालन और पशुपालन को अपनाकर एक-दूसरे के ज़रिये लाभ को बढ़ाया. साथ ही डीप इरीगेशन, ऑर्गेनिक फ़ार्मिंग, रोग व कीट नियंत्रण, मृदा संरक्षण, उन्नत कृषि, फ़सल चक्र, ज़ीरो टिलेज, कार्बनिक खाद, उन्नत बीजों का इस्तेमाल, कृषि यंत्रों का बेहतर उपयोग कर उन्होंने सराहनीय कृषि प्रदर्शन किया है. किसानों में खेतीबाड़ी की नित नई तकनीकों के प्रति जागरूकता बढ़ रही है.
बहरहाल, पुरानी बातों से सबक़ लेते हुए कृषि की अत्याधुनिक तकनीकों के साथ फ़ायदेमंद पारंपरिक विधियों के इस्तेमाल से दूसरी हरित क्रांति के सपने को साकार किया जा सकता है. भारत में जैविक संसाधन प्रचुर मात्रा में मौजूद हैं. विभिन्न फ़सलों में जैविक उत्पादन की तकनीक विकसित करके ज़्यादा उपज ली जा सकती है. इससे जहां खाद्यान्न का संकट हल होगा, वहीं किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी.





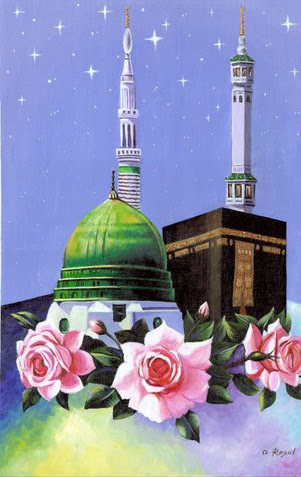











.jpg)
.jpg)









