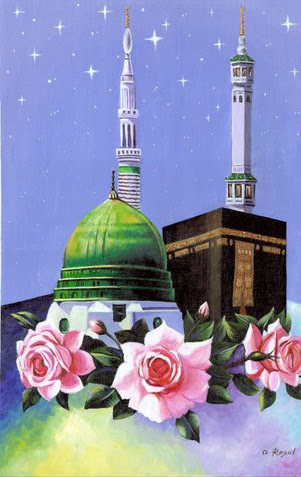फ़िरदौस ख़ान
आदि अदृश्य नदी सरस्वती के तट पर बसा हरित प्रदेश हरियाणा हमेशा से ही हरित क्रांति के क्षेत्र में अग्रणी रहा है. पिछले कुछ अरसे से हरियाणा के किसानों ने पारंपरिक खेती को प्रोत्साहित करने का बीड़ा उठा हुआ है. किसानों का कहना है कि कीटनाषकों और रसायनों के अंधाधुंध इस्तेमाल से जहां कृषि भूमि के बंजर होने का ख़तरा पैदा हो गया है, वहीं कृषि उत्पाद भी ज़हरीले हो रहे हैं. अनाज ही नहीं, दलहन, फल और सब्ज़ियों में भी रसायनों के विषैले तत्व पाए गए हैं, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक हैं. जैविक खेती के ज़रिये पैदा हुआ अनाज स्वास्थ्य के लिए बेहद फ़ायदेमंद है. इसका बाज़ार भाव भी अन्य खाद्यान्न के मुक़ाबले ज़्यादा है. मसलन, जैविक खेती के माध्यम से उगाया गया गेहूं सामान्य गेहूं से 500 से 600 रुपये प्रति क्विंटल ज़्यादा क़ीमत पर बिकता है और इसकी मांग दिनोदिन बढ़ रही है.
ग़ौरतलब है कि जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए नाबार्ड योजना चला रही है. इसके तहत वाणिज्यिक जैव खाद उत्पादन इकाई की स्थापना के लिए 20 लाख रुपये तक की राशि 25 प्रतिशत सब्सिडी पर दी जाती है. इसके अलावा वर्मी कल्चर हैचरी यूनिट के लिए डेढ़ लाख रुपये और ख़राब हुए फल-सब्जियां व कूड़े-कर्कट से खाद बनाने की इकाई के लिए 40 लाख रुपये तक का क़र्ज़ विभिन्न बैंकों के ज़रिये दिया जाता है. इस पर भी 25 प्रतिशत सब्सिडी है.
क़ाबिले-गौर है कि देश में 5.38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती की जा रही है और 2010 यह क्षेत्र बढ़कर 20 लाख हैक्टेयर होने की उम्मीद है. साल 2003 में देश में महज़ 73 हजार हैक्टेयर क्षेत्र पर ही जैविक खेती होती थी. जैविक खेती को मिले प्रोत्साहन से 2007 तक यह क्षेत्र बढ़कर 2.27 लाख हैक्टेयर हो गया. जैविक खेती के चलते जैविक उत्पाद का कारोबार भी दिन-दूनी रात चैगुनी तरक़्क़ी कर रहा है. अगले पांच वर्षों में इसके सात गुना बढ़ने की उम्मीद की जा रही है. इस तरह विश्व के कुल जैविक उत्पाद की हिस्सेदारी 2.5 फ़ीसद हो जाएगी. वर्ष 2003 में भारत से 73 करोड़ रुपये के जैविक उत्पादों का निर्यात किया जा रहा था, जो 2007 में बढ़कर तीन अरब हो गया. अगले पांच वर्षों में जैविक उत्पादों का निर्यात 25 अरब तक होने की उम्मीद है. साथ ही जैविक उत्पादों का घरेलू बाज़ार भी 15 करोड़ से ज़्यादा हो सकता है.
जैविक खेती अपनाने वाले किसानों का कहना है कि जब उन्होंने रासायनिक उर्वरकों की खेती छोड़कर जैविक खेती अपनाने का फ़ैसला किया, तो उनके साथियों ने इसे घाटे का सौदा क़रार दिया. उनका कहना था कि इससे जैविक खेती से उत्पादन पर असर पड़ेगा और उन्हें मज़दूरी तक नहीं मिल पाएगी. मगर किसानों ने हार नहीं मानी. नतीजतन, आज वह जैविक खेती कर पहले से कहीं ज़्यादा आमदनी हासिल कर रहे हैं. उनसे प्रभावित होकर अन्य किसान भी इसे बख़ूबी अपनाकर एक नई क्रांति का अहम हिस्सा बनने को आतुर हैं. यह सस्ती और सुलभ होने के कारण लोकप्रिय बन गई है. जैविक खेती कर रहे हरियाणा के गुड़गांव ज़िले के फ़र्रूख़नगर के निवासी राव मानसिंह कहते हैं कि परंपरागत जैविक खेती सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम है. जब उन्होंने इसे अपनाया, तो उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा. मसलन जैविक खोद और वर्मीवाश कैसे तैयार की जाए और इनका इस्तेमाल किस प्रकार किया जाए. मगर कृषि विभाग के अधिकारियों ने उनकी हरसंभव मदद की, जिसके चलते आज वे खेती के लिए रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों पर निर्भर न होकर स्वयं जैविक खाद और कीटनाशक तैयार कर रहे हैं. वे कहते हैं कि बढ़ती जनसंख्या और घटती कृषि भूमि के कारण किसान खेती की पैदावार बढ़ाने के लिए आज अनेक प्रकार के रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल कर रहे हैं. फ़सल को कीट पतंगों से नुक़सान न पहुंचे, इसके लिए भी कीटनाशक छिड़के जाते हैं. इसके अलावा फसलों को हानि पहुंचाने वाले बैक्टीरिया और फफूंद को नष्ट करने के लिए बैक्टीरिया नाशक और फफूंद नाशक रसायनों का धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जा रहा है. इसी तरह खरपतवार से फ़सल को बचाने के लिए खरपतवार नाशक रसायनों का छिड़काव किया जाता है. इसमें कोई शक नहीं कि इनके इस्तेमाल से पैदावार बढ़ती है, लेकिन यह भी कड़वी सच्चाई है कि फ़ौरी तौर पर लाभ देने वाले इन रसायनों के दूरगामी नतीजे कृषि के लिए बेहद घातक सिद्ध होते हैं. इन महंगे रसायनों से जहां कृषि लागत बढ़ी है, वहीं इनके लगातार इस्तेमाल से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति ख़त्म होती जाती है और एक दिन सोना उगलने वाली उपजाऊ धरती बंजर भूमि में बदल जाती है. इतना ही नहीं, इन रसायनों से फ़सलों के मित्र कीट भी मर जाते हैं. अत्यधिक विषैले रसायनों का काफ़ी अंश फ़सल में भी मौजूद रहता है, जो मानव शरीर के लिए बेहद नुक़सानदेह है. इन रसायनों का खेतों में छिड़काव करने में ज़रा भी असावधानी बरती गई, तो किसान अकाल मौत का ग्रास बन जाता है. अख़बारों में ऐसी कितनी ही ख़बरें प्रकाशित होती रहती हैं कि फ़सल पर कीटनाशक का छिड़काव करते समय अमुक व्यक्ति बेहोश हो गया या उसकी मौत हो गई. इस लिहाज़ से भी जैविक खेती पूरी तरह सुरक्षित है.
राव मानसिंह कहते हैं कि वह अपने खेतों में उत्पन्न होने वाले पत्तियों के कचरे और गोबर से केंचुआ खाद बनाते हैं. केंचुए से ही कीटनाशक वर्मीवाश तैयार करते हैं और इसके अलावा गोमूत्र को भी कीटनाशक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है. उन्होंने जैविक खाद और कीटनाशक बनाने का प्रशिक्षण कृषि विभाग के अधिकारियों से लिया था. आज वे अन्य किसानों को इसका प्रशिक्षण दे रहे हैं. वे कहते हैं कि किसान अपने खेत में आसानी से केंचुआ खाद तैयार कर सकते हैं. इसके लिए छायादार स्थान पर 20 फ़ीट लंबा, चार फ़ीट चैड़ा और दो फीट ऊंचा वर्मी बैड बना लें. इसमें 10 क्विंटल गोबर और कूड़ा-कर्कट भरकर घास-फूस या बोरी से ढककर एक महीने तक सड़ने के लिए छोड़ दें. इसके बाद घास-फूस हटाकर इसमें एक हज़ार केंचुएं डाल दें और इसे फिर ढक दें. कचरे में पर्याप्त नमी बरकरार रहे, इसलिए समय-समय पर पानी का छिड़काव करते रहें. मिट्टी में पाया जाने वाला केंचुआ प्रतिदिन अपने वजन के बराबर कचरा खा जाता है और इसी से मिट्टी की तरह दानेदार खाद तैयार होती है. केंचुआ डालने के डेढ़ महीने बाद वर्मी बैड पर से घास-फूस या बोरी हटा दें. आप पाएंगे कि बेहतरीन जैविक खाद तैयार हो चुकी है. इसमें एक बात ध्यान देने लायक़ यह है कि वर्मी बैड के आसपास चींटियां न पनपने दें, क्योंकि ये केंचुए के लिए जानलेवा हैं. इसी तरह मुंर्ग़ियों व अन्य पक्षियों से भी केंचुए को ख़तरा होता है.
केंचुआ खाद फ़सलों के लिए बेहद फ़ायदेमंद है. केंचुआ मिट्टी के ऊपर-नीचे आवागमन करता है, जिससे मिट्टी जमती नहीं और इसमें हवा का संचार होता है. साथ ही इससे मिट्टी में पानी सोखने की क्षमता बढ़ती है. केंचुआ खाद में पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन, फ़ास्फ़ोरस और पोटेशियम सहित सभी 16 प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं. इस खाद के इस्तेमाल से भूमि दो साल में पूरी तरह उपजाऊ हो जाती है. इसमें किसी भी तरह के रासायनिक उर्वरक डालने की ज़रूरत नहीं होती. इसके साथ ही कीटों का प्रकोप भी कम होता है.
वह बताते हैं कि केंचुआ खाद की तरह ही वर्मीवाश बनाने की विधि भी बेहद आसान है. इसके लिए क़रीब 50 लीटर की बाल्टी या ड्रम की ज़रूरत होती है. बाल्टी की तली में एक छोटा छेद होता है. इस बर्तन में सड़ा गोबर और कूड़ा-कर्कट भरकर क़रीब तीन सौ केंचुए छोड़ देते हैं. इसे भी छायादार जगह पर रखा जाता है और इसमें भी समय-समय पर पानी का छिड़काव करते रहना चाहिए. एक महीने के लिए बर्तन के छेद को अस्थाई रूप से बंद कर दिया जाता है. केंचुए रात में भोजन लेने के लिए ऊपर आते हैं और दिन में नीचे चले जाते हैं. इस तरह केंचुए के लगातार चलने से कम्पोस्ट बैड में बारीक-बारीक नालिकाएं बन जाती हैं और केंचुए के शरीर से पसीने या मूत्र के रूप में निकलने वाला द्रव्य इन नालिकाओं में चिपक जाता है. जब इसमें पानी का छिड़काव किया जाता है तो यह द्रव्य उसमें मिल जाता है. केंचुए डालने के एक महीने के बाद छेद को खोलकर यह द्रव्य बर्तन में इकट्ठा कर लिया जाता है. लीजिए, तैयार हो गया सर्वोत्तम कीटनाशक वर्मीवाश. फ़सलों के लिए यह बहुत ही पोषक तत्व है. इसे फ़सलों का टॊनिक कहें तो ग़लत न होगा. इसमें पौधों के लिए उपयुक्त हारमोन्स और एंजाइम्स सहित सभी पोषक तत्व होते हैं, जो पैदावार में बढ़ोतरी करते हैं. यह फूल और सब्ज़ियों की खेती के लिए अत्यधिक लाभदायक है. इसके अलावा गोमूत्र को भी कीटनाशक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है. हरियाणा के कई किसान केंचुआ खाद के उत्पादन का कार्य कर रहे हैं. उन्होंने कृषि विभाग से अनुदान लेकर वर्मी कम्पोस्ट बैड बनाए हुए हैं. वे केंचुआ खाद तैयार करके कृषि विभाग और किसानों को सप्लाई करते हैं. नर्सरियों के लिए खाद के एक किलो के पैकेट भी उपलब्ध हैं. बाज़ार में केंचुए की क़ीमत दो सौ से पांच सौ रुपये प्रति किलो है.
चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि रसायनों के अंधाधुंध इस्तेमाल से मिट्टी में आवश्यक तत्वों की कमी हो जाती है. मिट्टी के ज़हरीला होने से सर्वाधिक असर केंचुओं की तादाद पर पड़ता है. इससे भूमि की उर्वरा शक्ति क्षीण हो जाती है और फ़सलों की उत्पादकता भी प्रभावित होती. साथ ही मिट्टी में कीटनाशकों के अवशेषों की मौजूदगी का असर जैविक प्रक्रियाओं पर भी पड़ता है. उन्होंने बताया कि यूरिया खाद को पौधे सीधे तौर पर अवशोषित कर सकते हैं. इसके लिए यूरिया को नाइट्रेट में बदलने का कार्य विशेष प्रकार के बैक्टीरिया द्वारा किया जाता है. अगर भूमि ज़हरीली हो गई, तो बैक्टीरिया की तादाद पर प्रभावित होगी. जैविक खेती से भूमि की उपजाऊ शक्ति बरक़रार रहती है.
केंद्र सरकार हर साल क़रीब 40 हज़ार करोड़ रुपये उर्वरकों की सब्सिडी पर ख़र्च करती है. अगर सरकार जैविक खेती के प्रोत्साहन की योजनाओं को बढ़ावा दे तो जहां उर्वरकों की सब्सिडी पर ख़र्च होने वाली राशि में कमी आएगी, वहीं अंधाधुंध रसायनों के इस्तेमाल से भूमि की उर्वरा शक्ति को होने वाले नुक़सान को भी कम किया जा सकेगा. बेशक, जैविक खेती मौजूदा दौर की ज़रूरत है.
आदि अदृश्य नदी सरस्वती के तट पर बसा हरित प्रदेश हरियाणा हमेशा से ही हरित क्रांति के क्षेत्र में अग्रणी रहा है. पिछले कुछ अरसे से हरियाणा के किसानों ने पारंपरिक खेती को प्रोत्साहित करने का बीड़ा उठा हुआ है. किसानों का कहना है कि कीटनाषकों और रसायनों के अंधाधुंध इस्तेमाल से जहां कृषि भूमि के बंजर होने का ख़तरा पैदा हो गया है, वहीं कृषि उत्पाद भी ज़हरीले हो रहे हैं. अनाज ही नहीं, दलहन, फल और सब्ज़ियों में भी रसायनों के विषैले तत्व पाए गए हैं, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक हैं. जैविक खेती के ज़रिये पैदा हुआ अनाज स्वास्थ्य के लिए बेहद फ़ायदेमंद है. इसका बाज़ार भाव भी अन्य खाद्यान्न के मुक़ाबले ज़्यादा है. मसलन, जैविक खेती के माध्यम से उगाया गया गेहूं सामान्य गेहूं से 500 से 600 रुपये प्रति क्विंटल ज़्यादा क़ीमत पर बिकता है और इसकी मांग दिनोदिन बढ़ रही है.
ग़ौरतलब है कि जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए नाबार्ड योजना चला रही है. इसके तहत वाणिज्यिक जैव खाद उत्पादन इकाई की स्थापना के लिए 20 लाख रुपये तक की राशि 25 प्रतिशत सब्सिडी पर दी जाती है. इसके अलावा वर्मी कल्चर हैचरी यूनिट के लिए डेढ़ लाख रुपये और ख़राब हुए फल-सब्जियां व कूड़े-कर्कट से खाद बनाने की इकाई के लिए 40 लाख रुपये तक का क़र्ज़ विभिन्न बैंकों के ज़रिये दिया जाता है. इस पर भी 25 प्रतिशत सब्सिडी है.
क़ाबिले-गौर है कि देश में 5.38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती की जा रही है और 2010 यह क्षेत्र बढ़कर 20 लाख हैक्टेयर होने की उम्मीद है. साल 2003 में देश में महज़ 73 हजार हैक्टेयर क्षेत्र पर ही जैविक खेती होती थी. जैविक खेती को मिले प्रोत्साहन से 2007 तक यह क्षेत्र बढ़कर 2.27 लाख हैक्टेयर हो गया. जैविक खेती के चलते जैविक उत्पाद का कारोबार भी दिन-दूनी रात चैगुनी तरक़्क़ी कर रहा है. अगले पांच वर्षों में इसके सात गुना बढ़ने की उम्मीद की जा रही है. इस तरह विश्व के कुल जैविक उत्पाद की हिस्सेदारी 2.5 फ़ीसद हो जाएगी. वर्ष 2003 में भारत से 73 करोड़ रुपये के जैविक उत्पादों का निर्यात किया जा रहा था, जो 2007 में बढ़कर तीन अरब हो गया. अगले पांच वर्षों में जैविक उत्पादों का निर्यात 25 अरब तक होने की उम्मीद है. साथ ही जैविक उत्पादों का घरेलू बाज़ार भी 15 करोड़ से ज़्यादा हो सकता है.
जैविक खेती अपनाने वाले किसानों का कहना है कि जब उन्होंने रासायनिक उर्वरकों की खेती छोड़कर जैविक खेती अपनाने का फ़ैसला किया, तो उनके साथियों ने इसे घाटे का सौदा क़रार दिया. उनका कहना था कि इससे जैविक खेती से उत्पादन पर असर पड़ेगा और उन्हें मज़दूरी तक नहीं मिल पाएगी. मगर किसानों ने हार नहीं मानी. नतीजतन, आज वह जैविक खेती कर पहले से कहीं ज़्यादा आमदनी हासिल कर रहे हैं. उनसे प्रभावित होकर अन्य किसान भी इसे बख़ूबी अपनाकर एक नई क्रांति का अहम हिस्सा बनने को आतुर हैं. यह सस्ती और सुलभ होने के कारण लोकप्रिय बन गई है. जैविक खेती कर रहे हरियाणा के गुड़गांव ज़िले के फ़र्रूख़नगर के निवासी राव मानसिंह कहते हैं कि परंपरागत जैविक खेती सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम है. जब उन्होंने इसे अपनाया, तो उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा. मसलन जैविक खोद और वर्मीवाश कैसे तैयार की जाए और इनका इस्तेमाल किस प्रकार किया जाए. मगर कृषि विभाग के अधिकारियों ने उनकी हरसंभव मदद की, जिसके चलते आज वे खेती के लिए रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों पर निर्भर न होकर स्वयं जैविक खाद और कीटनाशक तैयार कर रहे हैं. वे कहते हैं कि बढ़ती जनसंख्या और घटती कृषि भूमि के कारण किसान खेती की पैदावार बढ़ाने के लिए आज अनेक प्रकार के रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल कर रहे हैं. फ़सल को कीट पतंगों से नुक़सान न पहुंचे, इसके लिए भी कीटनाशक छिड़के जाते हैं. इसके अलावा फसलों को हानि पहुंचाने वाले बैक्टीरिया और फफूंद को नष्ट करने के लिए बैक्टीरिया नाशक और फफूंद नाशक रसायनों का धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जा रहा है. इसी तरह खरपतवार से फ़सल को बचाने के लिए खरपतवार नाशक रसायनों का छिड़काव किया जाता है. इसमें कोई शक नहीं कि इनके इस्तेमाल से पैदावार बढ़ती है, लेकिन यह भी कड़वी सच्चाई है कि फ़ौरी तौर पर लाभ देने वाले इन रसायनों के दूरगामी नतीजे कृषि के लिए बेहद घातक सिद्ध होते हैं. इन महंगे रसायनों से जहां कृषि लागत बढ़ी है, वहीं इनके लगातार इस्तेमाल से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति ख़त्म होती जाती है और एक दिन सोना उगलने वाली उपजाऊ धरती बंजर भूमि में बदल जाती है. इतना ही नहीं, इन रसायनों से फ़सलों के मित्र कीट भी मर जाते हैं. अत्यधिक विषैले रसायनों का काफ़ी अंश फ़सल में भी मौजूद रहता है, जो मानव शरीर के लिए बेहद नुक़सानदेह है. इन रसायनों का खेतों में छिड़काव करने में ज़रा भी असावधानी बरती गई, तो किसान अकाल मौत का ग्रास बन जाता है. अख़बारों में ऐसी कितनी ही ख़बरें प्रकाशित होती रहती हैं कि फ़सल पर कीटनाशक का छिड़काव करते समय अमुक व्यक्ति बेहोश हो गया या उसकी मौत हो गई. इस लिहाज़ से भी जैविक खेती पूरी तरह सुरक्षित है.
राव मानसिंह कहते हैं कि वह अपने खेतों में उत्पन्न होने वाले पत्तियों के कचरे और गोबर से केंचुआ खाद बनाते हैं. केंचुए से ही कीटनाशक वर्मीवाश तैयार करते हैं और इसके अलावा गोमूत्र को भी कीटनाशक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है. उन्होंने जैविक खाद और कीटनाशक बनाने का प्रशिक्षण कृषि विभाग के अधिकारियों से लिया था. आज वे अन्य किसानों को इसका प्रशिक्षण दे रहे हैं. वे कहते हैं कि किसान अपने खेत में आसानी से केंचुआ खाद तैयार कर सकते हैं. इसके लिए छायादार स्थान पर 20 फ़ीट लंबा, चार फ़ीट चैड़ा और दो फीट ऊंचा वर्मी बैड बना लें. इसमें 10 क्विंटल गोबर और कूड़ा-कर्कट भरकर घास-फूस या बोरी से ढककर एक महीने तक सड़ने के लिए छोड़ दें. इसके बाद घास-फूस हटाकर इसमें एक हज़ार केंचुएं डाल दें और इसे फिर ढक दें. कचरे में पर्याप्त नमी बरकरार रहे, इसलिए समय-समय पर पानी का छिड़काव करते रहें. मिट्टी में पाया जाने वाला केंचुआ प्रतिदिन अपने वजन के बराबर कचरा खा जाता है और इसी से मिट्टी की तरह दानेदार खाद तैयार होती है. केंचुआ डालने के डेढ़ महीने बाद वर्मी बैड पर से घास-फूस या बोरी हटा दें. आप पाएंगे कि बेहतरीन जैविक खाद तैयार हो चुकी है. इसमें एक बात ध्यान देने लायक़ यह है कि वर्मी बैड के आसपास चींटियां न पनपने दें, क्योंकि ये केंचुए के लिए जानलेवा हैं. इसी तरह मुंर्ग़ियों व अन्य पक्षियों से भी केंचुए को ख़तरा होता है.
केंचुआ खाद फ़सलों के लिए बेहद फ़ायदेमंद है. केंचुआ मिट्टी के ऊपर-नीचे आवागमन करता है, जिससे मिट्टी जमती नहीं और इसमें हवा का संचार होता है. साथ ही इससे मिट्टी में पानी सोखने की क्षमता बढ़ती है. केंचुआ खाद में पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन, फ़ास्फ़ोरस और पोटेशियम सहित सभी 16 प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं. इस खाद के इस्तेमाल से भूमि दो साल में पूरी तरह उपजाऊ हो जाती है. इसमें किसी भी तरह के रासायनिक उर्वरक डालने की ज़रूरत नहीं होती. इसके साथ ही कीटों का प्रकोप भी कम होता है.
वह बताते हैं कि केंचुआ खाद की तरह ही वर्मीवाश बनाने की विधि भी बेहद आसान है. इसके लिए क़रीब 50 लीटर की बाल्टी या ड्रम की ज़रूरत होती है. बाल्टी की तली में एक छोटा छेद होता है. इस बर्तन में सड़ा गोबर और कूड़ा-कर्कट भरकर क़रीब तीन सौ केंचुए छोड़ देते हैं. इसे भी छायादार जगह पर रखा जाता है और इसमें भी समय-समय पर पानी का छिड़काव करते रहना चाहिए. एक महीने के लिए बर्तन के छेद को अस्थाई रूप से बंद कर दिया जाता है. केंचुए रात में भोजन लेने के लिए ऊपर आते हैं और दिन में नीचे चले जाते हैं. इस तरह केंचुए के लगातार चलने से कम्पोस्ट बैड में बारीक-बारीक नालिकाएं बन जाती हैं और केंचुए के शरीर से पसीने या मूत्र के रूप में निकलने वाला द्रव्य इन नालिकाओं में चिपक जाता है. जब इसमें पानी का छिड़काव किया जाता है तो यह द्रव्य उसमें मिल जाता है. केंचुए डालने के एक महीने के बाद छेद को खोलकर यह द्रव्य बर्तन में इकट्ठा कर लिया जाता है. लीजिए, तैयार हो गया सर्वोत्तम कीटनाशक वर्मीवाश. फ़सलों के लिए यह बहुत ही पोषक तत्व है. इसे फ़सलों का टॊनिक कहें तो ग़लत न होगा. इसमें पौधों के लिए उपयुक्त हारमोन्स और एंजाइम्स सहित सभी पोषक तत्व होते हैं, जो पैदावार में बढ़ोतरी करते हैं. यह फूल और सब्ज़ियों की खेती के लिए अत्यधिक लाभदायक है. इसके अलावा गोमूत्र को भी कीटनाशक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है. हरियाणा के कई किसान केंचुआ खाद के उत्पादन का कार्य कर रहे हैं. उन्होंने कृषि विभाग से अनुदान लेकर वर्मी कम्पोस्ट बैड बनाए हुए हैं. वे केंचुआ खाद तैयार करके कृषि विभाग और किसानों को सप्लाई करते हैं. नर्सरियों के लिए खाद के एक किलो के पैकेट भी उपलब्ध हैं. बाज़ार में केंचुए की क़ीमत दो सौ से पांच सौ रुपये प्रति किलो है.
चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि रसायनों के अंधाधुंध इस्तेमाल से मिट्टी में आवश्यक तत्वों की कमी हो जाती है. मिट्टी के ज़हरीला होने से सर्वाधिक असर केंचुओं की तादाद पर पड़ता है. इससे भूमि की उर्वरा शक्ति क्षीण हो जाती है और फ़सलों की उत्पादकता भी प्रभावित होती. साथ ही मिट्टी में कीटनाशकों के अवशेषों की मौजूदगी का असर जैविक प्रक्रियाओं पर भी पड़ता है. उन्होंने बताया कि यूरिया खाद को पौधे सीधे तौर पर अवशोषित कर सकते हैं. इसके लिए यूरिया को नाइट्रेट में बदलने का कार्य विशेष प्रकार के बैक्टीरिया द्वारा किया जाता है. अगर भूमि ज़हरीली हो गई, तो बैक्टीरिया की तादाद पर प्रभावित होगी. जैविक खेती से भूमि की उपजाऊ शक्ति बरक़रार रहती है.
केंद्र सरकार हर साल क़रीब 40 हज़ार करोड़ रुपये उर्वरकों की सब्सिडी पर ख़र्च करती है. अगर सरकार जैविक खेती के प्रोत्साहन की योजनाओं को बढ़ावा दे तो जहां उर्वरकों की सब्सिडी पर ख़र्च होने वाली राशि में कमी आएगी, वहीं अंधाधुंध रसायनों के इस्तेमाल से भूमि की उर्वरा शक्ति को होने वाले नुक़सान को भी कम किया जा सकेगा. बेशक, जैविक खेती मौजूदा दौर की ज़रूरत है.