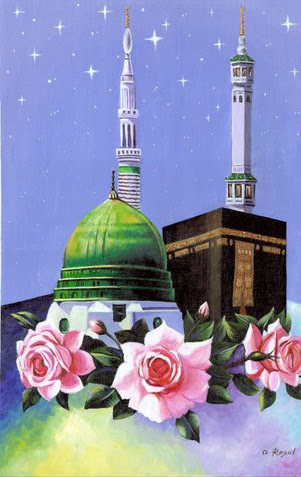रूहानी सफ़र का सबक़
-
हमने अपने रूहानी सफ़र में यही जाना है कि अल्लाह को सिर्फ़ वही शख़्स पा सकता
है, जिसका दिल साफ़ हो यानी जिसके दिल में किसी के लिए भी मैल न हो, यहां तक कि
अपन...
शहरीकरण ने लोक मानस से बहुत कुछ छीन लिया है. चौपालों के गीत-गान लुप्त हो चले हैं. लोक में सहज मुखरित होने वाले गीत अब टीवी कार्यक्रमों में सिमट कर रह गए हैं. फिर भी गांवों में, पर्वतों और वन्य क्षेत्रों में बिखरे लोक जीवन में अभी भी इनकी महक बाक़ी है. हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में पारम्परिक लोकगीतों और लोककथाओं के बिम्ब-प्रतिबिम्ब देखे जा सकते हैं, जबकि मौजूदा आधुनिक चकाचौंध के दौर में शहरों में लोकगीत अपना अस्तित्व खोते जा रहे हैं. संचार माध्यमों के अति तीव्र विकास और यातायात की सुविधा के चलते प्रियतम की प्रतीक्षा में पल-पल पलकें भिगोती नायिका अब केवल प्राचीन काव्यों में ही देखी जा सकती है. सारी प्रकृति संगीतमय है. इसके कण-कण में संगीत बसा है. मनुष्य भी प्रकृति का अभिन्न अंग है, इसलिए संगीत से अछूता नहीं रह सकता. साज़ और सुर का अटूट रिश्ता है. साज़ चाहे जैसे भी हों, संगीत के रूप चाहे कितने ही अलग-अलग क्यों न हों, अहम बात संगीत और उसके प्रभाव की है. जब कोई संगीत सुनता है तो यह सोचकर नहीं सुनता कि उसमें कौन से वाद्यों का इस्तेमाल हुआ है या गायक कौन है या राग कौन सा है या ताल कौन सी है. उसे तो केवल संगीत अच्छा लगता है, इसलिए वह संगीत सुनता है यानी असल बात है संगीत के अच्छे लगने की, दिल को छू जाने की. संगीत भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा है. भारतीय संस्कृति का प्रतिबिम्ब लोकगीतों में झलकता है. यह देश की सांस्कृतिक धरोहर होने के साथ-साथ प्रचार-प्रसार का सशक्त माध्यम भी है.
लोकगीत जनमानस को लुभाते रहे हैं. अस्सी वर्षीय कुमार का कहना है कि वर्षा ऋतु का आख्यान गीत आल्हा कभी जन-जन का कंठहार होता था. वीर रस से ओतप्रोत आल्हा जनमानस में जोश भर देता था. कहते हैं कि अंग्रेज़ अपने सैनिकों को आल्हा सुनवाकर ही जंग के लिए भेजा करते थे. हरियाणा के कलानौर में लोकगीत सुनाकर लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहे राजस्थान के चुरू निवासी लोकगायक वीर सिंह कहते हैं कि लोकगायकों में राजपूत, गूजर, भाट, भोपा, धानक व अन्य पिछड़ी जातियों के लोग शामिल हैं. वे रोज़ी-रोटी की तलाश में अपना घर-बार छोड़कर दूरदराज़ के शहरों और गांवों में निकल पड़ते हैं. वे बताते हैं कि लोकगीत हर मौसम और हर अवसर विशेष पर अलग-अलग महत्व रखते हैं. इनमें हर ऋतु का वर्णन मनमोहक ढंग से किया जाता है. दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद चांदनी रात में चौपालों पर बैठे किसान ढोल-मंजीरे की तान पर उनके लोकगीत सुनकर झूम उठते हैं. फ़सल की कटाई के वक़्त गांवों में काफ़ी चहल-पहल देखने को मिलती है. फ़सल पकने की ख़ुशी में किसान कुसुम-कलियों से अठखेलियां करती बयार, ठंडक और भीनी-भीनी महक को अपने रोम-रोम में महसूस करते हुए लोक संगीत की लय पर नाचने लगते हैं. वे बताते हैं कि किसान उनके लोकगीत सुनकर उन्हें बहुत-सा अनाज दे देते हैं, लेकिन वह पैसे लेना ज़्यादा पसंद करते हैं. अनाज को उठाकर घूमने में उन्हें काफ़ी परेशानी होती है. वे कहते हैं कि युवा वर्ग सुमधुर संगीत सुनने के बजाय कानफोड़ू संगीत को ज़्यादा महत्व देता है. शहरों में अब लोकगीत-संगीत को चाहने वाले लोग नहीं रहे. दिन भर गली-मोहल्लों की ख़ाक छानने के बाद उन्हें बामुश्किल 50 से 60 रुपये ही मिल पाते हैं. उनके बच्चे भी बचपन से ही इसी काम में लग जाते हैं. चार-पांच साल की खेलने-पढ़ने की उम्र में उन्हें घड़ुवा, बैंजू, ढोलक, मृदंग, पखावज, नक्कारा, सारंगी और इकतारा आदि वाद्य बजाने की शिक्षा शुरू कर दी जाती है. यही वाद्य उनके खिलौने होते हैं.
दस वर्षीय बिरजू ने बताया कि लोकगीत गाना उसका पुश्तैनी पेशा है. उसके पिता, दादा और परदादा को भी यह कला विरासत में मिली थी. इस लोकगायक ने पांच साल की उम्र से ही गीत गाना शुरू कर दिया था. इसकी मधुर आवाज़ को सुनकर किसी भी मुसाफ़िर के क़दम ख़ुद ब ख़ुद रुक जाते हैं. इसके सुर और ताल में भी ग़ज़ब का सामंजस्य है. मानसिंह ने इकतारे पर हीर-रांझा, सोनी-महिवाल, शीरी-फ़रहाद और लैला-मजनूं के क़िस्से सुनाते हुए अपनी उम्र के 55 साल गुज़ार दिए. उन्हें मलाल है कि सरकार और प्रशासन ने कभी लोकगायकों की सुध नहीं ली. काम की तलाश में उन्हें घर से बेघर होना पड़ता है. उनकी ज़िन्दगी ख़ानाबदोश बनकर रह गई है. ऐसे में दो वक़्त की रोटी का इंतज़ाम करना पहाड़ से दूध की नहर निकालने से कम नहीं है. उनका कहना है कि दयनीय आर्थिक स्थिति के कारण बच्चे शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से महरूम रहते हैं. सरकार की किसी भी जनकल्याणकारी योजना का लाभ उन्हें नहीं मिलता. साक्षरता, प्रौढ़ शिक्षा, वृद्धावस्था पेंशन और इसी तरह की अन्य योजनाओं से वे अनजान हैं. वह कहते हैं कि रोज़गार की तलाश में दर-दर की ठोंकरे खाने वाले लोगों को शिक्षा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है. अगर रोज़गार मिल जाए तो उन्हें पढ़ना भी अच्छा लगेगा. वे बताते हैं कि लोक सम्पर्क विभाग के कर्मचारी कई बार उन्हें सरकारी समारोह या मेले में ले जाते हैं और पारिश्रमिक के नाम पर 200 से 300 रुपये तक दे देते हैं, लेकिन इससे कितने दिन गुज़ारा हो सकता है. आख़िर रोज़गार की तलाश में भटकना ही उनकी नियति बन चुका है.
कई लोक गायकों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई. भूपेन हज़ारिका और कैलाश खैर इसकी बेहतरीन मिसालें हैं. असम के सादिया में जन्मे भूपेन हजारिका ने बचपन में एक गीत लिखा और दस साल की उम्र में उसे गाया. बारह साल की उम्र में उन्होंने असमिया फिल्म इंद्रमालती में काम किया था. उन्हें 1975 में सर्वोत्कृष्ट क्षेत्रीय फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, 1992 में सिनेमा जगत के सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहब फाल्के सम्मान से नवाज़ा गया. इसके अलावा उन्हें 2009 में असोम रत्न और संगीत नाटक अकादमी अवॉर्ड और 2011 में पद्मभूषण जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया. कैलाश खैर ने भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई और लोकगीतों को विदेशों तक पहुंचाया, मगर सभी लोक गायक भूपेन हजारिका और कैलाश खैर जैसे क़िस्मत वाले नहीं होते. ऐसे कई लोक गायक हैं, जो अनेक सम्मान पाने के बावजूद बदहाली में ज़िन्दगी गुज़ार रहे हैं. राजस्थान के थार रेगिस्तान की ख़ास पहचान मांड गायिकी को बुलंदियों तक पहुंचाने वाली लोक गायिका रुक्मा उम्र के सातवें दशक में बीमारियों से लड़ते-लड़ते ज़िन्दगी की जंग हार गईं और 20 जुलाई 2011 को उनकी मौत के साथ ही मांड गायिकी का एक युग भी समाप्त हो गया. थार की लता के नाम से प्रसिद्ध रुक्मा ज़िन्दगी के आख़िरी दिनों तक पेंशन के लिए कोशिश करती रहीं, लेकिन यह सरकारी सुविधा उन्हें नसीब नहीं हुई. वह मधुमेह और ब्लड प्रेशर से पीड़ित थीं, लेकिन पैसों की कमी के कारण वक़्त पर दवाएं नहीं ख़रीद पाती थीं. उनका कहना था कि वह प्रसिद्ध गायिका होने का ख़ामियाज़ा भुगत रही हैं. सरकार की तरफ़ से उन्हें कोई आर्थिक सहायता नहीं मिली. हालत इतनी बदतर है कि बीपीएल में भी उनका नाम शामिल नहीं है. विधवा और विकलांग पेंशन से भी वह वंचित हैं. सरकारी बाबू सोचते हैं कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है.
रुक्मा ने विकलांग होते हुए भी देश-विदेश में सैकड़ों कार्यक्रम पेश कर मांड गायिकी की सरताज मलिका रेशमा, अलनजिला बाई, मांगी बाई और गवरी देवी के बीच अपनी अलग पहचान बनाई. बाड़मेर के छोटे से गांव जाणकी में लोक गायक बसरा खान के घर जन्मी रुक्मा की सारी ज़िन्दगी ग़रीबी में बीती. रुक्मा की दादी अकला देवी और माता आसी देवी थार इलाक़े की ख्यातिप्राप्त मांड गायिका थीं. गायिकी की बारीकियां उन्होंने अपनी मां से ही सीखीं. केसरिया बालम आओ नी, पधारो म्हारे देस… उनके इस गीत को सुनकर श्रोता भाव विभोर हो उठते थे. उन्होंने पारम्परिक मांड गायिकी के स्वरूप को बरक़रार रखा. उनका मानना था कि पारम्परिक गायिकी से खिलवाड़ करने से उसकी नैसर्गिक मौलिकता ख़त्म हो जाती है. विख्यात रंगमंच कर्मी मल्लिका साराभाई ने उनके जीवन पर डिस्कवरी चैनल पर वृत्तचित्र प्रसारित किया था. विदेशों से भी संगीत प्रेमी उनसे मांड गायिकी सीखने आते थे. ऑस्ट्रेलिया की सेरहा मेडी ने बाडमेर के गांव रामसर में स्थित उनकी झोपड़ी में रहकर उनसे संगीत की शिक्षा ली और फिर गुलाबी नगरी जयपुर के जवाहर कला केन्द्र में आयोजित थार महोत्सव में मांड गीत प्रस्तुत कर ख़ूब सराहना पाई. रुक्मा की ज़िन्दगी के ये यादगार लम्हे थे. अब उनकी छोटी बहू हनीफ़ा मांड गायिकी को ज़िन्दा रखने की कोशिश कर रही हैं. एक तरफ़ सरकार कला संस्कृति के नाम पर बड़े-बड़े समारोहों का आयोजन कर उन पर करोड़ों रुपये पानी की तरह बहा देती है, वहीं दूसरी तरफ़ देश की कला-संस्कृति को विदेशों तक फैलाने वाले कलाकारों को ग़ुरबत में मरने के लिए छोड़ देती है.
क़ाबिले-ग़ौर है कि लोकगीत गाने वालों को लोक गायक कहा जाता है. लोकगीत से आशय है लोक में प्रचलित गीत, लोक रचित गीत और लोक विषयक गीत. कजरी, सोहर और चैती आदि लोकगीतों की प्रसिद्ध शैलियां हैं. त्यौहारों पर गाये जाने वाले मांगलिक गीतों को पर्व गीत कहा जाता है. ये गीत रंगों के पावन पर्व होली, दीपावली, छठ, तीज व अन्य मांगलिक अवसरों पर गाये जाते हैं. विभिन्न ऋतुओं में गाए जाने वाले गीतों को ऋतु गीत कहा जाता है. इनमें कजरी, चतुमार्सा, बारहमासा, चइता और हिंडोला आदि शामिल हैं. इसी तरह अलग-अलग काम-धंधे करने वालों के गीतों को पेशा गीत कहा जाता है. ये गीत लोग काम करते वक़्त गाते हैं, जैसे गेहूं पीसते समय महिलाएं जांत-पिसाई, छत की ढलाई करते वक़्त थपाई और छप्पर छाते वक़्त छवाई गाते हैं. इसी तरह गांव-देहात में अन्य कार्य करते समय सोहनी और रोपनी आदि गीत गाने का भी प्रचलन है. विभिन्न जातियों के गीतों को जातीय गीत कहा जाता है. इनमें नायक और नायिका की जाति का वर्णन होता है. इसके अलावा कई राज्यों में झूमर, बिरहा, प्रभाती, निर्गुण और देवी-देवताओं के गीत गाने का चलन है. ये गीत क्षेत्र विशेष की सांस्कृतिक धरोहर हैं, जिनसे वहां के बारे में जानकारी प्राप्त होती है.
सरफ़राज़ ख़ान
देश को स्वतंत्र हुए छह देशक से भी ज्यादा का समय हो गया है. हर साल 15 अगस्त को प्रधानमंत्री द्वारा लाल क़िले पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फ़हराया जाता है. मगर क्या कभी किसी ने यह सोचा है कि 15 अगस्त, 1947 की रात को जब देश आज़ाद हुआ था, उस वक़्त भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने लाल किले पर जो तिरंगा लहराया फहराया था, वह कहां है?
इसकी सही जानकारी किसी को नहीं है. राष्ट्रीय ध्वज पूरे राष्ट्र के लिए एक ऐसा प्रतीक चिन्ह होता है जो पूरे देश की अस्मिता से जुड़ा होता है. यूं तो आज़ादी के बाद से हर बरस लाल क़िले पर फहरया जाने वाला तिरंगा देश की धरोहर है, लेकिन 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर फहराये राष्ट्रीय ध्वज का अपना अलग ही एक महत्व है.
कुछ लोगों का कहना है कि 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर लहराया गया तिरंगा नेहरू स्मारक में रखा गया है, जबकि स्मारक के अधिकारी इस बात से इंकार करते हैं. हैरत की बात तो यह भी है कि यह विशेष तिरंगा राष्ट्रीय अभिलेखागार में भी मौजूद नहीं है. इस अभिलेखागार में 1946 में नौसेना विद्रोह के दौरान बाग़ी सैनिकों द्वारा फहराया गया ध्वज रखा हुआ है. बंबई में 1946 में नौसेना विद्रोह के वक्त तीन ध्वज फहराये गए थे. इनमें कांग्रेस का ध्वज, मुस्लिम लीग का ध्वज और कम्युनिस्ट पार्टी का ध्वज शामिल थे. इनमें से कांग्रेस का ध्वज अभिलेखागार में मौजूद है.
प्रथम स्वतंत्रता दिवस पर फहराया गया ध्वज राष्ट्रीय संग्रहालय में भी नहीं है. राष्ट्रीय संग्रहालय के एक पूर्व अधिकारी के मुताबिक़ आम तौर पर ऐतिहासिक महत्व की ऐसी धरोहर राष्ट्रीय संग्रहालय में रखने की बात हुई थी, लेकिन बाद में इसे भारतीय सेना को सौंप दिया गया था. इसके बाद इसे स्वतंत्रता दिवस तथा गणतंत्र दिवस के प्रबंध की देखरेख करने वाले केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को सौंप दिया गा, लेकिन केंद्रीय लोक निर्माण विभाग तथा सर्च द फ्लैग मिशन के पास उस तिरंगे के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध है.
15 अगस्त 1947 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ऑल इंडिया रेडियो पर देश के नाम संदेश देने दिया था और शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्ला ख़ां ने अपनी स्वर लहरियों से आज़ादी का स्वागत किया था.
डॉ. फ़िरदौस ख़ास
पर्यटन भी ज़िन्दगी का एक अहम हिस्सा है. कुछ लोग क़ुदरत की ख़ूबसूरती निहारने के लिए दूर-दराज़ के इलाक़ों में जाते हैं, तो कुछ लोगों को अक़ीदत इबादतगाहों और मज़ारों तक ले जाती है. पर्यटन रोज़गार का भी एक बड़ा साधन है. हमारे देश भारत में लाखों लोग पर्यटन से जुड़े हैं. यहां मज़हबी पर्यटन ख़ूब फल-फूल रहा है. हर साल विदेशों से लाखों लोग भारत भ्रमण के लिए आते हैं, जिनमें एक बड़ी तादाद धार्मिक स्थलों पर आने वाले ज़ायरीनों यानी पर्यटकों की होती है.
देश की राजधानी दिल्ली में जामा मस्जिद पर्यटकों का पसंदीदा स्थल है. यह मस्जिद लाल पत्थरों और संगमरमर से बनी हुई है. मुग़ल बादशाह शाहजहां ने इसे बनवाया था. इसके ख़ूबसूरत गुम्बद, शानदार मीनारें और हवादार झरोखे इसे बहुत ही दिलकश बनाते हैं. मस्जिद में उत्तर और दक्षिण के दरवाज़ों से दाख़िल हुआ जा सकता है. पूर्व का दरवाज़ा सिर्फ़ जुमे के दिन ही खुलता है. यह दरवाज़ा शाही परिवार के दाख़िले के लिए हुआ करता था.
इसके अलावा ज़ायरीन दिल्ली में दरगाहों पर भी हाज़िरी लगाते हैं. यहां बहुत सी दरगाहें अक़ीदत का मर्कज़ हैं, ख़ासकर सूफ़ियाना सिलसिले से जुड़े लोग यहां अपनी अक़ीदत के फूल चढ़ाते हैं. यहां महबूबे-इलाही हज़रत शेख़ निजामुद्दीन औलिया और उनके प्यारे मुरीद हज़रत अमीर खुसरो साहब की मज़ारें हैं. ज़ायरीन हज़रत ख़्वाजा क़ुतुबुद्दीन बख़्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत ख़्वाजा अब्दुल अज़ीज़ बिस्तामी, हज़रत ख़्वाजा बाक़ी बिल्लाह, हज़रत ख़्वाजा अलीअहमद एहरारी, हज़रत सैयद बदरुद्दीन शाह समरकंदी, हज़रत सैयद महमूद बहार, हज़रत सैयद सदरुद्दीन शाह, हज़रत सैयद आरिफ़ अली शाह, हज़रत सैयद अबुल कासिम सब्ज़वारी, हज़रत सैयद हसन रसूलनुमा, हज़रत सैयद शाह आलम, हज़रत मौलाना शेख़ जमाली और कमाली, हज़रत मौलाना फ़ख़रुद्दीन फ़ख़्र-ए-जहां, हज़रत मौलाना शेख़ मजदुद्दीन हाजी, हज़रत मौलाना नासेहुद्दीन, हज़रत शम्सुल आरफ़ीन तुर्कमान शाह, हज़रत शाह तुर्कमान बयाबानी सुहरवर्दी, हज़रत शाह सरमद शहीद, हज़रत शाह सादुल्लाह गुलशन, हज़रत शाह वलीउल्लाह, हज़रत शाह मुहम्मद आफ़ाक़, हज़रत शाह साबिर अली चिश्ती साबरी, हज़रत शेख़ सैयद जलालुद्दीन चिश्ती, हज़रत शेख़ कबीरुद्दीन औलिया, हज़रत शेख़ जैनुद्दीन अली, हज़रत शेख़ यूसुफ़ कत्ताल, हज़रत शेख़ नसीरुद्दीन महमूद चिराग़-ए-देहली, ख़लीफ़ा शेख़ चिराग़-ए-देहली, हज़रत शेख़ नजीबुद्दीन मुतवक्किल चिश्ती, हज़रत शेख़ नूरुद्दीन मलिक यारे-पर्रा, हज़रत शेख़ शम्सुद्दीन औता दुल्लाह, हज़रत शेख़ शहाबुद्दीन आशिक़उल्लाह, हज़रत शेख़ ज़ियाउद्दीन रूमी सुहरवर्दी, हज़रत मख़मूद शेख़ समाउद्दीन सुहरवर्दी, हज़रत शेख़ नजीबुद्दीन फ़िरदौसी, हज़रत शेख़ रुकनुद्दीन फ़िरदौसी, हज़रत शेख़ एमादुद्दीन इस्माईल फ़िरदौसी, हज़रत शेख़ उस्मान सय्याह, हज़रत शेख़ सलाहुद्दीन, हज़रत शेख़ अल्लामा कमालुद्दीन, हज़रत शेख़ बाबा फ़रीद (पोते), हज़रत शेख़ अलाउद्दीन, हज़रत शेख़ फ़रीदुद्दीन बुख़ारी, हज़रत शेख़ अब्दुलहक़ मुहद्दिस देहलवी, हज़रत शेख़ सुलेमान देहलवी, हज़रत शेख़ मुहम्मद चिश्ती साबरी, हज़रत मिर्ज़ा अब्दुल क़ादिर बेदिल, हज़रत शेख़ नूर मुहम्मद बदायूंनी, हज़रत शेख़ शाह कलीमुल्लाह, हज़रत शेख़ मुहम्मद फ़रहाद, हज़रत शेख़ मीर मुहम्मदी, हज़रत शेख़ हैदर, हज़रत क़ाज़ी शेख़ हमीदुद्दीन नागौरी, हज़रत अबूबकर तूसी हैदरी, हज़रत नासिरुद्दीन महमूद, हज़रत इमाम ज़ामिन, हज़रत हाफ़िज़ सादुल्लाह नक़्शबंदी, हज़रत शेख़ुल आलेमीन हाजी अताउल्लाह, हज़रत मिर्ज़ा मुल्लाह मज़हर जाने-जानां, हज़रत मीरानशाह नानू और शाह जलाल, हज़रत अब्दुस्सलाम फ़रीदी, हज़रत ख़ुदानुमा, हज़रत नूरनुमा और हज़रत मख़दूम रहमतुल्लाह अलैह की मज़ारों पर भी जाते हैं. यहां हज़रत बीबी हंबल साहिबा, हज़रत बीबी फ़ातिमा साम और हज़रत बीबी ज़ुलैख़ा की मज़ारें भी हैं, जहां महिला ज़ायरीन जाती हैं. यहां पंजा शरीफ़, शाहेमर्दां, क़दम शरीफ़ और चिल्लागाह पर भी ज़ायरीन हाज़िरी लगाते हैं.
यूं तो हर रोज़ ही मज़ारों पर ज़ायरीनों की भीड़ होती है, लेकिन जुमेरात के दिन यहां का माहौल कुछ अलग ही होता है. क़व्वाल क़व्वालियां गाते हैं. दरगाह के अहाते में अगरबत्तियों की भीनी-भीनी महक और उनका आसमान की तरफ़ उठता सफ़ेद धुआं कितना भला लगता है. ज़ायरीनों के हाथों में फूलों और तबर्रुक की तबाक़ होते हैं. मज़ारों के चारों तरफ़ बनी जालियों के पास बैठी औरतें क़ुरान शरीफ़ की सूरतें पढ़ रही होती हैं. कोई औरत जालियों में मन्नत के धागे बांध रही होती है, तो कोई दुआएं मांग रही होती है.
राजस्थान के अजमेर में ख़्वाजा मोईनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्ला अलैह का मज़ार है. ख़्वाजा अल्लाह के रसूल हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलादों में से हैं. ख़्वाजा की वजह से अजमेर को अजमेर शरीफ़ भी कहा जाता है. सूफ़ीवाद का चिश्तिया तरीक़ा हज़रत अबू इसहाक़ शामी ने ईरान के शहर चश्त में शुरू किया था. इसलिए इस तरीक़े या सिलसिले का नाम चिश्तिया पड़ गया. जब ख़्वाजा मोईनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्ला अलैह हिन्दुस्तान आए, तो उन्होंने इसे दूर-दूर तक फैला दिया. हिन्दुस्तान के अलावा पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी चिश्तिया सिलसिला ख़ूब फलफूल रहा है. दरअसल यह सिलसिला भी दूसरे सिलसिलों की तरह ही दुनियाभर में फैला हुआ है. यहां भी दुनियाभर से ज़ायरीन आते हैं.
महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में सैयद हाजी अली शाह बुख़ारी का मज़ार है. हाजी अली भी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलादों में से हैं. यह मज़ार मुम्बई के वर्ली तट के क़रीब एक टापू पर बनी मस्जिद के अन्दर है. सफ़ेद रंग की यह मस्जिद बहुत ही ख़ूबसूरत लगती है. मुख्य सड़क से मज़ार तक जाने के लिए एक पुल बना हुआ है. इसके दोनों तरफ़ समन्दर है. शाम के वक़्त समन्दर का पानी ऊपर आने लगता है और यह पुल पानी में डूब जाता है. सुबह होते ही पानी उतरने लगता है. यहां भी हिन्दुस्तान के कोने-कोने के अलावा दुनियाभर से ज़ायरीन आते हैं.
हरियाणा के पानीपत शहर में शेख़ शराफ़ुद्दीन बू अली क़लंदर का मज़ार है. यह मज़ार एक मक़बरे के अन्दर है, जो साढ़े सात सौ साल से भी ज़्यादा पुराना है. कहा जाता है कि शेख़ शराफ़ुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने लम्बे अरसे तक पानी में खड़े होकर इबादत की थी. जब उनकी इबादत क़ुबूल हुई, तो उन्हें बू अली का ख़िताब मिला. दुनिया में अब तक सिर्फ़ साढ़े तीन क़लन्दर हुए हैं. शेख़ शराफ़ुद्दीन बू अली क़लंदर, लाल शाहबाज़ क़लंदर और शम्स अली कलंदर. हज़रत राबिया बसरी भी क़लंदर हैं, लेकिन औरत होने की वजह से उन्हें आधा क़लंदर माना जाता है. बू अली क़लंदर रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के क़रीब ही उनके मुरीद हज़रत मुबारक अली शाह का भी मज़ार है. यहां भी दूर-दूर से ज़ायरीन आते हैं.
उत्तर प्रदेश के बाराबंकी ज़िले के देवा नामक क़स्बे में हाजी वारिस अली शाह का मज़ार है. आप अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलादों में से हैं. उनके वालिद क़ुर्बान अल्ली शाह भी जाने-माने औलिया थे.
उत्तर प्रदेश के ही कानपुर ज़िले के गांव मकनपुर में हज़रत बदीउद्दीन शाह ज़िन्दा क़ुतबुल मदार का मज़ार है.
इनके बारे में कहा जाता है कि ये योगी दुर्वेश थे और अकसर योग के ज़रिये महीनों साधना में रहते थे. एक बार वह योग समाधि में ऐसे लीन हुए कि लम्बे अरसे से तक उठे नहीं. उनके मुरीदों ने समझा कि उनका विसाल हो गया है. उन्होंने हज़रत बदीउद्दीन शाह को दफ़न कर दिया. दफ़न होने के बाद उन्होंने सांस ली. उनके मुरीद यह देखकर हैरान रह गए कि वे ज़िन्दा हैं. वे क़ब्र खोदकर उन्हें निकालने वाले ही थे, तभी एक बुज़ुर्ग ने हज़रत बदीउद्दीन शाह से मुख़ातिब होकर कहा कि दम न मार यानी अब तुम ज़िन्दा ही दफ़न हो जाओ. फिर उस क़ब्र को ऐसे ही छोड़ दिया गया. इसलिए उन्हें ज़िन्दा पीर भी कहा जाता है. आपकी उम्र मुबारक तक़रीबन छह सौ साल थी.
इनके अलावा देशभर में और भी औलियाओं की मज़ारें हैं, जहां दूर-दराज़ के इलाक़ों से ज़ायरीन आते हैं और सुकून हासिल करते हैं.
(लेखिका स्टार न्यूज़ एजेंसी में सम्पादक हैं)
लाल बिहारी लाल
सदियों की गुलामी के बाद आजादी की पहली मांग सन् 1857 ईस्वी में पुरजोर तरीके से उठी उसी समय राष्ट्र के ध्वज बनाने की योजना बनी परंतु पहले स्वतंत्रता संघर्ष के परिणाम को देखकर झंडे की मांग बीच में ही अटक गई। वर्तमान स्वरूप में विद्यमान झंडा कई चरणों से होकर गुजरा है। प्रथम चित्रित ध्वज स्वामी विवेकानंद की शिष्या भगिनी निवेदिता द्वारा 1904 में बनाया गया था औऱ इसे 7 अगस्त 1906 के कोलकाता में कांग्रेस के अधिवेशन में फहराया गया था ।इस ध्वज को क्षैतिज तीन रंगो लाल, पीला एवं हरे रंग की क्षौतिज पट्टियां बनाया गया था ।ऊपर की ओर हरी पट्टी में आठ कमल थे जिनका रंग सफेद था , नीचे की लाल पट्टी में सूरज और चांद बनाए गए सफेद रंग से बनाये गए थे बीच की पीली पट्टी पर नीले रंग से वंदे मातरम लिखा गया था।
द्वितीय ध्वज की बात करें तो सन 1907 ईस्वी में मैडम भीका जी कामा और कुछ अन्य निर्वाचित क्रांतिकारियों ने मिल कर पेरिस में पहली बार फहराया था। तृतीय चित्र ध्वज की बात करें तो 1917 ईस्वी में राजनीतिक संघर्ष के दौरान एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने घरेलू शासन आंदोलन के दौरान फहराया था। इस ध्वज में पांच लाल और चार हरे क्षैतिज पट्टियां एक के बाद एक और सप्तऋषि के अभिविन्यास में इस पर सात सितारे बने थे ।ऊपरी किनारे पर बायी और यूनियन जैक था । उपर दायी तरफ एक कोने में सफेद अर्द्धचंद्र और सितारा भी था । कांग्रेस के विजयवाड़ा अधिवेशन में एक युवक पिंगली वेंकैया ने एक चौथा झंडा बनाया था जिसमें दो रंगों का लाल और हरा रंग का था जो दो प्रमुख समुदाय अर्थात हिंदू और मुस्लिम का प्रतिनिधित्व करता था गांधी जी ने 1921 ईस्वी में सुझाव दिया कि भारत के शेष समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए इसे एक सफेद पट्टी मध्य में और सफेद पट्टी के बीच में प्रगति के लिए चलता हुआ चरखा होना चाहिए। वर्ष 1931 में झंडा के इतिहास में एक नया मोड़ आया तिरंगे ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने का एक प्रस्ताव पारित किया गया। इसमें तीन रंग उपर केसरिया बलिदान का प्रतीक बीच में सफेद शांति का प्रतिक और अशोक स्तंभ से लिया चक्र इसे विधि चक्र भी कहते हैं जिसमें 24 तिल्लिया प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देती है और सबसे नीचे हरा रंग हरियाली एवं खुशहाली का प्रतीक । तीनों पट्टियां समानुपात में आयताकार जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। इसे राष्ट्रध्वज के रूप में मान्यता मिली 22 जुलाई 1947 ई. को संविधान सभा ने वर्तमान भारत के तिरंगा को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया तथा आजादी के बाद भी इसका रंग और महत्व आज भी बना हुआ है। इस ध्वज को आज 26 जनवरी 1950 को संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुआ। ये था राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का रोचक इतिहास।
(लेखक-साहित्य टीवी के सम्पादक हैं)
हर तीसरा व्यक्ति किसी न किसी प्रकार के दर्द से परेशान है. किसी के पूरे जिस्म में दर्द है, किसी की पीठ में दर्द है, किसी के घुटनों में दर्द है और किसी के हाथ-पैरों में दर्द है. हालांकि दर्द की कई वजहें होती हैं. इनमें से एक वजह यूरिक एसिड भी है.
दरअसल, यूरिक एसिड एक अपशिष्ट पदार्थ है, जो खाद्य पदार्थों के पाचन से पैदा होता है और इसमें प्यूरिन होता है. जब प्यूरिन टूटता है, तो उससे यूरिक एसिड बनता है. किडनी यूरिक एसिड को फ़िल्टर करके इसे पेशाब के ज़रिये जिस्म से बाहर निकाल देती है. जब कोई व्यक्ति अपने खाने में ज़्यादा मात्रा में प्यूरिक का इस्तेमाल करता है, तो उसका जिस्म यूरिक एसिड को उस तेज़ी से जिस्म से बाहर नहीं निकाल पाता. इस वजह से जिस्म में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने लगती है. ऐसी हालत में यूरिक एसिड ख़ून के ज़रिये पूरे जिस्म में फैलने लगता है और यूरिक एसिड के क्रिस्टल जोड़ों में जमा हो जाते हैं, जिससे जोड़ों में सूजन आ जाती है. इसकी वजह से गठिया भी हो जाता है. जिस्म में असहनीय दर्द होता है. इससे किडनी में पथरी भी हो जाती है. इसकी वजह से पेशाब संबंधी बीमारियां पैदा हो जाती हैं. मूत्राशय में असहनीय दर्द होता है और पेशाब में जलन होती है. पेशाब बार-बार आता है. यह यूरिक एसिड स्वस्थ व्यक्ति को बीमार कर देता है.
यूरिक एसिड से बचने के लिए अपने खान-पान पर ख़ास तवज्जो दें. दाल पकाते वक़्त उसमें से झाग निकाल दें. कोशिश करें कि दाल कम इस्तेमाल करें. बिना छिलकों वाली दालों का इस्तेमाल करना बेहतर है. रात के वक़्त दाल, चावल और दही आदि खाने से परहेज़ करें. हो सके तो फ़ाइबर से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन करें.
जौ
यूरिक एसिड से निजात पाने के लिए जौ का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें. जौ की ख़ासियत है कि यह यूरिक एसिड को सोख लेता है और उसे जिस्म से बाहर करने में कारगर है. इसलिए जौ को अपने रोज़मर्रा के खाने में ज़रूर शामिल करें. गर्मियों के मौसम में जौ का सत्तू पी सकते हैं, जौ का दलिया बना सकते हैं, जौ के आटे की रोटी बनाई जा सकती है.
ज़ीरा
यूरिक एसिड के मरीज़ों के लिए ज़ीरा भी बहुत फ़ायदेमंद है. ज़ीरे में आयरन, कैल्शियम, ज़िंक और फ़ॉस्फ़ोरस पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं. इसके अलावा इसमें एंटीऑक्सीडेंट उच्च मात्रा में मौजूद होता है, जो यूरिक एसिड की वजह से होने वाले जोड़ों के दर्द और सूजन को कम करता है. यह टॉक्सिंस को जिस्म से बाहर करने में भी मददगार है.
नींबू
नींबू में मौजूद साइट्रिक एसिड शरीर में यूरिक एसिड के स्तर को बढ़ने से रोकता है. इसलिए नींबू का इस्तेमाल करना चाहिए.
ज़्यादा परेशानी होने पर चिकित्सक से परामर्श लें.
फूल पलाश के
वक़्त के समन्दर में
यादों का जज़ीरा हैं
जिसके हर ज़र्रे में
ख़्वाबों की धनक फूटती है
फ़िज़ाओं में
चाहत के गुलाब महकते हैं
जिसकी हवायें
रूमानी नगमें गुनगुनाती हैं
जिसके जाड़ों पर
क़ुर्बतों का कोहरा छाया होता है
जिसकी गर्मियों में
तमन्नायें अंगडाइयां लेती हैं
जिसकी बरसात
रफ़ाक़तों से भीगी होती है
फूल पलाश के
इक उम्र का
हसीन सरमाया ही तो हैं...
-डॉ. फ़िरदौस ख़ान
जिसके जाड़ों पर
क़ुर्बतों का कोहरा छाया होता है
जिसकी गर्मियों में
तमन्नायें अंगडाइयां लेती हैं
जिसकी बरसात
रफ़ाक़तों से भीगी होती है
फूल पलाश के
इक उम्र का
हसीन सरमाया ही तो हैं...
-डॉ. फ़िरदौस ख़ान
हर मौसम की अपनी ख़ूबसूरती हुआ करती है... मौसम पर एक नज़्म पेश है...
दहकते पलाश का मौसम...
मेरे महबूब !
ये दहकते पलाश का मौसम है
क्यारियों में
सुर्ख़ गुलाब महक रहे हैं
बर्फ़ीले पहाड़ों के लम्स से
बहकी सर्द हवायें
मुहब्बत के गीत गाती हैं
बनफ़शी सुबहें
कोहरे की चादर लपेटे हैं
अलसाई दोपहरें
गुनगुनी धूप सी खिली हैं
और
गुलाबी शामें
तुम्हारे मुहब्बत से भीगे पैग़ाम लाती हैं
लेकिन
तुम न जाने कब आओगे...
-डॉ. फ़िरदौस ख़ान
डॉ. फ़िरदौस ख़ान
सुर्ख़ फूल पलाश के, जब खिलते हैं तो फ़िज़ा सिंदूरी हो जाती है. पेड़ की शाख़ें दहकने लगती हैं और पेड़ के नीचे ज़मीन पर बिखरे पलाश के फूल माहौल को रूमानी कर देते हैं.
पलाश को कई नामों से जाना जाता है, जैसे पलास, परसा, ढाक, टेसू, किंशुक, केसू. पलाश का दरख़्त बहुत ऊंचा नहीं होता यानी दर्मियाने क़द का होता है. इसके फूल सुर्ख़ रंग के होते हैं, इसीलिए इसे ’जंगल की आग’ भी कहा जाता है. यह तीन रूपों में पाया जाता है, मसलन वृक्ष रूप में, झाड़ रूप में और बेल रूप में. लता पलाश दो क़िस्म का होता है. सुर्ख़ फूलों वाला पलाश और सफ़ेद फूलों वाला पलाश. सुर्ख़ फूलों वाले पलाश का वैज्ञानिक नाम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है, जबकि सफ़ेद फूलों वाले लता पलाश का वैज्ञानिक नाम ब्यूटिया पार्वीफ्लोरा है. एक पीले फूलों वाला पलाश भी होता है.
पलाश दुनियाभर में पाया जाता है. पलाश मैदानों, जंगलों और ऊंचे पहाड़ों पर भी अपनी ख़ूबसूरती के जलवे बिखेरता है. बग़ीचों में यह पेड़ के रूप में होता, जबकि जंगलों और पहाड़ों में ज़्यादातर झाड़ के रूप में पाया जाता है. लता रूप में यह बहुत कम मिलता है. सभी तरह के पलाश के पत्ते, फूल और फल एक जैसे ही होते हैं. इसके पत्ते गोल और बीच में कुछ नुकीले होते हैं, जिनका रंग हरा होता है. पत्ते सीकों में निकलते हैं और एक में तीन-तीन पत्ते होते हैं. इसकी छाल मोटी और रेशेदार होती है. पलाश की लकड़ी टेढ़ी-मेढ़ी होती है. इसका फूल बड़ा, आधे चांद जैसा और गहरा लाल होता है. फागुन के आख़िर में इसमें फूल लगते हैं. जिस वक़्त पलाश फूलों से लद जाता है, तब इसके हरे पत्ते झड़ चुके होते हैं. पलाश के दरख़्त पर सिर्फ़ फूल ही फूल नज़र आते हैं. फूल झड़ जाने पर इसमें चौड़ी फलियां लगती हैं, जिनमें गोल और चपटे बीज होते हैं.
पलाश के अमूमन सभी हिस्से यानी पत्ते, फूल, फल, छाल और जड़ बहुत काम आते हैं. पलाश के फूलों से रंग बनाए जाते हैं. फलाश के फूल कई बीमारियों के इलाज में भी काम आते हैं. पत्तों से पत्तल और दोने आदि बनाए जाते हैं. इनसे बीडियां भी बनाई जाती हैं. बीज दवाओं में इस्तेमाल किए जाते हैं. छाल से निकले रेशे जहाज़ के पटरों की दरारों में भरने के काम आते हैं. जड़ की छाल के रेशे से रस्सियां बटी जाती हैं. इससे दरी और काग़ज़ भी बनाया जाता है. इसकी छाल से गोंद बनाया जाता है, जिसे 'चुनियां गोंद' या पलाश का गोंद कहते हैं. इसकी पतली डालियों से कत्था बनाया जाता है, जबकि मोटी डालियों और तनों को जलाकर कोयला तैयार किया जाता है.
पलाश हिंदुओं के पवित्र माने जाने वाले वृक्षों में से है. इसका ज़िक्र वेदों तक में मिलता है. आयुर्वेद ने इसे ब्रह्मवृक्ष कहा है. मान्यता है कि इस वृक्ष में तीनों देवताओं ब्रह्मा, विष्णु, महेश का निवास है. पलाश का धार्मिक महत्व भी बहुत ज़्यादा है. पलाश का इस्तेमाल ग्रहों की शांति में किया जाता है. इसकी डंगाल हवन पूजन में काम आती है. पेड़ की जड़ से ग्रामीण सोहई बनाते हैं, जिसे दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजन को अपने गाय-बैलों को बांधते हैं.
पलाश कवियों और साहित्यकारों का भी प्रिय वृक्ष है, इस पर अनेक रचनाएं रची गई हैं और रची जा रही हैं.
कुहू-कुहू पीहू पीहू होने लगी
चेतना हरेक मन की खोने लगी
गाने लगे, गुनगुनाने लगे
सब अपनी मस्ती में झूमने लगे
आया बसंत फल-फूलने लगे
बागों में कलियां,चटकने लगी
वृक्षों की शाखें, मटकने लगी
हंसे फूल और येभंवरे तितलियां
फूलों के अधरों को चूमने लगे
आया बसंत फल फूलने लगे
सतरंगी फूलों की माला लिए
हाथों में मकरंदी प्याला लिए
आते हैं हर साल वैसे यह दिन
अबकी बार और भी ये घने लगे
आया बसंत फल फूलने लगे
-सत्यपाल सत्यम
यश मालवीय
मेरा यह अनुभव रहा है कि जब जब मन उदास होने होने को होता है कि ज़ेहन के बंद दरवाजों पर वसंत दस्तक सी देने लगता है और मन कभी गेंदे के फूलों की तरह,तो कभी सरसों के फूलों की तरह खिल उठता है, खिल उठती है अंतरात्मा, गुनगुनाने लगता है मौसम, पिया वसंती रे...। दरअसल वसंत, फागुन की ही भूमिका है और इस भूमिका से हम सबकी भूमिकाएं अपनी अपनी तरह से जुड़ जाती हैं और हमारी रहगुज़र ही फूलों की घाटी सी खुशबू के बादल उठाने लगती है । भीगने लगते हैं हमारे मन प्राण। एक वासंती आलोक की रेशमी परिधि हमें अपने दायरे में लेने लगती है । पत्ती पत्ती में आंखें उग आती हैं और वो हमें अनुराग भरी आंखों से निहारने लगती हैं, हमारे अन्तर में कुछ पिघलने सा लगता है। एक अलौकिक अनुभूति होती है। ऐसा महसूस होने लगता है कि यह संपूर्ण प्रकृति ही एक कविता हो गई है,जिसे वसंत अपने थरथराते अधरों से बांच रहा है , सुगन्ध की एक नदी सी प्रवहमान हो उठती है, तटों पर उत्सव का कलरव सा छा जाता है।
सचमुच यह ऋतु सरसों के फूलों की पीली हल्दी से नहाई चिट्ठियां ही लिख रही है और ऋतुराज के सिर पर पीली पगड़ी से दिन शोभित होने लगे हैं। प्रियतम के मन में मोतीचूर के लड्डू चूर चूर होकर यानी फूट फूटकर मिठास घोल रहे हैं और ज़िंदगी का ज़ायका ही बदल गया है।
यह केवल ऋतु का बदलना नहीं, हमारे मन का बदलना भी है। एकरस हो गए समय का रस से सराबोर हो जाना भी है। आत्मा तक पैठी ठंड की यह विदा हो जाने की बेला है । पूस की रात बीत चुकी है। शुभ दिन धीरे धीरे कदम आगे बढ़ा रहे हैं। ऊन पर रेशम भारी पड़ रहा है। ऊनी यादों का मौसम जा रहा है, सूती समय आ रहा है। एक कहावत याद आ रही है, माघ तिलातिल बाढ़े, फागुन गोड़ी काढ़े। वास्तव में फागुन गोड़ी काढ़ रहा है, संध्या सुंदरी भी बाल काढ़ रही है। उसके बालों में सिंदूरी कंघा फंसा हुआ है, जैसे दूर दूर तक फैली नदी की लहरों पर पुल कंघे की तरह कसा हुआ है। न चुकने वाली यादों की एक तहसील सी बस रही है, दोहा याद आ रहा है
दूर दूर तक बिछ गई, सरसों मीलों मील
बसते बसते बस गई, यादों की तहसील।।
आमों पर बौर आने शुरू हो गए हैं। कोयलों का स्वर संधान आहट देने लगा है। सब कुछ गुलाबी गुलाबी सा है । फरवरी फरफरा रही है । मटर की मुठ्ठी कस रही है। घरैतिन घुघनी बना रही है। चाय में भी मदिर मदिर मामला सांस ले रहा है। अंशु की कविता याद आ रही है, जिसमें वो कहता है
जाने क्या होता है
उन उंगलियों की मादक छुवन में
कि चाय शराब के आगे खड़ी हो जाती है ।
ऐसा ही कुछ है। कविवर नीरज की आवाज़ कहीं से गूंज रही है
शोखियों में घोला जाए फूलों का शवाब
उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब
होगा वो नशा जो तैयार, वो प्यार है।
वसन्त प्यार का ही मौसम है। भर मुंह कहता है, जो प्यार पा जाए उसका भी भला, जो न पाए उसका भी भला। उसका काम तो प्यार बांटना है, वह तो प्रेम का अग्रदूत है
ऐ इश्क़ कहीं ले चल, ये दैरो हरम छूटें
इन दोनों मकानों में झगड़ा नज़र आता है।
तभी तो कविता के किसान कैलाश गौतम को कहना पड़ता है
लगे फूंकने कान में, बौर गुलाबी शंख
कैसे रहें क़िताब में, हम मयूर के पंख।।
वसंत की कोई भी बात बिना निराला के कैसे पूरी हो सकती है, वह तो हिन्दी कविता के वसन्त हैं। महाप्राण निराला वसन्त पंचमी पर ही अपना जन्मदिन मनाते थे। हमारा शहर इलाहाबाद उनका जन्मदिन भी मनाने जा रहा है। उनकी रची सरस्वती वंदना में गंगा यमुना के बीच लुप्त हुई सरस्वती उजागर होने जा रही है, स्वर फूट रहे हैं
वर दे वीणावादिनि
वर दे
प्रिय स्वतंत्र रव,अमृत मंत्र नव
भारत में भर दे
वर दे! वीणावादिनि वर दे!!
डॉ. फ़िरदौस ख़ान
इस पर हज़रत अमीर ख़ुसरो ने सोचा कि वे भी अपने पीर मुर्शिद, अपने औलिया को पीले फूल देकर ख़ुश करेंगे. फिर क्या था. उन्होंने पीले फूलों के गुलदस्ते बनाए और कुछ पीले फूल अपने साफ़े में भी लगा लिए. फिर वे अपने पीर भाइयों और क़व्वालों को साथ लेकर नाचते-गाते हुए अपने मुर्शिद के पास पहुंच गए. अपने मुरीदों को इस तरह नाचते-गाते देखकर उनके चेहरे पर मुस्कराहट आ गई. और इस तरह बसंत पंचमी के दिन हज़रत अमीर ख़ुसरो को उनकी मनचाही मुराद मिल गई. तब से हज़रत अमीर ख़ुसरो हर साल बसंत पंचमी मनाने लगे.
अमीर ख़ुसरो को सरसों के पीले फूल इतने भाये कि उन्होंने इन पर एक गीत लिखा-
सगन बिन फूल रही सरसों
अम्बवा फूटे, टेसू फूले, कोयल बोले डार-डार
और गोरी करत सिंगार
मलनियां गेंदवा ले आईं कर सों
सगन बिन फूल रही सरसों
तरह तरह के फूल खिलाए
ले गेंदवा हाथन में आए
निज़ामुद्दीन के दरवज़्ज़े पर
आवन कह गए आशिक़ रंग
और बीत गए बरसों
बसंत पंचमी को जश्ने बहारा भी कहा जाता है, क्योंकि बसंत पंचमी बहार के मौसम का पैग़ाम लाती है. सूफ़ियों के लिए बंसत पंचमी का दिन बहुत ख़ास होता है. ख़ानकाहों में बसंत पंचमी मनाई जाती है. बसंत का पीला साफ़ा बांधे मुरीद बसंत के गीत गाते हैं. बसंत पंचमी के दिन मज़ारों पर पीली चादरें चढ़ाई जाती हैं. पीले फूलों की भी चादरें चढ़ाई जाती हैं, पीले फूल चढ़ाए जाते हैं. क़व्वाल पीले साफ़े बांधकर हज़रत अमीर ख़ुसरो के गीत गाते हैं.
आज बसंत मना ले सुहागन
आज बसंत मना ले
अंजन–मंजन कर पिया मोरी
लंबे नेहर लगाए
तू क्या सोवे नींद की माटी
सो जागे तेरे भाग सुहागन
आज बसंत मना ले
ऊंची नार के ऊंचे चितवन
ऐसो दियो है बनाय
शाहे अमीर तोहे देखन को
नैनों से नैना मिलाय
आज बसंत मना ले, सुहागन
आज बसंत मना ले
कहा जाता है कि ख़ानकाहों में बसंत पंचमी मनाने की यह रिवायत हज़रत अमीर ख़ुसरो ने शुरू की थी. हुआ यूं कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह को अपने भांजे हज़रत सैयद नूह के विसाल से बहुत सदमा पहुंचा और वह उदास रहने लगे. हज़रत अमीर ख़ुसरो से अपने मुर्शिद की यह हालत देखी न गई. वे उन्हें ख़ुश करने के जतन करने लगे, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए. एक दिन हज़रत अमीर ख़ुसरो अपने साथियों के साथ कहीं जा रहे थे. नीले आसमान पर सूरज दमक रहा था. उसकी सुनहरी किरनें ज़मीन पर पड़ रही थीं. उन्होंने रास्ते में सरसों के खेत देखे. सरसों के पीले फूल बहती हवा से लहलहा रहे थे. उनकी ख़ूबसूरती हज़रत अमीर ख़ुसरो की निगाहों में बस गई और वे वहीं खड़े होकर फूलों को निहारने लगे. तभी उन्होंने देखा कि एक मंदिर के पास कुछ हिन्दू श्रद्धालु हर्षोल्लास से नाच गा रहे हैं. यह देखकर उन्हें बहुत अच्छा लगा. उन्होंने इस बारे में पूछा तो श्रद्धालुओं ने बताया कि आज बसंत पंचमी है और वे लोग देवी सरस्वती पर पीले फूल चढ़ाने जा रहे हैं, ताकि देवी ख़ुश हो जाए.
आज बसंत मना ले सुहागन
आज बसंत मना ले
अंजन–मंजन कर पिया मोरी
लंबे नेहर लगाए
तू क्या सोवे नींद की माटी
सो जागे तेरे भाग सुहागन
आज बसंत मना ले
ऊंची नार के ऊंचे चितवन
ऐसो दियो है बनाय
शाहे अमीर तोहे देखन को
नैनों से नैना मिलाय
आज बसंत मना ले, सुहागन
आज बसंत मना ले
कहा जाता है कि ख़ानकाहों में बसंत पंचमी मनाने की यह रिवायत हज़रत अमीर ख़ुसरो ने शुरू की थी. हुआ यूं कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह को अपने भांजे हज़रत सैयद नूह के विसाल से बहुत सदमा पहुंचा और वह उदास रहने लगे. हज़रत अमीर ख़ुसरो से अपने मुर्शिद की यह हालत देखी न गई. वे उन्हें ख़ुश करने के जतन करने लगे, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए. एक दिन हज़रत अमीर ख़ुसरो अपने साथियों के साथ कहीं जा रहे थे. नीले आसमान पर सूरज दमक रहा था. उसकी सुनहरी किरनें ज़मीन पर पड़ रही थीं. उन्होंने रास्ते में सरसों के खेत देखे. सरसों के पीले फूल बहती हवा से लहलहा रहे थे. उनकी ख़ूबसूरती हज़रत अमीर ख़ुसरो की निगाहों में बस गई और वे वहीं खड़े होकर फूलों को निहारने लगे. तभी उन्होंने देखा कि एक मंदिर के पास कुछ हिन्दू श्रद्धालु हर्षोल्लास से नाच गा रहे हैं. यह देखकर उन्हें बहुत अच्छा लगा. उन्होंने इस बारे में पूछा तो श्रद्धालुओं ने बताया कि आज बसंत पंचमी है और वे लोग देवी सरस्वती पर पीले फूल चढ़ाने जा रहे हैं, ताकि देवी ख़ुश हो जाए.
इस पर हज़रत अमीर ख़ुसरो ने सोचा कि वे भी अपने पीर मुर्शिद, अपने औलिया को पीले फूल देकर ख़ुश करेंगे. फिर क्या था. उन्होंने पीले फूलों के गुलदस्ते बनाए और कुछ पीले फूल अपने साफ़े में भी लगा लिए. फिर वे अपने पीर भाइयों और क़व्वालों को साथ लेकर नाचते-गाते हुए अपने मुर्शिद के पास पहुंच गए. अपने मुरीदों को इस तरह नाचते-गाते देखकर उनके चेहरे पर मुस्कराहट आ गई. और इस तरह बसंत पंचमी के दिन हज़रत अमीर ख़ुसरो को उनकी मनचाही मुराद मिल गई. तब से हज़रत अमीर ख़ुसरो हर साल बसंत पंचमी मनाने लगे.
अमीर ख़ुसरो को सरसों के पीले फूल इतने भाये कि उन्होंने इन पर एक गीत लिखा-
सगन बिन फूल रही सरसों
अम्बवा फूटे, टेसू फूले, कोयल बोले डार-डार
और गोरी करत सिंगार
मलनियां गेंदवा ले आईं कर सों
सगन बिन फूल रही सरसों
तरह तरह के फूल खिलाए
ले गेंदवा हाथन में आए
निज़ामुद्दीन के दरवज़्ज़े पर
आवन कह गए आशिक़ रंग
और बीत गए बरसों
सगन बिन फूल रही सरसों
ग़ौरतलब है कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह चिश्ती सिलसिले के औलिया हैं. उनकी ख़ानकाह में बंसत पंचमी की शुरुआत होने के बाद दूसरी दरगाहों और ख़ानकाहों में भी बंसत पंचमी बड़ी धूमधाम से मनाई जाने लगी. इस दिन मुशायरों का भी आयोजन किया जाता है, जिनमें शायर बंसत पंचमी पर अपना कलाम पढ़ते हैं.
हिन्दुस्तान के अलावा पड़ौसी देशों पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी बंसत पंचमी को जश्ने बहारा के तौर पर ख़ूब धूमधाम से मनाया जाता है.
(लेखिका स्टार न्यूज़ एजेंसी में सम्पादक हैं)
ग़ौरतलब है कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह चिश्ती सिलसिले के औलिया हैं. उनकी ख़ानकाह में बंसत पंचमी की शुरुआत होने के बाद दूसरी दरगाहों और ख़ानकाहों में भी बंसत पंचमी बड़ी धूमधाम से मनाई जाने लगी. इस दिन मुशायरों का भी आयोजन किया जाता है, जिनमें शायर बंसत पंचमी पर अपना कलाम पढ़ते हैं.
हिन्दुस्तान के अलावा पड़ौसी देशों पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी बंसत पंचमी को जश्ने बहारा के तौर पर ख़ूब धूमधाम से मनाया जाता है.
(लेखिका स्टार न्यूज़ एजेंसी में सम्पादक हैं)
डॉ. फ़िरदौस ख़ान
सूफ़ियों के लिए बंसत पंचमी का दिन बहुत ख़ास होता है. हमारे पीर की ख़ानकाह में बसंत पंचमी मनाई गई. बसंत का साफ़ा बांधे मुरीदों ने बसंत के गीत गाये. हमने भी अपने पीर को मुबारकबाद दी. हमने भी अल सुबह अपने पीर को मुबारकबाद दी और उन्होंने हमेशा की तरह हमें दुआएं दीं.
बसंत पंचमी के दिन मज़ारों पीली चादरें चढ़ाई जाती हैं, पीले फूल चढ़ाए जाते हैं. क़व्वाल पीले साफ़े बांधकर हज़रत अमीर ख़ुसरो के गीत गाते हैं.
कहा जाता है कि यह रिवायत हज़रत अमीर ख़ुसरो ने शुरू की थी. हुआ यूं कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह को अपने भांजे सैयद नूह की मौत से बहुत सदमा पहुंचा और वह उदास रहने लगे. हज़रत अमीर ख़ुसरो से अपने पीर की ये हालत देखी न गई. वह उन्हें ख़ुश करने के जतन करने लगे. एक बार हज़रत अमीर ख़ुसरो अपने साथियों के साथ कहीं जा रहे थे. उन्होंने देखा कि एक मंदिर के पास हिन्दू श्रद्धालु नाच-गा रहे हैं. ये देखकर हज़रत अमीर ख़ुसरो को बहुत अच्छा लगा. उन्होंने इस बारे में मालूमात की कि तो श्रद्धालुओं ने बताया कि आज बसंत पंचमी है और वे लोग देवी सरस्वती पर पीले फूल चढ़ाने जा रहे हैं, ताकि देवी ख़ुश हो जाए.
इस पर हज़रत अमीर ख़ुसरो ने सोचा कि वह भी अपने औलिया को पीले फूल देकर ख़ुश करेंगे. फिर क्या था. उन्होंने पीले फूलों के गुच्छे बनाए और नाचते-गाते हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुंच गए. अपने मुरीद को इस तरह देखकर उनके चेहरे पर मुस्कराहट आ गई. तब से हज़रत अमीर ख़ुसरो बसंत पंचमी मनाने लगे.
सूफ़ियों के लिए बंसत पंचमी का दिन बहुत ख़ास होता है. हमारे पीर की ख़ानकाह में बसंत पंचमी मनाई गई. बसंत का साफ़ा बांधे मुरीदों ने बसंत के गीत गाये. हमने भी अपने पीर को मुबारकबाद दी. हमने भी अल सुबह अपने पीर को मुबारकबाद दी और उन्होंने हमेशा की तरह हमें दुआएं दीं.
बसंत पंचमी के दिन मज़ारों पीली चादरें चढ़ाई जाती हैं, पीले फूल चढ़ाए जाते हैं. क़व्वाल पीले साफ़े बांधकर हज़रत अमीर ख़ुसरो के गीत गाते हैं.
कहा जाता है कि यह रिवायत हज़रत अमीर ख़ुसरो ने शुरू की थी. हुआ यूं कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह को अपने भांजे सैयद नूह की मौत से बहुत सदमा पहुंचा और वह उदास रहने लगे. हज़रत अमीर ख़ुसरो से अपने पीर की ये हालत देखी न गई. वह उन्हें ख़ुश करने के जतन करने लगे. एक बार हज़रत अमीर ख़ुसरो अपने साथियों के साथ कहीं जा रहे थे. उन्होंने देखा कि एक मंदिर के पास हिन्दू श्रद्धालु नाच-गा रहे हैं. ये देखकर हज़रत अमीर ख़ुसरो को बहुत अच्छा लगा. उन्होंने इस बारे में मालूमात की कि तो श्रद्धालुओं ने बताया कि आज बसंत पंचमी है और वे लोग देवी सरस्वती पर पीले फूल चढ़ाने जा रहे हैं, ताकि देवी ख़ुश हो जाए.
इस पर हज़रत अमीर ख़ुसरो ने सोचा कि वह भी अपने औलिया को पीले फूल देकर ख़ुश करेंगे. फिर क्या था. उन्होंने पीले फूलों के गुच्छे बनाए और नाचते-गाते हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुंच गए. अपने मुरीद को इस तरह देखकर उनके चेहरे पर मुस्कराहट आ गई. तब से हज़रत अमीर ख़ुसरो बसंत पंचमी मनाने लगे.
डॉ. फ़िरदौस ख़ान
मानव सभ्यता में रंगों का काफ़ी महत्व रहा है. हर सभ्यता ने रंगों को अपने तरीक़े से अपनाया. दुनिया में रंगों के इस्तेमाल को जानना भी बेहद दिलचस्प है. कई सभ्यताओं को उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले रंगों की वजह से ही पहचाना गया. विक्टोरियन काल में ज़्यादातर लोग काला या स्लेटी रंग इस्तेमाल करते थे. एक तरह से ये रंग इनकी पहचान थे. फ़िरऔन हमेशा काले कपड़े पहनता था. वैसे भी हर रंग के अपने सकारात्मक और नकारात्मक असर होते हैं. इसलिए यह नहीं कर सकते कि काला रंग हमेशा बुरा ही होता है. हालांकि कई सभ्यताओं में इसे शोक का रंग माना जाता है. शिया मोहर्रम के दिनों में ज़्यादातर काले कपड़े ही पहनते हैं. विरोध जताने के लिए भी काले रंग का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे काले झंडे दिखाना, सर पर काला कपड़ा या काली पट्टी बांध लेना. ऐसा इस्लामी देशों में ज़्यादा होता है, लेकिन अब भारत में भी इस तरह विरोध जताया जाने लगा है, विशेषकर बाबरी मस्जिद की शहादत की बरसी यानी छह दिसंबर को मुस्लिम समुदाय के लोग काली पट्टी बांधकर ही अपना विरोध ज़ाहिर करते हैं.
महान दार्शनिक अरस्तु ने 4 ईसा पूर्व में नीले और पीले रंगों की गिनती शुरुआती रंगों में की. उन्होंने इसकी तुलना प्राकृतिक वस्तुओं से की, जैसे सूरज-चांद और दिन-रात आदि. उस वक़्त ज़्यादातर कलाकारों ने उनके सिद्धांत को माना और तक़रीबन दो हज़ार साल तक इसका असर देखने को मिला. इसी बीच मेडिकल प्रेक्टि्स के पितामाह कहे जाने वाले 11वीं शताब्दी के ईरान के चिकित्सा विशेषज्ञ हिप्पोकेट्स ने अरस्तु के सिद्धांत से अलग एक नया सिद्धांत पेश किया. उन्होंने रंगों का इस्तेमाल दवा के तौर पर किया और इसे इलाज के लिए बेहतर ज़रिया क़रार दिया. उनका मानना था कि सफ़ेद फूल और वॉयलेट फूल के अलग-अलग असर होते हैं. उन्होंने एक और सिद्धांत दिया, जिसके मुताबिक़ हर व्यक्ति की त्वचा के रंग से भी उसकी बीमारी का पता लगाया जा सकता है और रंगों के ज़रिये ही इसका इलाज भी मुमकिन है. उन्होंने इसका ख़ूब इस्तेमाल भी किया.
15वीं शताब्दी में स्विट्जरलैंड के चिकित्सक वॉन होहेनहैम ने ह्यूमन स्टडी पर काफ़ी शोध किया, लेकिन उनके तरीक़े हमेशा विवादों में रहे. उन्होंने ज़ख्म भरने के लिए रंगों का इस्तेमाल किया. 17-18वीं शताब्दी में न्यूटन के सिद्धांत ने अरस्तु के विशेष रंगों को सामान्य रंगों में बदल दिया. 1672 में न्यूटन ने रंगों पर अपना पहला परचा पेश किया. यह काफ़ी विवादों में रहा, क्योंकि अरस्तु के सिद्धांत के बाद इसे स्वीकार करना इतना आसान नहीं था. रंगों के विज्ञान पर काम करने वाले लोगों में जॉन्स वॉल्फगैंग वॉन गौथे भी शामिल थे. उन्होंने न्यूटन के सिद्धांत को पूरी तरह नकारते हुए थ्योरी ऑफ कलर पेश की. उनके सिद्धांत अरस्तु की थ्योरी से मिलते जुलते थे. उन्होंने कहा कि अंधेरे में से सबसे पहले नीला रंग निकलता है, वहीं सुबह के उगते हुए सूरज की किरणों से पीला रंग सामने आता है. नीला रंग गहरे रंगों का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि पीला रंग हल्के रंगों का. 19वीं शताब्दी में कलर थैरेपी का असर कम हुआ, लेकिन इसके बाद 20वीं शताब्दी में यह नए रूप में सामने आया. आज भी कई चिकित्सक कलर थैरेपी को इलाज का अच्छा ज़रिया मानते हैं और इससे अनेक बीमारियों का उपचार भी करते हैं. आयुर्वेद चिकित्सा में भी रंगों का विशेष महत्व है. रंग चिकित्सा के मुताबिक़ शरीर में रंगों के असंतुलन के कारण ही बीमारियां पैदा होती हैं. रंगों का समायोजन ठीक करके बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है. ऑस्टवाल्ड ने आठ आदर्श रंगों को विशेष क्रम में संयोजित किया. इस चक्र को ऑस्टवाल्ड वर्ण कहा जाता है. इसमें पीला, नारंगी, लाल, बैंगनी, नीला, आसमानी, समुद्री हरा और हरा रंग शामिल है. 60 के दशक में एंथ्रोपॉलिजिस्ट्स केन ने रंगों पर अध्ययन किया. उनके मुताबिक़ सभी सभ्यताओं ने रंगों को दो वर्गों में बांटा-पहला हल्के रंग और दूसरा गहरे रंग.
कौन-सा रंग क्या कहता है?
मूल रूप से इंद्रधनुष के सात रंगों को ही रंगों का जनक माना जाता है. ये सात रंग हैं लाल, नारंगी, पीला, हरा, आसमानी, नीला और बैंगनी. लाल रंग को रक्त रंग भी कहते हैं, क्योंकि ख़ून का रंग लाल होता है. यह शक्ति का प्रतीक है, जो जीने की इच्छाशक्ति और अभिलाषा को बढ़ाता है. यह प्रकाश का संयोजी प्राथमिक रंग है, जो क्यान रंग का संपूरक है. यह रंग क्रोध और हिंसा को भी दर्शाता है. हरा रंग प्रकृति से जुड़ा है. यह ख़ुशहाली का प्रतीक है. हमारे जीवन में इसका बहुत महत्व है. यह प्राथमिक रंग है. हरे रंग में ऑक्सीजन, एल्यूमीनियम, क्रोमियम, सोडियम, कैल्शियम, निकिल आदि होते हैं. इस्लाम में इसे पवित्र रंग माना जाता है. नीला रंग आसमान का रंग है. यह विशालता का प्रतीक है. भारत का क्रीड़ा रंग भी नीला ही है. यह धर्मनिरपेक्षता का भी प्रतीक है. यह एक संयोजी प्राथमिक रंग है. इसका संपूरक रंग पीला है. गहरा नीला रंग अवसाद और निराशा को भी प्रकट करता है. पीला रंग ख़ुशी और रंगीन मिज़ाजी को दर्शाता है. यह आत्मविश्वास बढ़ाता है. यह वैराग्य से भी संबंधित है. हिंदू धर्म में इसका विशेष महत्व है. विष्णु और कृष्ण को यह रंग प्रिय है. बसंत पंचमी तो इसी रंग से जुड़ा पर्व है. डल पीला रंग ईर्ष्या को दर्शाता है. स़फेद रंग पवित्रता और निर्मलता का प्रतीक माना जाता है. यह शांति और सुरक्षा का भाव पैदा करता है. यह अकेलेपन को भी प्रकट करता है. काला रंग रहस्य का प्रतीक है. यह बदलाव से रोकता है. यह नकारात्मकता को भी दर्शाता है.
सरफ़राज़ ख़ान
टोटकों का चलन
पुराना और अंधविश्वास से जुडा है. मगर हैरत की बात तो यह भी है कि अनेक विश्व
विख्यात लेखक भी इन पर यक़ीन करते थे और लेखन के समय इनका नियमित रूप से पालन करते थे,
जो बाद में उनकी आदत में शुमार भी हो
गया. महान फ्रांसीसी लेखक एलेक्जेंडर डयूमा का विचार था कि सभी प्रकार की रचनाएं
एक ही रंग के काग़ज़ पर नहीं लिखनी चाहिए. उनके मुताबिक़ उपन्यास आसमानी रंग के
काग़ज़ पर और अन्य रचनाएं गुलाबी रंग के काग़ज़ पर लिखनी चाहिए.
मगर प्रख्यात हिन्दी लेखक रांगेय राघव को फुलस्केप आकार का काग़ज़ भी बेहद छोटा लगता था. ब्राह्म ग्रीन बलकभ साफ़ लकीरदार वाले काग़ज़ पर लिखते थे. अगर उस पर ज़रा-सा भी कोई धब्बा लग जाता था, तो वे उसे फ़ौरन फाड़ देते थे और फिर नए साफ़ काग़ज़ पर लिखना शुरू करते थे. उनका यह भी मानना था कि जब वे ख़ुद को उदास महसूस करते थे और डेस्क पर बैठते, तो शब्द झरने की तरह फूट पड़ते थे. उदासी भरा दिन उनके लेखन के लिए बेहद कारगर साबित होता था.
इसी तरह चार्ल्स आउडिलायर (1821-1867) नामक फ्रेंच कवि को हरा रंग लिखने की प्रेरणा देता था. इसलिए उन्होंने अपने बाल ही हरे रंग में रंग डाले थे. प्रख्यात समीक्षक डॉ. सैम्युअल जॉन्सन अपनी पालतू बिल्ली लिली को मेज़ पर बिठाकर ही लिख पाते थे. गार्डन सेल्फ़िज़ शनिवार को दोपहर में और शेष दिनों में रात के समय लिखते थे. शनिवार को दोपहर में वह ख़ुद को विशेष उत्साहित महसूस करते थे.
विख्यात अंग्रेज़ी उपन्यासकार और समीक्षक मैक्स पैंबर सिर्फ़ सुबह दस बजे तक ही लिखते थे. इसलिए एक उपन्यास को पूरा करने में उन्हें बहुत ज़्यादा समय लगता था. इटली के लेखक जियो ऑक्चिनी रौसिनी (1791-1868) लिखने का मूड बनाने के लिए हमेशा नक़ली बालों की तीन विग पहना करते थे. प्रसिद्ध जर्मन कवि फेडरिक वान शिल्लर (1759-1805) की आदत भी कम अजीब नहीं थी. वे अपने पैरों को बर्फ़ के पानी में डुबोकर ही कविताएं लिख सकते थे. अगर वे ऐसा नहीं करते थे, तो उन्हें कविता का एक भी शब्द नहीं सूझता था.
फ्रांसीसी भाषा के सुप्रसिद्ध साहित्यकार तथा रमणी रसिक चिरकुमार मोंपासा मूड फ्रैश होने पर ही लिखते थे. अपने को तरोताज़ा करने के लिए वे नाव चलाते, मछलियां पकड़ते या फिर मित्रों के साथ हंसी-ठिठौली करते थे. राइज एंड फास्स ऑफ रोमन एंपायर के लेखक नाटककार गिब्सन को लिखने के लिए पहले एकाएक संजीदा होना पड़ता था. महान फ्रांसीसी लेखक बाल्लाजाक की आदत भी विचित्र थी. वह दिन में फैशन के कपड़े पहनते और रात को लिखते समय पादरियों जैसा लिबास पहनते थे.
सुप्रसिद्ध लेखक बर्टेड रसेल का अपनी लेखन प्रक्रिया के बारे में कहना था कि उनका लेखन मौसम पर ही आधारित होता है खु़शगवार मौसम में वे रात-दिन लिखते थे और गर्मी वाले उमस भरे दिन में वे लिखने से कतराते थे. एईडब्ल्यू मेसन भी मूडी स्वभाव के थे. जब उनका मन करता, तभी लिखने बैठते. वे रात या दिन मूड होने पर कभी भी लिख सकते थे.
गोल्जस्मिथ को लिखने से पहले सैर करने का भी शौक़ था. अपने उपन्यास, कविताएं और नाटक रचने के दौरान उन्होंने दूर-दराज़ के इलाक़ों की यात्राएं कीं. गिलबर्टफ़्रेंको सुबह नौ बजे से दोपहर दो बजे तक लिखा करते थे. दोपहर के भोजन के बाद एक घंटे लिखते थे और फिर वह शाम को भी दो घंटे तक लिखते थे. रात को लिखना उन्हें ज़रा भी पसंद नहीं था. सर ऑर्थर पिनेरी को केवल रात में ही लिखना पसंद था. दिन में अगर वे लिखने बैठते, तो उन्हें कुछ सूझता ही नहीं था. इसी तरह की आदत लुई पार्कर को भी थी. वे दिनभर सोते और रात को जागकर लिखते थे. अमेरिकी लेखक मार्क ट्वेन को औंधे मुंह लेटकर लिखने की अजीब आदत थी.
अर्नेस्ट हेमिंगवे फ्रांस के क्रांतिकारी लेखक विक्टर ह्यूमो और पंजाबी के उपन्यासकार नानक सिंह को खड़े होकर लिखने की आदत थी. विस्मयली लैक्स सुबह चार बजे से दिन के 11 बजे तक और शाम को साढ़े सात बजे तक तथा रात को फिर 11 बजे तक लिखते थे. उनका बाक़ी का समय सोने और चाय पीने में बीतता था. प्रख्यात रूसी लेखक फीडिन ने जब उपन्यास असाधारण ग्रीष्म ऋतु लिखा, तब वह समुद्र किनारे रह रहे थे. उनका मानना था कि समुद्र की लहरों की गूंज की आवाज़ उन्हें निरंतर लिखने के लिए प्रेरित करती थी.
हैरसवासिल सुबह नौ बजे से दोपहर 12 बजे तक और शाम को पांच बजे से सात बजे तक लिखते थे. डेलिस ब्रेडकी केवल तीन घंटे ही लिखते थे और वह भी सुबह 11 बजे से दोपहर दो बजे तक. सर ऑर्थर कान डायल केवल सुकून महसूस करने पर ही लिखते थे. अगर किसी बात से उनका मन जरा भी विचलित होता, तो वे एक पंक्ति भी नहीं लिख पाते थे. जर्मनी के कार्लबेन को लिखने की प्रेरणा संगीत से मिलती थी. उन्होंने अपनी पसंद के गाने रिकॉर्ड कर रखे थे. पहले वे टेप चलाते और फिर लिखने बैठते.
मगर प्रख्यात हिन्दी लेखक रांगेय राघव को फुलस्केप आकार का काग़ज़ भी बेहद छोटा लगता था. ब्राह्म ग्रीन बलकभ साफ़ लकीरदार वाले काग़ज़ पर लिखते थे. अगर उस पर ज़रा-सा भी कोई धब्बा लग जाता था, तो वे उसे फ़ौरन फाड़ देते थे और फिर नए साफ़ काग़ज़ पर लिखना शुरू करते थे. उनका यह भी मानना था कि जब वे ख़ुद को उदास महसूस करते थे और डेस्क पर बैठते, तो शब्द झरने की तरह फूट पड़ते थे. उदासी भरा दिन उनके लेखन के लिए बेहद कारगर साबित होता था.
इसी तरह चार्ल्स आउडिलायर (1821-1867) नामक फ्रेंच कवि को हरा रंग लिखने की प्रेरणा देता था. इसलिए उन्होंने अपने बाल ही हरे रंग में रंग डाले थे. प्रख्यात समीक्षक डॉ. सैम्युअल जॉन्सन अपनी पालतू बिल्ली लिली को मेज़ पर बिठाकर ही लिख पाते थे. गार्डन सेल्फ़िज़ शनिवार को दोपहर में और शेष दिनों में रात के समय लिखते थे. शनिवार को दोपहर में वह ख़ुद को विशेष उत्साहित महसूस करते थे.
विख्यात अंग्रेज़ी उपन्यासकार और समीक्षक मैक्स पैंबर सिर्फ़ सुबह दस बजे तक ही लिखते थे. इसलिए एक उपन्यास को पूरा करने में उन्हें बहुत ज़्यादा समय लगता था. इटली के लेखक जियो ऑक्चिनी रौसिनी (1791-1868) लिखने का मूड बनाने के लिए हमेशा नक़ली बालों की तीन विग पहना करते थे. प्रसिद्ध जर्मन कवि फेडरिक वान शिल्लर (1759-1805) की आदत भी कम अजीब नहीं थी. वे अपने पैरों को बर्फ़ के पानी में डुबोकर ही कविताएं लिख सकते थे. अगर वे ऐसा नहीं करते थे, तो उन्हें कविता का एक भी शब्द नहीं सूझता था.
फ्रांसीसी भाषा के सुप्रसिद्ध साहित्यकार तथा रमणी रसिक चिरकुमार मोंपासा मूड फ्रैश होने पर ही लिखते थे. अपने को तरोताज़ा करने के लिए वे नाव चलाते, मछलियां पकड़ते या फिर मित्रों के साथ हंसी-ठिठौली करते थे. राइज एंड फास्स ऑफ रोमन एंपायर के लेखक नाटककार गिब्सन को लिखने के लिए पहले एकाएक संजीदा होना पड़ता था. महान फ्रांसीसी लेखक बाल्लाजाक की आदत भी विचित्र थी. वह दिन में फैशन के कपड़े पहनते और रात को लिखते समय पादरियों जैसा लिबास पहनते थे.
सुप्रसिद्ध लेखक बर्टेड रसेल का अपनी लेखन प्रक्रिया के बारे में कहना था कि उनका लेखन मौसम पर ही आधारित होता है खु़शगवार मौसम में वे रात-दिन लिखते थे और गर्मी वाले उमस भरे दिन में वे लिखने से कतराते थे. एईडब्ल्यू मेसन भी मूडी स्वभाव के थे. जब उनका मन करता, तभी लिखने बैठते. वे रात या दिन मूड होने पर कभी भी लिख सकते थे.
गोल्जस्मिथ को लिखने से पहले सैर करने का भी शौक़ था. अपने उपन्यास, कविताएं और नाटक रचने के दौरान उन्होंने दूर-दराज़ के इलाक़ों की यात्राएं कीं. गिलबर्टफ़्रेंको सुबह नौ बजे से दोपहर दो बजे तक लिखा करते थे. दोपहर के भोजन के बाद एक घंटे लिखते थे और फिर वह शाम को भी दो घंटे तक लिखते थे. रात को लिखना उन्हें ज़रा भी पसंद नहीं था. सर ऑर्थर पिनेरी को केवल रात में ही लिखना पसंद था. दिन में अगर वे लिखने बैठते, तो उन्हें कुछ सूझता ही नहीं था. इसी तरह की आदत लुई पार्कर को भी थी. वे दिनभर सोते और रात को जागकर लिखते थे. अमेरिकी लेखक मार्क ट्वेन को औंधे मुंह लेटकर लिखने की अजीब आदत थी.
अर्नेस्ट हेमिंगवे फ्रांस के क्रांतिकारी लेखक विक्टर ह्यूमो और पंजाबी के उपन्यासकार नानक सिंह को खड़े होकर लिखने की आदत थी. विस्मयली लैक्स सुबह चार बजे से दिन के 11 बजे तक और शाम को साढ़े सात बजे तक तथा रात को फिर 11 बजे तक लिखते थे. उनका बाक़ी का समय सोने और चाय पीने में बीतता था. प्रख्यात रूसी लेखक फीडिन ने जब उपन्यास असाधारण ग्रीष्म ऋतु लिखा, तब वह समुद्र किनारे रह रहे थे. उनका मानना था कि समुद्र की लहरों की गूंज की आवाज़ उन्हें निरंतर लिखने के लिए प्रेरित करती थी.
हैरसवासिल सुबह नौ बजे से दोपहर 12 बजे तक और शाम को पांच बजे से सात बजे तक लिखते थे. डेलिस ब्रेडकी केवल तीन घंटे ही लिखते थे और वह भी सुबह 11 बजे से दोपहर दो बजे तक. सर ऑर्थर कान डायल केवल सुकून महसूस करने पर ही लिखते थे. अगर किसी बात से उनका मन जरा भी विचलित होता, तो वे एक पंक्ति भी नहीं लिख पाते थे. जर्मनी के कार्लबेन को लिखने की प्रेरणा संगीत से मिलती थी. उन्होंने अपनी पसंद के गाने रिकॉर्ड कर रखे थे. पहले वे टेप चलाते और फिर लिखने बैठते.
डॉ. फ़िरदौस ख़ान
सीमाप्रांत और बलूचिस्तान के महान राजनेता ख़ान अब्दुल ग़फ़्फ़ार ख़ान का हरियाणा के फ़रीदाबाद से गहरा रिश्ता है. दरअसल आज के नये औद्योगिक शहर फ़रीदाबाद के विकास की बुनियाद ख़ान अब्दुल ग़फ़्फ़ार ख़ान ने ही रखी थी और इसे परवान चढ़ाने में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की भी अहम भूमिका थी.
हुआ यूं कि देश के बंटवारे के वक़्त उत्तर-पश्चिमी सीमांत प्रांत के बन्नू, डेरा इस्माइल ख़ान, कोहाट, हज़ारा, मरदान और पेशावर आदि ज़िलों के तक़रीबन 50 हज़ार लोग उजड़कर आशियाने की तलाश में हिन्दुस्तान आ गए. इनमें से ज़्यादातर लोगों ने हरियाणा के ऐतिहासिक नगर कुरुक्षेत्र में पनाह ली. यहां वे शरणार्थी शिविरों में रहने लगे. चूंकि ये लोग ख़ान अब्दुल ग़फ़्फ़ार ख़ान के समर्थक थे, इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ख़ुद उनका ख़्याल रखा करते थे. कहा जाता है कि हिन्दुस्तान की हुकूमत उन्हें राजस्थान के अलवर और भरतपुर ज़िलों में बसाना चाहती थी, लेकिन वे लोग दिल्ली के आसपास ही रहना चाहते थे. शायद वे राजस्थान की प्राकृतिक परिस्थितियों में ख़ुद को ढाल पाने में असमर्थ महसूस कर रहे थे. ख़ान अब्दुल ग़फ़्फ़ार ख़ान के ख़ुदाई ख़िदमतगार संगठन के सदस्यों ने एकजुट होकर अपनी मांगों को लेकर धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया. इस प्रदर्शन के ज़रिये वे हुकूमत तक अपनी मांगें पहुंचाना चाहते थे. इन लोगों में कन्हैया, निहाल चंद, सुखराम, पंडित गोबिन्द दास, पंडित अनंत राम, ख़ुशीराम, चौधरी दयालागंद, दुली चौधरी, जेठा नंद और छत्तू राम गेरा आदि शामिल थे. जब उन्होंने देखा कि उनके प्रदर्शन का हुकूमत पर कोई असर नहीं हो रहा है, तो वे जुलाई 1948 में कुरुक्षेत्र छोड़कर दिल्ली चले गए और पुन: स्थापना मंत्रालय के सामने अपना आन्दोलन शुरू कर दिया. इस आन्दोलन के दौरान वे अपनी गिरफ़्तारियां देने लगे. जब आन्दोलन तेज़ होने लगा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रदर्शनकारियों से बात करने के लिए अपने ख़ास सलाहकार मृदुला साराभाई को उनके पास भेजा. उन्होंने प्रदर्शनकारियों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे किसी भी हाल में राजस्थान में बसने के लिए तैयार नहीं हुए. आख़िरकार सरकार को उनके लिए नया शहर बसाने का फ़ैसला लेना पड़ा. पहले कई शहरों के विकास के बारे में सलाह-मशविरा किया गया. फिर बात फ़रीदाबाद पर आकर ख़त्म हुई. इस तरह 17 अक्टूबर 1949 को दिल्ली के क़रीबी राज्य हरियाणा में नये औद्योगिक शहर फ़रीदाबाद की बुनियाद रखी गई.
डॉ. मुनीश परवेज़ बताते हैं कि प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फ़रीदाबाद के विकास में ख़ास दिलचस्पी ली. फ़रीदाबाद के विकास के लिए उन्होंने कैबिनेट मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई और फ़रीदाबाद विकास बोर्ड के गठन को मंज़ूरी दी. उन्होंने देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया और महात्मा गांधी के क़रीबी सुधीर घोष को बोर्ड के मुख्य प्रशासक की ज़िम्मेदारी सौंपी गई. बोर्ड की ख़ास बात यह भी थी कि प्रधानमंत्री ख़ुद इसके आमंत्रित सदस्य थे और उन्होंने बोर्ड की कुल 24 बैठकों में से 21 में शिरकत की, ताकि इसके काम पर निगरानी रख सकें. इसका असर ये हुआ कि काम तयशुदा वक़्त यानी अढाई साल में पूरा हो गया और लागत भी इसके लिए जारी की गई रक़म पांच करोड़ से कम यानी 4.64 करोड़ रुपये आई. बोर्ड ने बाक़ी रक़म सरकार को वापस लौटा दी. उस वक़्त बोर्ड ने 5196 मकान बनाने का फ़ैसला किया था. ये सभी मकान 233 वर्ग गज़ के थे. मकान की क़ीमत बहुत ही वाजिब रखी गई और लोगों को मामूली मासिक क़िस्तों पर मकान दिए गए. शहर को पांच हिस्सों में तक़सीम किया गया. इसके अलावा शहर में सड़कें, विद्यालय, स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल, सिनेमाघर, पावर हाउस, वाटर वर्क्स और एक औद्योगिक क्षेत्र बनाया गया. यहां इन लोगों को रहने के लिए मकान मिले और रोज़गार मिला. इस तरह सरकार ने शरणार्थियों को रोटी, कपड़ा और मकान दिया. शहर दिनोदिन तरक़्क़ी करने लगा. आज फ़रीदाबाद औद्योगिक शहर किसी परिचय का मोहताज नहीं है. क़ाबिले-ग़ौर है कि बादशाह जहांगीर के ख़ज़ांची शेख़ फ़रीद ने इस शहर को बसाया था. उन्होंने यहां एक क़िला, एक तालाब और एक मस्जिद बनवाई थी. उन्हीं के नाम पर इस शहर का नाम फ़रीदाबाद पड़ा.
स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रहे एलसी जैन ने ख़ान अब्दुल ग़फ़्फ़ार ख़ान के फ़रीदाबाद से रिश्ते को लेकर 330 पृष्ठों की एक पुस्तक लिखी है- द सिटी ऑफ़ होप : द फ़रीदाबाद स्टोरी. साल 1998 में प्रकाशित इस पुस्तक में जैन दावा करते हैं कि फ़रीदाबाद में विस्थापितों को बसाने के लिए देश का यह पहला प्रयोग था. लेखक ने शहर बसाने से लेकर इसके औद्योगीकरण को बहुत क़रीब से देखा है. उन्हें उम्मीद है कि उम्मीदों का यह शहर किसी न किसी दिन बहुत ऊंचाइयों को छुएगा. हालांकि हाल के दिनों में शहर की स्थिति बदतर ही हुई है.
ग़ौरतलब है कि ख़ान अब्दुल ग़फ़्फ़ार ख़ान का जन्म 6 फ़रवरी 1890 को पेशावर में हुआ था। उन्होंने अपनी ज़िन्दगी का एक बड़ा हिस्सा जेल में बिताया. उन्होंने हिन्दुस्तान की सरज़मीन को अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद कराने की मुहिम में बढ़-चढ़कर शिरकत की थी. जंगे-आज़ादी में वे महात्मा गांधी के साथ थे. वे भी महात्मा गांधी की तरह अहिंसा के हिमायती थे. महात्मा गांधी उनके विचारों और उनकी निष्ठा के क़ायल थे. महात्मा गांधी उनके बारे में लिखते हैं- “वह तो असंदिग्ध रूप से ईश्वर-भीरू पुरुष हैं. उनकी प्रतिरक्षण की अखंड उपस्थिति में उनकी परम श्रद्धा है और वह बख़ूबी जानते हैं कि उनका आन्दोलन तभी प्रगति करेगा जब ईश्वर की वैसी इच्छा होगी. ईश्वर के इस कार्य में अपनी सारी आत्मा को उड़ेलकर परिणाम की वह बहुत ज़्यादा फ़िक्र नहीं करते.”
ख़ान अब्दुल ग़फ़्फ़ार ख़ान ने साल 1929 में ख़ुदाई ख़िदमतगार नाम के संगठन की स्थापना की थी. इस संगठन को सुर्ख़ पोश यानी लाल कुर्ती दल के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि इसके सदस्य लाल कुर्ती पहनते थे, जो क़ुर्बानी का प्रतीक थी. उन्होंने उत्तर-पश्चिम सीमा प्रांत में जातीय समूहों ख़ासकर पठानों को एकजुट करके ब्रिटिश हुकूमत के ख़िलाफ़ एक अहिंसक आंदोलन चलाया था. इसीलिए उन्हें सरहदी गांधी या सीमान्त गांधी भी कहा जाता है. उन्हें बच्चा ख़ान और बादशाह ख़ान भी कहा जाता है.
उन्होंने हमेशा देश के बंटवारे का विरोध किया. वे मुस्लिम लीग द्वारा की जाने वाली देश के बंटवारे की मांग के सख़्त ख़िलाफ़ थे. लेकिन जब कांग्रेस ने देश का बंटवारा क़ुबूल कर लिया, तो उन्हें बहुत दुख हुआ. बंटवारे के बाद उन्होंने अपनी जन्मभूमि पेशावर में ही रहने का फ़ैसला किया. उन्होंने पख़्तूनों के हक़ की लड़ाई जारी रखी. उन्होंने पाकिस्तान हुकूमत से पख़्तूनों के लिए अलग पख़्तूनिस्तान की मांग की, जिससे वहां की हुकूमत उनके ख़िलाफ़ हो गई और उन पर नज़र रखी जाने लगी. साल 1988 में पाकिस्तान हुकूमत ने उन्हें उनके घर में ही नज़रबंद कर दिया. उसी दौरान 20 जनवरी 1988 को उनकी मौत हो गई. ताउम्र उन्हें बंटवारे का दुख रहा. वे एकता और अखंडता के हिमायती थे. साल 1987 में भारत सरकार ने उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ‘भारत रत्न’ से नवाज़ा था. वे पहले ग़ैर भारतीय थे, जिन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया.
क़ाबिले-ग़ौर है कि प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 5 जून 1951 को फ़रीदाबाद में शरणार्थियों के लिए एक अस्पताल बनवाया था. उन्होंने इस अस्पताल का नाम ख़ान अब्दुल ग़फ़्फ़ार ख़ान के नाम पर बादशाह ख़ान अस्पताल रखा था. साल 2020 में हरियाणा सरकार ने इसका नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी सामान्य अस्पताल कर दिया. भले ही सरकार ने अस्पताल का नाम बदल दिया है, लेकिन बादशाह ख़ान अपने उत्कृष्ट कार्यों की बदौलत लोगों के दिलों में हमेशा ज़िन्दा रहेंगे.
महात्मा गांधी के पौत्र राजमोहन गांधी ने ख़ान अब्दुल ग़फ़्फ़ार ख़ान पर एक किताब लिखी है, जिसका नाम है ‘ग़फ़्फ़ार ख़ान: नॉनवाइलेंट बादशाह ऑफ़ द पख़्तूंस’. किताब के लेखक राजमोहन गांधी का कहना है कि महात्मा गांधी ख़ान अब्दुल ग़फ़्फ़ार ख़ान को अपना भाई मानते थे, लेकिन भारत ने उन्हें भुला दिया है. अपनी किताब का ज़िक्र करते हुए वे कहते हैं कि हर किताब की एक यात्रा और इतिहास होता है। मेरी इस किताब की शुरुआत तबसे होती है जब मैं 10 साल का था. मेरे पिताजी गांधीजी के चौथे बेटे देवदास गांधी दिल्ली में हिन्दुस्तान टाइम्स के संपादक थे. उस समय बादशाह ख़ान हमारे घर दो बार रुके. तब से मेरा उनसे संबंध रहा. 1969 में उनका एक ज़बरदस्त भाषण हुआ, जिसमें उन्होंने ग़रीबी, भ्रष्टाचार और नागरिक अधिकारों के हनन पर बहुत प्रभावी बातें कही थीं. फिर 1987 में देहांत से एक साल पहले इलाज के सिलसिले में वह मुंबई आए थे, तब भी कुछ बातें हुई थीं. 2001 में मैं पाकिस्तान गया और असफंदयार ख़ान, जो बादशाह ख़ान के पोते हैं, उनसे मिला. उन्होंने मुझसे कहा कि बहुत अफ़सोस है कि कोई अच्छी बायोग्राफ़ी बादशाह ख़ान की नहीं है. तब मुझे लगा कि मुझे उन पर काम करना चाहिए. उन पर बहुत दस्तावेज़ मौजूद नहीं थे, लेकिन अमेरिका के इलिनॉय विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में मुझे उनकी लिखी आत्मकथा मिल गई. उससे भी मुझे इस किताब को लिखने में मदद मिली. एक और चीज़ मैं बताना चाहूंगा, मेरे पिताजी जब 30-31 साल के थे, तब वे दोनों जेल में साथ ही रहे थे. उन दोनों का जो संबंध था, उसकी भी मेरे किताब लिखने के पीछे एक भूमिका है. जिस उद्देश्य के लिए उन्होंने अपना जीवन जिया, उनमें निर्भीकता, त्याग, तकलीफ़ के लिए तैयार रहना और अहिंसा प्रमुख है. दुनिया में जेल में लंबे समय तक रहने का उनका रिकॉर्ड है. 1987 में उनके देहांत से एक साल पहले उनसे मैं मिला, तो उन्होंने कहा कि क़ुरान में जो एक शब्द सबसे ज़्यादा है- सब्र, सब्र करो. बादशाह ख़ान की राय में अहिंसा और धैर्य का एक-दूसरे से ज़बरदस्त संबंध है.
(लेखिका स्टार न्यूज़ एजेंसी में सम्पादक हैं)
साभार आवाज़
तस्वीर गूगल
विनय अंजू कुमार
रहस्य रोमांच की कहानियाँ या उपन्यास मैंने बहुत कम पढ़ा है, लेकिन किश्वर अंजुम जी का कहानी संग्रह “परछाइयाँ अंधेरों की” दो दिन पहले मँगवाया था और आज पढ़कर समाप्त किया. मैंने पहले भी किश्वर जी को पढ़ा है और इनकी भाषा मुझे बहुत प्रभावित करती है, ख़ासकर इनके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले उर्दू ज़बान के शब्द. वैसे मुझे जाती तौर पर पारलौकिक ताक़तों या मृत्योपरांत जीवन में कोई यक़ीन नहीं होता है लेकिन कहानियाँ तो कल्पना की उड़ान ही होती हैं और इन कहानियों को भी इसी नज़रिए से मैंने पढ़ा.
संग्रह में कुल 15 कहानियाँ हैं और सब रहस्य, रोमांच से भरपूर हैं. हम लोगों ने भी अपने बचपन से लेकर आज तक तमाम ऐसे क़िस्से सुने हैं जिनपे यक़ीन नहीं होता है लेकिन चूँकि उनका कोई तात्कालिक उत्तर नहीं होता तो ऐसे क़िस्से चकित कर देते हैं. बहरहाल अगर कहानियों की बात करें तो पहली कहानी “संयोग” सच्चाई के क़रीब है क्योंकि ऐसा संयोग बहुतेरे लोगों के साथ घटता है. दूसरी कहानी “पच्चीस कलदार” हमको पुराने समय में ले जाती है और बहुत कमाल की कल्पना है इसमें. “चिड़िया” बहुत भावपूर्ण कहानी है और माँ की बच्चों के लिए ममता का सजीव चित्रण करती है. “मैकी मास्टर” ने भी बहुत प्रभावित किया और अंत ने चकित कर दिया. “पोस्टमार्टम” पढ़कर मन अजीब सा हो गया और “केर घाटी” बहुत दिलचस्प लगी और कुछ क़िस्से हमें भी याद आ गए.
“कोयला” और “दामिश एक इफरीत” अलग स्तर की कहानियाँ हैं जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था. “बू”, “लौ”, “आग” सभी कहानियों में रहस्य भी है और रोमांच भी. कुल मिलाकर बहुत बेहतरीन किस्सागोई है इन कहानियों में और भाषा शैली के चलते पढ़ने का आनंद दोगुना हो जाता है.
आ किश्वर जी को बहुत बहुत बधाई इस कहानी संग्रह के लिए और भविष्य के लिए शुभकामनाएँ. ख़ैर किस्सा मुख्तसर यह है कि अगर आपकी दिलचस्पी रूहानी ताक़तों, रहस्य रोमांच में है तो यकीनन यह किताब आपको मुसलसल तौर पर बहुत पसंद आएगी.
संग्रह शुभदा बुक्स ने प्रकाशित किया है





.jpg)