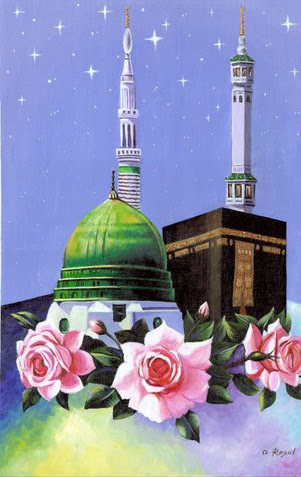डॉ. शीतल कपूर
उपभोक्ता मामलों में आजकल उपभोक्ता कल्याण के सभी पहलू शामिल हैं और इसे हाल में अंतरराष्ट्रीय पहचान भी मिली है। उपभोक्ता सामाजिक-आर्थिक- राजनीतिक प्रणाली का अभिन्न हिस्सा समझा जाता है, जहां क्रेता और विक्रेता के बीच के किसी भी विनिमय एवं लेन-देन का तीसरे पक्ष यानि समाज पर गहरा असर पड़ता है। व्यापक उत्पादन एवं बिक्री में सन्निहित फायदे की मंशा कई विनिर्माताओं एवं डीलरों को उपभोक्ताओं का शोषण करने का अवसर प्रदान करती है। बाजारों का वैश्वीकरण हो रहा है। उपभोक्ताओं पर उत्पादों के ढेरों विकल्प लादे जा रहे हैं, ऐसे में, कौन-सा उत्पाद खरीदा जाए- इस संबंध में निर्णय लेना कठिन होता जा रहा है। इंटरनेट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और एटीएम जैसी नई प्रौद्योगिकियां एक तरफ उपभोक्ता का जीवन आसान बना रही हैं तो दूसरी तरफ वे सुरक्षा और संरक्षण संबंधी चुनौतियां भी खड़ी कर रही हैं। उपभोक्ता के रूप में हमें सही सामान का चुनाव करना है। खरीददारी के दौरान ठगे जाने और मेहनत की गाढी क़माई अदा कर घटिया उत्पाद या सेवा मिलने का डर व जोखिम भी बना रहता है। अतएव, उपभोक्ता की संतुष्टि और सुरक्षा की आवश्यकता को पहचान दी गई। फिलिप कोटलर ने कहा है कि उपभोक्तावाद विक्रेता से संबंध के दौरान क्रेता के अधिकारों और शक्तियों को मजबूती प्रदान करने का एक सामाजिक आंदोलन है। हर उपभोक्ता आजकल अपनी मुद्रा का मूल्य और ऐसा उत्पाद व सेवा चाहता है जो उसकी तर्कसंगत उम्मीदों पर खरी उतरें। इन्हीं उम्मीदों को उपभोक्ता अधिकार कहा जाता है।
उपभोक्ताओं का शोषण
खराब सामान, सेवाओं में त्रुटियां, घटिया और नकली ब्रांड, भ्रामक विज्ञापन जैसी समस्याएं आम हो गयी हैं तथा भोले-भाले उपभोक्ता इनके शिकार हो जाते हैं। ज्यादातर उपभोक्ता, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, अशिक्षित होते हैं और उनमें जागरूकता एवं ज्ञान की कमी होती है। उपभोक्ताओं को सामानों और सेवाओं की खरीददारी के दौरान कई जोखिम उठाने पड़ते हैं।
इसके अलावा, वित्तीय जोखिम भी हैं। उपभोक्ताओं को व्यय की गई राशि का मूल्य नहीं मिल पाता या उनसे ज्यादा पैसे ऐंठ लिये जाते हैं, जिससे वे शोषण के शिकार हो जाते हैं। बीमा पॉलिसी के दावे के निबटान में अनावश्यक देरी, अधिक बिल आने, त्रऽण के दोगुना होने, बिल आने में देरी, पेंशन में देरी, गलत बिलों में सुधार न होना, भ्रामक विज्ञापन, ऑफर में आनाकानी, पऊलैट का मालिकाना हक दिए जाने में देरी, चेक को गलत तरीके से अमान्य करना, बैंक में जमा किये गये चेक का गायब होना, फर्जी हस्ताक्षर वाले चेक, आदि जैसे इसके ढेरों उदाहरण हैं।
ऐसे भी उदाहरण सामने आते हैं जब कंपनियां आकर्षक ब्याज दर या कुछ समय में धन दोगुना करने की स्कीम का भ्रामक विज्ञापन देती हैं। जब वे अच्छी खासी धनराशि एकत्र कर लेती हैं तो अपनी दुकान बंद कर फरार हो जाती हैं। कई बार लोगों को जमीन खरीदने के बाद पता चलता है कि जो जमीन उन्होंने खरीदी है वह या तो पहले से बिकी हुई है या साथ ही किसी और को भी बेची गई है। एक ही पऊलैट एक ही साथ दो-दो लोगों को आबंटित कर दिया जाता है और असली हकदार को लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ती है। इसी तरह, शेयर के लिए आवेदन करने वाले कई बार ऐसी स्थिति में फंस जाते हैं जहां न तो उन्हें शेयर आवंटित होते हैं और न ही रिफंड मिलता है। इनमें से अधिकांश मामलों में उपभोक्ताओं को अपने निवेश या अपनी मेहनत की गाढ़ी बचत के एक बड़े हिस्से से हाथ धोना पड़ता है। उपभोक्ताओं को एटीएम की गड़बड़ी के कारण भी नुकसान उठाना पड़ता है। उपभोक्ता मंत्रालय का इस वर्ष का ध्येय उपभोक्ताओं को वित्तीय साक्षर बनाना है ताकि वे बाजार से गुमराह न हों ।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986
देश में प्रगतिशील कानून लागू करने के मामले में भारत किसी भी देश से पीछे नहीं रहा हह। हमारे देश के इतिहास में 24 दिसम्बर, 1986 को उपभोक्ता आंदोलन का श्री गणेश हुआ। भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति ने इसी दिन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 को स्वीकृति दी थी। इस अधिनियम के फलस्वरूप उपभोक्ता अधिकारों के क्षेत्र में ऐसी क्रांति आई, जिसकी मिसाल इतिहास में शायद कहीं नहीं मिलती। यह अधिनियम उन सभी उत्पादों और सेवाओं पर लागू होता है, जो निजी, सार्वजनिक या सहकारी-किसी भी क्षेत्र से संबंधित हों। केवल केन्द्र सरकार द्वारा विशेष रूप से छूट प्राप्त वस्तुओं या सेवाओं पर यह अधिनियम लागू नहीं होता।
इस अधिनियम में अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत सभी उपभोक्ता कानून निहित हैं। इस अधिनियम के अनुसार, केन्द्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर उपभोक्ता संरक्षण परिषदें कायम की गई हैं। उपभोक्ता अदालत नाम से ऐसी न्यायिक संस्थायें स्थापित की गई हैं, जहां उपभोक्ता की शिकायतों की सुनवाई आसानी से हो जाती है।
उपभोक्ता मार्ग-निर्देश एवं शिक्षा
जागरूक उपभोक्ता किसी भी समाज की एक सम्पत्ति है। कोई भी उपभोक्ता जब बीमा पालिसी लेता है तो उसे छपी हुई जानकारी को सावधानीपूर्वक पढ लेना चाहिए, पालिसी के विवरणों को इकट्ठा कर लेना चाहिए, भरोसेमंद एजेंट से बीमा लेना चाहिए और उससे यह भी पता करना चाहिए कि उक्त पालिसी में बीमा कवर कितना है और दावे को दर्ज करने की प्रक्रिया क्या है।
बैंक ऋण के लिए आवेदन करते समय उपभोक्ता को लिखित जानकारी सावधानीपूर्वक पढ़ लेनी चाहिए, लागू ऋण शर्तों की पुष्टि कर लेनी चाहिए, पुनर्भुगतान और समय सीमा के बारे में भी जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए तथा अन्य ऋण विकल्पों से उसकी तुलना भी कर लेनी चाहिए, चिह्नित प्रभारों की जांच कर लेनी चाहिए, ब्याज की दर और जुर्माने आदि के बारे में दी गई जानकारी के साथ-साथ शर्तों तथा अन्य विवरणों को पूरी तरह पढ़ने और बिल को ठीक से परखने के बाद ही क्रेडिट कार्ड सेवा का ग्राहक बनना चाहिए। बैंकिंग और बीमा से सम्बध्द समस्याओं के समाधान के लिए बैंक लोकपाल सबसे उपयुक्त, स्वतंत्र और निष्पक्ष माध्यम है।
किसी भी व्यक्ति को ऐसे विज्ञापनों के बहकावे में नहीं आना चाहिए जो उपभोक्ताओं के सूचना अधिकारों का उल्लंघन करते हैं और उन्हें वित्तीय हानि और मानसिक दुख पहुंचा सकते हैं। इसलिए रकम को दुगुना करें जैसे प्रलोभनों वाले विज्ञापनों से हमेशा सावधान रहें।
इसलिए मुक्त बाजार की ताकतों और उपभोक्ता संरक्षण के बीच संतुलन बनाना चाहिए। कोई भी उपभोक्ता आंदोलन तभी सफल हो सकता है, जब उपभोक्ता संतुष्ट हों। उपभोक्ता तभी संतुष्ट होते हैं जब वे अपने उत्पादों और सेवाओं का मूल्य प्राप्त करते हैं। इस प्रकार सरकार, न्यायपालिका, व्यापारियों और उपभोक्ताओं के बीच सहक्रिया और सहयोग का होना आवश्यक है।
(लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय के कन्ज्यूमर क्लब, वाणिज्य विभाग, कमला नेहरू कॉलेज में एसोसियेट प्रोफेसर व कंवीनर हैं)
(लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय के कन्ज्यूमर क्लब, वाणिज्य विभाग, कमला नेहरू कॉलेज में एसोसियेट प्रोफेसर व कंवीनर हैं)